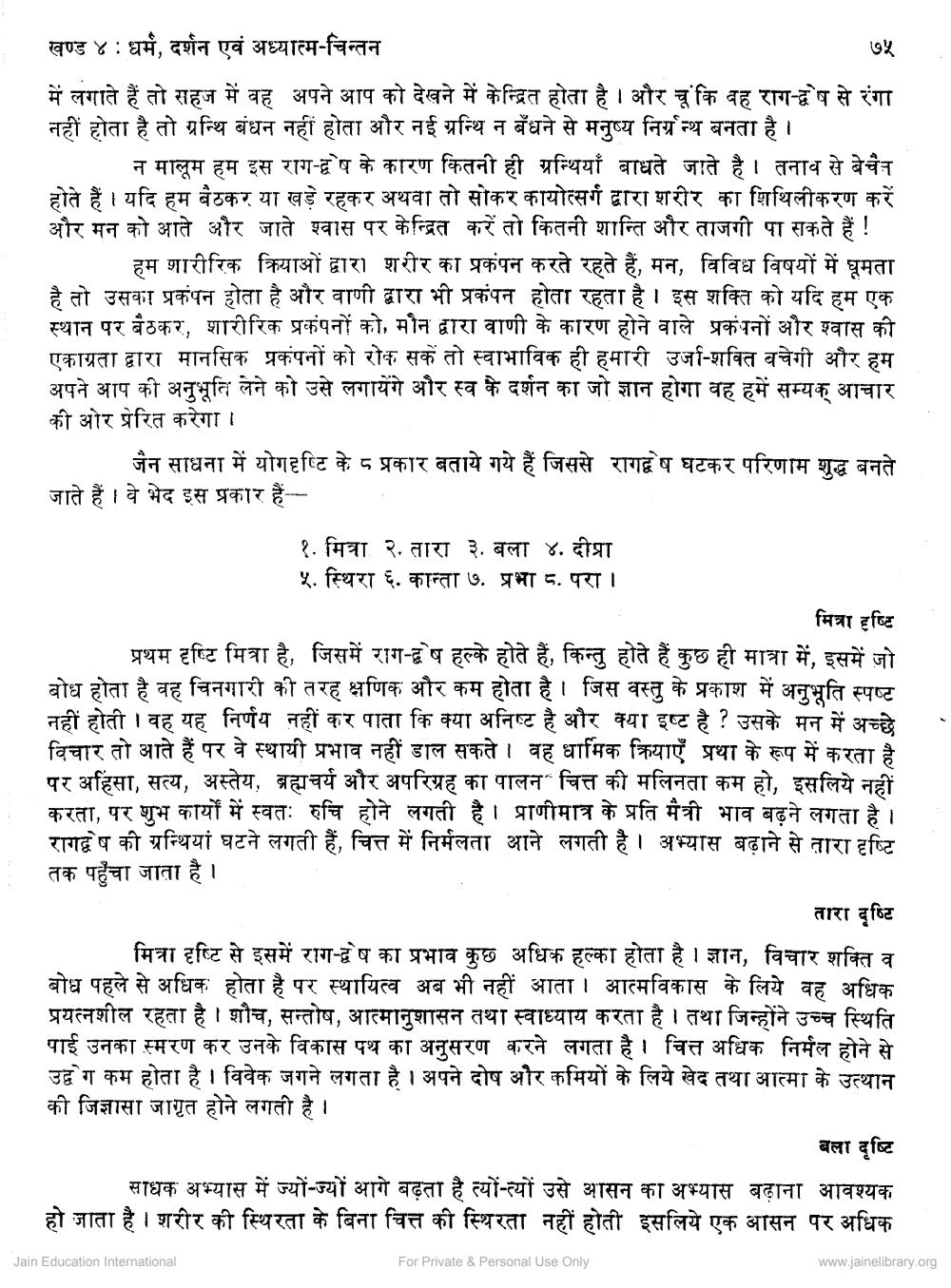________________
खण्ड ४ : धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म-चिन्तन में लगाते हैं तो सहज में वह अपने आप को देखने में केन्द्रित होता है । और चूकि वह राग-द्वष से रंगा नहीं होता है तो ग्रन्थि बंधन नहीं होता और नई ग्रन्थि न बँधने से मनुष्य निर्ग्रन्थ बनता है।
न मालूम हम इस राग-द्वेष के कारण कितनी ही ग्रन्थियाँ बाधते जाते है। तनाव से बेचैन होते हैं। यदि हम बैठकर या खड़े रहकर अथवा तो सोकर कायोत्सर्ग द्वारा शरीर का शिथिलीकरण करें और मन को आते और जाते श्वास पर केन्द्रित करें तो कितनी शान्ति और ताजगी पा सकते हैं !
हम शारीरिक क्रियाओं द्वार। शरीर का प्रकंपन करते रहते हैं, मन, विविध विषयों में घूमता है तो उसका प्रकंपन होता है और वाणी द्वारा भी प्रकंपन होता रहता है । इस शक्ति को यदि हम एक स्थान पर बैठकर, शारीरिक प्रकंपनों को, मौन द्वारा वाणी के कारण होने वाले प्रकंपनों और श्वास की एकाग्रता द्वारा मानसिक प्रकंपनों को रोक सकें तो स्वाभाविक ही हमारी उर्जा-शवित बचेगी और हम अपने आप की अनुभूति लेने को उसे लगायेंगे और स्व के दर्शन का जो ज्ञान होगा वह हमें सम्यक् आचार की ओर प्रेरित करेगा।
जैन साधना में योगदृष्टि के ८ प्रकार बताये गये हैं जिससे रागद्वेष घटकर परिणाम शुद्ध बनते जाते हैं। वे भेद इस प्रकार हैं
१. मित्रा २. तारा ३. बला ४. दीपा ५. स्थिरा ६. कान्ता ७. प्रभा ८. परा ।
मित्रा दृष्टि प्रथम दृष्टि मित्रा है, जिसमें राग-द्वष हल्के होते हैं, किन्तु होते हैं कुछ ही मात्रा में, इसमें जो बोध होता है वह चिनगारी की तरह क्षणिक और कम होता है। जिस वस्तु के प्रकाश में अनुभूति स्पष्ट नहीं होती । वह यह निर्णय नहीं कर पाता कि क्या अनिष्ट है और क्या इष्ट है ? उसके मन में अच्छे विचार तो आते हैं पर वे स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकते। वह धार्मिक क्रियाएँ प्रथा के रूप में करता है पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन चित्त की मलिनता कम हो, इसलिये नहीं करता, पर शुभ कार्यों में स्वतः रुचि होने लगती है। प्राणीमात्र के प्रति मैत्री भाव बढ़ने लगता है। रागद्वेष की ग्रन्थियां घटने लगती हैं, चित्त में निर्मलता आने लगती है। अभ्यास बढ़ाने से तारा दृष्टि तक पहुँचा जाता है।
तारा दृष्टि मित्रा दृष्टि से इसमें राग-द्वोष का प्रभाव कुछ अधिक हल्का होता है । ज्ञान, विचार शक्ति व बोध पहले से अधिक होता है पर स्थायित्व अब भी नहीं आता। आत्मविकास के लिये वह अधिक प्रयत्नशील रहता है । शौच, सन्तोष, आत्मानुशासन तथा स्वाध्याय करता है । तथा जिन्होंने उच्च स्थिति पाई उनका स्मरण कर उनके विकास पथ का अनुसरण करने लगता है। चित्त अधिक निर्मल होने से उद्वेग कम होता है । विवेक जगने लगता है । अपने दोष और कमियों के लिये खेद तथा आत्मा के उत्थान की जिज्ञासा जागृत होने लगती है।
बला दृष्टि साधक अभ्यास में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों-त्यों उसे आसन का अभ्यास बढ़ाना आवश्यक हो जाता है । शरीर की स्थिरता के बिना चित्त की स्थिरता नहीं होती इसलिये एक आसन पर अधिक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org