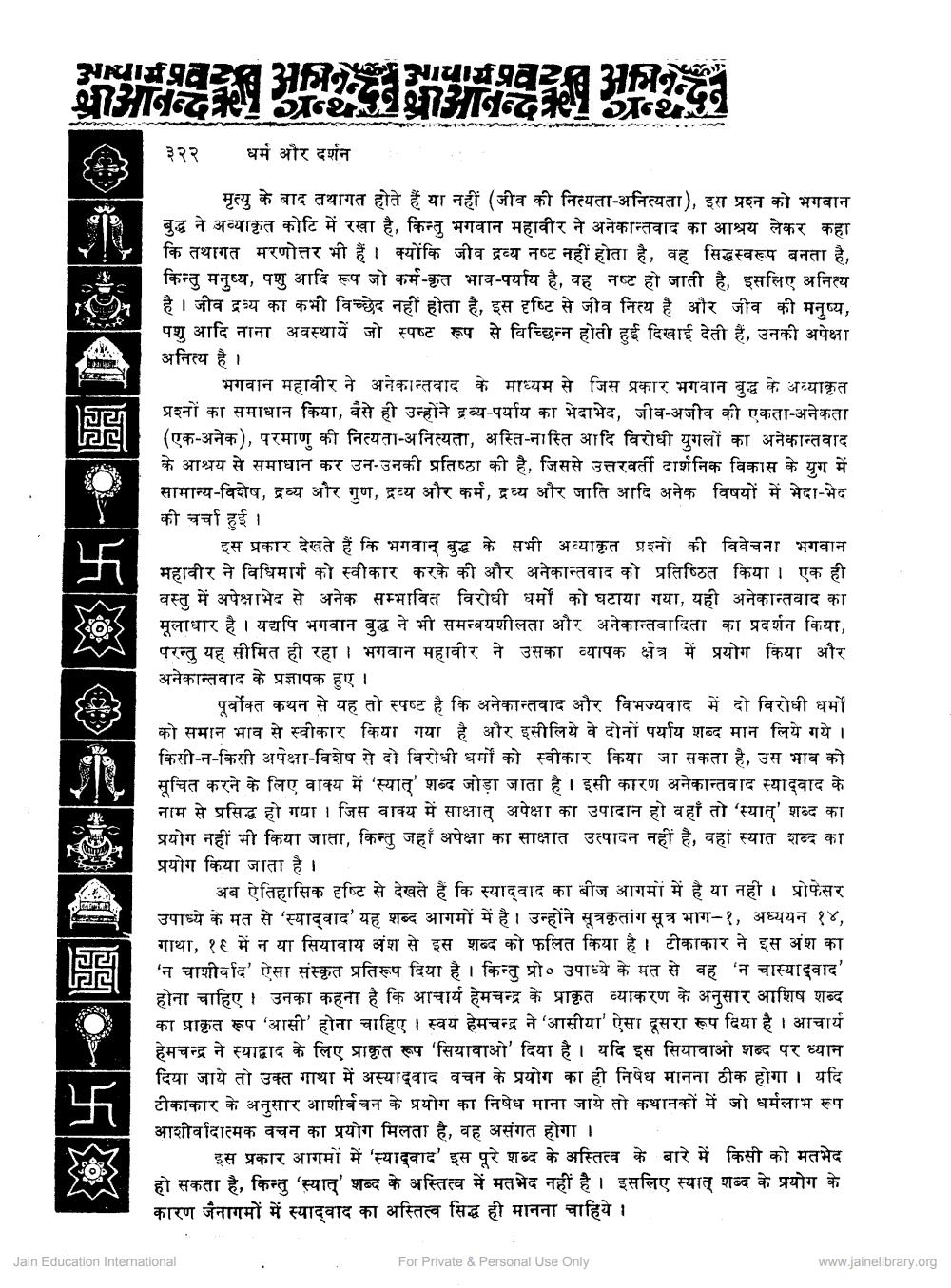________________
भावार्यप्रवर अभिनय श्रीआनन्द अन्य
श्रीआनन्द
३२२
... twanormation
-
--
धर्म और दर्शन
मृत्यु के बाद तथागत होते हैं या नहीं (जीव की नित्यता-अनित्यता), इस प्रश्न को भगवान बुद्ध ने अव्याकृत कोटि में रखा है, किन्तु भगवान महावीर ने अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर कहा कि तथागत मरणोत्तर भी हैं। क्योंकि जीव द्रव्य नष्ट नहीं होता है, वह सिद्धस्वरूप बनता है, किन्तु मनुष्य, पशु आदि रूप जो कर्म-कृत भाव-पर्याय है, वह नष्ट हो जाती है, इसलिए अनित्य है । जीव द्रव्य का कभी विच्छेद नहीं होता है, इस दृष्टि से जीव नित्य है और जीव की मनुष्य, पशू आदि नाना अवस्थायें जो स्पष्ट रूप से विच्छिन्न होती हुई दिखाई देती हैं, उनकी अपेक्षा अनित्य है।
भगवान महावीर ने अनेकान्तवाद के माध्यम से जिस प्रकार भगवान बुद्ध के अव्याकृत प्रश्नों का समाधान किया, वैसे ही उन्होंने द्रव्य-पर्याय का भेदाभेद, जीव-अजीव की एकता-अनेकता (एक-अनेक), परमाणु की नित्यता-अनित्यता, अस्ति-नास्ति आदि विरोधी युगलों का अनेकान्तवाद के आश्रय से समाधान कर उन-उनकी प्रतिष्ठा की है, जिससे उत्तरवर्ती दार्शनिक विकास के युग में सामान्य-विशेष, द्रव्य और गुण, द्रव्य और कर्म, द्रव्य और जाति आदि अनेक विषयों में भेदा-भेद की चर्चा हुई।
इस प्रकार देखते हैं कि भगवान् बुद्ध के सभी अव्याकृत प्रश्नों की विवेचना भगवान महावीर ने विधिमार्ग को स्वीकार करके की और अनेकान्तवाद को प्रतिष्ठित किया। एक ही वस्तु में अपेक्षाभेद से अनेक सम्भावित विरोधी धर्मों को घटाया गया, यही अनेकान्तवाद का मूलाधार है । यद्यपि भगवान बुद्ध ने भी समन्वयशीलता और अनेकान्तवादिता का प्रदर्शन किया, परन्तु यह सीमित ही रहा। भगवान महावीर ने उसका व्यापक क्षेत्र में प्रयोग किया और अनेकान्तवाद के प्रज्ञापक हुए।
पूर्वोक्त कथन से यह तो स्पष्ट है कि अनेकान्तवाद और विभज्यवाद में दो विरोधी धर्मों को समान भाव से स्वीकार किया गया है और इसीलिये वे दोनों पर्याय शब्द मान लिये गये । किसी-न-किसी अपेक्षा-विशेष से दो विरोधी धर्मों को स्वीकार किया जा सकता है, उस भाव को सूचित करने के लिए वाक्य में 'स्यात्' शब्द जोड़ा जाता है। इसी कारण अनेकान्तवाद स्याद्वाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया । जिस वाक्य में साक्षात् अपेक्षा का उपादान हो वहाँ तो 'स्यात्' शब्द का प्रयोग नहीं भी किया जाता, किन्तु जहाँ अपेक्षा का साक्षात उत्पादन नहीं है, वहां स्यात शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अब ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं कि स्याद्वाद का बीज आगमों में है या नहीं। प्रोफेसर उपाध्ये के मत से 'स्याद्वाद' यह शब्द आगमों में है। उन्होंने सूत्रकृतांग सूत्र भाग-१, अध्ययन १४, गाथा, १६ में न या सियावाय अंश से इस शब्द को फलित किया है। टीकाकार ने इस अंश का 'न चाशीर्वाद' ऐसा संस्कृत प्रतिरूप दिया है। किन्तु प्रो० उपाध्ये के मत से वह 'न चास्याद्वाद' होना चाहिए। उनका कहना है कि आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के अनुसार आशिष शब्द का प्राकृत रूप 'आसी' होना चाहिए । स्वयं हेमचन्द्र ने 'आसीया' ऐसा दूसरा रूप दिया है । आचार्य हेमचन्द्र ने स्याद्वाद के लिए प्राकृत रूप 'सियावाओ' दिया है। यदि इस सियावाओ शब्द पर ध्यान दिया जाये तो उक्त गाथा में अस्याद्वाद वचन के प्रयोग का ही निषेध मानना ठीक होगा। यदि टीकाकार के अनुसार आशीर्वचन के प्रयोग का निषेध माना जाये तो कथानकों में जो धर्मलाभ रूप आशीर्वादात्मक वचन का प्रयोग मिलता है, वह असंगत होगा।
इस प्रकार आगमों में 'स्याद्वाद' इस पूरे शब्द के अस्तित्व के बारे में किसी को मतभेद हो सकता है, किन्तु 'स्यात्' शब्द के अस्तित्व में मतभेद नहीं है। इसलिए स्यात् शब्द के प्रयोग के कारण जैनागमों में स्याद्वाद का अस्तित्व सिद्ध ही मानना चाहिये।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org