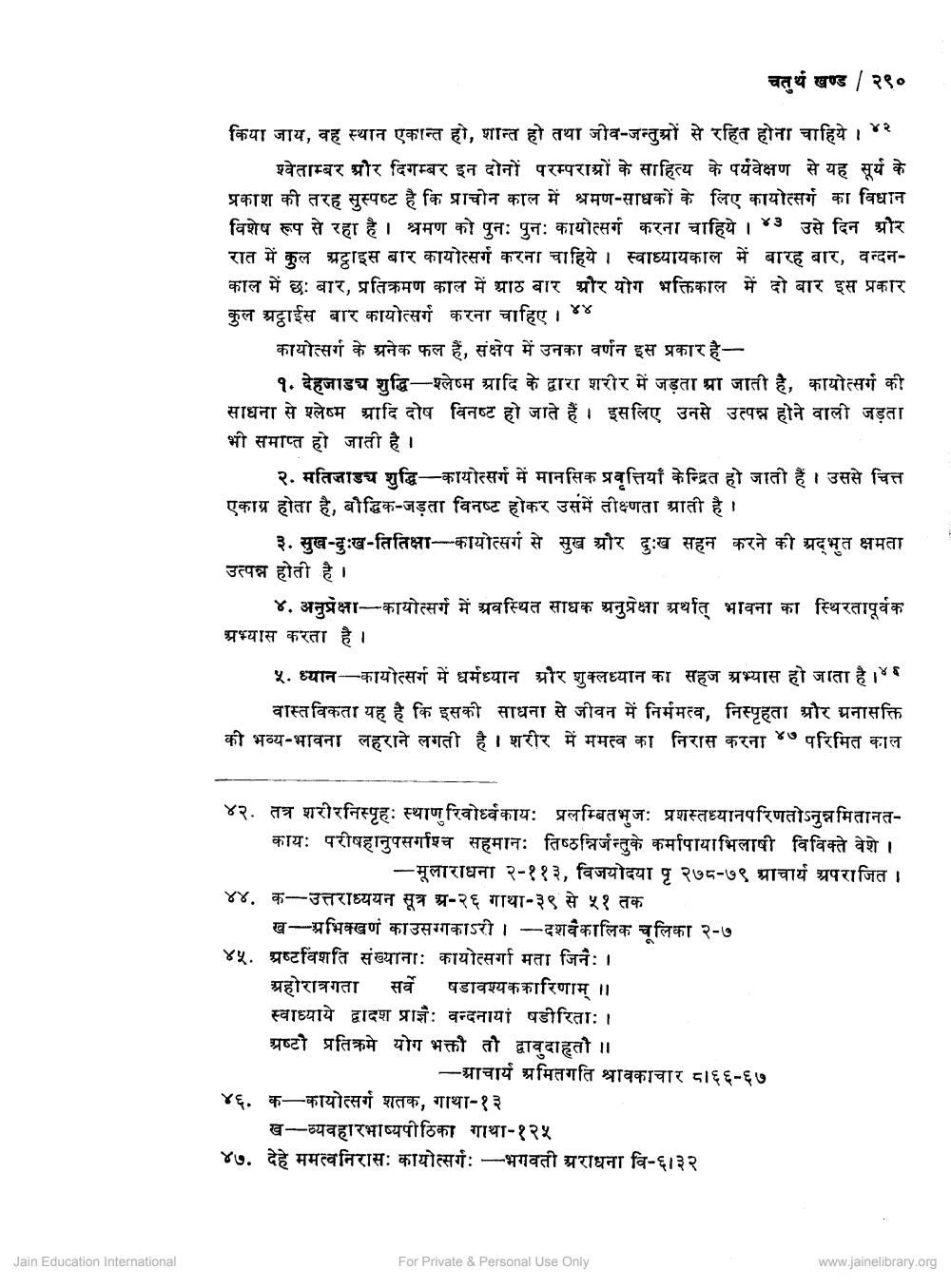________________
Jain Education International
चतुर्थ खण्ड / २९०
किया जाय, वह स्थान एकान्त हो, शान्त हो तथा जीव-जन्तुनों से रहित होना चाहिये ।
૨
श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दोनों परम्पराम्रों के साहित्य के पर्यवेक्षण से यह सूर्य के प्रकाश की तरह सुस्पष्ट है कि प्राचीन काल में भ्रमण साधकों के लिए कायोत्सर्ग का विधान विशेष रूप से रहा है। श्रमण को पुनः पुनः कायोत्सर्ग करना चाहिये । ४३ उसे दिन और रात में कुल अट्ठाइस बार कायोत्सर्ग करना चाहिये । स्वाध्यायकाल में बारह बार, वन्दनकाल में छ: बार, प्रतिक्रमण काल में ग्राठ बार और योग भक्तिकाल में दो बार इस प्रकार कुल अट्ठाईस बार कायोत्सर्ग करना चाहिए। ४४
कायोत्सर्ग के अनेक फल हैं, संक्षेप में उनका वर्णन इस प्रकार है
१. बेहजाप शुद्धि - श्लेष्म आदि के द्वारा शरीर में जड़ता था जाती है, कायोत्सर्ग की साधना से श्लेष्म आदि दोष विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए उनसे उत्पन्न होने वाली जड़ता भी समाप्त हो जाती है ।
२. मतिजा शुद्धि कायोत्सर्ग में मानसिक प्रवृत्तियाँ केन्द्रित हो जाती हैं। उससे चित्त एकाग्र होता है, बौद्धिक जड़ता विनष्ट होकर उसमें तीक्ष्णता भाती है।
३. सुख-दुःख तितिक्षा कायोत्सर्ग से सुख और दुःख सहन करने की अद्भूत क्षमता उत्पन्न होती है ।
४. अनुप्रेक्षा कायोत्सर्ग में अवस्थित साधक अनुप्रेक्षा अर्थात् भावना का स्थिरतापूर्वक अभ्यास करता है ।
-
५. ध्यान – कायोत्सर्ग में धर्मध्यान और शुक्लध्यान का सहज अभ्यास हो जाता है । ४६ वास्तविकता यह है कि इसकी साधना से जीवन में निर्ममत्य, निस्पृहता धौर मनासक्ति की भव्य भावना लहराने लगती है। शरीर में ममत्व का निरास करना ४७ परिमित काल
४२. तत्र शरीरनिस्पृहः स्थाणुरिवोध्वंकायः प्रलम्बितभुजः प्रणस्तध्यानपरिणतोऽनुन्नमितानतकाय: परषहानुपसर्गाश्व सहमान: तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायाभिलाषी विविक्ते वेशे । - मूलाराधना २-११३, विजयोदया पृ २७८-७९ प्राचार्य अपराजित । ४४. क — उत्तराध्ययन सूत्र - २६ गाथा - ३९ से ५१ तक ख - अभिक्खणं काउसरगकारी दशकालिक चूलिका २ ७ ४५. भ्रष्टविंशति संख्याना: कायोत्सर्गा मता जिनैः ।
।
महोरात्रगता सर्वे पढावश्यककारिणाम् ॥ स्वाध्याये द्वादश प्राज्ञः वन्दनायां पढीरिताः । अष्टौ प्रतिक्रमे योग भक्तौ तौ द्वावुदाहृतौ ॥
आचार्य प्रमितगति श्रावकाचार ८६६-६७
४६. कायोत्सर्ग शतक, गाया- १३
-
खव्यवहारभाष्यपीठिका गाथा १२५
४७. देहे ममत्वनिरास: कायोत्सर्गः भगवती अराधना वि ६।३२
—
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org