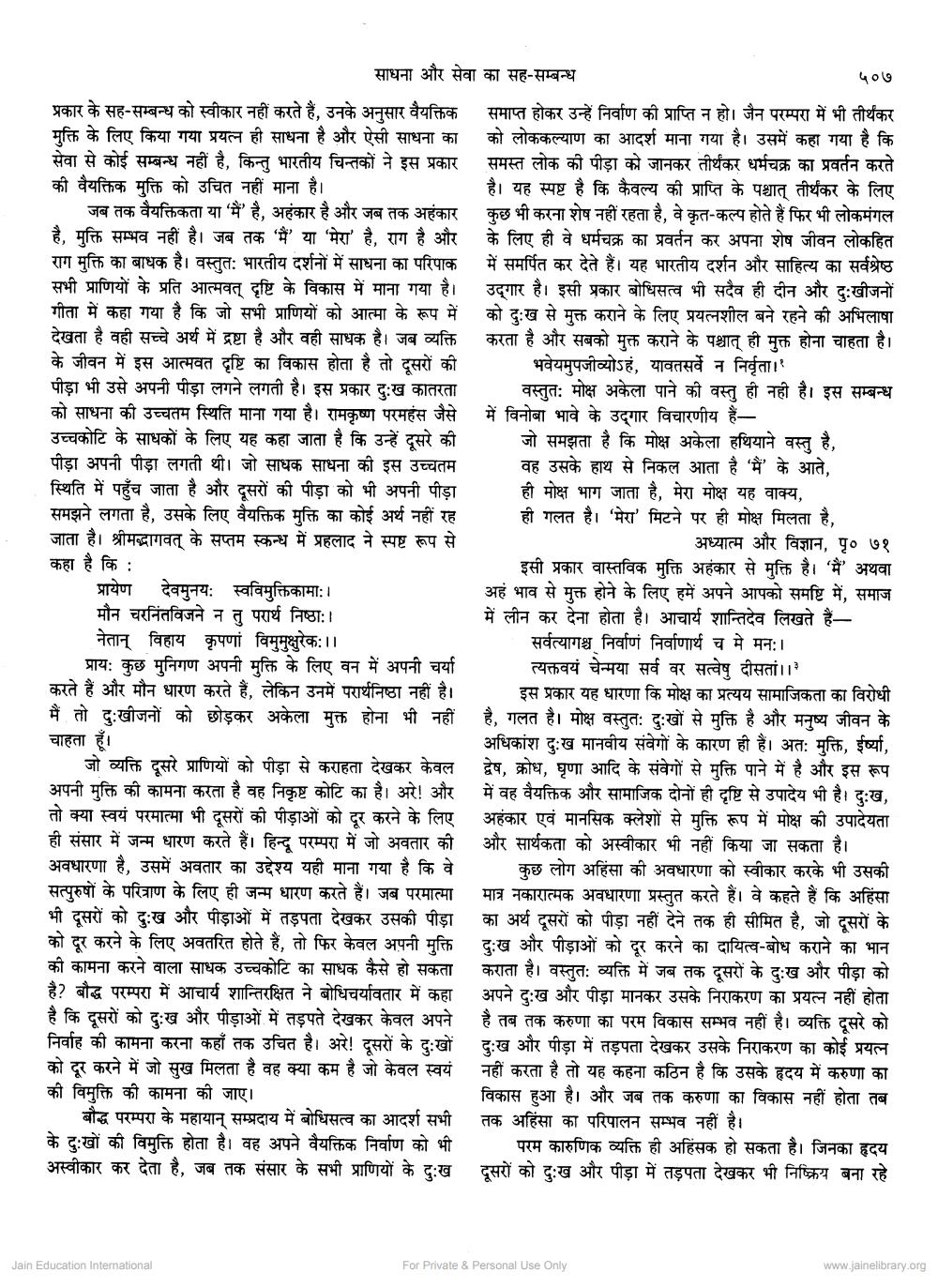________________
साधना और सेवा का सह-सम्बन्ध
५०७
प्रकार के सह-सम्बन्ध को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अनुसार वैयक्तिक समाप्त होकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति न हो। जैन परम्परा में भी तीर्थंकर मुक्ति के लिए किया गया प्रयत्न ही साधना है और ऐसी साधना का को लोककल्याण का आदर्श माना गया है। उसमें कहा गया है कि सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु भारतीय चिन्तकों ने इस प्रकार समस्त लोक की पीड़ा को जानकर तीर्थंकर धर्मचक्र का प्रवर्तन करते की वैयक्तिक मुक्ति को उचित नहीं माना है।
है। यह स्पष्ट है कि कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात् तीर्थकर के लिए जब तक वैयक्तिकता या 'मैं' है, अहंकार है और जब तक अहंकार कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, वे कृत-कल्प होते हैं फिर भी लोकमंगल है, मुक्ति सम्भव नहीं है। जब तक 'मैं' या 'मेरा' है, राग है और के लिए ही वे धर्मचक्र का प्रवर्तन कर अपना शेष जीवन लोकहित राग मुक्ति का बाधक है। वस्तुत: भारतीय दर्शनों में साधना का परिपाक में समर्पित कर देते हैं। यह भारतीय दर्शन और साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत् दृष्टि के विकास में माना गया है। उद्गार है। इसी प्रकार बोधिसत्व भी सदैव ही दीन और दुःखीजनों गीता में कहा गया है कि जो सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में को दुःख से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील बने रहने की अभिलाषा देखता है वही सच्चे अर्थ में द्रष्टा है और वही साधक है। जब व्यक्ति करता है और सबको मुक्त कराने के पश्चात् ही मुक्त होना चाहता है। के जीवन में इस आत्मवत दृष्टि का विकास होता है तो दूसरों की भवेयमुपजीव्योऽहं, यावतसर्वे न निर्वृता। पीड़ा भी उसे अपनी पीड़ा लगने लगती है। इस प्रकार दुःख कातरता वस्तुत: मोक्ष अकेला पाने की वस्तु ही नही है। इस सम्बन्ध को साधना की उच्चतम स्थिति माना गया है। रामकृष्ण परमहंस जैसे में विनोबा भावे के उद्गार विचारणीय हैंउच्चकोटि के साधकों के लिए यह कहा जाता है कि उन्हें दूसरे की जो समझता है कि मोक्ष अकेला हथियाने वस्तु है, पीड़ा अपनी पीड़ा लगती थी। जो साधक साधना की इस उच्चतम वह उसके हाथ से निकल आता है 'मैं' के आते, स्थिति में पहुँच जाता है और दूसरों की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा ही मोक्ष भाग जाता है, मेरा मोक्ष यह वाक्य, समझने लगता है, उसके लिए वैयक्तिक मुक्ति का कोई अर्थ नहीं रह ही गलत है। 'मेरा' मिटने पर ही मोक्ष मिलता है, जाता है। श्रीमद्भागवत् के सप्तम स्कन्ध में प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से
अध्यात्म और विज्ञान, पृ० ७१ कहा है कि :
इसी प्रकार वास्तविक मुक्ति अहंकार से मुक्ति है। 'मैं' अथवा प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामाः।
अहं भाव से मुक्त होने के लिए हमें अपने आपको समष्टि में, समाज मौन चरनिंतविजने न तु परार्थ निष्ठाः।
में लीन कर देना होता है। आचार्य शान्तिदेव लिखते हैंनेतान् विहाय कृपणां विमुमुक्षुरेकः।।
सर्वत्यागश्च निर्वाणं निर्वाणार्थ च मे मनः। प्रायः कुछ मुनिगण अपनी मुक्ति के लिए वन में अपनी चर्या त्यक्तवयं चेन्मया सर्व वर सत्वेषु दीसतां।।' करते हैं और मौन धारण करते हैं, लेकिन उनमें परार्थनिष्ठा नहीं है। इस प्रकार यह धारणा कि मोक्ष का प्रत्यय सामाजिकता का विरोधी मैं तो दु:खीजनों को छोड़कर अकेला मुक्त होना भी नहीं है, गलत है। मोक्ष वस्तुत: दुःखों से मुक्ति है और मनुष्य जीवन के चाहता हूँ।
अधिकांश दुःख मानवीय संवेगों के कारण ही हैं। अत: मुक्ति, ईर्ष्या, जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों को पीड़ा से कराहता देखकर केवल द्वेष, क्रोध, घृणा आदि के संवेगों से मुक्ति पाने में है और इस रूप अपनी मुक्ति की कामना करता है वह निकृष्ट कोटि का है। अरे! और में वह वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से उपादेय भी है। दुःख, तो क्या स्वयं परमात्मा भी दूसरों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए अहंकार एवं मानसिक क्लेशों से मुक्ति रूप में मोक्ष की उपादेयता ही संसार में जन्म धारण करते हैं। हिन्दू परम्परा में जो अवतार की और सार्थकता को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। अवधारणा है, उसमें अवतार का उद्देश्य यही माना गया है कि वे कुछ लोग अहिंसा की अवधारणा को स्वीकार करके भी उसकी सत्पुरुषों के परित्राण के लिए ही जन्म धारण करते हैं। जब परमात्मा मात्र नकारात्मक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि अहिंसा भी दूसरों को दुःख और पीड़ाओं में तड़पता देखकर उसकी पीड़ा का अर्थ दूसरों को पीड़ा नहीं देने तक ही सीमित है, जो दूसरों के को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं, तो फिर केवल अपनी मुक्ति दुःख और पीड़ाओं को दूर करने का दायित्व-बोध कराने का भान की कामना करने वाला साधक उच्चकोटि का साधक कैसे हो सकता कराता है। वस्तुतः व्यक्ति में जब तक दूसरों के दुःख और पीड़ा को है? बौद्ध परम्परा में आचार्य शान्तिरक्षित ने बोधिचर्यावतार में कहा अपने दुःख और पीड़ा मानकर उसके निराकरण का प्रयत्न नहीं होता है कि दूसरों को दुःख और पीड़ाओं में तड़पते देखकर केवल अपने है तब तक करुणा का परम विकास सम्भव नहीं है। व्यक्ति दूसरे को निर्वाह की कामना करना कहाँ तक उचित है। अरे! दूसरों के दुःखों दुःख और पीड़ा में तड़पता देखकर उसके निराकरण का कोई प्रयत्न को दूर करने में जो सुख मिलता है वह क्या कम है जो केवल स्वयं नहीं करता है तो यह कहना कठिन है कि उसके हृदय में करुणा का की विमुक्ति की कामना की जाए।
विकास हुआ है। और जब तक करुणा का विकास नहीं होता तब बौद्ध परम्परा के महायान् सम्प्रदाय में बोधिसत्व का आदर्श सभी तक अहिंसा का परिपालन सम्भव नहीं है। के दुःखों की विमुक्ति होता है। वह अपने वैयक्तिक निर्वाण को भी परम कारुणिक व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है। जिनका हृदय अस्वीकार कर देता है, जब तक संसार के सभी प्राणियों के दुःख दूसरों को दुःख और पीड़ा में तड़पता देखकर भी निष्क्रिय बना रहे
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org