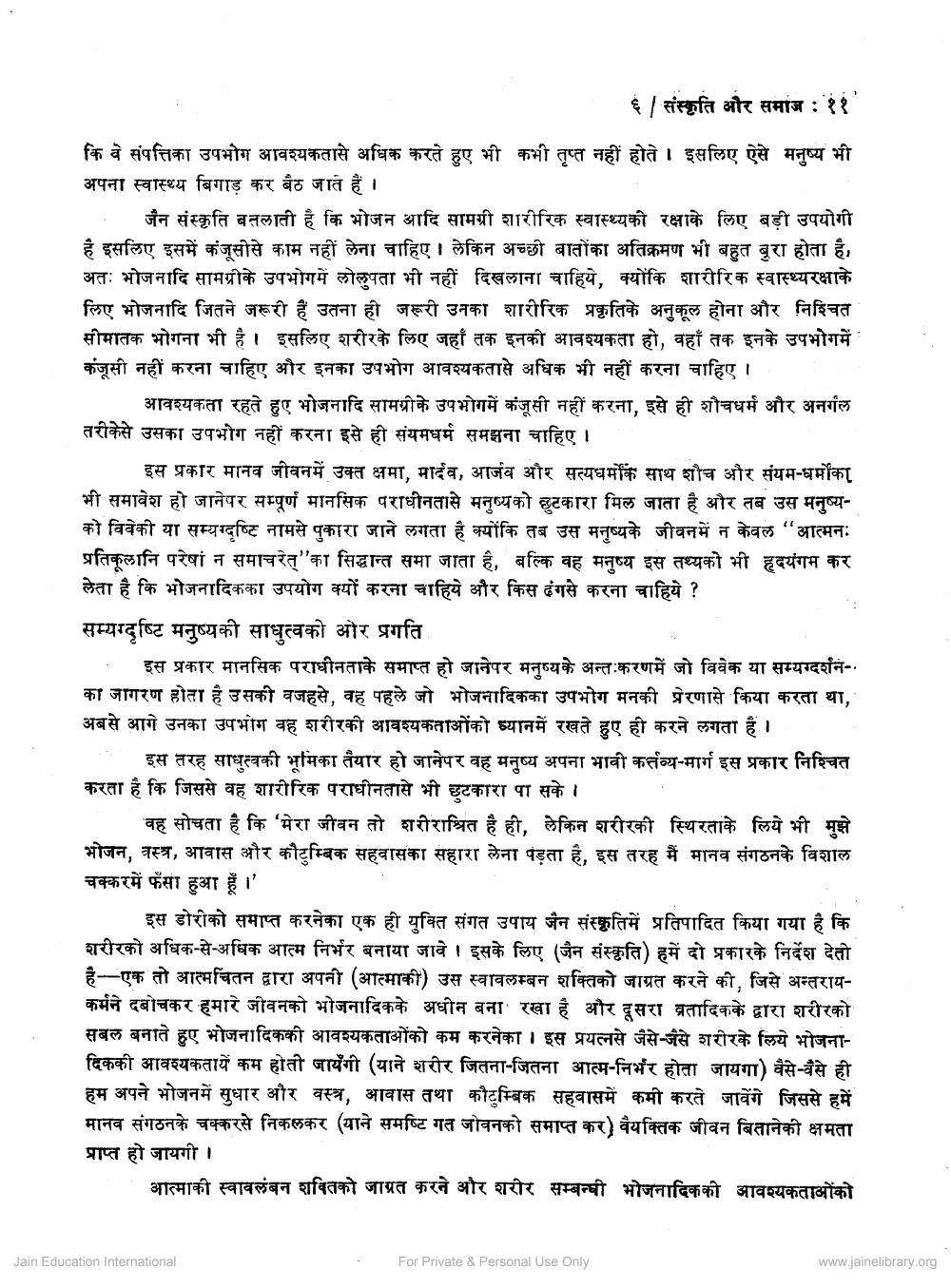________________
६ / संस्कृति और समाज : ११ कि वे संपत्तिका उपभोग आवश्यकतासे अधिक करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते । इसलिए ऐसे मनुष्य भी अपना स्वास्थ्य बिगाड़ कर बैठ जाते हैं ।
जैन संस्कृति बतलाती है कि भोजन आदि सामग्री शारीरिक स्वास्थ्यको रक्षाके लिए बड़ी उपयोगी है इसलिए इसमें कंजूसीसे काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बातोंका अतिक्रमण भी बहुत बुरा होता है, अतः भोजनादि सामग्रीके उपभोग में लोलुपता भी नहीं दिखलाना चाहिये, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्यरक्षाके लिए भोजनादि जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी उनका शारीरिक प्रकृतिके अनुकूल होना और निश्चित सीमातक भोगना भी है । इसलिए शरीर के लिए जहाँ तक इनकी आवश्यकता हो, वहाँ तक इनके उपभोग में कंजूसी नहीं करना चाहिए और इनका उपभोग आवश्यकतासे अधिक भी नहीं करना चाहिए ।
आवश्यकता रहते हुए भोजनादि सामग्री के उपभोगमें कंजूसी नहीं करना, इसे ही शौचधर्म और अनगंल तरीकेसे उसका उपभोग नहीं करना इसे ही संयमधर्म समझना चाहिए ।
इस प्रकार मानव जीवनमें उक्त क्षमा, मार्दव, आर्जव और सत्यधर्मोक साथ शौच और संयम- धर्मोका भी समावेश हो जानेपर सम्पूर्ण मानसिक पराधीनतासे मनुष्यको छुटकारा मिल जाता है और तब उस मनुष्यविवेकीया सम्यग्दृष्टि नामसे पुकारा जाने लगता है क्योंकि तब उस मनुष्यके जीवन में न केवल " आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् " का सिद्धान्त समा जाता है, बल्कि वह मनुष्य इस तथ्यको भी हृदयंगम कर लेता है कि भोजनादिकका उपयोग क्यों करना चाहिये और किस ढंगसे करना चाहिये ?
सम्यग्दृष्टि मनुष्य की साधुत्वको ओर प्रगति
इस प्रकार मानसिक पराधीनताके समाप्त हो जानेपर मनुष्य के अन्तःकरणमें जो विवेक या सम्यग्दर्शन-का जागरण होता है उसकी वजहसे, वह पहले जो भोजनादिकका उपभोग मनकी प्रेरणासे किया करता था, अबसे आगे उनका उपभोग वह शरीरकी आवश्यकताओंको ध्यान में रखते हुए ही करने लगता हैं ।
इस तरह साधुत्वकी भूमिका तैयार हो जानेपर वह मनुष्य अपना भावी कर्तव्य मार्ग इस प्रकार निश्चित करता है कि जिससे वह शारीरिक पराधीनतासे भी छुटकारा पा सके ।
वह सोचता है कि 'मेरा जीवन तो शरीराश्रित है ही, लेकिन शरीरकी स्थिरताके लिये भी मुझे भोजन, वस्त्र, आवास और कौटुम्बिक सहवासका सहारा लेना पड़ता है, इस तरह मैं मानव संगठनके विशाल चक्कर में फँसा हुआ हूँ ।'
इस डोरीको समाप्त करनेका एक ही युक्ति संगत उपाय जैन संस्कृति में प्रतिपादित किया गया है कि शरीरको अधिक-से-अधिक आत्म निर्भर बनाया जावे। इसके लिए (जैन संस्कृति) हमें दो प्रकारके निर्देश देती है— एक तो आत्मचिंतन द्वारा अपनी (आत्माकी) उस स्वावलम्बन शक्तिको जाग्रत करने की, जिसे अन्तरायकर्मने दबोचकर हमारे जीवनको भोजनादिकके अधीन बना रखा है और दूसरा व्रतादिकके द्वारा शरीरको सबल बनाते हुए भोजनादिककी आवश्यकताओंको कम करनेका । इस प्रयत्नसे जैसे-जैसे शरीर के लिये भोजनादिककी आवश्यकतायें कम होती जायेंगी (याने शरीर जितना जितना आत्म-निर्भर होता जायगा ) वैसे-वैसे ही हम अपने भोजन में सुधार और वस्त्र, आवास तथा कौटुम्बिक सहवासमें कमी करते जावेंगे जिससे हमें मानव संगठनके चक्करसे निकलकर (याने समष्टि गत जोवनको समाप्त कर ) वैयक्तिक जीवन बितानेकी क्षमता प्राप्त हो जायगी ।
आत्मा की स्वावलंबन शक्तिको जाग्रत करने और शरीर सम्बन्धी भोजनादिककी आवश्यकताओंको
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org