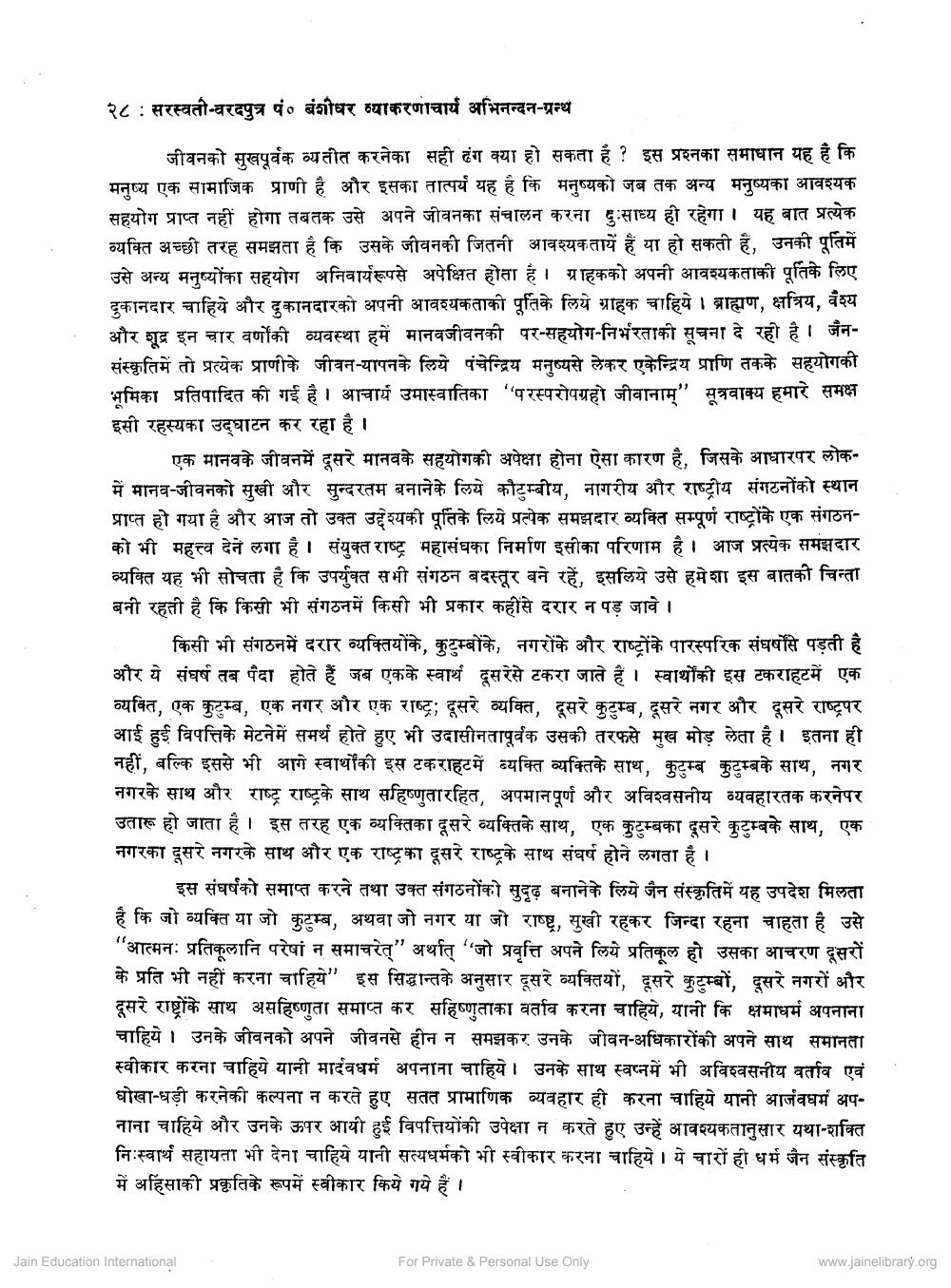________________
२८ : सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ
जीवनको सुखपूर्वक व्यतीत करनेका सही ढंग क्या हो सकता है ? इस प्रश्नका समाधान यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यको जब तक अन्य मनुष्यका आवश्यक सहयोग प्राप्त नहीं होगा तबतक उसे अपने जीवनका संचालन करना दुःसाध्य ही रहेगा। यह बात प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह समझता है कि उसके जीवनकी जितनी आवश्यकतायें हैं या हो सकती है, उनकी पूर्तिमें उसे अन्य मनुष्योंका सहयोग अनिवार्यरूपसे अपेक्षित होता है। ग्राहकको अपनी आवश्यकताकी पूतिके लिए दुकानदार चाहिये और दुकानदारको अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये ग्राहक चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों की व्यवस्था हमें मानवजीवनकी पर-सहयोग-निर्भरताकी सूचना दे रही है। जैनसंस्कृतिमें तो प्रत्येक प्राणीके जीवन-यापनके लिये पंचेन्द्रिय मनुष्यसे लेकर एकेन्द्रिय प्राणि तकके सहयोगकी भूमिका प्रतिपादित की गई है। आचार्य उमास्वातिका 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्" सूत्रवाक्य हमारे समक्ष इसी रहस्यका उद्घाटन कर रहा है ।
एक मानवके जीवनमें दूसरे मानवके सहयोगको अपेक्षा होना ऐसा कारण है. जिसके आधारपर लोकमें मानव-जीवनको सुखी और सुन्दरतम बनाने के लिये कौटुम्बीय, नागरीय और राष्ट्रीय संगठनोंको स्थान प्राप्त हो गया है और आज तो उक्त उद्देश्यकी पूर्तिके लिये प्रत्येक समझदार व्यक्ति सम्पूर्ण राष्ट्रोंके एक संगठनको भी महत्त्व देने लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासंघका निर्माण इसीका परिणाम है। आज प्रत्येक समझदार व्यक्ति यह भी सोचता है कि उपर्युक्त सभी संगठन बदस्तूर बने रहें, इसलिये उसे हमेशा इस बातकी चिन्ता बनी रहती है कि किसी भी संगठनमें किसी भी प्रकार कहींसे दरार न पड़ जावे ।
किसी भी संगठनमें दरार व्यक्तियोंके, कुटुम्बोंके, नगरोंके और राष्ट्रोंके पारस्परिक संघर्षोंसे पड़ती है और ये संघर्ष तब पैदा होते हैं जब एकके स्वार्थ दूसरेसे टकरा जाते है । स्वार्थोंकी इस टकराहटमें एक व्यक्ति, एक कुटुम्ब, एक नगर और एक राष्ट्र; दूसरे व्यक्ति, दूसरे कुटुम्ब, दूसरे नगर और दूसरे राष्ट्रपर आई हई विपत्तिके मेटने में समर्थ होते हुए भी उदासीनतापूर्वक उसकी तरफसे मुख मोड़ लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी आगे स्वार्थोकी इस टकराहटमें ब्यक्ति व्यक्तिके साथ, कूटम्ब कुटुम्बके साथ, नगर नगरके साथ और राष्ट्र राष्ट्र के साथ सहिष्णुतारहित, अपमानपूर्ण और अविश्वसनीय व्यवहारतक करनेपर उतारू हो जाता है। इस तरह एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिके साथ, एक कुटम्बका दूसरे कुटुम्बके साथ, एक नगरका दूसरे नगरके साथ और एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रके साथ संघर्ष होने लगता है ।
इस संघर्षको समाप्त करने तथा उक्त संगठनोंको सुदृढ़ बनानेके लिये जैन संस्कृतिमें यह उपदेश मिलता है कि जो व्यक्ति या जो कुटुम्ब, अथवा जो नगर या जो राष्ष्ट्र, सुखी रहकर जिन्दा रहना चाहता है उसे "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" अर्थात् “जो प्रवृत्ति अपने लिये प्रतिकूल हो उसका आचरण दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिये" इस सिद्धान्तके अनुसार दूसरे व्यक्तियों, दूसरे कुटुम्बों, दूसरे नगरों और दूसरे राष्ट्रोंके साथ असहिष्णुता समाप्त कर सहिष्णुताका वर्ताव करना चाहिये, यानी कि क्षमाधर्म अपनाना चाहिये। उनके जीवनको अपने जीवनसे हीन न समझकर उनके जीवन-अधिकारोंकी अपने साथ समानता स्वीकार करना चाहिये यानी मार्दवधर्म अपनाना चाहिये। उनके साथ स्वप्न में भी अविश्वसनीय वर्ताव एवं धोखा-धड़ी करनेकी कल्पना न करते हुए सतत प्रामाणिक व्यवहार ही करना चाहिये यानी आर्जवधर्म अपनाना चाहिये और उनके ऊपर आयी हुई विपत्तियोंकी उपेक्षा न करते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार यथा-शक्ति निःस्वार्थ सहायता भी देना चाहिये यानी सत्यधर्मको भी स्वीकार करना चाहिये । ये चारों ही धर्म जैन संस्कृति में अहिंसाकी प्रकृतिके रूपमें स्वीकार किये गये हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org