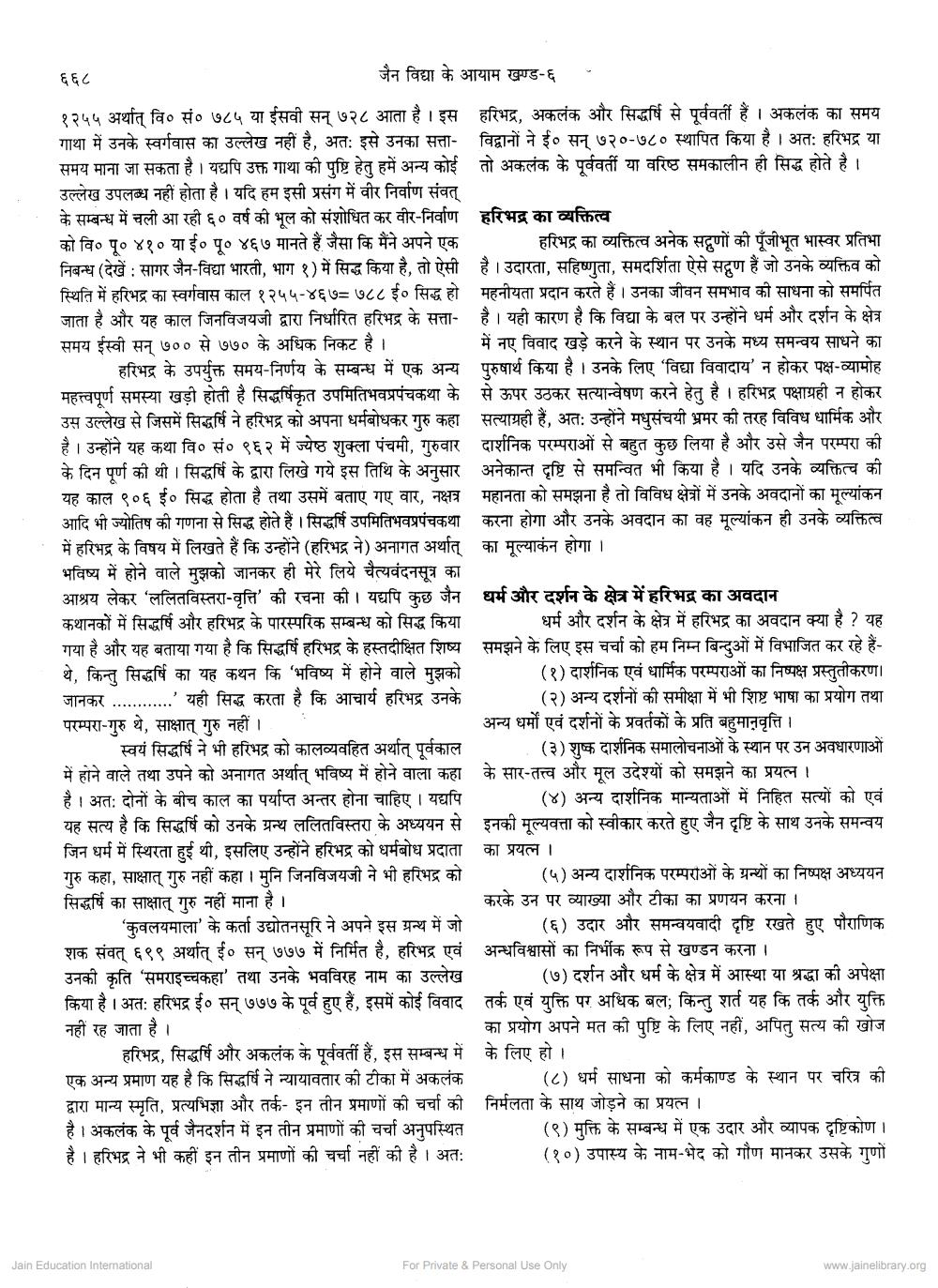________________
जैन विद्या के आयाम खण्ड ६
६६८
१२५५ अर्थात् वि० सं० ७८५ या ईसवी सन् ७२८ आता है। इस गाथा में उनके स्वर्गवास का उल्लेख नहीं है, अतः इसे उनका सत्तासमय माना जा सकता है। यद्यपि उक्त गाथा की पुष्टि हेतु हमें अन्य कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है। यदि हम इसी प्रसंग में वीर निर्वाण संवत के सम्बन्ध में चली आ रही ६० वर्ष की भूल को संशोधित कर वीर निर्वाण को वि० पू० ४१० या ई० पू० ४६७ मानते हैं जैसा कि मैंने अपने एक निबन्ध (देखें : सागर जैन-विद्या भारती, भाग १ ) में सिद्ध किया है, तो ऐसी स्थिति में हरिभद्र का स्वर्गवास काल १२५५-४६७= ७८८ ई० सिद्ध हो जाता है और यह काल जिनविजयजी द्वारा निर्धारित हरिभद्र के सत्ता समय ईस्वी सन् ७०० से ७७० के अधिक निकट है ।
है अतः दोनों के बीच काल का पर्याप्त अन्तर होना चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि सिद्धर्षि को उनके ग्रन्थ ललितविस्तरा के अध्ययन से जिन धर्म में स्थिरता हुई थी, इसलिए उन्होंने हरिभद्र को धर्मबोध प्रदाता गुरु कहा, साक्षात् गुरु नहीं कहा। मुनि जिनविजयजी ने भी हरिभद्र को सिद्धर्षि का साक्षात् गुरु नहीं माना है।
हरिभद्र के उपर्युक्त समय-निर्णय के सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण समस्या खड़ी होती है सिद्धर्षिकृत उपमितिभवप्रपंचकथा के उस उल्लेख से जिसमें सिद्धर्षि ने हरिभद्र को अपना धर्मबोधकर गुरु कहा है। उन्होंने यह कथा वि० सं० ९६२ में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, गुरुवार के दिन पूर्ण की थी। सिद्धर्षि के द्वारा लिखे गये इस तिथि के अनुसार यह काल ९०६ ई० सिद्ध होता है तथा उसमें बताए गए वार, नक्षत्र आदि भी ज्योतिष की गणना से सिद्ध होते हैं। सिद्धर्षि उपमितिभवप्रपंचकथा में हरिभद्र के विषय में लिखते है कि उन्होंने (हरिभद्र ने) अनागत अर्थात् भविष्य में होने वाले मुझको जानकर ही मेरे लिये चैत्यवंदनसूत्र का
आश्रय लेकर 'ललितविस्तरावृत्ति' की रचना की यद्यपि कुछ जैन धर्म और दर्शन के क्षेत्र में हरिभद्र का अवदान
कथानकों में सिद्धर्षि और हरिभद्र के पारस्परिक सम्बन्ध को सिद्ध किया गया है और यह बताया गया है कि सिद्धर्षि हरिभद्र के हस्तदीक्षित शिष्य थे, किन्तु सिद्धर्षि का यह कथन कि 'भविष्य में होने वाले मुझको जानकर ......... यही सिद्ध करता है कि आचार्य हरिभद्र उनके परम्परा-गुरु थे, साक्षात् गुरु नहीं।
स्वयं सिद्धर्षि ने भी हरिभद्र को कालव्यवहित अर्थात् पूर्वकाल
में होने वाले तथा उपने को अनागत अर्थात् भविष्य में होने वाला कहा के सार तत्त्व और मूल उदेश्यों को समझने का प्रयत्न ।
'कुवलयमाला' के कर्ता उद्योतनसूरि ने अपने इस ग्रन्थ में जो शक संवत् ६९९ अर्थात् ई० सन् ७७७ में निर्मित है, हरिभद्र एवं उनकी कृति 'समराइच्चकहा' तथा उनके भवविरह नाम का उल्लेख किया है। अतः हरिभद्र ई० सन् ७७७ के पूर्व हुए हैं, इसमें कोई विवाद नहीं रह जाता है ।
हरिभद्र, सिद्धर्षि और अकलंक के पूर्ववर्ती हैं, इस सम्बन्ध में एक अन्य प्रमाण यह है कि सिद्धर्षि ने न्यायावतार की टीका में अकलंक द्वारा मान्य स्मृति, प्रत्यभिज्ञा और तर्क- इन तीन प्रमाणों की चर्चा की है। अकलंक के पूर्व जैनदर्शन में इन तीन प्रमाणों की चर्चा अनुपस्थित है। हरिभद्र ने भी कहीं इन तीन प्रमाणों की चर्चा नहीं की है। अतः
Jain Education International
हरिभद्र, अकलंक और सिद्धर्षि से पूर्ववर्ती हैं। अकलंक का समय विद्वानों ने ई० सन् ७२० ७८० स्थापित किया है। अतः हरिभद्र या तो अकलंक के पूर्ववर्ती या वरिष्ठ समकालीन ही सिद्ध होते है।
हरिभद्र का व्यक्तित्व
हरिभद्र का व्यक्तित्व अनेक सद्गुणों की पूँजीभूत भास्वर प्रतिभा है । उदारता, सहिष्णुता, समदर्शिता ऐसे सगुण हैं जो उनके व्यक्तिव को महनीयता प्रदान करते हैं। उनका जीवन समभाव की साधना को समर्पित है। यही कारण है कि विद्या के बल पर उन्होंने धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विवाद खड़े करने के स्थान पर उनके मध्य समन्वय साधने का पुरुषार्थ किया है। उनके लिए 'विद्या विवादाय' न होकर पक्ष- व्यामोह से ऊपर उठकर सत्यान्वेषण करने हेतु है। हरिभद्र पक्षाग्रही न होकर सत्याग्रही है, अतः उन्होंने मधुसंचयी भ्रमर की तरह विविध धार्मिक और दार्शनिक परम्पराओं से बहुत कुछ लिया है और उसे जैन परम्परा की अनेकान्त दृष्टि से समन्वित भी किया है। यदि उनके व्यक्तित्व की महानता को समझना है तो विविध क्षेत्रों में उनके अवदानों का मूल्यांकन करना होगा और उनके अवदान का वह मूल्यांकन ही उनके व्यक्तित्व का मूल्याकंन होगा।
धर्म और दर्शन के क्षेत्र में हरिभद्र का अवदान क्या है? यह समझने के लिए इस चर्चा को हम निम्न बिन्दुओं में विभाजित कर रहे हैं
(१) दार्शनिक एवं धार्मिक परम्पराओं का निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण । (२) अन्य दर्शनों की समीक्षा में भी शिष्ट भाषा का प्रयोग तथा अन्य धर्मों एवं दर्शनों के प्रवर्तकों के प्रति बहुमानवृत्ति ।
(३) शुष्क दार्शनिक समालोचनाओं के स्थान पर उन अवधारणाओं
(४) अन्य दार्शनिक मान्यताओं में निहित सत्यों को एवं इनकी मूल्यवत्ता को स्वीकार करते हुए जैन दृष्टि के साथ उनके समन्वय का प्रयत्न ।
(५) अन्य दार्शनिक परम्पराओं के ग्रन्थों का निष्पक्ष अध्ययन करके उन पर व्याख्या और टीका का प्रणयन करना ।
(६) उदार और समन्वयवादी दृष्टि रखते हुए पौराणिक अन्धविश्वासों का निर्भीक रूप से खण्डन करना ।
(७) दर्शन और धर्म के क्षेत्र में आस्था या श्रद्धा की अपेक्षा तर्क एवं युक्ति पर अधिक बल किन्तु शर्त यह कि तर्क और युक्ति का प्रयोग अपने मत की पुष्टि के लिए नहीं, अपितु सत्य की खोज के लिए हो।
(८) धर्म साधना को कर्मकाण्ड के स्थान पर चरित्र की निर्मलता के साथ जोड़ने का प्रयत्न ।
(९) मुक्ति के सम्बन्ध में एक उदार और व्यापक दृष्टिकोण । (१०) उपास्य के नाम-भेद को गौण मानकर उसके गुणों
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.