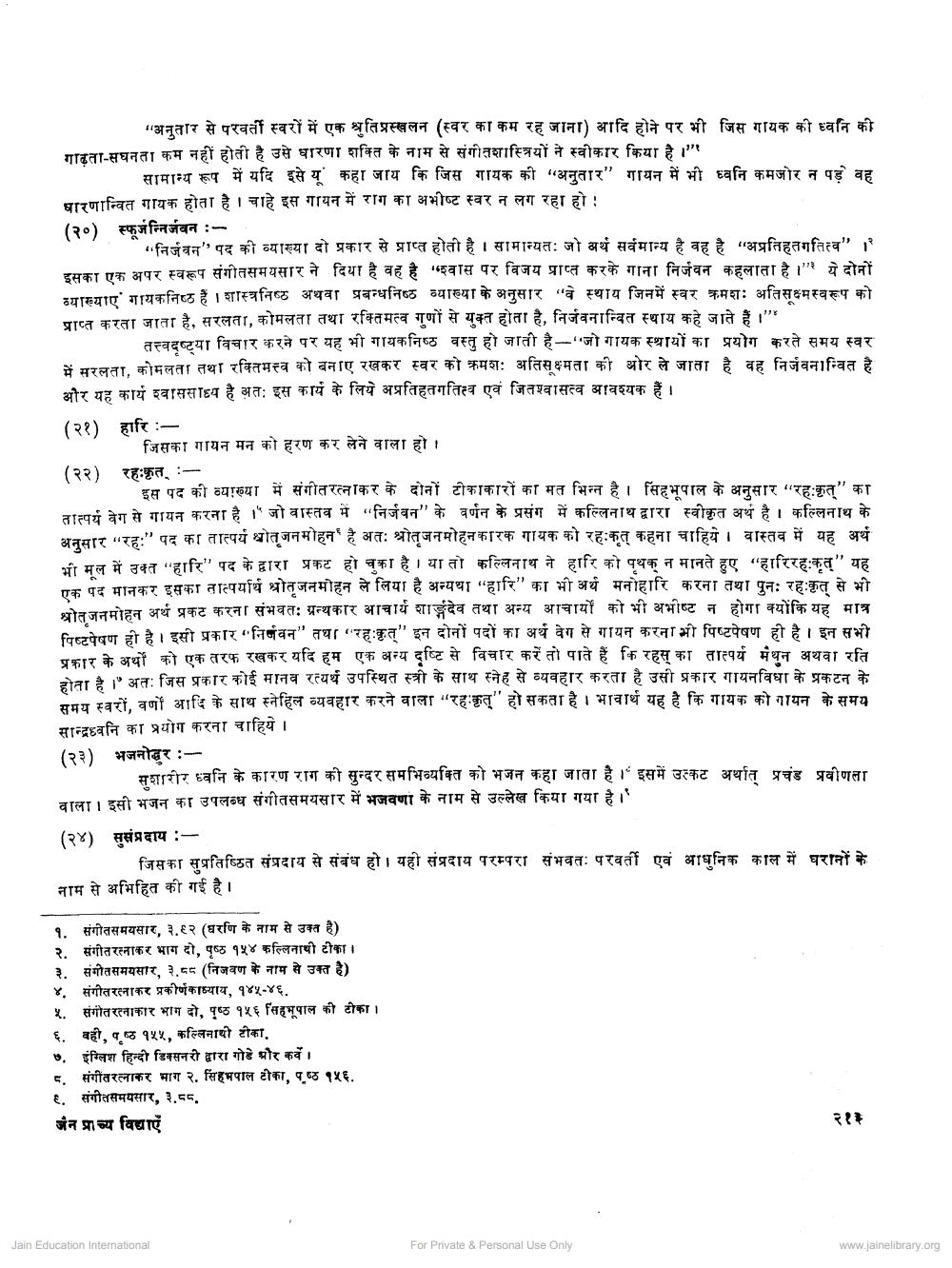________________
"अनुतार से परवर्ती स्वरों में एक श्रुतिप्रस्खलन (स्वर का कम रह जाना) आदि होने पर भी जिस गायक की ध्वनि की गाढता-सघनता कम नहीं होती है उसे धारणा शक्ति के नाम से संगीतशास्त्रियों ने स्वीकार किया है।"
सामान्य रूप में यदि इसे यू' कहा जाय कि जिस गायक की “अनुतार" गायन में भी ध्वनि कमजोर न पड़े वह धारणान्वित गायक होता है । चाहे इस गायन में राग का अभीष्ट स्वर न लग रहा हो। (२०) स्फूर्जन्निर्जवन :
निर्जवन' पद की व्याख्या दो प्रकार से प्राप्त होती है । सामान्यत: जो अर्थ सर्वमान्य है वह है "अप्रतिहतगतित्व" ।' इसका एक अपर स्वरूप संगीतसमयसार ने दिया है वह है “वास पर विजय प्राप्त करके गाना निर्जबन कहलाता है। ये दोनों माया गायकनिष्ठ हैं । शास्त्रनिष्ठ अथवा प्रबन्धनिष्ठ व्याख्या के अनुसार "वे स्थाय जिनमें स्वर क्रमशः अतिसक्षमस्वरूप को प्राप्त करता जाता है, सरलता, कोमलता तथा रक्तिमत्व गुणों से युक्त होता है, निर्जवनान्वित स्थाय कहे जाते हैं।"
तत्वदष्ट्या विचार करने पर यह भी गायकनिष्ठ वस्तु हो जाती है- 'जो गायक स्थायों का प्रयोग करते समय स्वर में सरलता, कोमलता तथा रक्तिमत्त्व को बनाए रखकर स्वर को क्रमशः अतिसक्षमता की ओर ले जाता है वह निर्जवनान्वित है और यह कार्य श्वाससाध्य है अत: इस कार्य के लिये अप्रतिहतगतित्व एवं जितश्वासत्व आवश्यक हैं। (२१) हारि:
जिसका गायन मन को हरण कर लेने वाला हो। (२२) रहःकृत :
इस पद की व्याख्या में संगीतरत्नाकर के दोनों टीकाकारों का मत भिन्न है। सिंहभूपाल के अनुसार "रहःकृत्" का तात्पर्य वेग से गायन करना है । जो वास्तव में “निर्जवन" के वर्णन के प्रसंग में कल्लिनाथ द्वारा स्वीकृत अर्थ है। कल्लिनाथ के अनसार "रहः" पद का तात्पर्य धोतृजनमोहन' है अतः श्रोतृजनमोहन कारक गायक को रहःकत् कहना चाहिये । वास्तव में यह अर्थ भी मल में उक्त "हारि" पद के द्वारा प्रकट हो चुका है। या तो कल्लिनाथ ने हारि को पृथक् न मानते हुए "हारिरहःकृत्" यह एक पद मानकर इसका तात्पर्याथ श्रोत जनमोहन ले लिया है अन्यथा "हारि" का भी अर्थ मनोहारि करना तथा पूनः रहःकृत से भी श्रोत जनमोहन अर्थ प्रकट करना संभवतः ग्रन्थकार आचार्य शाङ्गंदेव तथा अन्य आचार्यों को भी अभीष्ट न होगा क्योंकि यह मात्र विनोखणही है। इसी प्रकार निर्जवन" तथा रहःकृत्" इन दोनों पदों का अर्थ वेग से गायन करना भी पिष्टपेषण ही है। इन सभी प्रकार के अर्थों को एक तरफ रखकर यदि हम एक अन्य दृष्टि से विचार करें तो पाते हैं कि रहस् का तात्पर्य मैथन अथवा रति होता है। अतः जिस प्रकार कोई मानव रत्यर्थ उपस्थित स्त्री के साथ स्नेह से व्यवहार करता है उसी प्रकार गायनविधा के प्रकटन के
य स्वरों, वर्णों आदि के साथ स्नेहिल व्यवहार करने वाला "रह कृत्" हो सकता है । भावार्थ यह है कि गायक को गायन के समय सान्द्रध्वनि का प्रयोग करना चाहिये । (२३) भजनोद्धर :
मशारीर ध्वनि के कारण राग की सुन्दर समभिव्यक्ति को भजन कहा जाता है । इसमें उत्कट अर्थात् प्रचंड प्रवीणला वाला। इसी भजन का उपलब्ध संगीतसमयसार में भजवणा के नाम से उल्लेख किया गया है। (२४) सुसंप्रदाय :
जिसका सुप्रतिष्ठित संप्रदाय से संबंध हो। यही संप्रदाय परम्परा संभवतः परवर्ती एवं आधुनिक काल में घरानों के नाम से अभिहित की गई है।
१. संगीतसमयसार, ३.६२ (घरणि के नाम से उक्त है) २. संगीतरत्नाकर भाग दो, पृष्ठ १५४ कल्लिनाथी टीका। ३. संगीतसमयसार, ३.८८ (निजवण के नाम से उक्त है) ४. संगीतरत्नाकर प्रकीर्णकाध्याय, १४५-४६. ५. संगीतरत्नाकार भाग दो, पृष्ठ १५६ सिंहभूपाल की टीका। ६. वही, पृष्ठ १५५, कल्लिनाथी टीका, ७. इंग्लिश हिन्दी डिक्सनरी द्वारा गोडे और कर्वे। ५. संगीतरत्नाकर भाग २. सिंहभपाल टीका, प.ष्ठ १५६. ९. संगीतसमयसार, ३.८८. जैन प्राच्य विद्याएँ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org