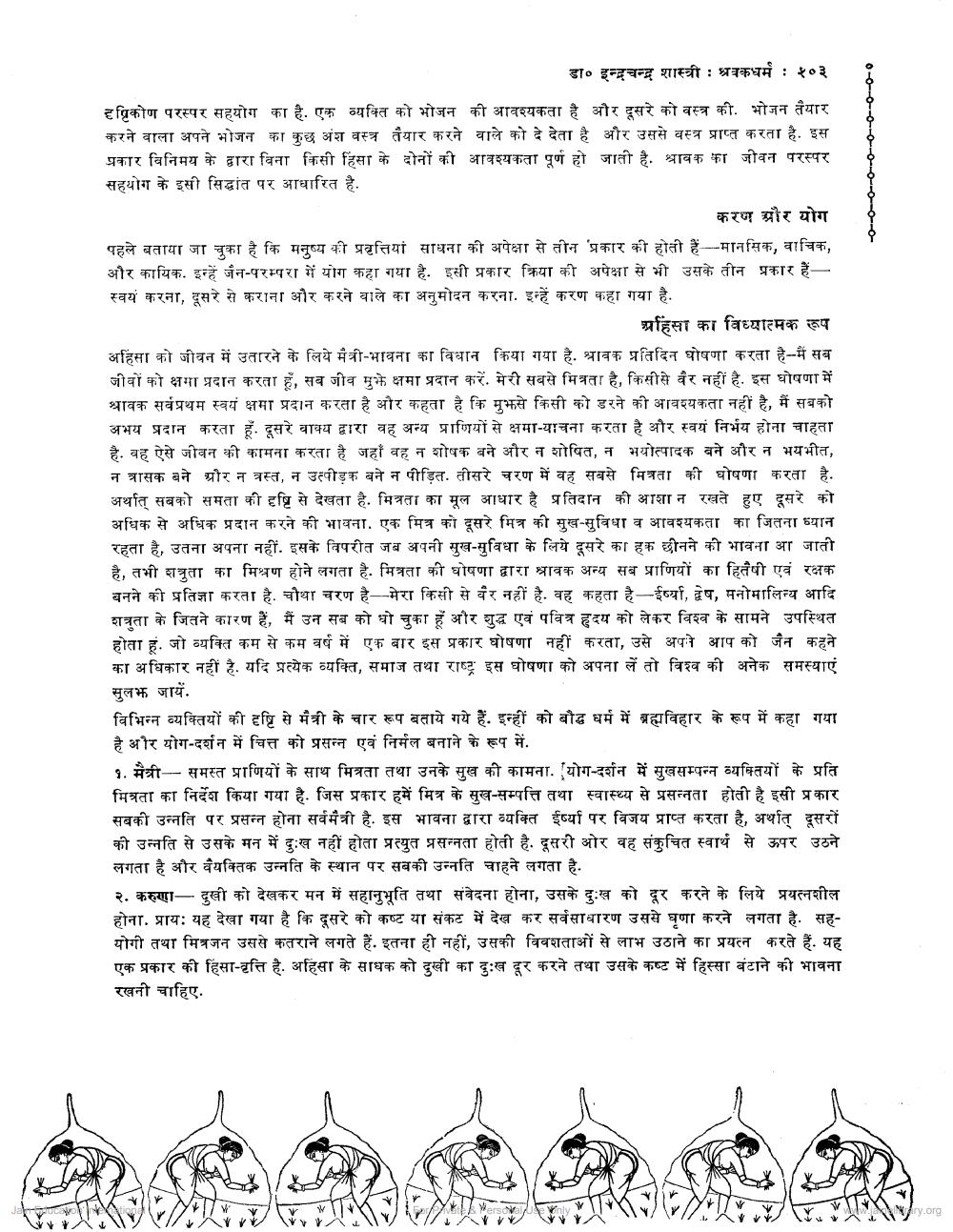________________
डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री : श्रवकधर्म : १०३
------------------
दृट्टिकोण परस्पर सहयोग का है. एक व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है और दूसरे को वस्त्र की. भोजन तैयार करने वाला अपने भोजन का कुछ अंश वस्त्र तैयार करने वाले को दे देता है और उससे वस्त्र प्राप्त करता है. इस प्रकार विनिमय के द्वारा बिना किसी हिंसा के दोनों की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है. श्रावक का जीवन परस्पर सहयोग के इसी सिद्धांत पर आधारित है.
करण और योग पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य की प्रवृत्तियां साधना की अपेक्षा से तीन प्रकार की होती हैं.-.-मानसिक, वाचिक, और कायिक. इन्हें जन-परम्परा में योग कहा गया है. इसी प्रकार क्रिया की अपेक्षा से भी उसके तीन प्रकार हैंस्वयं करना, दूसरे से कराना और करने वाले का अनुमोदन करना. इन्हें करण कहा गया है.
___ अहिंसा का विध्यात्मक रूप अहिंसा को जीवन में उतारने के लिये मैत्री-भावना का विधान किया गया है. श्रावक प्रतिदिन घोषणा करता है-मैं सब जीवों को क्षमा प्रदान करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें. मेरी सबसे मित्रता है, किसीसे वैर नहीं है. इस घोषणा में श्रावक सर्वप्रथम स्वयं क्षमा प्रदान करता है और कहता है कि मुझसे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं सबको अभय प्रदान करता हूँ. दूसरे वाक्य द्वारा वह अन्य प्राणियों से क्षमा-याचना करता है और स्वयं निर्भय होना चाहता है. वह ऐसे जीवन की कामना करता है जहाँ वह न शोषक बने और न शोषित, न भयोत्पादक बने और न भयभीत, न त्रासक बने और न त्रस्त, न उत्पीड़क बने न पीड़ित. तीसरे चरण में वह सबसे मित्रता की घोषणा करता है. अर्थात् सबको समता की दृष्टि से देखता है. मित्रता का मूल आधार है प्रतिदान की आशा न रखते हुए दूसरे को अधिक से अधिक प्रदान करने की भावना. एक मित्र को दूसरे मित्र की सुख-सुविधा व आवश्यकता का जितना ध्यान रहता है, उतना अपना नहीं. इसके विपरीत जब अपनी सुख-सुविधा के लिये दूसरे का हक छीनने की भावना आ जाती है, तभी शत्रुता का मिश्रण होने लगता है. मित्रता की घोषणा द्वारा श्रावक अन्य सब प्राणियों का हितैषी एवं रक्षक बनने की प्रतिज्ञा करता है. चौथा चरण है-मेरा किसी से वैर नहीं है. वह कहता है-ईर्ष्या, द्वेष, मनोमालिन्य आदि शत्रुता के जितने कारण हैं, मैं उन सब को धो चुका हूँ और शुद्ध एवं पवित्र हृदय को लेकर विश्व के सामने उपस्थित होता हूं. जो व्यक्ति कम से कम वर्ष में एक बार इस प्रकार घोषणा नहीं करता, उसे अपने आप को जैन कहने का अधिकार नहीं है. यदि प्रत्येक व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र इस घोषणा को अपना लें तो विश्व की अनेक समस्याएं सुलझ जायें. विभिन्न व्यक्तियों की दृष्टि से मैत्री के चार रूप बताये गये हैं. इन्हीं को बौद्ध धर्म में ब्रह्मविहार के रूप में कहा गया है और योग-दर्शन में चित्त को प्रसन्न एवं निर्मल बनाने के रूप में. १. मैत्री- समस्त प्राणियों के साथ मित्रता तथा उनके सुख की कामना. योग-दर्शन में सुखसम्पन्न व्यक्तियों के प्रति मित्रता का निर्देश किया गया है. जिस प्रकार हमें मित्र के सुख-सम्पत्ति तथा स्वास्थ्य से प्रसन्नता होती है इसी प्रकार सबकी उन्नति पर प्रसन्न होना सर्वमैत्री है. इस भावना द्वारा व्यक्ति ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करता है, अर्थात् दूसरों की उन्नति से उसके मन में दुःख नहीं होता प्रत्युत प्रसन्नता होती है. दूसरी ओर वह संकुचित स्वार्थ से ऊपर उठने लगता है और वैयक्तिक उन्नति के स्थान पर सबकी उन्नति चाहने लगता है. २. करुणा- दुखी को देखकर मन में सहानुभूति तथा संवेदना होना, उसके दुःख को दूर करने के लिये प्रयत्नशील होना. प्रायः यह देखा गया है कि दूसरे को कष्ट या संकट में देख कर सर्वसाधारण उससे घृणा करने लगता है. सहयोगी तथा मित्रजन उससे कतराने लगते हैं. इतना ही नहीं, उसकी विवशताओं से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं. यह एक प्रकार की हिंसा-वृत्ति है. अहिंसा के साधक को दुखी का दु:ख दूर करने तथा उसके कष्ट में हिस्सा बंटाने की भावना रखनी चाहिए.
RANry.org