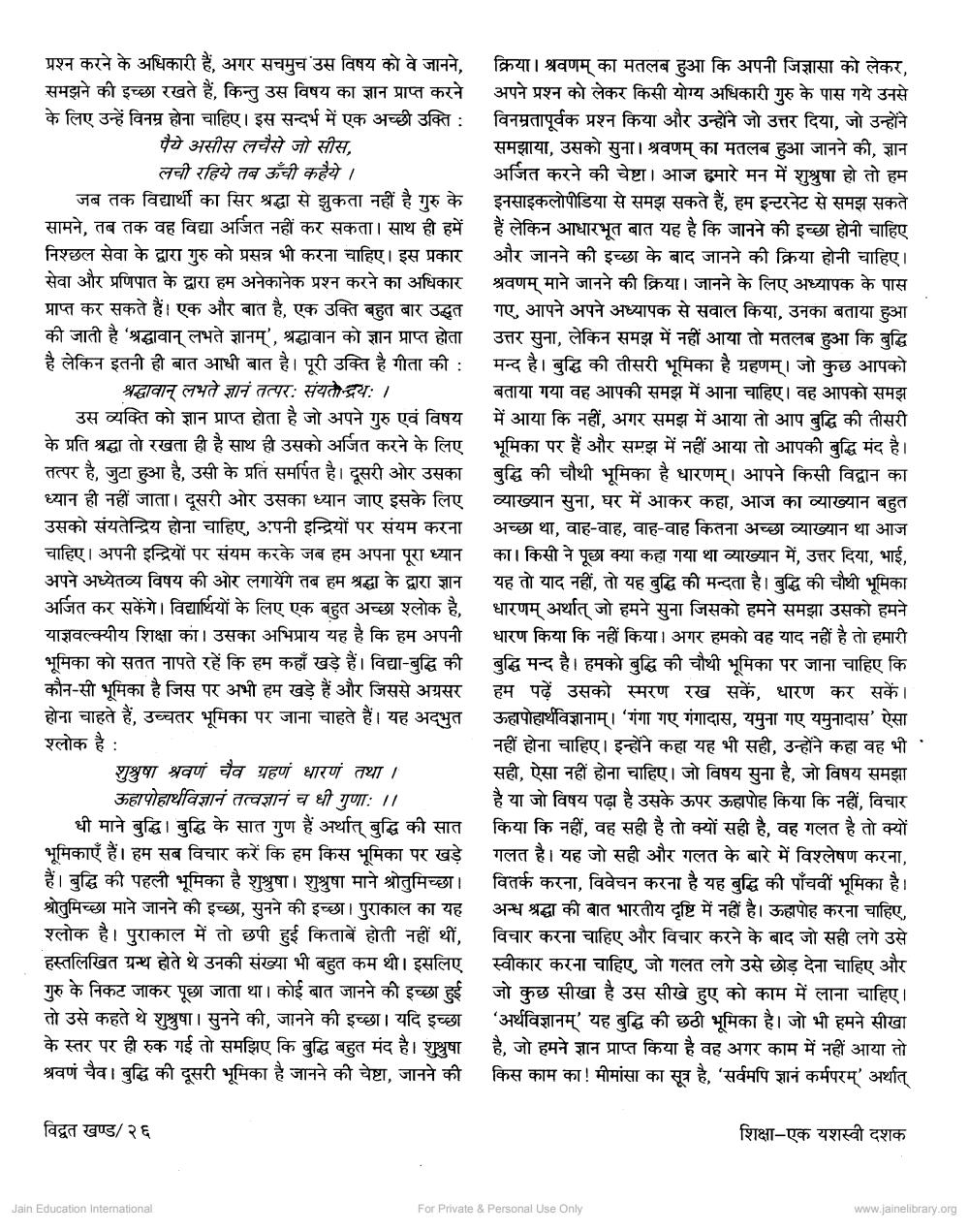________________
प्रश्न करने के अधिकारी हैं, अगर सचमुच उस विषय को वे जानने, समझने की इच्छा रखते हैं, किन्तु उस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें विनम्र होना चाहिए। इस सन्दर्भ में एक अच्छी उक्ति पैये असीस लवैसे जो सीस, लवी रहिये तब ऊँची कहैये ।
:
जब तक विद्यार्थी का सिर श्रद्धा से झुकता नहीं है गुरु के सामने, तब तक वह विद्या अर्जित नहीं कर सकता। साथ ही हमें निश्छल सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न भी करना चाहिए। इस प्रकार सेवा और प्रणिपात के द्वारा हम अनेकानेक प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात है, एक उक्ति बहुत बार उद्धत की जाती है श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन इतनी ही बात आधी बात है पूरी उक्ति है गीता की श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर: संयतोन्द्रयः । उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है जो अपने गुरु एवं विषय प्रति श्रद्धा तो रखता ही है साथ ही उसको अर्जित करने के लिए तत्पर है, जुटा हुआ है, उसी के प्रति समर्पित है। दूसरी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। दूसरी ओर उसका ध्यान जाए इसके लिए उसको संयतेन्द्रिय होना चाहिए, अपनी इन्द्रियों पर संयम करना चाहिए। अपनी इन्द्रियों पर संयम करके जब हम अपना पूरा ध्यान अपने अध्येतव्य विषय की ओर लगायेंगे तब हम श्रद्धा के द्वारा ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, याज्ञवल्क्यीय शिक्षा का उसका अभिप्राय यह है कि हम अपनी भूमिका को सतत नापते रहें कि हम कहाँ खड़े हैं। विद्या - बुद्धि की कौन-सी भूमिका है जिस पर अभी हम खड़े हैं और जिससे अग्रसर होना चाहते हैं, उच्चतर भूमिका पर जाना चाहते हैं। यह अद्भुत श्लोक है :
शुश्रुषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा । ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्वज्ञानं च धी गुणाः ।। धीमाने बुद्धि । बुद्धि के सात गुण हैं अर्थात् बुद्धि की सात भूमिकाएँ हैं। हम सब विचार करें कि हम किस भूमिका पर खड़े हैं। बुद्धि की पहली भूमिका है शुश्रूषा शुश्रूषा माने श्रोतुमिच्छा। श्रोतुमिच्छा माने जानने की इच्छा, सुनने की इच्छा। पुराकाल का यह श्लोक है। पुराकाल में तो छपी हुई किताबें होती नहीं थीं, 'हस्तलिखित ग्रन्थ होते थे उनकी संख्या भी बहुत कम थी इसलिए गुरु के निकट जाकर पूछा जाता था कोई बात जानने की इच्छा हुई तो उसे कहते थे शुश्रुषा । सुनने की, जानने की इच्छा। यदि इच्छा के स्तर पर ही रुक गई तो समझिए कि बुद्धि बहुत मंद है । शुश्रुषा श्रवणं चैव बुद्धि की दूसरी भूमिका है जानने की चेष्टा, जानने की
विद्वत खण्ड / २६
Jain Education International
क्रिया श्रवणम् का मतलब हुआ कि अपनी जिज्ञासा को लेकर, अपने प्रश्न को लेकर किसी योग्य अधिकारी गुरु के पास गये उनसे विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया और उन्होंने जो उत्तर दिया, जो उन्होंने समझाया, उसको सुना। श्रवणम् का मतलब हुआ जानने की, ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा । आज हमारे मन में शुश्रुषा हो तो हम इनसाइक्लोपीडिया से समझ सकते हैं, हम इन्टरनेट से समझ सकते हैं लेकिन आधारभूत बात यह है कि जानने की इच्छा होनी चाहिए और जानने की इच्छा के बाद जानने की क्रिया होनी चाहिए। श्रवणम् माने जानने की क्रिया जानने के लिए अध्यापक के पास गए, आपने अपने अध्यापक से सवाल किया, उनका बताया हुआ उत्तर सुना, लेकिन समझ में नहीं आया तो मतलब हुआ कि बुद्धि मन्द है । बुद्धि की तीसरी भूमिका है ग्रहणम् । जो कुछ आपको बताया गया वह आपकी समझ में आना चाहिए। वह आपको समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तो आप बुद्धि की तीसरी भूमिका पर हैं और समझ में नहीं आया तो आपकी बुद्धि मंद है । बुद्धि की चौथी भूमिका है धारणम्। आपने किसी विद्वान का व्याख्यान सुना, घर में आकर कहा, आज का व्याख्यान बहुत अच्छा था, वाह-वाह, वाह-वाह कितना अच्छा व्याख्यान था आज का। किसी ने पूछा क्या कहा गया था व्याख्यान में, उत्तर दिया, भाई, यह तो याद नहीं, तो यह बुद्धि की मन्दता है । बुद्धि की चौथी भूमिक धारणम् अर्थात् जो हमने सुना जिसको हमने समझा उसको हम धारण किया कि नहीं किया अगर हमको वह याद नहीं है तो हमारी बुद्धि मन्द है हमको बुद्धि की चौथी भूमिका पर जाना चाहिए कि हम पढ़ें उसको स्मरण रख सकें, धारण कर सकें। ऊहापोहार्थविज्ञानाम् । 'गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास' ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा यह भी सही, उन्होंने कहा वह भी सही, ऐसा नहीं होना चाहिए जो विषय सुना है, जो विषय समझा है या जो विषय पढ़ा है उसके ऊपर ऊहापोह किया कि नहीं, विचार किया कि नहीं, वह सही है तो क्यों सही है, वह गलत है तो क्यों गलत है। यह जो सही और गलत के बारे में विश्लेषण करना, वितर्क करना, विवेचन करना है यह बुद्धि की पाँचवीं भूमिका है। अन्धश्रद्धा की बात भारतीय दृष्टि में नहीं है। ऊहापोह करना चाहिए, विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद जो सही लगे उसे स्वीकार करना चाहिए, जो गलत लगे उसे छोड़ देना चाहिए और जो कुछ सीखा है उस सीखे हुए को काम में लाना चाहिए। 'अर्थविज्ञानम्' यह बुद्धि की छठी भूमिका है। जो भी हमने सीखा है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वह अगर काम में नहीं आया तो किस काम का मीमांसा का सूत्र है, 'सर्वमपि ज्ञानं कर्मपरम्' अर्थात्
शिक्षा एक यशस्वी दशक
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org