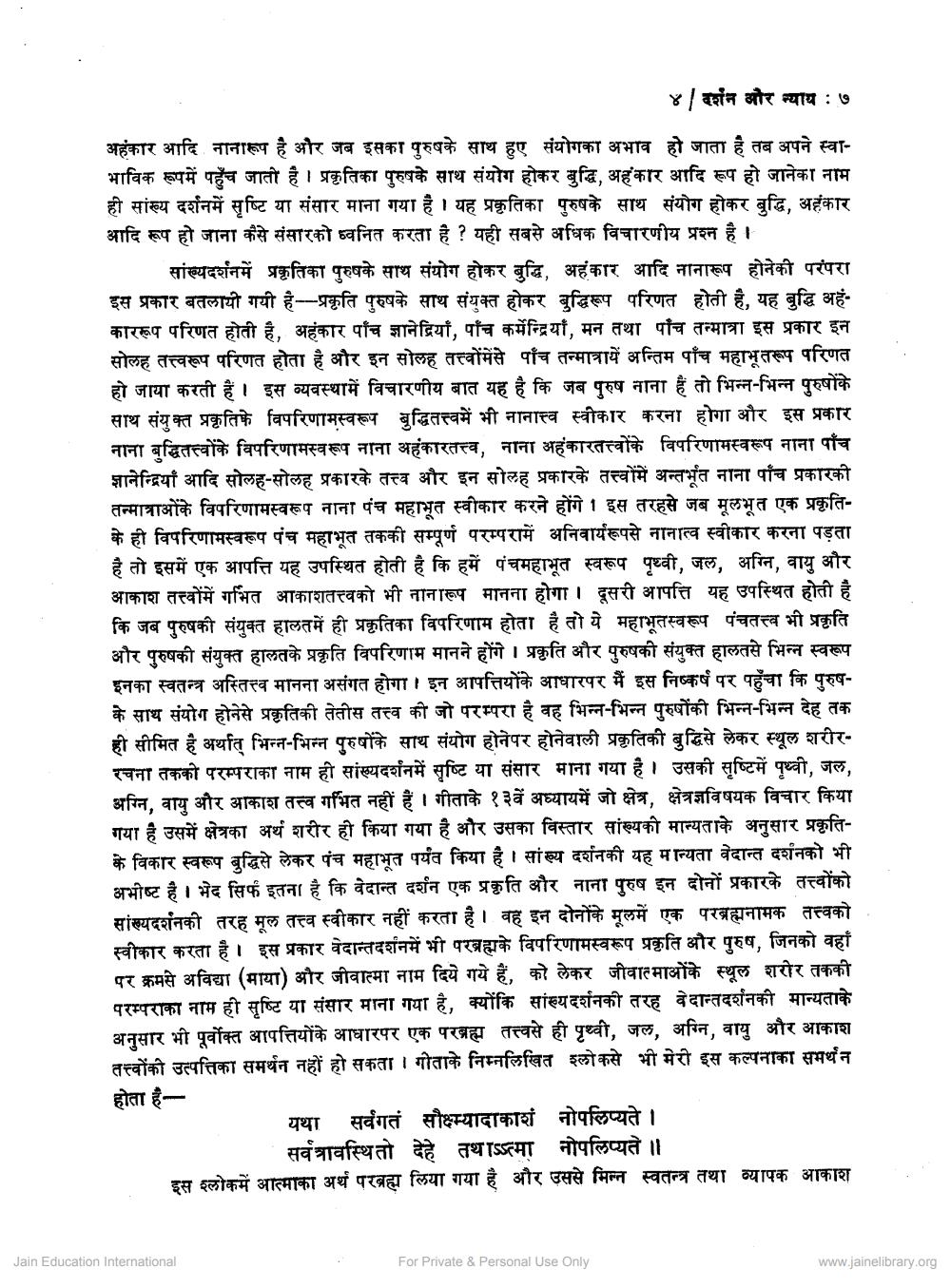________________
४/दर्शन और न्याय : ७
अहंकार आदि नानारूप है और जब इसका पुरुषके साथ हुए संयोगका अभाव हो जाता है तब अपने स्वाभाविक रूपमें पहुँच जाती है। प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, अहंकार आदि रूप हो जानेका नाम ही सांख्य दर्शनमें सृष्टि या संसार माना गया है। यह प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, अहंकार आदि रूप हो जाना कैसे संसारको ध्वनित करता है ? यही सबसे अधिक विचारणीय प्रश्न है।
सांख्यदर्शनमें प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, अहंकार आदि नानारूप होनेकी परंपरा इस प्रकार बतलायी गयी है-प्रकृति पुरुषके साथ संयुक्त होकर बुद्धिरूप परिणत होती है, यह बुद्धि अहंकाररूप परिणत होती है, अहंकार पाँच ज्ञानेद्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन तथा पांच तन्मात्रा इस प्रकार इन सोलह तत्त्वरूप परिणत होता है और इन सोलह तत्त्वोंमेंसे पाँच तन्मात्रायें अन्तिम पाँच महाभूतरूप परिणत हो जाया करती है। इस व्यवस्थामें विचारणीय बात यह है कि जब पुरुष नाना है तो भिन्न-भिन्न पुरुषोंके साथ संयुक्त प्रकृतिके विपरिणामस्वरूप बुद्धितत्त्वमें भी नानात्त्व स्वीकार करना होगा और इस प्रकार नाना बुद्धितत्त्वोंके विपरिणामस्वरूप नाना अहंकारतत्त्व, नाना अहंकारतत्त्वोंके विपरिणामस्वरूप नाना पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ आदि सोलह-सोलह प्रकारके तत्त्व और इन सोलह प्रकारके तत्त्वोंमें अन्तर्भूत नाना पाँच प्रकारको तन्मात्राओंके विपरिणामस्वरूप नाना पंच महाभूत स्वीकार करने होंगे। इस तरहसे जब मूलभूत एक प्रकृतिके ही विपरिणामस्वरूप पंच महाभूत तककी सम्पूर्ण परम्परामें अनिवार्यरूपसे नानात्व स्वीकार करना पड़ता है तो इसमें एक आपत्ति यह उपस्थित होती है कि हमें पंचमहाभूत स्वरूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वोंमें गर्भित आकाशतत्त्वको भी नानारूप मानना होगा। दूसरी आपत्ति यह उपस्थित होती है कि जब पुरुषको संयुक्त हालतमें ही प्रकृतिका विपरिणाम होता है तो ये महाभूतस्वरूप पंचतत्त्व भी प्रकृति
और पुरुषकी संयुक्त हालतके प्रकृति विपरिणाम मानने होंगे । प्रकृति और पुरुषकी संयुक्त हालतसे भिन्न स्वरूप इनका स्वतन्त्र अस्तित्त्व मानना असंगत होगा। इन आपत्तियोंके आधारपर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पुरुषके साथ संयोग होनेसे प्रकृतिकी तेतीस तत्त्व की जो परम्परा है वह भिन्न-भिन्न पुरुषोंकी भिन्न-भिन्न देह तक ही सीमित है अर्थात् भिन्न-भिन्न पुरुषोंके साथ संयोग होनेपर होनेवाली प्रकृतिकी बुद्धिसे लेकर स्थूल शरीररचना तकको परम्पराका नाम ही सांख्यदर्शनमें सृष्टि या संसार माना गया है। उसकी सृष्टिमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्व गर्भित नहीं हैं । गीताके १३वें अध्यायमें जो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञविषयक विचार किया गया है उसमें क्षेत्रका अर्थ शरीर ही किया गया है और उसका विस्तार सांख्यकी मान्यताके अनुसार प्रकृतिके विकार स्वरूप बुद्धिसे लेकर पंच महाभूत पर्यत किया है। सांख्य दर्शनकी यह मान्यता वेदान्त दर्शनको भी अभीष्ट है । भेद सिर्फ इतना है कि वेदान्त दर्शन एक प्रकृति और नाना पुरुष इन दोनों प्रकारके तत्त्वोंको सांख्यदर्शनकी तरह मूल तत्त्व स्वीकार नहीं करता है। वह इन दोनोंके मूलमें एक परब्रह्मनामक तत्त्वको . स्वीकार करता है। इस प्रकार वेदान्तदर्शनमें भी परब्रह्मके विपरिणामस्वरूप प्रकृति और पुरुष, जिनको वहाँ पर क्रमसे अविद्या (माया) और जीवात्मा नाम दिये गये हैं, को लेकर जीवात्माओंके स्थूल शरीर तककी परम्पराका नाम ही सृष्टि या संसार माना गया है, क्योंकि सांख्यदर्शनकी तरह वेदान्तदर्शनकी मान्यताके अनुसार भी पूर्वोक्त आपत्तियोंके आधारपर एक परब्रह्म तत्त्वसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वोंकी उत्पत्तिका समर्थन नहीं हो सकता। गीताके निम्नलिखित श्लोकसे भी मेरी इस कल्पनाका समर्थन होता है
यथा सर्वगतं सौक्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते ।
सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ इस श्लोकमें आत्माका अर्थ परब्रह्म लिया गया है और उससे मिन्न स्वतन्त्र तथा व्यापक आकाश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org