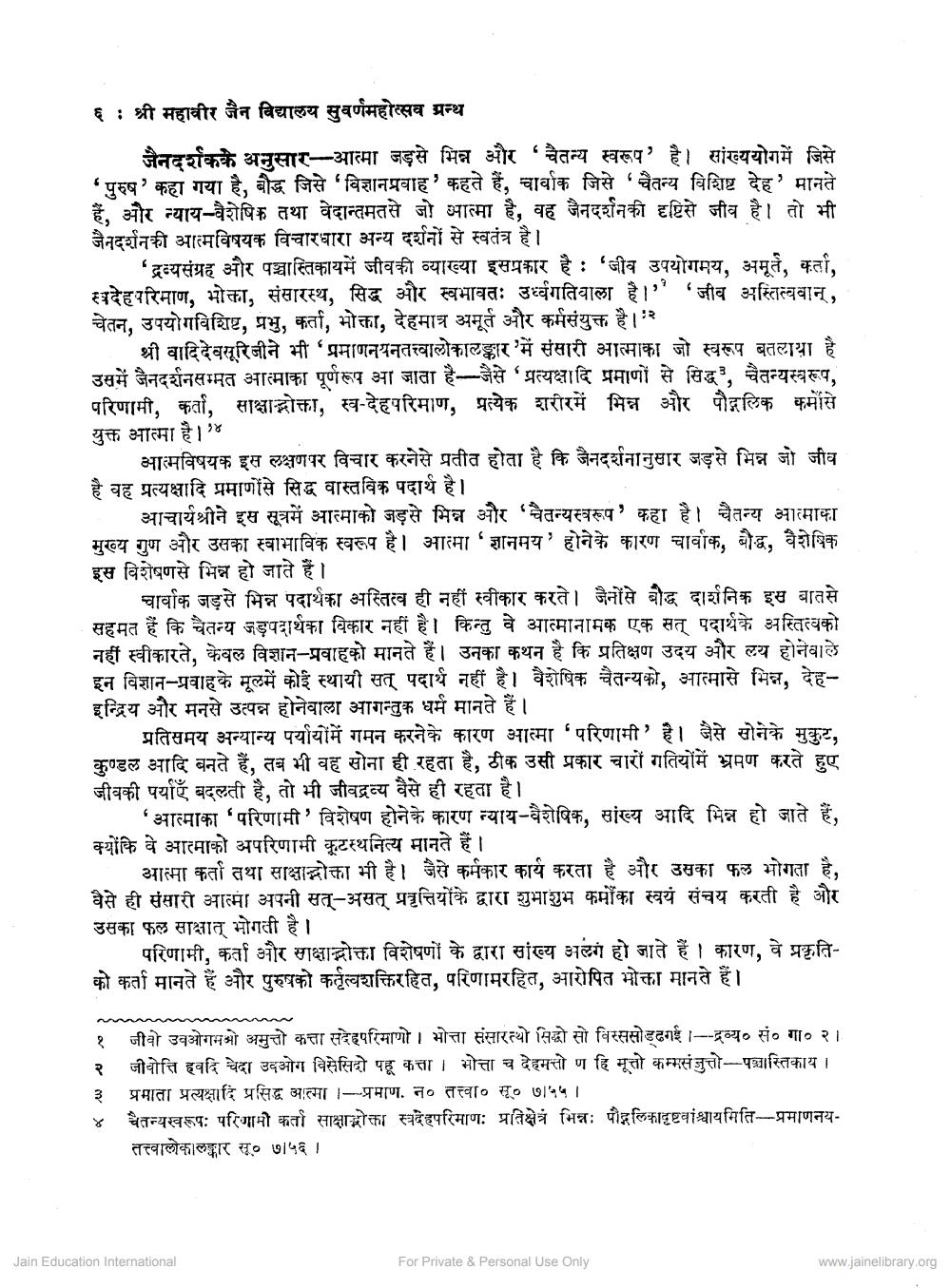________________
६ : श्री महावीर जैन विद्यालय सुवर्णमहोत्सव ग्रन्थ
जैनदर्शकके अनुसार - आत्मा जड़से भिन्न और ' चैतन्य स्वरूप' है। सांख्ययोग में जिसे 'पुरुष' कहा गया है, बौद्ध जिसे 'विज्ञानप्रवाह' कहते हैं, चार्वाक जिसे ' 'चैतन्य विशिष्ट देह' मानते हैं, और न्याय-वैशेषिक तथा वेदान्तमतसे जो आत्मा है, वह जैनदर्शन की दृष्टिसे जीव है । तो भी जैनदर्शन की आत्मविषयक विचारधारा अन्य दर्शनों से स्वतंत्र है ।
' द्रव्यसंग्रह और पञ्चास्तिकायमें जीवकी व्याख्या इसप्रकार है : 'जीव उपयोगमय, अमूर्त, कर्ता, स्वदेह परिमाण, भोक्ता, संसारस्थ, सिद्ध और स्वभावतः उर्ध्वगतिवाला है । " 'जीव अस्तित्ववान्, चेतन, उपयोगविशिष्ट, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देहमात्र अमूर्त और कर्मसंयुक्त है।
श्री वादिदेवसूरिजीने भी ' प्रमाणनयनतत्त्वालोकालङ्कार ' में संसारी आत्माका जो स्वरूप बतलाया है उसमें जैनदर्शनसम्मत आत्माका पूर्णरूप आ जाता है - जैसे 'प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध, चैतन्यस्वरूप, परिणामी, कर्ता, साक्षाद्भोक्ता, स्व- देहपरिमाण, प्रत्येक शरीर में भिन्न और पौद्गलिक कमसे युक्त आत्मा है । १४
आत्मविषयक इस लक्षणपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि जैनदर्शनानुसार जड़ से भिन्न जो जीव है वह प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध वास्तविक पदार्थ है ।
आचार्यश्रीने इस सूत्र आत्माको जड़से भिन्न और 'चैतन्यस्वरूप' कहा है। चैतन्य आत्माका मुख्य गुण और उसका स्वाभाविक स्वरूप है। आत्मा 'ज्ञानमय' होनेके कारण चार्वाक, बौद्ध, वैशेषिक इस विशेषणसे भिन्न हो जाते हैं।
चार्वाक जड़ से भिन्न पदार्थका अस्तित्व ही सहमत हैं कि चैतन्य जड़पदार्थका विकार नहीं है । नहीं स्वीकारते, केवल विज्ञान - प्रवाहको मानते हैं। इन विज्ञान - प्रवाह के मूलमें कोई स्थायी सत् पदार्थ नहीं है। वैशेषिक चैतन्यको, आत्मासे भिन्न, देहइन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाला आगन्तुक धर्म मानते हैं ।
नहीं स्वीकार करते। जैनोंसे बौद्ध दार्शनिक इस बात से किन्तु वे आत्मानामक एक सत् पदार्थके अस्तित्वको उनका कथन है कि प्रतिक्षण उदय और लय होनेवाले
प्रतिसमय अन्यान्य पर्यायों में गमन करनेके कारण आत्मा 'परिणामी ' है । जैसे सोनेके मुकुट, कुण्डल आदि बनते हैं, तब भी वह सोना ही रहता है, ठीक उसी प्रकार चारों गतियोंमें भ्रमण करते हुए जीवकी पर्याएँ बदलती है, तो भी जीवद्रव्य वैसे ही रहता है ।
'आत्माका 'परिणामी ' विशेषण होनेके कारण न्याय-वैशेषिक, सांख्य आदि भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे आत्माको अपरिणामी कूटस्थनित्य मानते हैं ।
आत्मा कर्ता तथा साक्षाद्भोक्ता भी है। जैसे कर्मकार कार्य करता है और उसका फल भोगता है, वैसे ही संसारी आत्मा अपनी सत्-असत् प्रवृत्तियोंके द्वारा शुभाशुभ कर्मोंका स्वयं संचय करती है और उसका फल साक्षात् भोगती है ।
परिणामी, कर्ता और साक्षाद्भोक्ता विशेषणों के द्वारा सांख्य अलग हो जाते हैं । कारण, वे प्रकृतिको कर्ता मानते हैं और पुरुषको कर्तृत्वशक्तिरहित, परिणामरहित, आरोपित भोक्ता मानते हैं ।
१
जीव उवओगमभ अमुत्तो कत्ता सदेहपरिमाणो । भोत्ता संसार त्यो सिद्धो सो विरससोड्ढगई । - द्रव्य० सं० गा० २ । २ जीवोत्ति हवदि चेदा उदओग विसेसिदो पहू कत्ता । भोत्ता च देहमत्तो ण हि मूत्तो कम्मसंजुत्तो - पञ्चास्तिकाय ।
३
૪
प्रमाता प्रत्यक्षादि प्रसिद्ध आत्मा । प्रमाण न० तत्त्वा० सू० ७।५५ ।
चैतन्यखरूपः परिणामी कर्ता साक्षाद्भोका स्वदेहपरिमाणः प्रतिक्षेत्रं भिन्न: पौगलिकादृष्टवांश्चायमिति प्रमाणनयतत्त्वाकालङ्कार सू० ७/५६ |
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org