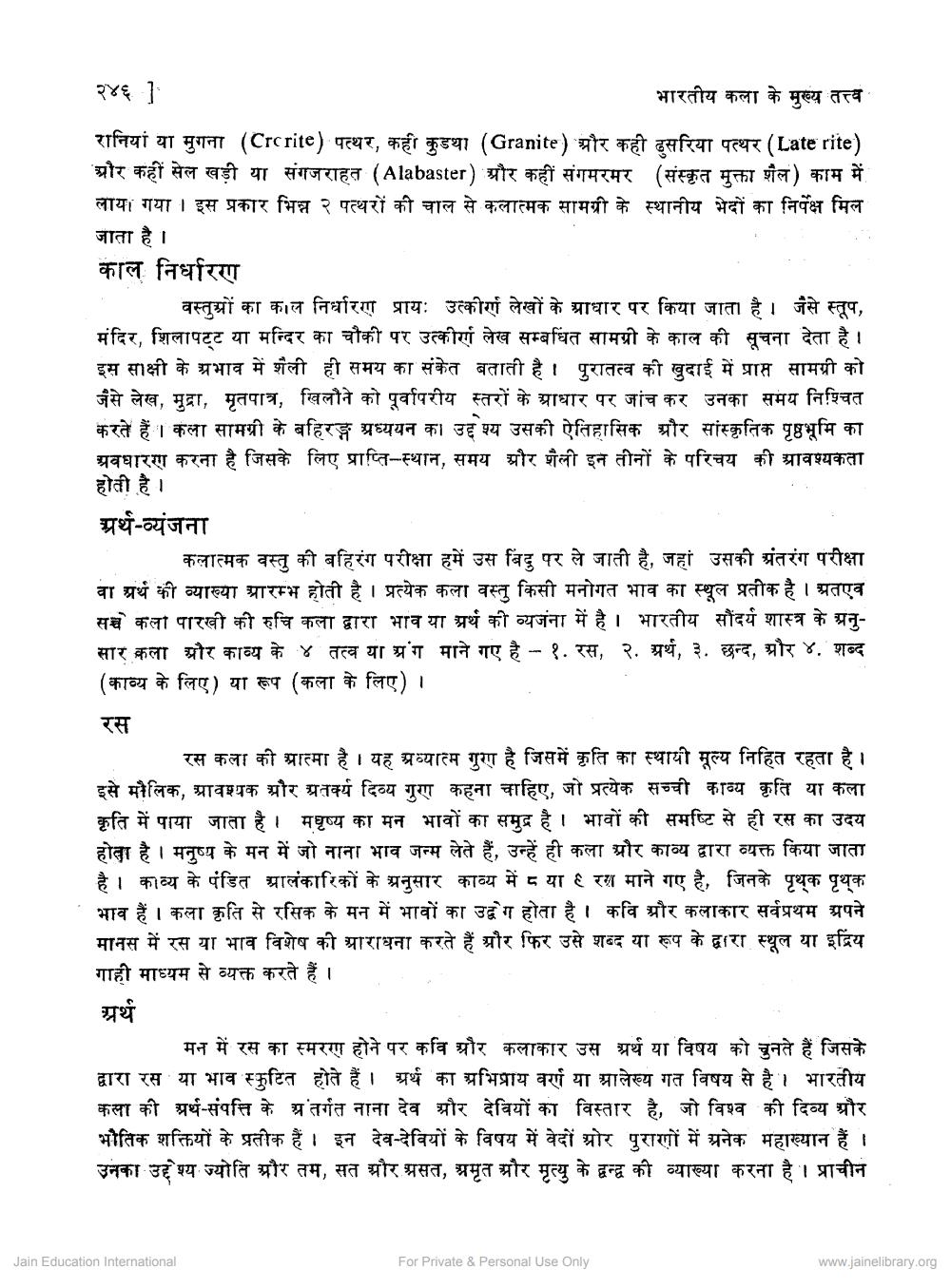________________
२४६ ]
भारतीय कला के मुख्य तत्त्व
रानियां या मुगना (Crcrite) पत्थर, कही कुडथा (Granite) और कही ढुसरिया पत्थर (Late rite) और कहीं सेल खड़ी या संगजराहत (Alabaster) और कहीं संगमरमर (संस्कृत मुक्ता शैल) काम में लाया गया । इस प्रकार भिन्न २ पत्थरों की चाल से कलात्मक सामग्री के स्थानीय भेदों का निर्पक्ष मिल जाता है। काल निर्धारण
वस्तुओं का काल निर्धारण प्रायः उत्कीर्ण लेखों के आधार पर किया जाता है। जैसे स्तूप, मंदिर, शिलापट्ट या मन्दिर का चौकी पर उत्कीर्ण लेख सम्बधित सामग्री के काल की सूचना देता है । इस साक्षी के अभाव में शैली ही समय का संकेत बताती है। पुरातत्व की खुदाई में प्राप्त सामग्री को जैसे लेख, मुद्रा, मृतपात्र, खिलौने को पूर्वापरीय स्तरों के आधार पर जांच कर उनका समय निश्चित करते हैं। कला सामग्री के बहिरङ्ग अध्ययन का उद्दश्य उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवधारण करना है जिसके लिए प्राप्ति-स्थान, समय और शैली इन तीनों के परिचय की आवश्यकता होती है। अर्थ-व्यंजना
कलात्मक वस्तु की बहिरंग परीक्षा हमें उस बिंदु पर ले जाती है, जहां उसकी अंतरंग परीक्षा वा अर्थ की व्याख्या प्रारम्भ होती है । प्रत्येक कला वस्तु किसी मनोगत भाव का स्थूल प्रतीक है । अतएव सच्चे कला पारखी की रुचि कला द्वारा भाव या अर्थ की व्यजंना में है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला और काव्य के ४ तत्व या अंग माने गए है -- १. रस, २. अर्थ, ३. छन्द, और ४. शब्द (काव्य के लिए) या रूप (कला के लिए)। रस
रस कला की आत्मा है । यह अव्यात्म गुण है जिसमें कृति का स्थायी मूल्य निहित रहता है। इसे मौलिक, आवश्यक और अतयं दिव्य गुण कहना चाहिए, जो प्रत्येक सच्ची काव्य कृति या कला कृति में पाया जाता है। मघृष्य का मन भावों का समुद्र है । भावों की समष्टि से ही रस का उदय होता है । मनुष्य के मन में जो नाना भाव जन्म लेते हैं, उन्हें ही कला और काव्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। काव्य के पंडित पालंकारिकों के अनुसार काव्य में ८ या ६ रण माने गए है, जिनके पृथक पृथक भाव हैं। कला कृति से रसिक के मन में भावों का उद्वेग होता है। कवि और कलाकार सर्वप्रथम अपने मानस में रस या भाव विशेष की आराधना करते हैं और फिर उसे शब्द या रूप के द्वारा स्थूल या इद्रिय गाही माध्यम से व्यक्त करते हैं । अर्थ
मन में रस का स्मरण होने पर कवि और कलाकार उस अर्थ या विषय को चुनते हैं जिसके द्वारा रस या भाव स्फुटित होते हैं। अर्थ का अभिप्राय वर्ण या आलेख्य गत विषय से है। भारतीय कला की अर्थ-संपत्ति के अंतर्गत नाना देव और देवियों का विस्तार है, जो विश्व की दिव्य और भौतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। इन देव-देवियों के विषय में वेदों और पुराणों में अनेक महाख्यान हैं । उनका उद्देश्य ज्योति और तम, सत और असत, अमृत और मृत्यु के द्वन्द्व की व्याख्या करना है। प्राचीन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org