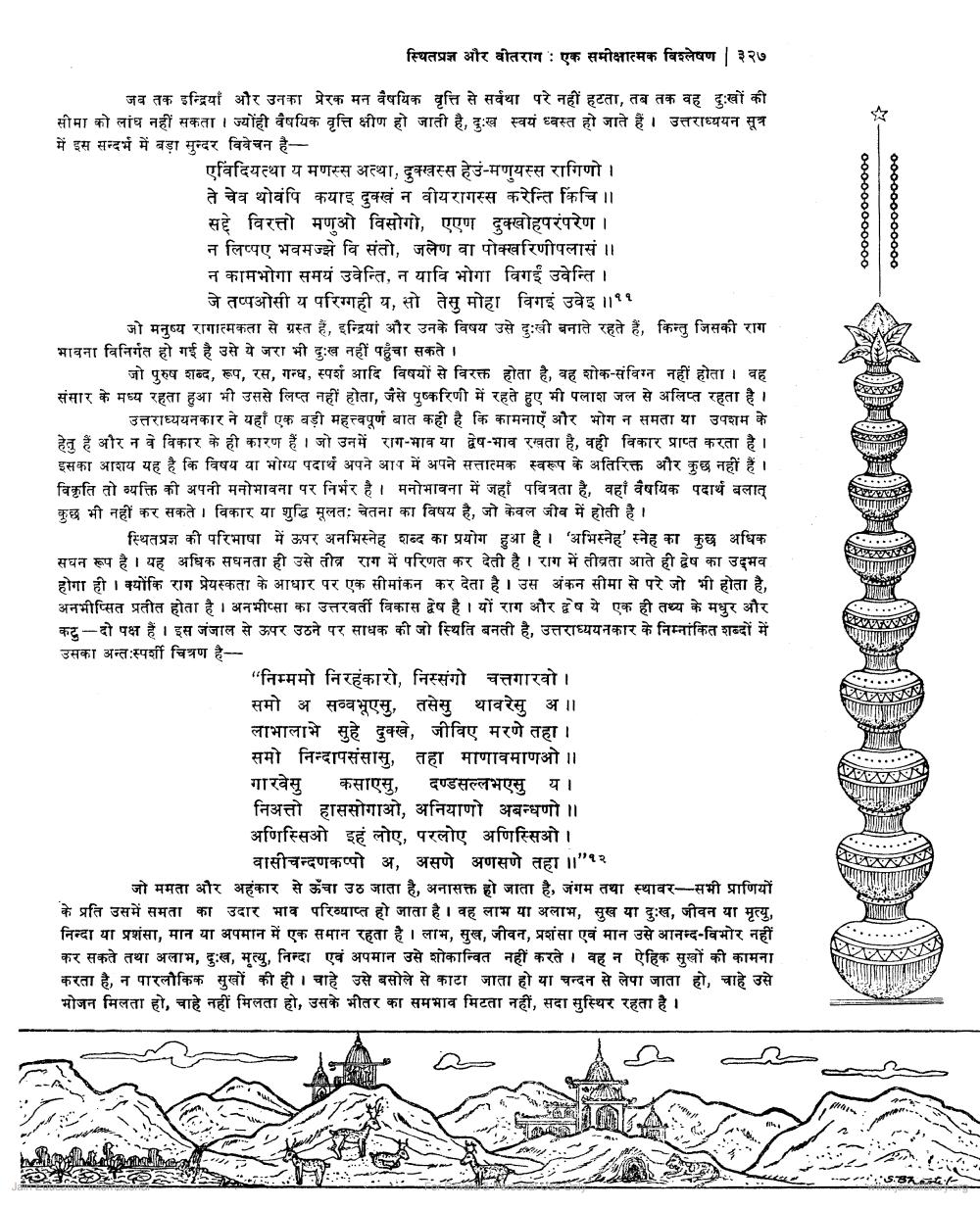________________
स्थितप्रज्ञ और वीतराग : एक समीक्षात्मक विश्लेषण | ३२७
000000000000
००००००००००००
...
भाव या द्वेषक स्वरूप के अतिरिक्तवायिक
......2 ख
जब तक इन्द्रियाँ और उनका प्रेरक मन वैषयिक वृत्ति से सर्वथा परे नहीं हटता, तब तक वह दुःखों की सीमा को लांघ नहीं सकता । ज्योंही वैषयिक वृत्ति क्षीण हो जाती है, दुःख स्वयं ध्वस्त हो जाते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में इस सन्दर्भ में बड़ा सुन्दर विवेचन है
एविदियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउं-मणुयस्स रागिणो। ते चेव थोपि कयाइ दुक्खं न वीयरागस्स करेन्ति किंचि ॥ सद्दे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पए भवमज्झे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ।। न कामभोगा समयं उवेन्ति, न यावि भोगा विगईं उवेन्ति ।
जे तप्पओसी य परिग्गही य, सो तेसु मोहा विगई उवेइ ॥११ जो मनुष्य रागात्मकता से ग्रस्त हैं, इन्द्रियां और उनके विषय उसे दुःखी बनाते रहते हैं, किन्तु जिसकी राग भावना विनिर्गत हो गई है उसे ये जरा भी दुःख नहीं पहुँचा सकते ।
जो पुरुष शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयों से विरक्त होता है, वह शोक-संविग्न नहीं होता। वह संसार के मध्य रहता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, जैसे पुष्करिणी में रहते हुए भी पलाश जल से अलिप्त रहता है।
उत्तराध्ययनकार ने यहाँ एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात कही है कि कामनाएँ और भोग न समता या उपशम के हेतु हैं और न वे विकार के ही कारण हैं । जो उनमें राग-भाव या द्वेष-भाव रखता है, वही विकार प्राप्त करता है। इसका आशय यह है कि विषय या भोग्य पदार्थ अपने आप में अपने सत्तात्मक स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। विकृति तो व्यक्ति को अपनी मनोभावना पर निर्भर है। मनोभावना में जहाँ पवित्रता है, वहाँ वैषयिक पदार्थ बलात् कुछ भी नहीं कर सकते। विकार या शुद्धि मूलत: चेतना का विषय है, जो केवल जीव में होती है।
स्थितप्रज्ञ की परिभाषा में ऊपर अनभिस्नेह शब्द का प्रयोग हुआ है। 'अभिस्नेह' स्नेह का कुछ अधिक सघन रूप है। यह अधिक सघनता ही उसे तीव्र राग में परिणत कर देती है। राग में तीव्रता आते ही द्वेष का उद्भव होगा ही। क्योंकि राग प्रेयस्कता के आधार पर एक सीमांकन कर देता है । उस अंकन सीमा से परे जो भी होता है, अनभीप्सित प्रतीत होता है । अनभीप्सा का उत्तरवर्ती विकास द्वेष है। यों राग और द्वेष ये एक ही तथ्य के मधुर और कटु-दो पक्ष हैं । इस जंजाल से ऊपर उठने पर साधक की जो स्थिति बनती है, उत्तराध्ययनकार के निम्नांकित शब्दों में उसका अन्त:स्पर्शी चित्रण है
"निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो। समो अ सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु अ॥ लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा। समो निन्दापसंसासु, तहा माणावमाणओ ।। गारवेसु कसाएसु, दण्डसल्लभएसु य। निअत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अबन्धणो॥ अणिस्सिओ इह लोए, परलोए अणिस्सिओ।
वासीचन्दणकप्पो अ, असणे अणसणे तहा।"१२ जो ममता और अहंकार से ऊँचा उठ जाता है, अनासक्त हो जाता है, जंगम तथा स्थावर-सभी प्राणियों के प्रति उसमें समता का उदार भाव परिव्याप्त हो जाता है । वह लाभ या अलाभ, सुख या दुःख, जीवन या मृत्यु, निन्दा या प्रशंसा, मान या अपमान में एक समान रहता है । लाभ, सुख, जीवन, प्रशंसा एवं मान उसे आनन्द-विभोर नहीं कर सकते तथा अलाभ, दुःख, मृत्यु, निन्दा एवं अपमान उसे शोकान्वित नहीं करते। वह न ऐहिक सुखों की कामना करता है, न पारलौकिक सुखों की ही। चाहे उसे बसोले से काटा जाता हो या चन्दन से लेपा जाता हो, चाहे उसे भोजन मिलता हो, चाहे नहीं मिलता हो, उसके भीतर का समभाव मिटता नहीं, सदा सुस्थिर रहता है।
ARTWESH
LAAIVANVI
.
DAANA
.
Shank