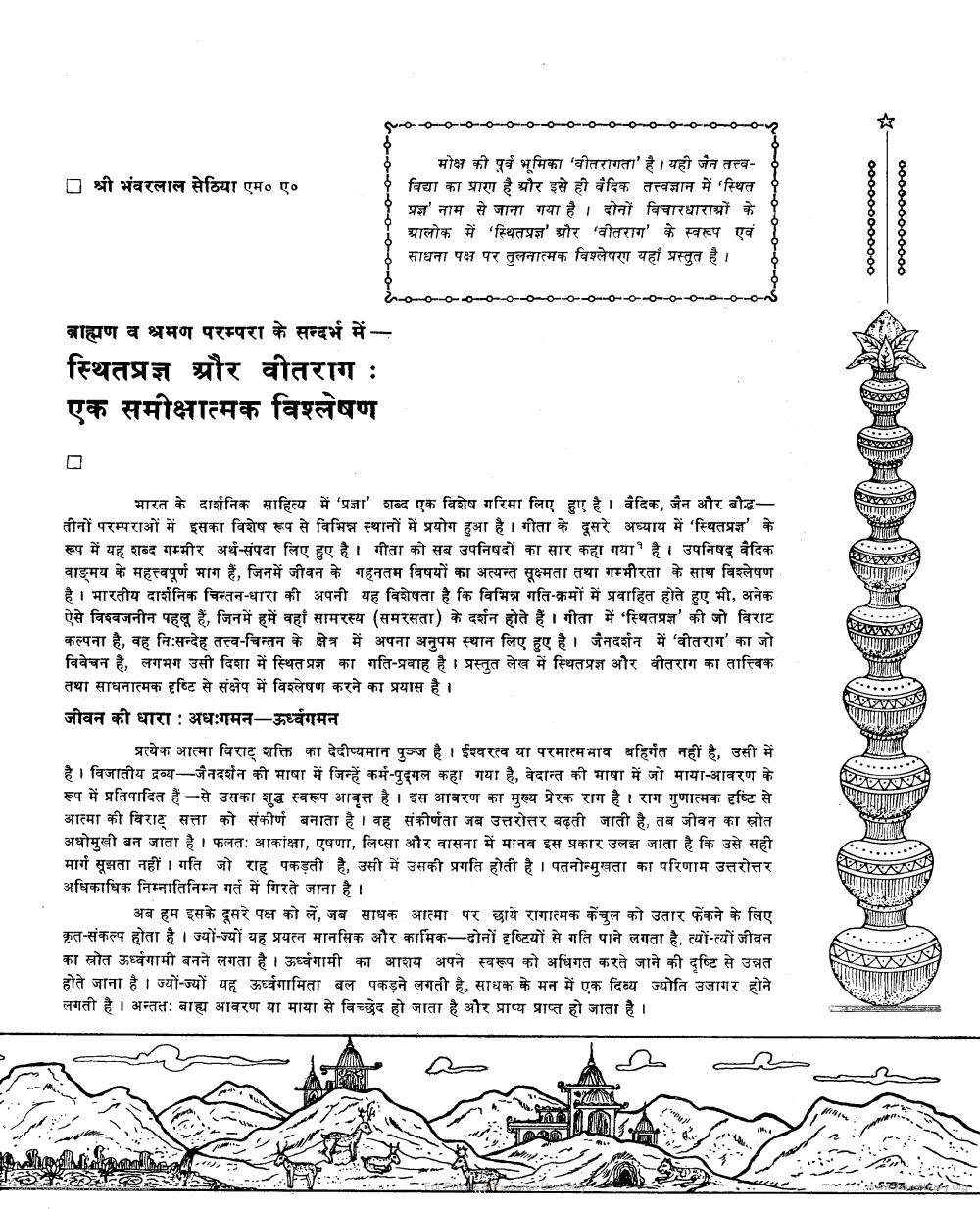________________
श्री भंवरलाल सेठिया एम० ए०
Some
ब्राह्मण व भ्रमण परम्परा के सन्दर्भ में -
:
स्थितप्रज्ञ और श्रौर वीतराग एक समीक्षात्मक विश्लेषण
मोक्ष की पूर्व भूमिका 'वीतरागता' है। यही जैन तत्त्वविद्या का प्रारण है और इसे ही वैदिक तत्त्वज्ञान में स्थित प्रज्ञ' नाम से जाना गया है। दोनों विचारधाराओं के आलोक में 'स्थितप्रज्ञ' और 'वीतराग' के स्वरूप एवं साधना पक्ष पर तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है ।
भारत के दार्शनिक साहित्य में 'प्रज्ञा' शब्द एक विशेष गरिमा लिए हुए है। तीनों परम्पराओं में इसका विशेष रूप से विभिन्न स्थानों में प्रयोग हुआ है। गीता के दूसरे रूप में यह शब्द गम्भीर अर्थ संपदा लिए हुए है। वाङ्मय के महत्त्वपूर्ण माग हैं, जिनमें जीवन के है । भारतीय दार्शनिक चिन्तन-धारा की अपनी ऐसे विश्वजनीन पहलू हैं, जिनमें हमें वहाँ सामरस्य कल्पना है, वह निःसन्देह तत्त्व- चिन्तन के क्षेत्र में विवेचन है, लगभग उसी दिशा में स्थितप्रज्ञ का तथा साधनात्मक दृष्टि से संक्षेप में विश्लेषण करने का प्रयास है । जीवन की धारा : अधः गमन-ऊर्ध्वगमन
वैदिक, जैन और बौद्धअध्याय में 'स्थितप्रज्ञ' के गीता को सब उपनिषदों का सार कहा गया है । उपनिषद् वैदिक गहनतम विषयों का अत्यन्त सूक्ष्मता तथा गम्भीरता के साथ विश्लेषण - यह विशेषता है कि विभिन्न गति क्रमों में प्रवाहित होते हुए भी, अनेक ( समरसता ) के दर्शन होते हैं। गीता में 'स्थितप्रज्ञ' की जो विराट अपना अनुपम स्थान लिए हुए है। जैनदर्शन में 'वीतराग' का जो गति प्रवाह है। प्रस्तुत लेख में स्थितप्रज्ञ और वीतराग का तात्त्विक
with Babaa
प्रत्येक आत्मा विराट् शक्ति का देदीप्यमान पुञ्ज है । ईश्वरत्व या परमात्मभाव बहिर्गत नहीं है, उसी में है। विजातीय द्रव्य - जैनदर्शन की भाषा में जिन्हें कर्म- पुद्गल कहा गया है, वेदान्त की भाषा में जो माया आवरण के रूप में प्रतिपादित हैं - से उसका शुद्ध स्वरूप आवृत्त है। इस आवरण का मुख्य प्रेरक राग है । राग गुणात्मक दृष्टि से आत्मा की विराट् सत्ता को संकीर्ण बनाता है। वह संकीर्णता जब उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तब जीवन का स्रोत अधोमुखी बन जाता है । फलतः आकांक्षा, एषणा, लिप्सा और वासना में मानव इस प्रकार उलझ जाता है कि उसे सही मार्ग सूझता नहीं । गति जो राह पकड़ती है, उसी में उसकी प्रगति होती है । पतनोन्मुखता का परिणाम उत्तरोत्तर अधिकाधिक निम्नातिनिम्न गर्त में गिरते जाना है ।
-
अब हम इसके दूसरे पक्ष को लें, जब साधक आत्मा पर छाये रागात्मक केंचुल को उतार फेंकने के लिए कृत-संकल्प होता है । ज्यों-ज्यों यह प्रयत्न मानसिक और कार्मिक — दोनों दृष्टियों से गति पाने लगता है, त्यों-त्यों जीवन का स्रोत ऊर्ध्वगामी बनने लगता है। ऊर्ध्वगामी का आशय अपने स्वरूप को अधिगत करते जाने की दृष्टि से उन्नत होते जाना है । ज्यों-ज्यों यह ऊर्ध्वगामिता बल पकड़ने लगती है, साधक के मन में एक दिव्य ज्योति उजागर होने लगती है । अन्ततः बाह्य आवरण या माया से विच्छेद हो जाता है और प्राप्य प्राप्त हो जाता है ।
AM
T
000000000000
par
000000000000
0010110006