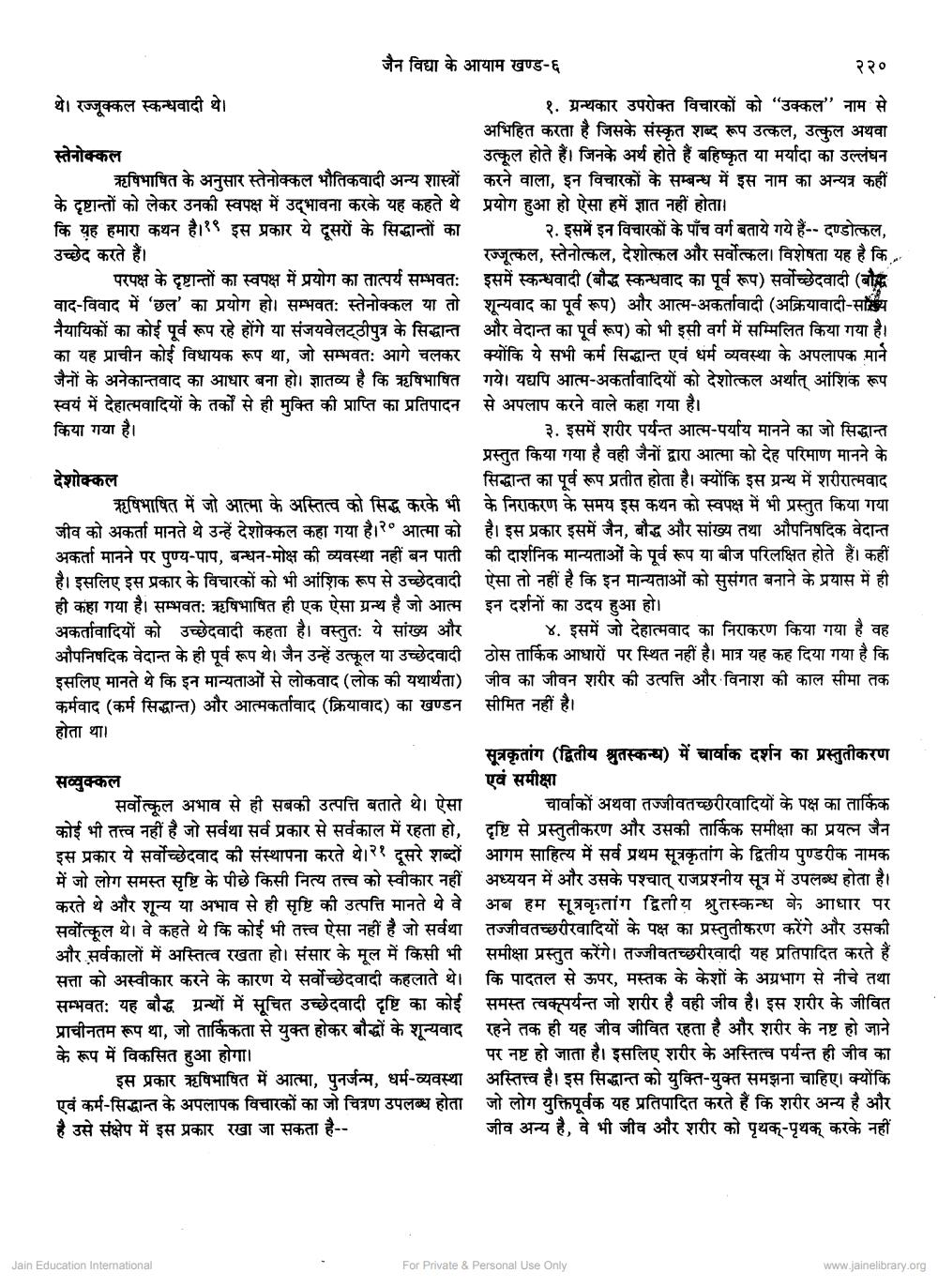________________
जैन विद्या के आयाम खण्ड ६
थे। रज्जुक्कल स्कन्धवादी थे।
स्तेनोक्कल
ऋषिभाषित के अनुसार स्तेनोक्कल भौतिकवादी अन्य शास्त्रों के दृष्टान्तों को लेकर उनकी स्वपक्ष में उद्भावना करके यह कहते थे कि यह हमारा कथन है। १९ इस प्रकार ये दूसरों के सिद्धान्तों का उच्छेद करते हैं।
परपक्ष के दृष्टान्तों का स्वपक्ष में प्रयोग का तात्पर्य सम्भवतः वाद-विवाद में 'छल' का प्रयोग हो। सम्भवतः स्तेनोक्कल या तो नैयायिकों का कोई पूर्व रूप रहे होंगे या संजयवेलट्ठीपुत्र के सिद्धान्त का यह प्राचीन कोई विधायक रूप था, जो सम्भवतः आगे चलकर जैनों के अनेकान्तवाद का आधार बना हो। ज्ञातव्य है कि ऋषिभाषित स्वयं में देहात्मवादियों के तर्कों से ही मुक्ति की प्राप्ति का प्रतिपादन किया गया है।
देशोक्कल
ऋषिभाषित में जो आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करके भी जीव को अकर्ता मानते थे उन्हें देशोक्कल कहा गया है। २० आत्मा को अकर्ता मानने पर पुण्य-पाप बन्धन मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन पाती है। इसलिए इस प्रकार के विचारकों को भी आंशिक रूप से उच्छेदवादी ही कहा गया है। सम्भवतः ऋषिभाषित ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो आत्म अकर्तावादियों को उच्छेदवादी कहता है। वस्तुतः ये सांख्य और औपनिषदिक वेदान्त के ही पूर्व रूप थे। जैन उन्हें उत्कूल या उच्छेदवादी इसलिए मानते थे कि इन मान्यताओं से लोकवाद (लोक की यथार्थता) कर्मवाद (कर्म सिद्धान्त) और आत्मकर्तावाद (क्रियावाद) का खण्डन होता था।
सव्बुक्कल
सर्वोत्कूल अभाव से ही सबकी उत्पत्ति बताते थे। ऐसा कोई भी तत्त्व नहीं है जो सर्वथा सर्व प्रकार से सर्वकाल में रहता हो, इस प्रकार ये सर्वोच्छेदवाद की संस्थापना करते थे । २१ दूसरे शब्दों में जो लोग समस्त सृष्टि के पीछे किसी नित्य तत्त्व को स्वीकार नहीं करते थे और शून्य या अभाव से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानते थे वे सर्वोत्कूल थे। वे कहते थे कि कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है जो सर्वथा और सर्वकालों में अस्तित्व रखता हो। संसार के मूल में किसी भी सत्ता को अस्वीकार करने के कारण ये सर्वोच्छेदवादी कहलाते थे। सम्भवतः यह बौद्ध ग्रन्थों में सूचित उच्छेदवादी दृष्टि का कोई प्राचीनतम रूप था, जो तार्किकता से युक्त होकर बौद्धों के शून्यवाद के रूप में विकसित हुआ होगा।
इस प्रकार ऋषिभाषित में आत्मा, पुनर्जन्म, धर्म-व्यवस्था एवं कर्म-सिद्धान्त के अपलापक विचारकों का जो चित्रण उपलब्ध होता है उसे संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है-
Jain Education International
२२०
१. ग्रन्थकार उपरोक्त विचारकों को "उक्कल" नाम से अभिहित करता है जिसके संस्कृत शब्द रूप उत्कल, उत्कुल अथवा उत्कूल होते हैं जिनके अर्थ होते हैं बहिष्कृत या मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, इन विचारकों के सम्बन्ध में इस नाम का अन्यत्र कहीं प्रयोग हुआ हो ऐसा हमें ज्ञात नहीं होता ।
२. इसमें इन विचारकों के पाँच वर्ग बताये गये हैं-- दण्डोत्कल, रज्जूत्कल, स्तेनोत्कल, देशोत्कल और सर्वोत्कल विशेषता यह है कि इसमें स्कन्धवादी (बौद्ध स्कन्धवाद का पूर्व रूप) सर्वोच्छेदवादी (बौद्ध शून्यवाद का पूर्व रूप) और आत्म अकर्तावादी (अक्रियावादी सांप और वेदान्त का पूर्व रूप) को भी इसी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि ये सभी कर्म सिद्धान्त एवं धर्म व्यवस्था के अपलापक माने गये। यद्यपि आत्म-अकर्तावादियों को देशोत्कल अर्थात् आंशिक रूप से अपलाप करने वाले कहा गया है।
३. इसमें शरीर पर्यन्त आत्म-पर्याय मानने का जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है वही जैनों द्वारा आत्मा को देह परिमाण मानने के सिद्धान्त का पूर्व रूप प्रतीत होता है। क्योंकि इस ग्रन्थ में शरीरात्मवाद के निराकरण के समय इस कथन को स्वपक्ष में भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इसमें जैन, बौद्ध और सांख्य तथा औपनिषदिक वेदान्त की दार्शनिक मान्यताओं के पूर्व रूप या बीज परिलक्षित होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन मान्यताओं को सुसंगत बनाने के प्रयास में ही इन दर्शनों का उदय हुआ हो।
४. इसमें जो देहात्मवाद का निराकरण किया गया है वह ठोस तार्किक आधारों पर स्थित नहीं है। मात्र यह कह दिया गया है कि जीव का जीवन शरीर की उत्पत्ति और विनाश की काल सीमा तक सीमित नहीं है।
सूत्रकृतांग (द्वितीय श्रुतस्कन्ध) में चार्वाक दर्शन का प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा
चार्वाकों अथवा तज्जीवतच्छरीरवादियों के पक्ष का तार्किक दृष्टि से प्रस्तुतीकरण और उसकी तार्किक समीक्षा का प्रयत्न जैन आगम साहित्य में सर्व प्रथम सूत्रकृतांग के द्वितीय पुण्डरीक नामक अध्ययन में और उसके पश्चात् राजप्रश्नीय सूत्र में उपलब्ध होता है। अब हम सूत्रकृतांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध के आधार पर तज्जीवतच्छरीरवादियों के पक्ष का प्रस्तुतीकरण करेंगे और उसकी समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। तज्जीवतच्छरीरवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि पादतल से ऊपर, मस्तक के केशों के अग्रभाग से नीचे तथा समस्त त्वक्पर्यन्त जो शरीर है वही जीव है। इस शरीर के जीवित रहने तक ही यह जीव जीवित रहता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए शरीर के अस्तित्व पर्यन्त ही जीव का अस्तित्त्व है। इस सिद्धान्त को युक्तियुक्त समझना चाहिए। क्योंकि जो लोग युक्तिपूर्वक यह प्रतिपादित करते हैं कि शरीर अन्य है और जीव अन्य है, वे भी जीव और शरीर को पृथक-पृथक करके नहीं
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.