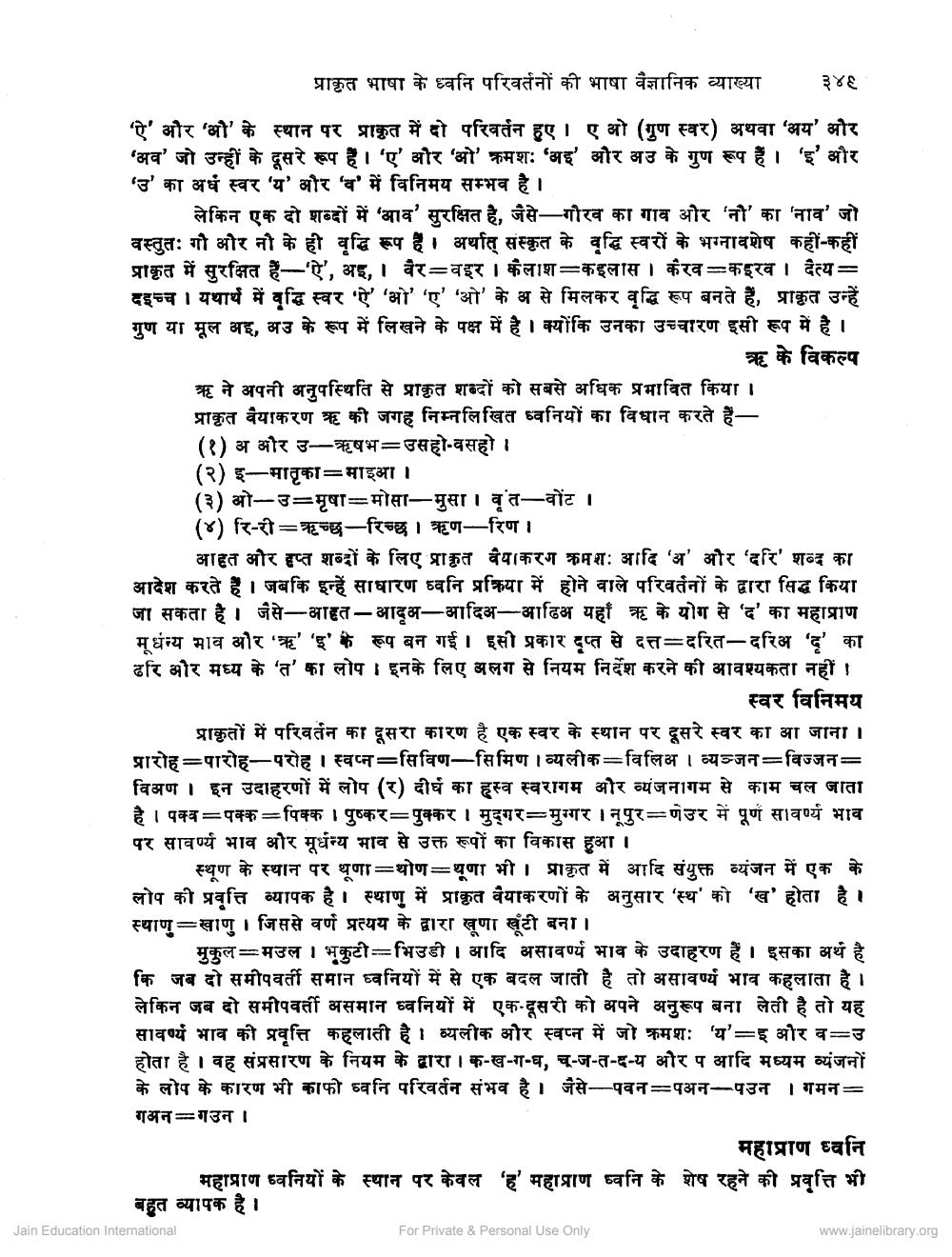________________
प्राकृत भाषा के ध्वनि परिवर्तनों की भाषा वैज्ञानिक व्याख्या
'ऐ' और 'औ' के स्थान पर प्राकृत में दो परिवर्तन हुए। ए ओ (गुण स्वर) अथवा 'अय' और 'अव' जो उन्हीं के दूसरे रूप हैं। 'ए' और 'ओ' क्रमशः 'अई' और अउ के गुण रूप हैं। 'इ' और 'उ' का अर्घ स्वर 'य' और 'व' में विनिमय सम्भव है।
लेकिन एक दो शब्दों में 'आव' सुरक्षित है, जैसे—गौरव का गाव और 'नो' का 'नाव' जो वस्तुतः गौ और नौ के ही वृद्धि रूप है। अर्थात् संस्कृत के वृद्धि स्वरों के भग्नावशेष कहीं-कहीं प्राकृत में सुरक्षित हैं-'ऐ', अइ,। वैर=बइर । कैलाश=कइलास । कैरव-कइरव । दैत्य = दइच्च । यथार्थ में वृद्धि स्वर 'ऐ' 'ओ' 'ए' 'ओ' के अ से मिलकर वृद्धि रूप बनते हैं, प्राकृत उन्हें गुण या मूल अइ, अउ के रूप में लिखने के पक्ष में है। क्योंकि उनका उच्चारण इसी रूप में है।
ऋके विकल्प ऋ ने अपनी अनुपस्थिति से प्राकृत शब्दों को सबसे अधिक प्रभावित किया । प्राकृत वैयाकरण ऋ की जगह निम्नलिखित ध्वनियों का विधान करते हैं(१) अ और उ-ऋषभ =उसहो-वसहो । (२) इ-मातृका=माइआ। (३) ओ-उ=मृषा=मोसा-मुसा । वृत-वोट । (४) रि-री=ऋच्छ-रिच्छ । ऋण-रिण।
आहत और दृप्त शब्दों के लिए प्राकृत वैयाकरण क्रमशः आदि 'अ' और 'दरि' शब्द का आदेश करते हैं। जबकि इन्हें साधारण ध्वनि प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। जैसे-आहत-आदअ-आदिअ-आढिम यहाँ ऋ के योग से 'द' का महाप्राण मधन्य माव और 'ऋ' 'इ' के रूप बन गई। इसी प्रकार दप्त से दत्त=दरित-दरिअ 'द' का ढरि और मध्य के 'त' का लोप । इनके लिए अलग से नियम निर्देश करने की आवश्यकता नहीं।
स्वर विनिमय प्राकृतों में परिवर्तन का दूसरा कारण है एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर का आ जाना। प्रारोह =पारोह-परोह । स्वप्न =सिविण-सिमिण । व्यलीक=विलिअ । व्यञ्जन=विज्जन= विअण । इन उदाहरणों में लोप (र) दीर्घ का हस्व स्वरागम और व्यंजनागम से काम चल जाता है । पक्व =पक्क =पिक्क । पुष्कर पुक्कर । मुद्गर-मुग्गर । नूपुर=णेउर में पूर्ण सावर्ण्य भाव पर सावर्ण्य भाव और मूर्धन्य भाव से उक्त रूपों का विकास हुआ।
स्थूण के स्थान पर थूणा=थोण=थूणा भी। प्राकृत में आदि संयुक्त व्यंजन में एक के लोप की प्रवृत्ति व्यापक है। स्थाणु में प्राकृत वैयाकरणों के अनुसार 'स्थ' को 'ख' होता है। स्थाणु =खाणु । जिससे वर्ण प्रत्यय के द्वारा खूणा खूटी बना।।
मुकुल मउल । भकुटी भिउडी । आदि असावर्ण्य भाव के उदाहरण हैं। इसका अर्थ है कि जब दो समीपवर्ती समान ध्वनियों में से एक बदल जाती है तो असावर्ण्य भाव कहलाता है। लेकिन जब दो समीपवर्ती असमान ध्वनियों में एक-दूसरी को अपने अनुरूप बना लेती है तो यह सावर्ण्य भाव की प्रवृत्ति कहलाती है। व्यलीक और स्वप्न में जो क्रमशः 'य'=इ और व=उ होता है। वह संप्रसारण के नियम के द्वारा । क-ख-ग-घ, चू-ज-त-द-य और प आदि मध्यम व्यंजनों के लोप के कारण भी काफी ध्वनि परिवर्तन संभव है। जैसे-पवनपअन-पउन । गमन = गअन=गउन ।
महाप्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर केवल 'ह' महाप्राण ध्वनि के शेष रहने की प्रवृत्ति भी
बहुत व्यापक है। Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org