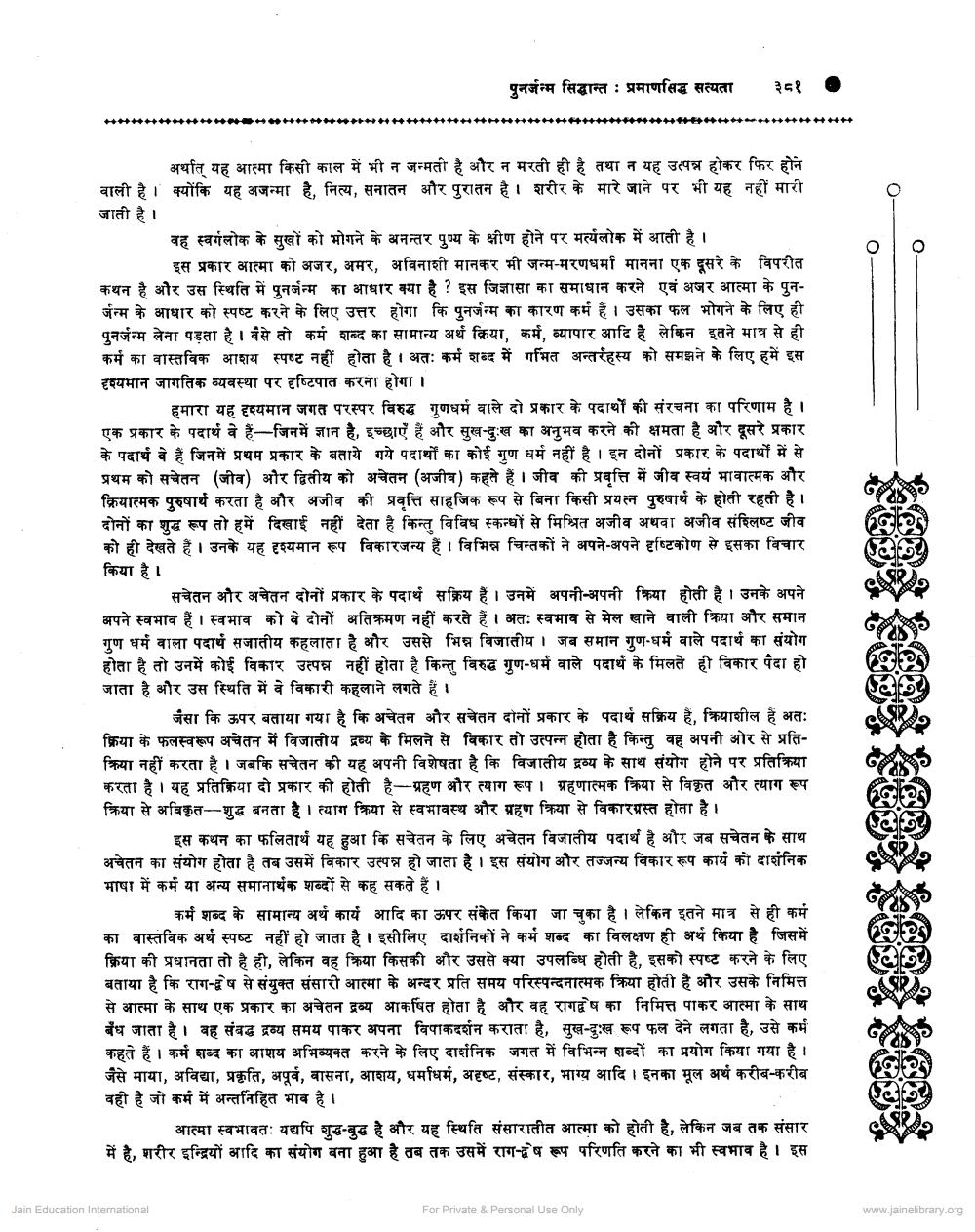________________
पुनर्जन्म सिद्धान्त : प्रमाणसिद्ध सत्यता
__ अर्थात् यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न मरती ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती है।
वह स्वर्गलोक के सुखों को भोगने के अनन्तर पुण्य के क्षीण होने पर मर्त्यलोक में आती है।
इस प्रकार आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी मानकर भी जन्म-मरणधर्मा मानना एक दूसरे के विपरीत कथन है और उस स्थिति में पुनर्जन्म का आधार क्या है ? इस जिज्ञासा का समाधान करने एवं अजर आत्मा के पुनजन्म के आधार को स्पष्ट करने के लिए उत्तर होगा कि पुनर्जन्म का कारण कर्म हैं। उसका फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वैसे तो कर्म शब्द का सामान्य अर्थ क्रिया, कर्म, व्यापार आदि है लेकिन इतने मात्र से ही कर्म का वास्तविक आशय स्पष्ट नहीं होता है। अतः कर्म शब्द में गर्मित अन्तर्रहस्य को समझने के लिए हमें इस दृश्यमान जागतिक व्यवस्था पर दृष्टिपात करना होगा।
हमारा यह दृश्यमान जगत परस्पर विरुद्ध गुणधर्म वाले दो प्रकार के पदार्थों की संरचना का परिणाम है । एक प्रकार के पदार्थ वे हैं-जिनमें ज्ञान है, इच्छाएँ हैं और सुख-दुःख का अनुभव करने की क्षमता है और दूसरे प्रकार के पदार्थ वे हैं जिनमें प्रथम प्रकार के बताये गये पदार्थों का कोई गुण धर्म नहीं है । इन दोनों प्रकार के पदार्थों में से प्रथम को सचेतन (जीव) और द्वितीय को अचेतन (अजीव) कहते हैं । जीव की प्रवृत्ति में जीव स्वयं भावात्मक और क्रियात्मक पुरुषार्थ करता है और अजीव की प्रवृत्ति साहजिक रूप से बिना किसी प्रयत्न पुरुषार्थ के होती रहती है। दोनों का शुद्ध रूप तो हमें दिखाई नहीं देता है किन्तु विविध स्कन्धों से मिश्रित अजीव अथवा अजीव संश्लिष्ट जीव को ही देखते हैं। उनके यह दृश्यमान रूप विकारजन्य हैं । विभिन्न चिन्तकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इसका विचार किया है।
सचेतन और अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थ सक्रिय हैं। उनमें अपनी-अपनी क्रिया होती है । उनके अपने अपने स्वभाव हैं । स्वभाव को वे दोनों अतिक्रमण नहीं करते हैं । अतः स्वभाव से मेल खाने वाली क्रिया और समान गुण धर्म वाला पदार्थ सजातीय कहलाता है और उससे भिन्न विजातीय । जब समान गुण-धर्म वाले पदार्थ का संयोग होता है तो उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है किन्तु विरुद्ध गुण-धर्म वाले पदार्थ के मिलते ही विकार पैदा हो जाता है और उस स्थिति में वे विकारी कहलाने लगते हैं।
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अचेतन और सचेतन दोनों प्रकार के पदार्थ सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं अतः क्रिया के फलस्वरूप अचेतन में विजातीय द्रव्य के मिलने से विकार तो उत्पन्न होता है किन्तु वह अपनी ओर से प्रतिक्रिया नहीं करता है । जबकि सचेतन की यह अपनी विशेषता है कि विजातीय द्रव्य के साथ संयोग होने पर प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती है-ग्रहण और त्याग रूप। ग्रहणात्मक क्रिया से विकृत और त्याग रूप क्रिया से अविकृत-शुद्ध बनता है । त्याग क्रिया से स्वभावस्थ और ग्रहण क्रिया से विकारग्रस्त होता है।
इस कथन का फलितार्थ यह हुआ कि सचेतन के लिए अचेतन विजातीय पदार्थ है और जब सचेतन के साथ अचेतन का संयोग होता है तब उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है । इस संयोग और तज्जन्य विकार रूप कार्य को दार्शनिक भाषा में कर्म या अन्य समानार्थक शब्दों से कह सकते हैं।
कर्म शब्द के सामान्य अर्थ कार्य आदि का ऊपर संकेत किया जा चुका है। लेकिन इतने मात्र से ही कर्म का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हो जाता है। इसीलिए दार्शनिकों ने कर्म शब्द का विलक्षण ही अर्थ किया है जिसमें क्रिया की प्रधानता तो है ही, लेकिन वह क्रिया किसकी और उससे क्या उपलब्धि होती है, इसको स्पष्ट करने के लिए बताया है कि राग-द्वेष से संयुक्त संसारी आत्मा के अन्दर प्रति समय परिस्पन्दनात्मक क्रिया होती है और उसके निमित्त से आत्मा के साथ एक प्रकार का अचेतन द्रव्य आकर्षित होता है और वह रागद्वेष का निमित्त पाकर आत्मा के साथ बँध जाता है। वह संबद्ध द्रव्य समय पाकर अपना विपाकदर्शन कराता है, सुख-दुःख रूप फल देने लगता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म शब्द का आशय अभिव्यक्त करने के लिए दार्शनिक जगत में विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है । जैसे माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आशय, धर्माधर्म, अदृष्ट, संस्कार, भाग्य आदि । इनका मूल अर्थ करीब-करीब वही है जो कर्म में अन्तनिहित भाव है।
आत्मा स्वभावतः यद्यपि शुद्ध-बुद्ध है और यह स्थिति संसारातीत आत्मा को होती है, लेकिन जब तक संसार में है, शरीर इन्द्रियों आदि का संयोग बना हुआ है तब तक उसमें राग-द्वेष रूप परिणति करने का भी स्वभाव है। इस
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org