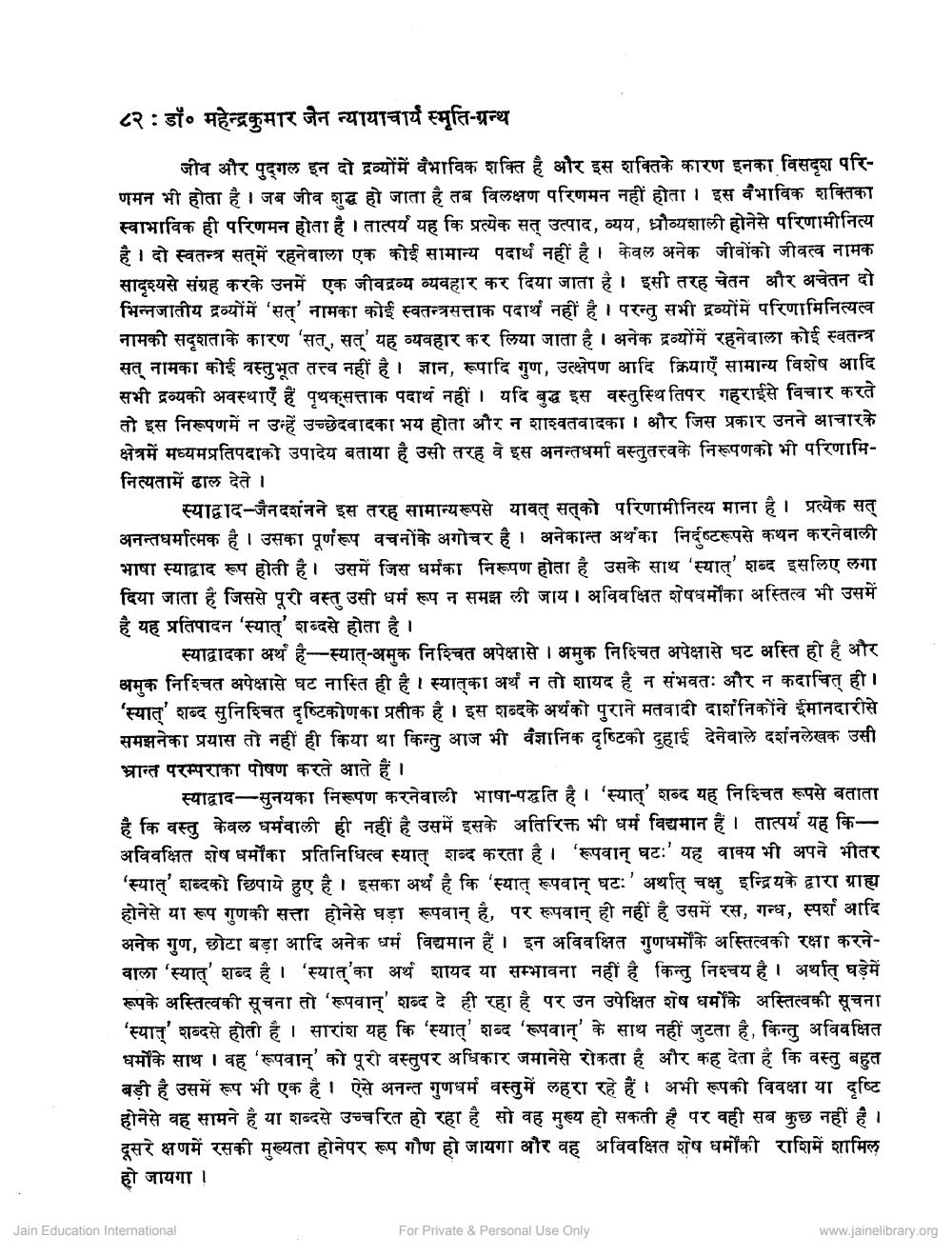________________
८२ : डॉ. महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ
जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें वैभाविक शक्ति है और इस शक्तिके कारण इनका विसदृश परिणमन भी होता है । जब जीव शुद्ध हो जाता है तब विलक्षण परिणमन नहीं होता। इस वैभाविक शक्तिका स्वाभाविक ही परिणमन होता है । तात्पर्य यह कि प्रत्येक सत् उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यशाली होनेसे परिणामी नित्य है। दो स्वतन्त्र सत्में रहनेवाला एक कोई सामान्य पदार्थ नहीं है। केवल अनेक जीवोंको जीवत्व नामक सादृश्यसे संग्रह करके उनमें एक जीवद्रव्य व्यवहार कर दिया जाता है। इसी तरह चेतन और अचेतन दो भिन्नजातीय द्रव्योंमें 'सत्' नामका कोई स्वतन्त्रसत्ताक पदार्थ नहीं है। परन्तु सभी द्रव्योंमें परिणामिनित्यत्व नामकी सदृशताके कारण 'सत , सत्' यह व्यवहार कर लिया जाता है । अनेक द्रव्योंमें रहनेवाला कोई स्वतन्त्र सत् नामका कोई वस्तुभूत तत्त्व नहीं है। ज्ञान, रूपादि गुण, उत्क्षेपण आदि क्रियाएँ सामान्य विशेष आदि सभी द्रव्यको अवस्थाएँ हैं पृथक्सत्ताक पदार्थ नहीं। यदि बुद्ध इस वस्तुस्थितिपर गहराईसे विचार करते तो इस निरूपणमें न उन्हें उच्छेदवादका भय होता और न शाश्वतवादका । और जिस प्रकार उनने आचारके क्षेत्रमें मध्यमप्रतिपदाको उपादेय बताया है उसी तरह वे इस अनन्तधर्मा वस्तुतत्त्वके निरूपणको भी परिणामिनित्यतामें ढाल देते।
स्याद्वाद-जैनदर्शनने इस तरह सामान्यरूपसे यावत् सत्को परिणामीनित्य माना है। प्रत्येक सत् अनन्तधर्मात्मक है । उसका पूर्णरूप वचनोंके अगोचर है। अनेकान्त अर्थका टरूपसे कथन करनेवाली भाषा स्याद्वाद रूप होती है। उसमें जिस धर्मका निरूपण होता है उसके साथ 'स्यात्' शब्द इसलिए लगा दिया जाता है जिससे पूरी वस्तु उसी धर्म रूप न समझ ली जाय । अविवक्षित शेषधर्मोका अस्तित्व भी उसमें है यह प्रतिपादन 'स्यात्' शब्दसे होता है।
स्याद्वादका अर्थ है-स्यात्-अमुक निश्चित अपेक्षासे । अमुक निश्चित अपेक्षासे घट अस्ति हो है और अमुक निश्चित अपेक्षासे घट नास्ति ही है। स्यातका अर्थ न तो शायद है न संभवतः और न कदाचित् ही। 'स्यात्' शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणका प्रतीक है । इस शब्दके अर्थको पुराने मतवादी दार्शनिकोंने ईमानदारीसे समझनेका प्रयास तो नहीं ही किया था किन्तु आज भी वैज्ञानिक दृष्टिको दुहाई देनेवाले दर्शनलेखक उसी भ्रान्त परम्पराका पोषण करते आते हैं।
स्याद्वाद-सुनयका निरूपण करनेवाली भाषा-पद्धति है। 'स्यात्' शब्द यह निश्चित रूपसे बताता है कि वस्तु केवल धर्मवाली ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हैं। तात्पर्य यह किअविवक्षित शेष धर्मोंका प्रतिनिधित्व स्यात् शब्द करता है। 'रूपवान् घटः' यह वाक्य भी अपने भीतर 'स्यात्' शब्दको छिपाये हुए है। इसका अर्थ है कि 'स्यात् रूपवान् घटः' अर्थात् चक्षु इन्द्रियके द्वारा ग्राह्य होनेसे या रूप गुणकी सत्ता होनेसे घड़ा रूपवान् है, पर रूपवान् ही नहीं है उसमें रस, गन्ध, स्पर्श आदि अनेक गुण, छोटा बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान है। इन अविवक्षित गुणधर्मों के अस्तित्वकी रक्षा करनेवाला 'स्यात्' शब्द है । 'स्यात्'का अर्थ शायद या सम्भावना नहीं है किन्तु निश्चय है । अर्थात् घड़ेमें रूपके अस्तित्वकी सूचना तो 'रूपवान्' शब्द दे ही रहा है पर उन उपेक्षित शेष धर्मोके अस्तित्वकी सूचना 'स्यात' शब्दसे होती है । सारांश यह कि 'स्यात्' शब्द 'रूपवान्' के साथ नहीं जुटता है, किन्तु अविवक्षित
। वह 'रूपवान् को पूरी वस्तुपर अधिकार जमानेसे रोकता है और कह देता है कि वस्तु बहुत बड़ी है उसमें रूप भी एक है। ऐसे अनन्त गुणधर्म वस्तुमें लहरा रहे हैं। अभी रूपको विवक्षा या दृष्टि होनेसे वह सामने है या शब्दसे उच्चरित हो रहा है सो वह मुख्य हो सकती है पर वही सब कुछ नहीं है। दूसरे क्षणमें रसकी मुख्यता होनेपर रूप गौण हो जायगा और वह अविवक्षित शेष धर्मोंकी राशिमें शामिल हो जायगा।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org