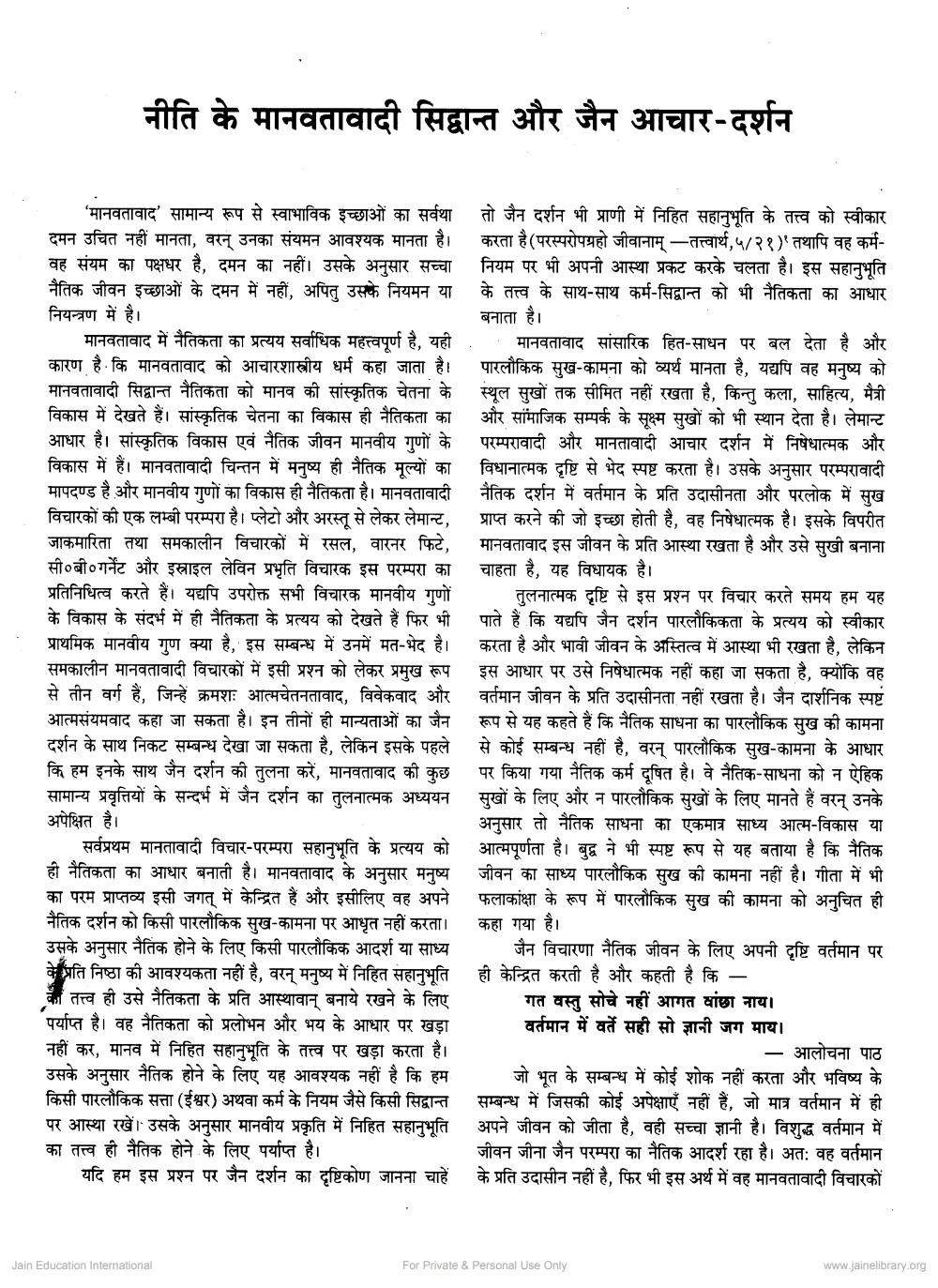________________
नीति के मानवतावादी सिद्धान्त और जैन आचार दर्शन
-
'मानवतावाद' सामान्य रूप से स्वाभाविक इच्छाओं का सर्वथा दमन उचित नहीं मानता, वरन् उनका संयमन आवश्यक मानता है। वह संयम का पक्षधर है, दमन का नहीं उसके अनुसार सच्चा नैतिक जीवन इच्छाओं के दमन में नहीं, अपितु उसके नियमन या नियन्त्रण में है।
मानवतावाद में नैतिकता का प्रत्यय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यही कारण है कि मानवतावाद को आचारशास्त्रीय धर्म कहा जाता है। मानवतावादी सिद्वान्त नैतिकता को मानव की सांस्कृतिक चेतना के विकास में देखते हैं सांस्कृतिक चेतना का विकास ही नैतिकता का आधार है। सांस्कृतिक विकास एवं नैतिक जीवन मानवीय गुणों के विकास में हैं। मानवतावादी चिन्तन में मनुष्य ही नैतिक मूल्यों का मापदण्ड है और मानवीय गुणों का विकास ही नैतिकता है मानवतावादी विचारकों की एक लम्बी परम्परा है। प्लेटो और अरस्तू से लेकर लेमान्ट, जाकमारिता तथा समकालीन विचारकों में रसल, वारनर फिटे, सी०बी० गर्नेट और इस्राइल लेविन प्रभृति विचारक इस परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि उपरोक्त सभी विचारक मानवीय गुणों के विकास के संदर्भ में ही नैतिकता के प्रत्यय को देखते हैं फिर भी प्राथमिक मानवीय गुण क्या है, इस सम्बन्ध में उनमें मतभेद है। समकालीन मानवतावादी विचारकों में इसी प्रश्न को लेकर प्रमुख रूप से तीन वर्ग है जिन्हें क्रमश: आत्मचेतनतावाद, विवेकवाद और आत्मसंयमवाद कहा जा सकता है। इन तीनों ही मान्यताओं का जैन दर्शन के साथ निकट सम्बन्ध देखा जा सकता है, लेकिन इसके पहले कि हम इनके साथ जैन दर्शन की तुलना करें, मानवतावाद की कुछ सामान्य प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में जैन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है।
सर्वप्रथम मानतावादी विचार - परम्परा सहानुभूति के प्रत्यय को ही नैतिकता का आधार बनाती है। मानवतावाद के अनुसार मनुष्य का परम प्राप्तव्य इसी जगत् में केन्द्रित हैं और इसीलिए वह अपने नैतिक दर्शन को किसी पारलौकिक सुख-कामना पर आधृत नहीं करता । उसके अनुसार नैतिक होने के लिए किसी पारलौकिक आदर्श या साध्य
प्रति निष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वरन् मनुष्य में निहित सहानुभूति के तत्त्व ही उसे नैतिकता के प्रति आस्थावान् बनाये रखने के लिए पर्याप्त है। वह नैतिकता को प्रलोभन और भय के आधार पर खड़ा नहीं कर, मानव में निहित सहानुभूति के तत्त्व पर खड़ा करता है। उसके अनुसार नैतिक होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी पारलौकिक सत्ता (ईश्वर) अथवा कर्म के नियम जैसे किसी सिद्वान्त पर आस्था रखें। उसके अनुसार मानवीय प्रकृति में निहित सहानुभूति का तत्त्व ही नैतिक होने के लिए पर्याप्त है।
यदि हम इस प्रश्न पर जैन दर्शन का दृष्टिकोण जानना चाहें
Jain Education International
तो जैन दर्शन भी प्राणी में निहित सहानुभूति के तत्व को स्वीकार करता है (परस्परोपग्रहो जीवानाम् – तत्त्वार्थ, ५ / २१) तथापि वह कर्मनियम पर भी अपनी आस्था प्रकट करके चलता है। इस सहानुभूति के तत्त्व के साथ-साथ कर्म सिद्धान्त को भी नैतिकता का आधार बनाता है।
मानवतावाद सांसारिक हित साधन पर बल देता है और पारलौकिक सुख-कामना को व्यर्थ मानता है, यद्यपि वह मनुष्य को स्थूल सुखों तक सीमित नहीं रखता है, किन्तु कला, साहित्य, मैत्री और सामाजिक सम्पर्क के सूक्ष्म सुखों को भी स्थान देता है। लेमान्ट परम्परावादी और मानतावादी आचार दर्शन में निषेधात्मक और विधानात्मक दृष्टि से भेद स्पष्ट करता है। उसके अनुसार परम्परावादी नैतिक दर्शन में वर्तमान के प्रति उदासीनता और परलोक में सुख प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, वह निषेधात्मक है। इसके विपरीत मानवतावाद इस जीवन के प्रति आस्था रखता है और उसे सुखी बनाना चाहता है, यह विधायक है।
तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करते समय हम यह पाते हैं कि यद्यपि जैन दर्शन पारलौकिकता के प्रत्यय को स्वीकार करता है और भावी जीवन के अस्तित्व में आस्था भी रखता है, लेकिन इस आधार पर उसे निषेधात्मक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह वर्तमान जीवन के प्रति उदासीनता नहीं रखता है जैन दार्शनिक स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि नैतिक साधना का पारलौकिक सुख की कामना से कोई सम्बन्ध नहीं है, वरन् पारलौकिक सुख-कामना के आधार पर किया गया नैतिक कर्म दूषित है। वे नैतिक-साधना को न ऐहिक सुखों के लिए और न पारलौकिक सुखों के लिए मानते हैं वरन् उनके अनुसार तो नैतिक साधना का एकमात्र साध्य आत्म-विकास या आत्मपूर्णता है । बुद्ध ने भी स्पष्ट रूप से यह बताया है कि नैतिक जीवन का साध्य पारलौकिक सुख की कामना नहीं है। गीता में भी फलाकांक्षा के रूप में पारलौकिक सुख की कामना को अनुचित ही कहा गया है।
जैन विचारणा नैतिक जीवन के लिए अपनी दृष्टि वर्तमान पर ही केन्द्रित करती है और कहती है कि
गत वस्तु सोचे नहीं आगत वांछा नाय । वर्तमान में वर्ते सही सो जानी जग माय ।
-
आलोचना पाठ जो भूत के सम्बन्ध में कोई शोक नहीं करता और भविष्य के सम्बन्ध में जिसकी कोई अपेक्षाएँ नहीं हैं, जो मात्र वर्तमान में ही अपने जीवन को जीता है, वही सच्चा ज्ञानी है। विशुद्ध वर्तमान में जीवन जीना जैन परम्परा का नैतिक आदर्श रहा है। अतः वह वर्तमान के प्रति उदासीन नहीं है, फिर भी इस अर्थ में वह मानवतावादी विचारकों
For Private & Personal Use Only
—
www.jainelibrary.org.