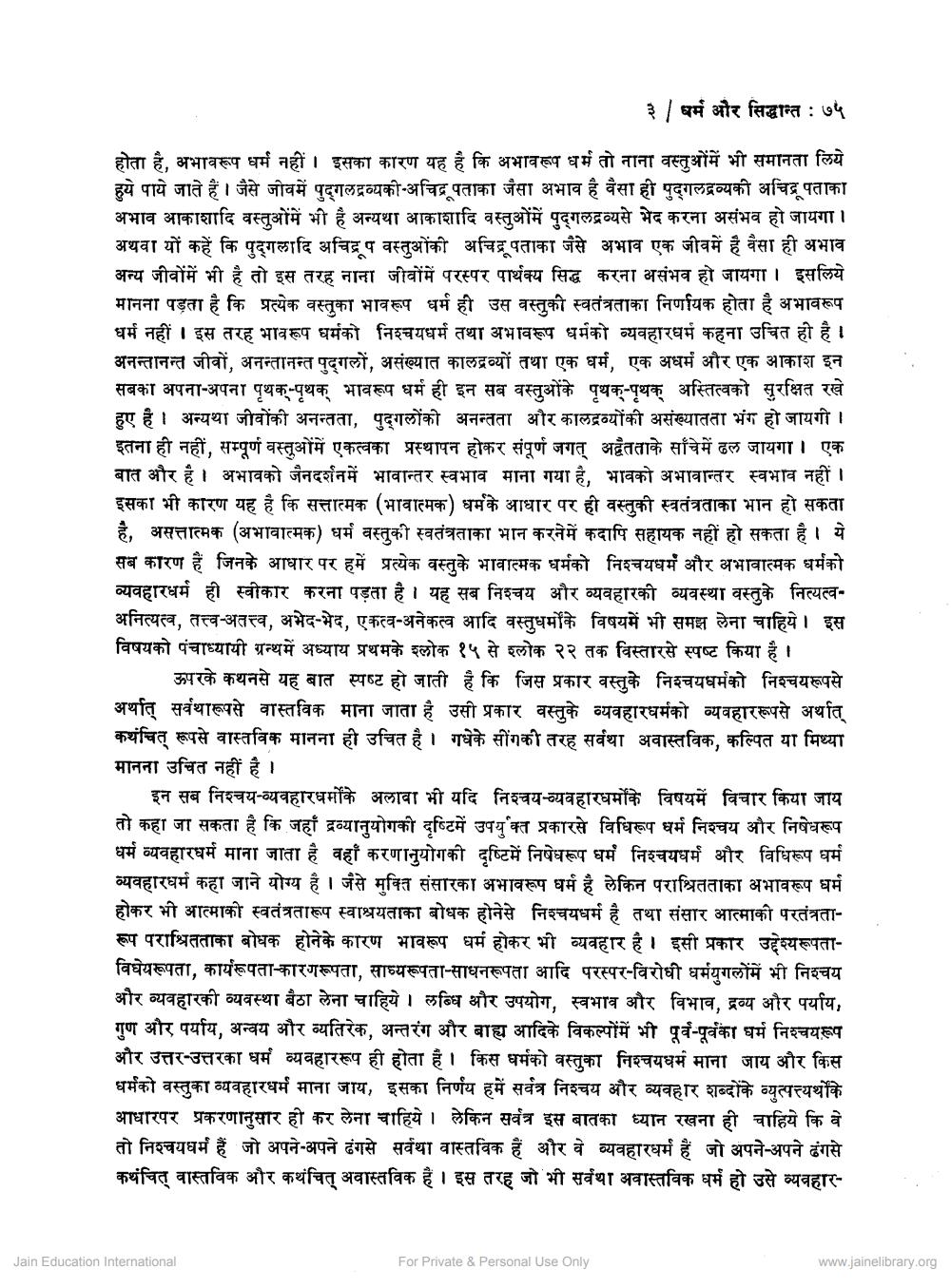________________
३/ धर्म और सिद्धान्त : ७५
होता है, अभावरूप धर्म नहीं। इसका कारण यह है कि अभावरूप धर्म तो नाना वस्तुओंमें भी समानता लिये हुये पाये जाते हैं। जैसे जीवमें पुद्गलद्रव्यकी-अचिद्र पताका जैसा अभाव है वैसा ही पुद्गलद्रव्यकी अचिद् पताका अभाव आकाशादि वस्तुओंमें भी है अन्यथा आकाशादि वस्तुओंमें पुद्गलद्रव्यसे भेद करना असंभव हो जायगा। अथवा यों कहें कि पुद्गलादि अचिद्रप वस्तुओंकी अचिद्रूपताका जैसे अभाव एक जीवमें है वैसा ही अभाव अन्य जीवोंमें भी है तो इस तरह नाना जीवोंमें परस्पर पार्थक्य सिद्ध करना असंभव हो जायगा। इसलिये मानना पड़ता है कि प्रत्येक वस्तूका भावरूप धर्म ही उस वस्तुकी स्वतंत्रताका निर्णायक होता है अभावरूप धर्म नहीं । इस तरह भावरूप धर्मको निश्चयधर्म तथा अभावरूप धर्मको व्यवहारधर्म कहना उचित ही है। अनन्तानन्त जीवों, अनन्तानन्त पदगलों, असंख्यात कालद्रव्यों तथा एक धर्म, एक अधर्म और एक आकाश इन सबका अपना-अपना पृथक्-पृथक् भावरूप धर्म ही इन सब वस्तुओंके पृथक-पृथक् अस्तित्वको सुरक्षित रखे हुए है। अन्यथा जीवोंकी अनन्तता, पुद्गलोंको अनन्तता और कालद्रव्योंकी असंख्यातता भंग हो जायगी। इतना ही नहीं, सम्पूर्ण वस्तुओंमें एकत्वका प्रस्थापन होकर संपूर्ण जगत अद्वैतताके साँचे में ढल जायगा। एक बात और है। अभावको जैनदर्शनमें भावान्तर स्वभाव माना गया है, भावको अभावान्तर स्वभाव नहीं। इसका भी कारण यह है कि सत्तात्मक (भावात्मक) धर्मके आधार पर ही वस्तुकी स्वतंत्रताका भान हो सकता है, असत्तात्मक (अभावात्मक) धर्म वस्तुकी स्वतंत्रताका भान करने में कदापि सहायक नहीं हो सकता है। ये सब कारण हैं जिनके आधार पर हमें प्रत्येक वस्तुके भावात्मक धर्मको निश्चयधर्म और अभावात्मक धर्मको व्यवहारधर्म ही स्वीकार करना पड़ता है। यह सब निश्चय और व्यवहारकी व्यवस्था वस्तुके नित्यत्वअनित्यत्व, तत्त्व-अतत्त्व, अभेद-भेद, एकत्व-अनेकत्व आदि वस्तुधर्मों के विषयमें भी समझ लेना चाहिये। इस विषयको पंचाध्यायी ग्रन्थमें अध्याय प्रथमके श्लोक १५ से श्लोक २२ तक विस्तारसे स्पष्ट किया है ।
ऊपरके कथनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार वस्तुके निश्चयधर्मको निश्चयरूपसे अर्थात् सर्वथारूपसे वास्तविक माना जाता है उसी प्रकार वस्तुके व्यवहारधर्मको व्यवहाररूपसे अर्थात् कथंचित् रूपसे वास्तविक मानना ही उचित है। गधेके सींगकी तरह सर्वथा अवास्तविक, कल्पित या मिथ्या मानना उचित नहीं है।
इन सब निश्चय-व्यवहारधर्मोके अलावा भी यदि निश्चय-व्यवहारधर्मोंके विषयमें विचार किया जाय तो कहा जा सकता है कि जहाँ द्रव्यानुयोगको दृष्टिमें उपयुक्त प्रकारसे विधिरूप धर्म निश्चय और निषेधरूप धर्म व्यवहारधर्म माना जाता है वहाँ करणानुयोगकी दृष्टिमें निषेधरूप धर्म निश्चयधर्म और विधिरूप धर्म व्यवहारधर्म कहा जाने योग्य है । जैसे मुक्ति संसारका अभावरूप धर्म है लेकिन पराश्रितताका अभावरूप धर्म होकर भी आत्माकी स्वतंत्रतारूप स्वाश्रयताका बोधक होनेसे निश्चयधर्म है तथा संसार आत्माकी परतंत्रतारूप पराश्रितताका बोधक होनेके कारण भावरूप धर्म होकर भी व्यवहार है। इसी प्रकार उद्देश्यरूपताविधेयरूपता, कार्यरूपता-कारणरूपता, साध्यरूपता-साधनरूपता आदि परस्पर-विरोधी धर्मयुगलोंमें भी निश्चय
और व्यवहारकी व्यवस्था बैठा लेना चाहिये । लब्धि और उपयोग, स्वभाव और विभाव, द्रव्य और पर्याय, गुण और पर्याय, अन्वय और व्यतिरेक, अन्तरंग और बाह्य आदिके विकल्पों में भी पूर्व-पूर्वका धर्म निश्चयरूप और उत्तर-उत्तरका धर्म व्यवहाररूप ही होता है। किस धर्मको वस्तुका निश्चयधर्म माना जाय और किस धर्मको वस्तुका व्यवहारधर्म माना जाय, इसका निर्णय हमें सर्वत्र निश्चय और व्यवहार शब्दोंके व्युत्पत्त्यर्थोके आधारपर प्रकरणानुसार ही कर लेना चाहिये । लेकिन सर्वत्र इस बातका ध्यान रखना ही चाहिये कि वे तो निश्चयधर्म हैं जो अपने-अपने ढंगसे सर्वथा वास्तविक हैं और वे व्यवहारधर्म हैं जो अपने-अपने ढंगसे कथंचित् वास्तविक और कथंचित् अवास्तविक है । इस तरह जो भी सर्वथा अवास्तविक धर्म हो उसे व्यवहार
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org