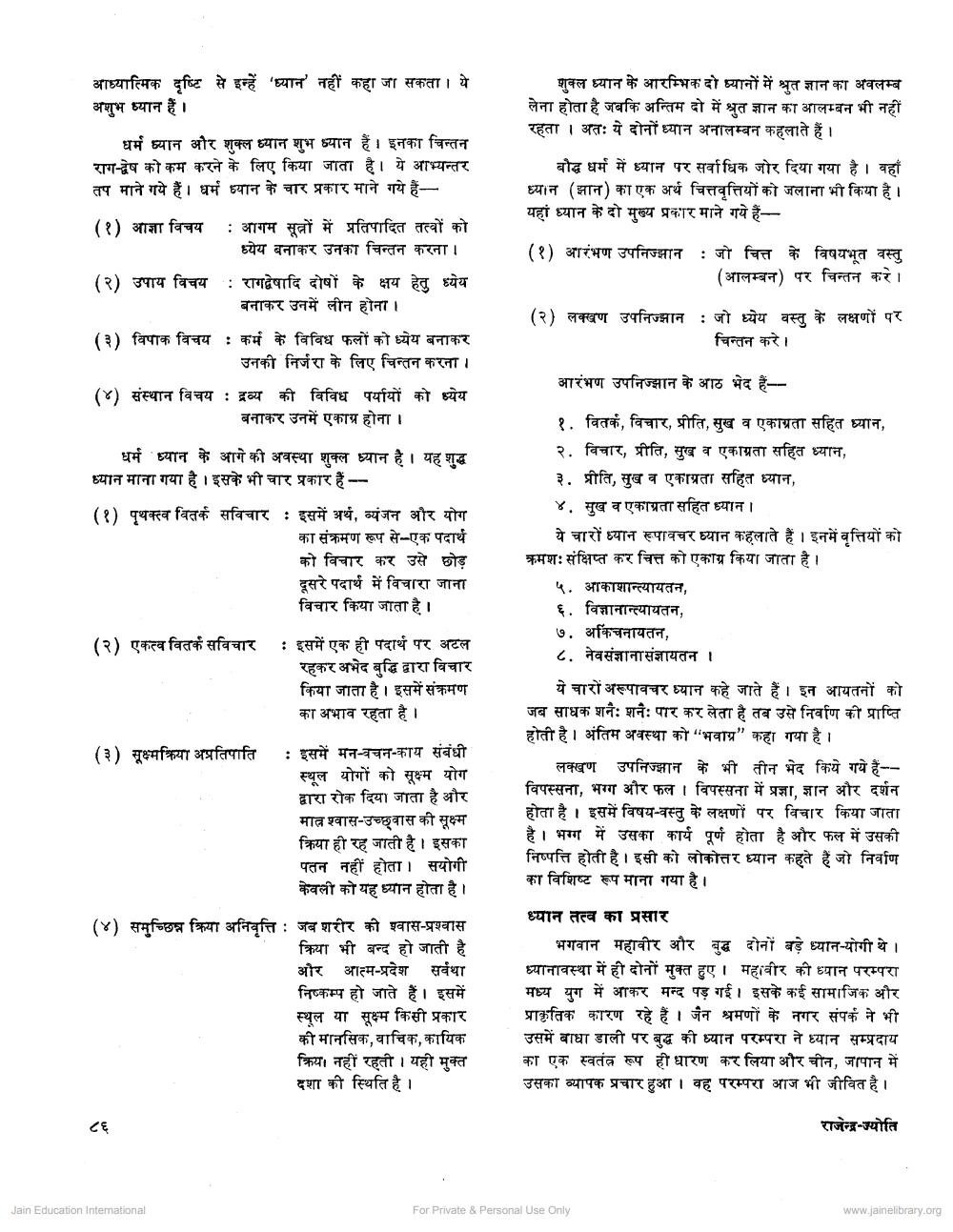________________
आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें 'ध्यान' नहीं कहा जा सकता। ये अशुभ ध्यान हैं ।
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान हैं। इनका चिन्तन राग-द्वेष को कम करने के लिए किया जाता है। ये आभ्यन्तर तप माने गये हैं। धर्म ध्यान के चार प्रकार माने गये हैं
(१) आज्ञा विचय
(२) उपाय विचय
: आगम सूत्रों में प्रतिपादित तत्वों को ध्येय बनाकर उनका चिन्तन करना ।
(३) विपाक विचय: कर्म के विविध फलों को ध्येय बनाकर उनकी निर्जरा के लिए चिन्तन करना ।
: रागद्वेषादि दोषों के क्षय हेतु ध्येय बनाकर उनमें लीन होना ।
( ४ ) संस्थान विचय द्रव्य की विविध पर्यायों को ध्येय बनाकर उनमें एकाग्र होना ।
धर्म ध्यान के आगे की अवस्था शुक्ल ध्यान है । यह शुद्ध ध्यान माना गया है। इसके भी चार प्रकार हैं-
(१) पृथक्व वितर्क सविचार
(२) एक वितर्क सविचार
( ३ ) सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति
८६
Jain Education International
"
इसमें अर्थ व्यंजन और योग का संक्रमण रूप से एक पदार्थ को विचार कर उसे छोड़ दूसरे पदार्थ में विचारा जाना विचार किया जाता है ।
: इसमें एक ही पदार्थ पर अटल रहकर अभेद बुद्धि द्वारा विचार किया जाता है। इसमें संक्रमण का अभाव रहता है ।
(४) समुच्छिन्न किया अनिवृत्ति जब शरीर की श्वास-प्रश्वास
क्रिया भी बन्द हो जाती है। और आत्म- प्रदेश सर्वथा निष्कम्प हो जाते हैं । इसमें स्थूल या सूक्ष्म किसी प्रकार की मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया नहीं रहती। यही मुक्त दशा की स्थिति है ।
: इसमें मन-वचन-काय संबंधी स्थूल योगों को सूक्ष्म योग द्वारा रोक दिया जाता है और मात्र श्वास- उच्छ्वास की सूक्ष्म क्रिया ही रह जाती है। इसका पतन नहीं होता। सयोगी केवली को यह ध्यान होता है।
शुक्ल ध्यान के आरम्भिक दो ध्यानों में श्रुत ज्ञान का अवलम्ब लेना होता है जबकि अन्तिम दो में श्रुत ज्ञान का आलम्बन भी नहीं रहता । अतः ये दोनों ध्यान अनालम्बन कहलाते हैं ।
बौद्ध धर्म में ध्यान पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। वहाँ ध्यान (ज्ञान) का एक अर्थ चित्तवृत्तियों को जलाना भी किया है। यहां ध्यान के दो मुख्य प्रकार माने गये हैं
:
(१) आरंभण उपनिनान जो वित्त के विषयभूत वस्तु (आलम्बन) पर चिन्तन करे।
(२) लक्खण उपनिज्झान : जो ध्येय वस्तु के लक्षणों पर चिन्तन करे ।
आरंभण उपनिज्झान के आठ भेद हैं-
१. वितर्क, विचार, प्रीति, सुख व एकाग्रता सहित ध्यान, २. विचार, प्रीति, सुख व एकाग्रता सहित ध्यान,
३. प्रीति, सुख व एकाग्रता सहित ध्यान,
४. सुख व एकाग्रता सहित ध्यान ।
ये चारों ध्यान रूपावचर ध्यान कहलाते हैं। इनमें वृत्तियों को क्रमशः संक्षिप्त कर चित्त को एकाग्र किया जाता है।
५. आकाशान्त्यायतन,
६. विज्ञानान्त्यायतन,
७. अकिंचनायतन,
८. नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ।
ये चारों अरूपावचर ध्यान कहे जाते हैं। इन आयतनों को जब साधक शनै: शनैः पार कर लेता है तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। अंतिम अवस्था को “भवाग्र" कहा गया है ।
लक्खण उपनिज्झान के भी तीन भेद किये गये हैं-विपस्सना, भग्ग और फल । विपस्सना में प्रज्ञा, ज्ञान और दर्शन होता है । इसमें विषय-वस्तु के लक्षणों पर विचार किया जाता है । भग्ग में उसका कार्य पूर्ण होता है और फल में उसकी निष्पत्ति होती है। इसी को लोकोत्तर ध्यान कहते हैं जो निर्वाण का विशिष्ट रूप माना गया है।
ध्यान तत्व का प्रसार
भगवान महावीर और बुद्ध दोनों बड़े ध्यान-योगी थे । ध्यानावस्था में ही दोनों मुक्त हुए। महावीर की ध्यान परम्परा मध्य युग में आकर मन्द पड़ गई। इसके कई सामाजिक और प्राकृतिक कारण रहे हैं। जैन श्रमणों के नगर संपर्क ने भी उसमें बाधा डाली पर बुद्ध की ध्यान परम्परा ने ध्यान सम्प्रदाय का एक स्वतंत्र रूप ही धारण कर लिया और चीन, जापान में उसका व्यापक प्रचार हुआ। वह परम्परा आज भी जीवित है ।
राजेन्द्र- ज्योति
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org