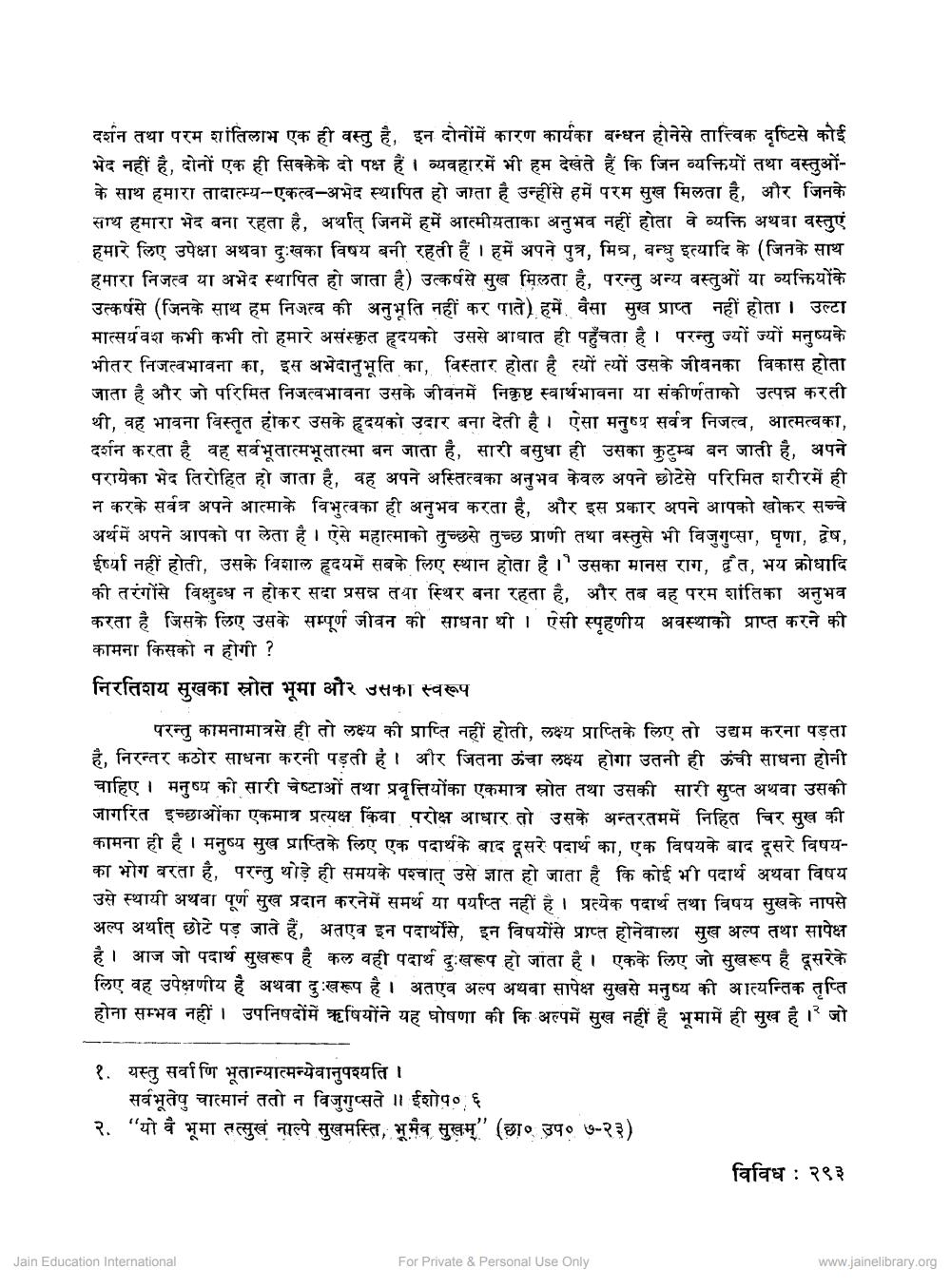________________
1
,
दर्शन तथा परम शांतिलाभ एक ही वस्तु है, इन दोनोंमें कारण कार्यका बन्धन होनेसे तात्त्विक दृष्टिसे कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही सिक्केके दो पक्ष हैं। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जिन व्यक्तियों तथा वस्तुओंके साथ हमारा तादात्म्य एकत्व अभेद स्थापित हो जाता है उन्होंने हमें परम सुख मिलता है, और जिनके साथ हमारा भेद बना रहता है, अर्थात् जिनमें हमें आत्मीयताका अनुभव नहीं होता वे व्यक्ति अथवा वस्तुएं हमारे लिए उपेक्षा अथवा दुःखका विषय बनी रहती हैं । हमें अपने पुत्र, मित्र, बन्धु इत्यादि के ( जिनके साथ हमारा निजत्व या अभेद स्थापित हो जाता है) उत्कर्षसे सुख मिलता है, परन्तु अन्य वस्तुओं या व्यक्तियोंके उत्कर्षसे (जिनके साथ हम निजत्व की अनुभूति नहीं कर पाते ) हमें वैसा सुख प्राप्त नहीं होता । उल्टा मात्सर्यवश कभी कभी तो हमारे असंस्कृत हृदयको उससे आघात ही पहुँचता है । परन्तु ज्यों ज्यों मनुष्य के भीतर निजत्वभावना का इस अभेदानुभूति का विस्तार होता है स्यों त्यों उसके जीवनका विकास होता जाता है और जो परिमित निजत्वभावना उसके जीवन में निकृष्ट स्वार्थभावना या संकीर्णताको उत्पन्न करती थी, वह भावना विस्तृत होकर उसके हृदयको उदार बना देती है। ऐसा मनुष्य सर्वत्र निजत्व आत्मत्वका दर्शन करता है वह सर्वभूतात्मभूतात्मा बन जाता है, सारी वसुधा ही उसका कुटुम्ब बन जाती है, अपने परायेका भेद तिरोहित हो जाता है, वह अपने अस्तित्वका अनुभव केवल अपने छोटेसे परिमित शरीरमें ही न करके सर्वत्र अपने आत्माके विभुत्वका ही अनुभव करता है, और इस प्रकार अपने आपको खोकर सच्चे अर्थ में अपने आपको पा लेता है। ऐसे महात्माको तुच्छसे तुच्छ प्राणी तथा वस्तुसे भी विजुगुप्सा, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या नहीं होती, उसके विशाल हृदयमें सबके लिए स्थान होता है ।' उसका मानस राग, द्वैत, भय क्रोधादि की तरंगोंसे विक्षुब्ध न होकर सदा प्रसन्न तथा स्थिर बना रहता है, और तब वह परम शांतिका अनुभव करता है जिसके लिए उसके सम्पूर्ण जीवन की साधना थो ऐसी स्पृहणीय अवस्थाको प्राप्त करने की कामना किसको न होगी ?
1
निरतिशय सुखका स्रोत भूमा और उसका स्वरूप
परन्तु कामनामात्र से ही तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्य प्राप्तिके लिए तो उद्यम करना पड़ता है, निरन्तर कठोर साधना करनी पड़ती है । और जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतनी ही ऊंची साधना होनी चाहिए। मनुष्य को सारी चेष्टाओं तथा प्रवृत्तियों का एकमात्र स्रोत तथा उसकी सारी सुप्त अथवा उसकी जागरित इच्छाओंका एकमात्र प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष आधार तो उसके अन्तरतममें निहित चिर सुख की कामना ही है। मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए एक पदार्थके बाद दूसरे पदार्थ का एक विषयके बाद दूसरे विषयका भोग वरता है, परन्तु थोड़े ही समयके पश्चात् उसे ज्ञात हो जाता है कि कोई भी पदार्थ अथवा विषय उसे स्थायी अथवा पूर्ण सुख प्रदान करनेमें समर्थ या पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक पदार्थ तथा विषय सुखके नापसे अल्प अर्थात् छोटे पड़ जाते हैं, अतएव इन पदार्थोंसे इन विषयोंसे प्राप्त होनेवाला सुख अल्प तथा सापेक्ष है । आज जो पदार्थ सुखरूप है कल वही पदार्थ दुःखरूप हो जाता है । एकके लिए जो सुखरूप है दूसरेके लिए वह उपेक्षणीय है अथवा दुःखरूप है । अतएव अल्प अथवा सापेक्ष सुखसे मनुष्य की आत्यन्तिक तृप्ति होना सम्भव नहीं । उपनिषदों में ऋषियोंने यह घोषणा की कि अल्पमें सुख नहीं है भूमामें ही सुख है ।" जो
१. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ईशोप० ६
२. "यो वै भूमा सत्सुखं नाल्पे सुलमस्ति, भूमैव सुखम् ( छा० उप० ७-२३)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
विविध: २९३
www.jainelibrary.org