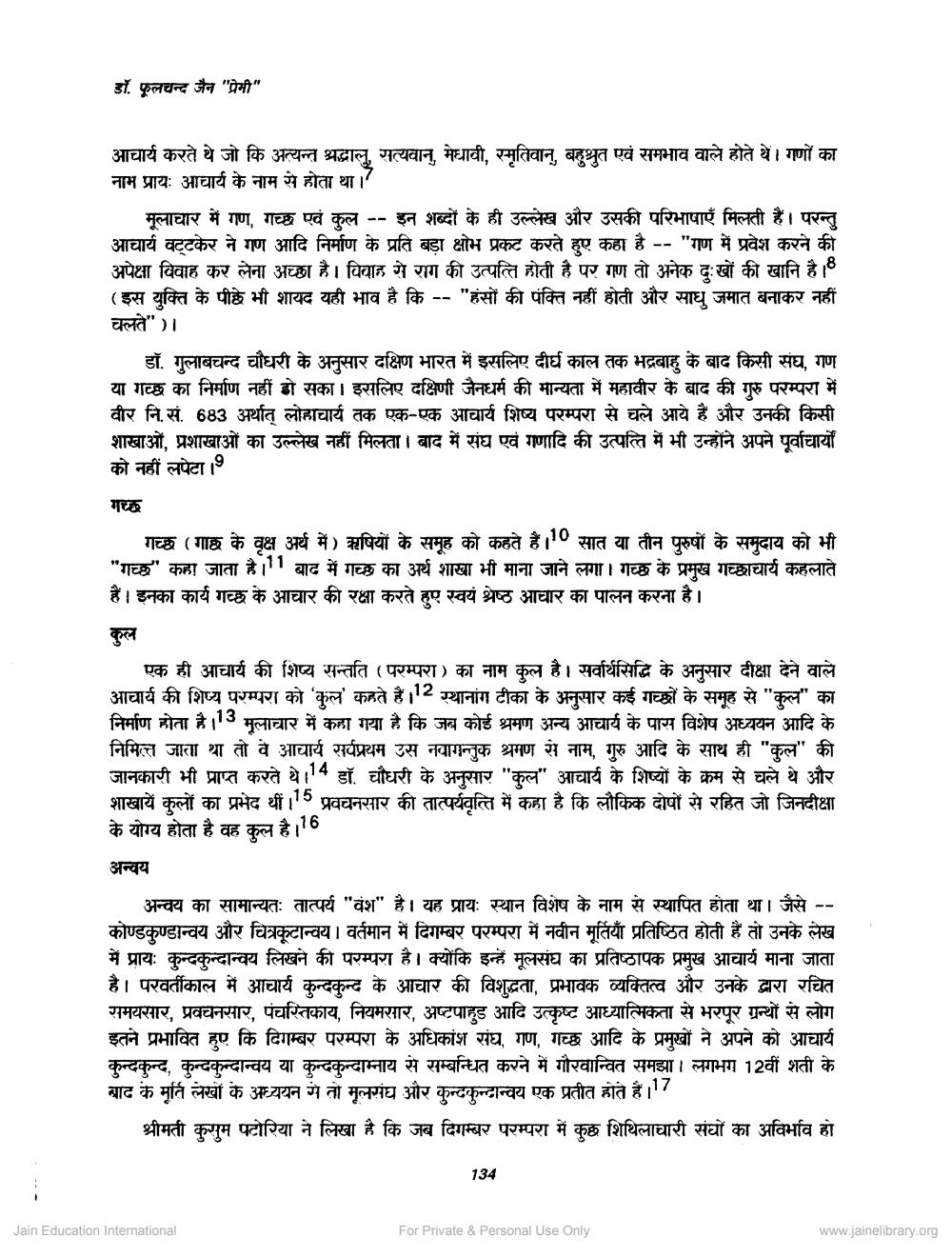________________
डॉ. फूलचन्द जैन "प्रेमी"
आचार्य करते थे जो कि अत्यन्त श्रद्धालु, सत्यवान, मेधावी, स्मृतिवान्, बहुश्रुत एवं समभाव वाले होते थे। गणों का नाम प्रायः आचार्य के नाम से होता था।
मूलाचार में गण, गच्छ एवं कुल -- इन शब्दों के ही उल्लेख और उसकी परिभाषाएँ मिलती है। परन्तु आचार्य वट्टकेर ने गण आदि निर्माण के प्रति बड़ा क्षोभ प्रकट करते हुए कहा है -- "गण में प्रवेश करने की अपेक्षा विवाह कर लेना अच्छा है। विवाह से राग की उत्पत्ति होती है पर गण तो अनेक दुःखों की खानि है। (इस युक्ति के पीछे भी शायद यही भाव है कि -- "हंसों की पंक्ति नहीं होती और साधु जमात बनाकर नहीं चलते")।
डॉ. गुलाबचन्द चौधरी के अनुसार दक्षिण भारत में इसलिए दीर्घकाल तक भद्रबाहु के बाद किसी संघ, गण या गच्छ का निर्माण नहीं हो सका। इसलिए दक्षिणी जैनधर्म की मान्यता में महावीर के बाद की गुरु परम्परा में वीर नि.सं. 683 अर्थात् लोहाचार्य तक एक-एक आचार्य शिष्य परम्परा से चले आये हैं और उनकी किसी शाखाओं, प्रशाखाओं का उल्लेख नहीं मिलता। बाद में संघ एवं गणादि की उत्पत्ति में भी उन्होंने अपने पूर्वाचार्यों को नहीं लपेटा।
गच्छ
गच्छ (गाछ के वृक्ष अर्थ में) ऋषियों के समूह को कहते हैं। सात या तीन पुरुषों के समुदाय को भी "गच्छ" कहा जाता है। बाद में गच्छ का अर्थ शाखा भी माना जाने लगा। गच्छ के प्रमुख गच्छाचार्य कहलाते हैं। इनका कार्य गच्छ के आचार की रक्षा करते हुए स्वयं श्रेष्ठ आचार का पालन करना है।
__एक ही आचार्य की शिष्य सन्तति ( परम्परा) का नाम कूल है। सर्वार्थसिद्धि के अनुसार दीक्षा देने वाले आचार्य की शिष्य परम्परा को 'कुल' कहते हैं। 2 स्थानांग टीका के अनुसार कई गच्छों के समूह से "कुल" का निर्माण होता है।13 मूलाचार में कहा गया है कि जब कोई श्रमण अन्य आचार्य के पास विशेष अध्ययन आदि के निमित्त जाता था तो वे आचार्य सर्वप्रथम उस नवागन्तुक श्रमण से नाम, गुरु आदि के साथ ही "कुल" की जानकारी भी प्राप्त करते थे।14 डॉ. चौधरी के अनुसार "कुल" आचार्य के शिष्यों के क्रम से चले थे और शाखायें कुलों का प्रभेद थीं।15 प्रवचनसार की तात्पर्यवत्ति में कहा है कि लौकिक दोषों से रहित जो जिनदीक्षा के योग्य होता है वह कुल है।16
अन्वय
अन्वय का सामान्यतः तात्पर्य "वंश" है। यह प्रायः स्थान विशेष के नाम से स्थापित होता था। जैसे -- कोण्डकुण्डान्वय और चित्रकूटान्वय । वर्तमान में दिगम्बर परम्परा में नवीन मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होती हैं तो उनके लेख में प्रायः कुन्दकुन्दान्वय लिखने की परम्परा है। क्योंकि इन्हें मूलसंघ का प्रतिष्ठापक प्रमुख आचार्य माना जाता है। परवर्तीकाल में आचार्य कुन्दकुन्द के आचार की विशुद्धता, प्रभावक व्यक्तित्व और उनके द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार, पंचस्तिकाय, नियमसार, अष्टपाहुड आदि उत्कृष्ट आध्यात्मिकता से भरपूर ग्रन्थों से लोग इतने प्रभावित हुए कि दिगम्बर परम्परा के अधिकांश संघ, गण, गच्छ आदि के प्रमुखों ने अपने को आचार्य कुन्दकुन्द, कुन्दकुन्दान्वय या कुन्दकुन्दाम्नाय से सम्बन्धित करने में गौरवान्वित समझा। लगभग 12वीं शती के बाद के मूर्ति लेखों के अध्ययन गे तो मृलसंघ और कुन्दकुन्दान्वय एक प्रतीत होते हैं।7
श्रीमती कुसुम पटोरिया ने लिखा है कि जब दिगम्बर परम्परा में कुछ शिथिलाचारी संघों का अविर्भाव हो
134
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org