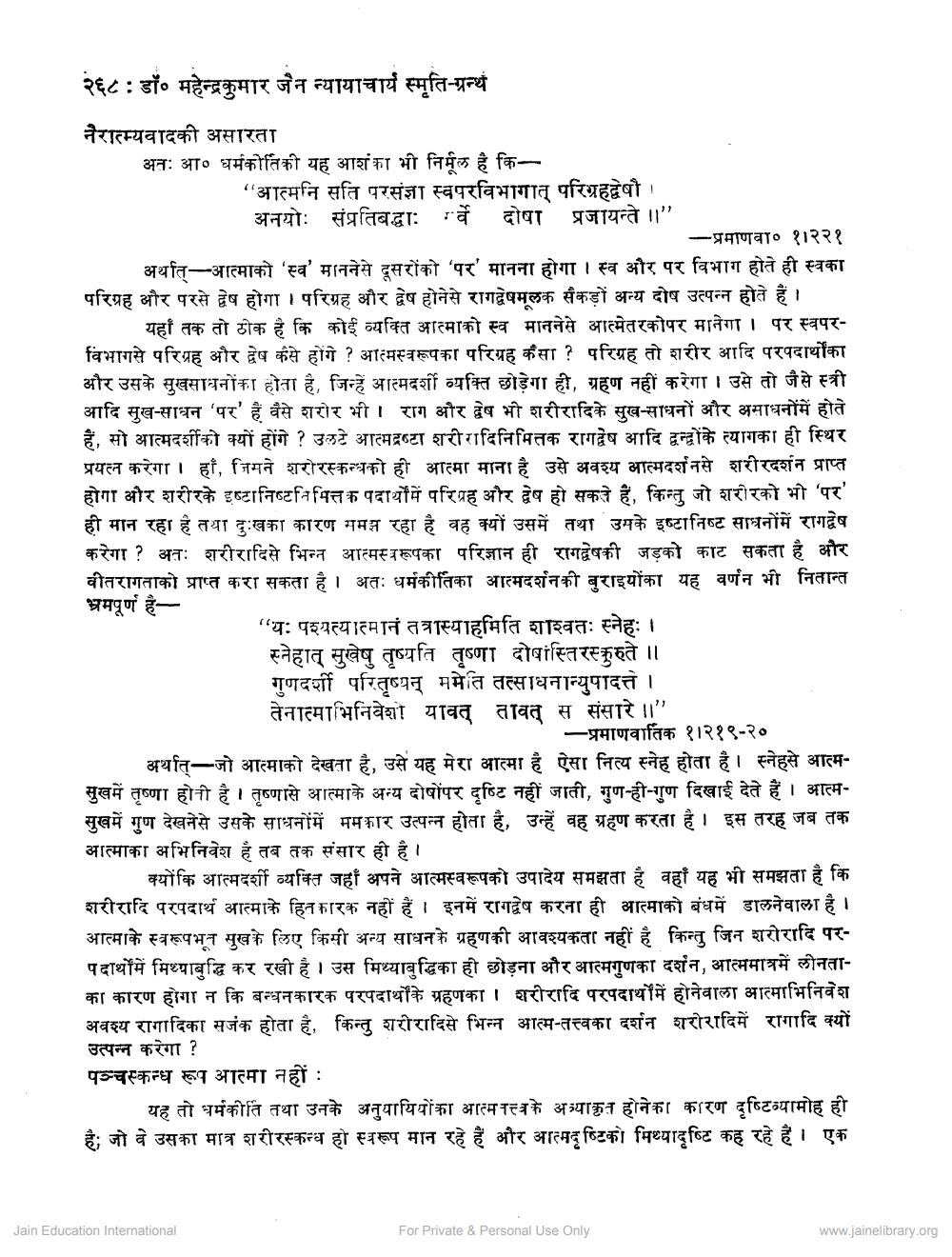________________
२६८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ
नैरात्म्यवादकी असारता
अतः आ० धर्मकीर्तिकी यह आशंका भी निर्मूल है कि
" आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात् परिग्रहद्वेषौ । अनयोः संप्रतिबद्धा: गर्वे दोषा प्रजायन्ते || "
-प्रमाणवा० १२२१
अर्थात् - आत्माको 'स्व' माननेसे दूसरोंको 'पर' मानना होगा। स्व और पर विभाग होते ही स्वका परिग्रह और परसे द्वेष होगा । परिग्रह और द्वेष होनेसे रागद्वेषमूलक सैकड़ों अन्य दोष उत्पन्न होते हैं । यहाँ तक तो ठीक है कि कोई व्यक्ति आत्माको स्व माननेसे आत्मेतरकोपर मानेगा । पर स्वपरविभागसे परिग्रह और द्वेष कैसे होंगे ? आत्मस्वरूपका परिग्रह कैसा ? परिग्रह तो शरीर आदि परपदार्थोंका और उसके सुखसानोंका होता है, जिन्हें आत्मदर्शी व्यक्ति छोड़ेगा ही, ग्रहण नहीं करेगा । उसे तो जैसे स्त्री आदि सुख-साधन 'पर' हैं वैसे शरोर भी । राग और द्वेष भी शरीरादिके सुख-साधनों और असाधनोंमें होते हैं, सो आत्मदर्शीको क्यों होंगे ? उलटे आत्मद्रष्टा शरीरादिनिमित्तक रागद्वेष आदि द्वन्द्वोंके त्यागका ही स्थिर प्रयत्न करेगा। हाँ, जिमने शरोरस्कन्धको ही आत्मा माना है उसे अवश्य आत्मदर्शनसे शरीरदर्शन प्राप्त होगा और शरीरके इष्टानिष्टनिमित्तक पदार्थों में परिग्रह और द्वेष हो सकते हैं, किन्तु जो शरीरको भी 'पर' ही मान रहा है तथा दुःखका कारण समझ रहा है वह क्यों उसमें तथा उसके इष्टानिष्ट साधनों में रागद्वेष करेगा ? अतः शरीरादिसे भिन्न आत्मस्वरूपका परिज्ञान ही रागद्वेषकी जड़को काट सकता है और वीतरागताको प्राप्त करा सकता है । अतः धर्मकीर्तिका आत्मदर्शन की बुराइयोंका यह वर्णन भी नितान्त भ्रमपूर्ण है—
“थः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः । स्नेहात् सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ गुणदर्शी परितुष्यन् ममेति तत्साधनान्युपादत्ते । तेनात्माभिनिवेशो यावत् तावत् स संसारे ॥”
- प्रमाणवार्तिक १।२१९-२० अर्थात् - जो आत्माको देखता है, उसे यह मेरा आत्मा है ऐसा नित्य स्नेह होता है। स्नेहसे आत्मसुखमें तृष्णा होती है । तृष्णासे आत्मा के अन्य दोषोंपर दृष्टि नहीं जाती, गुण-ही-गुण दिखाई देते हैं । आत्मसुखमें गुण देखनेसे उसके साधनोंमें ममकार उत्पन्न होता है, उन्हें वह ग्रहण करता है। इस तरह जब तक आत्माका अभिनिवेश है तब तक संसार ही है ।
क्योंकि आत्मदर्शी व्यक्ति जहाँ अपने आत्मस्वरूपको उपादेय समझता है वहाँ यह भी समझता है कि शरीरादि परपदार्थ आत्माके हितकारक नहीं हैं । इनमें रागद्वेष करना ही आत्माको बंध में डालनेवाला है । आत्मा स्वरूपभूत सुखके लिए किसी अन्य साधनके ग्रहणकी आवश्यकता नहीं किन्तु जिन शरीरादि परपदार्थों में मिथ्याबुद्धि कर रखी है। उस मिथ्याबुद्धिका हो छोड़ना और आत्मगुणका दर्शन, आत्ममात्रमें लीनताका कारण होगा न कि बन्धनकारक परपदार्थों के ग्रहणका । शरीरादि परपदार्थों में होनेवाला आत्माभिनिवेश अवश्य रागादिका सर्जक होता है, किन्तु शरीरादिसे भिन्न आत्म-तत्त्वका दर्शन शरीरादिमें रागादि क्यों उत्पन्न करेगा ?
पञ्चस्कन्ध रूप आत्मा नहीं :
यह तो धर्मकीर्ति तथा उनके अनुयायियों का आत्मतत्त्व अत्र्याकृत होनेका कारण दृष्टिव्यामोह ही है; जो वे उसका मात्र शरीरस्कन्ध हो स्वरूप मान रहे हैं और आत्मदृष्टिको मिथ्यादृष्टि कह रहे हैं । एक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org