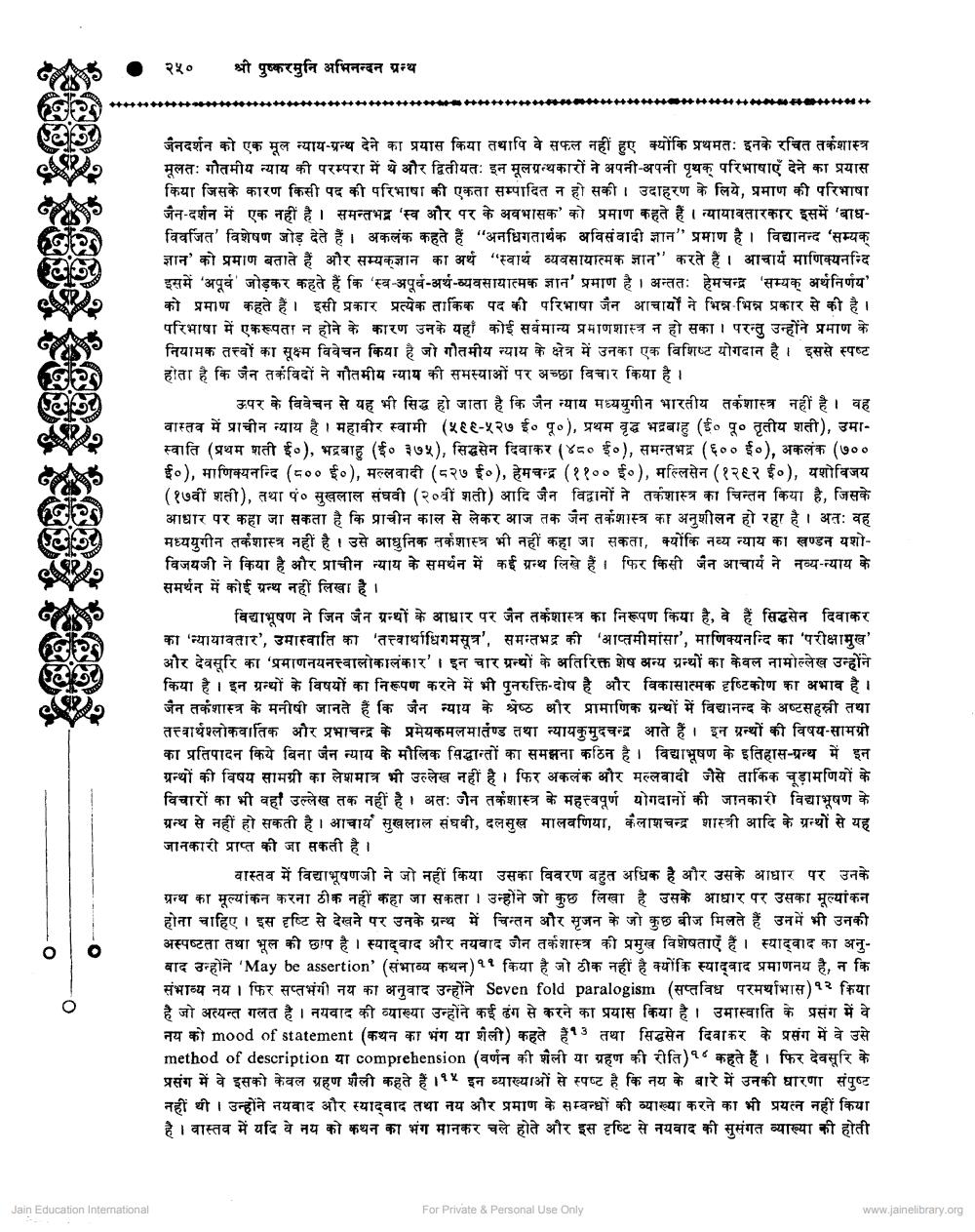________________
। २५०
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ
रण किसी पद की परिभाव और पर के अवभासक को विसंवादा ज्ञान" प्रमाण
जनदर्शन को एक मूल न्याय-ग्रन्थ देने का प्रयास किया तथापि वे सफल नहीं हुए क्योंकि प्रथमतः इनके रचित तर्कशास्त्र मूलतः गौतमीय न्याय की परम्परा में थे और द्वितीयतः इन मूलग्रन्थकारों ने अपनी-अपनी पृथक् परिभाषाएँ देने का प्रयास किया जिसके कारण किसी पद की परिभाषा की एकता सम्पादित न हो सकी। उदाहरण के लिये, प्रमाण की परिभाषा जैन-दर्शन में एक नहीं है। समन्तभद्र 'स्व और पर के अवभासक' को प्रमाण कहते हैं । न्यायावतारकार इसमें 'बाधविवर्जित' विशेषण जोड़ देते हैं। अकलंक कहते हैं "अनधिगतार्थक अविसंवादी ज्ञान" प्रमाण है। विद्यानन्द 'सम्यक् ज्ञान' को प्रमाण बताते हैं और सम्यकज्ञान का अर्थ "स्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञान" करते हैं। आचार्य माणिक्यनन्दि इसमें 'अपूर्व' जोड़कर कहते हैं कि 'स्व-अपूर्व-अर्थ-व्यवसायात्मक ज्ञान' प्रमाण है । अन्ततः हेमचन्द्र 'सम्यक् अर्थनिर्णय' को प्रमाण कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक तार्किक पद की परिभाषा जैन आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है । परिभाषा में एकरूपता न होने के कारण उनके यहाँ कोई सर्वमान्य प्रमाणशास्त्र न हो सका। परन्तु उन्होंने प्रमाण के नियामक तत्त्वों का सूक्ष्म विवेचन किया है जो गौतमीय न्याय के क्षेत्र में उनका एक विशिष्ट योगदान है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन तकविदों ने गौतमीय न्याय की समस्याओं पर अच्छा विचार किया है।
ऊपर के विवेचन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि जैन न्याय मध्ययुगीन भारतीय तर्कशास्त्र नहीं है। वह वास्तव में प्राचीन न्याय है । महावीर स्वामी (५९६-५२७ ई० पू०), प्रथम वृद्ध भद्रबाहु (ई० पू० तृतीय शती), उमास्वाति (प्रथम शती ई०), भद्रबाहु (ई० ३७५), सिद्धसेन दिवाकर (४८० ई०), समन्तभद्र (६०० ई०), अकलंक (७०० ई०), माणिक्यनन्दि (८०० ई०), मल्लवादी (८२७ ई०), हेमचन्द्र (११०० ई०), मल्लिसेन (१२६२ ई०), यशोविजय (१७वीं शती), तथा पं० सुखलाल संघवी (२०वीं शती) आदि जैन विद्वानों ने तर्कशास्त्र का चिन्तन किया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक जैन तर्कशास्त्र का अनुशीलन हो रहा है । अत: वह मध्ययुगीन तर्कशास्त्र नहीं है । उसे आधुनिक तर्कशास्त्र भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नव्य न्याय का खण्डन यशोविजयजी ने किया है और प्राचीन न्याय के समर्थन में कई ग्रन्थ लिखे हैं। फिर किसी जैन आचार्य ने नव्य-न्याय के समर्थन में कोई ग्रन्थ नहीं लिखा है।
विद्याभूषण ने जिन जैन ग्रन्थों के आधार पर जैन तर्कशास्त्र का निरूपण किया है, वे हैं सिद्धसेन दिवाकर का न्यायावतार', उमास्वाति का 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र', समन्तभद्र की 'आप्तमीमांसा', माणिक्यनन्दि का परीक्षामुख' और देवसूरि का 'प्रमाणनयनत्त्वालोकालंकार'। इन चार ग्रन्थों के अतिरिक्त शेष अन्य ग्रन्थों का केवल नामोल्लेख उन्होंने किया है। इन ग्रन्थों के विषयों का निरूपण करने में भी पुनरुक्ति-दोष है और विकासात्मक दृष्टिकोण का अभाव है। जैन तर्कशास्त्र के मनीषी जानते हैं कि जैन न्याय के श्रेष्ठ और प्रामाणिक ग्रन्थों में विद्यानन्द के अष्टसहस्री तथा तत्त्वार्थश्लोकवातिक और प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्र आते हैं। इन ग्रन्थों की विषय-सामग्री का प्रतिपादन किये बिना जैन न्याय के मौलिक सिद्धान्तों का समझना कठिन है। विद्याभूषण के इतिहास-ग्रन्थ में इन ग्रन्थों की विषय सामग्री का लेशमात्र भी उल्लेख नहीं है। फिर अकलंक और मल्लवादी जैसे ताकिक चूड़ामणियों के विचारों का भी वहाँ उल्लेख तक नहीं है। अत: जैन तर्कशास्त्र के महत्त्वपूर्ण योगदानों की जानकारी विद्याभूषण के ग्रन्थ से नहीं हो सकती है। आचार्य सुखलाल संघवी, दलसुख मालवणिया, कैलाशचन्द्र शास्त्री आदि के ग्रन्थों से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
वास्तव में विद्याभूषणजी ने जो नहीं किया उसका विवरण बहुत अधिक है और उसके आधार पर उनके ग्रन्थ का मूल्यांकन करना ठीक नहीं कहा जा सकता । उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर उनके ग्रन्थ में चिन्तन और सृजन के जो कुछ बीज मिलते हैं उनमें भी उनकी अस्पष्टता तथा भूल की छाप है । स्याद्वाद और नयवाद जैन तर्कशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्याद्वाद का अनुबाद उन्होंने 'May be assertion' (संभाव्य कथन)११ किया है जो ठीक नहीं है क्योंकि स्याद्वाद प्रमाणनय है, न कि संभाव्य नय । फिर सप्तभंगी नय का अनुवाद उन्होंने Seven fold paralogism (सप्तविध परमर्थाभास) १२ किया है जो अत्यन्त गलत है । नयवाद की व्याख्या उन्होंने कई ढंग से करने का प्रयास किया है। उमास्वाति के प्रसंग में वे नय को mood of statement (कथन का भंग या शैली) कहते हैं13 तथा सिद्धसेन दिवाकर के प्रसंग में वे उसे method of description या comprehension (वर्णन की शैली या ग्रहण की रीति)१४ कहते हैं। फिर देवसूरि के प्रसंग में वे इसको केवल ग्रहण शैली कहते हैं । १५ इन व्याख्याओं से स्पष्ट है कि नय के बारे में उनकी धारणा संपुष्ट नहीं थी। उन्होंने नयवाद और स्याद्वाद तथा नय और प्रमाण के सम्बन्धों की व्याख्या करने का भी प्रयत्न नहीं किया है। वास्तव में यदि वे नय को कथन का भंग मानकर चले होते और इस दृष्टि से नयवाद की सुसंगत व्याख्या की होती
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org