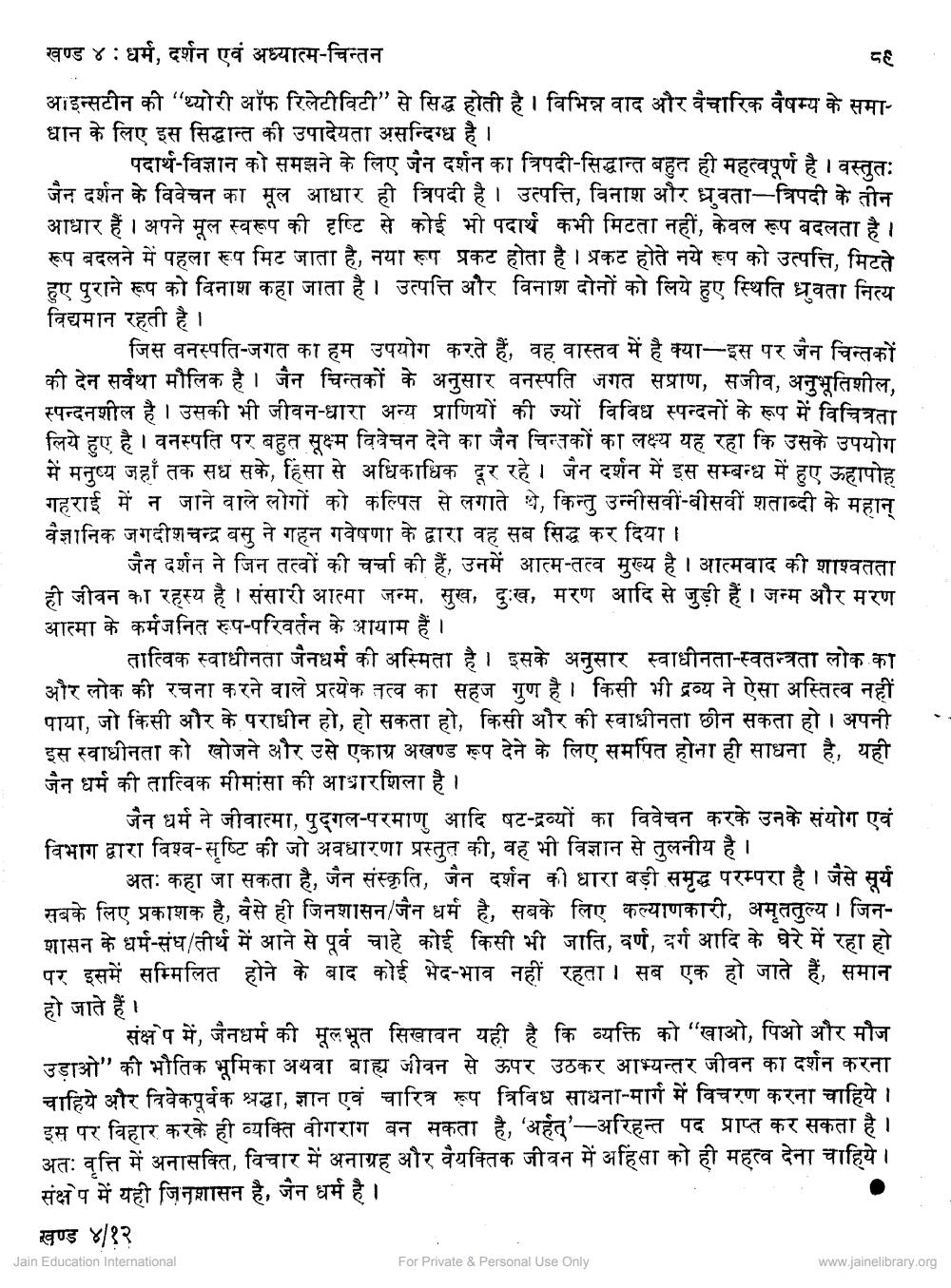________________ 89 खण्ड 4 : धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म-चिन्तन आइन्सटीन की “थ्योरी ऑफ रिलेटीविटी" से सिद्ध होती है / विभिन्न वाद और वैचारिक वैषम्य के समा. धान के लिए इस सिद्धान्त की उपादेयता असन्दिग्ध है। पदार्थ-विज्ञान को समझने के लिए जैन दर्शन का त्रिपदी-सिद्धान्त बहुत ही महत्वपूर्ण है / वस्तुतः जैन दर्शन के विवेचन का मूल आधार ही त्रिपदी है। उत्पत्ति, विनाश और ध्रुवता-त्रिपदी के तीन आधार हैं / अपने मूल स्वरूप की दृष्टि से कोई भी पदार्थ कभी मिटता नहीं, केवल रूप बदलता है। रूप बदलने में पहला रूप मिट जाता है, नया रूप प्रकट होता है। प्रकट होते नये रूप को उत्पत्ति, मिटते हुए पुराने रूप को विनाश कहा जाता है। उत्पत्ति और विनाश दोनों को लिये हुए स्थिति ध्रवता नित्य विद्यमान रहती है। जिस वनस्पति-जगत का हम उपयोग करते हैं, वह वास्तव में है क्या-इस पर जैन चिन्तकों की देन सर्वथा मौलिक है। जैन चिन्तकों के अनुसार वनस्पति जगत सप्राण, सजीव, अनुभूतिशील, स्पन्दनशील है। उसकी भी जीवन-धारा अन्य प्राणियों की ज्यों विविध स्पन्दनों के रूप में विचित्रता लिये हुए है / वनस्पति पर बहुत सूक्ष्म विवेचन देने का जैन चिन्तकों का लक्ष्य यह रहा कि उसके उपयोग में मनुष्य जहाँ तक सध सके, हिंसा से अधिकाधिक दूर रहे। जैन दर्शन में इस सम्बन्ध में हुए ऊहापोह गहराई में न जाने वाले लोगों को कल्पित से लगाते थे, किन्तु उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बसु ने गहन गवेषणा के द्वारा वह सब सिद्ध कर दिया। जैन दर्शन ने जिन तत्वों की चर्चा की हैं, उनमें आत्म-तत्व मुख्य है / आत्मवाद की शाश्वतता ही जीवन का रहस्य है / संसारी आत्मा जन्म, सुख, दुःख, मरण आदि से जुड़ी हैं। जन्म और मरण आत्मा के कर्मजनित रूप-परिवर्तन के आयाम हैं। तात्विक स्वाधीनता जैनधर्म की अस्मिता है। इसके अनुसार स्वाधीनता-स्वतन्त्रता लोक का और लोक की रचना करने वाले प्रत्येक तत्व का सहज गुण है। किसी भी द्रव्य ने ऐसा अस्तित्व नहीं पाया, जो किसी और के पराधीन हो, हो सकता हो, किसी और की स्वाधीनता छीन सकता हो / अपनी इस स्वाधीनता को खोजने और उसे एकाग्र अखण्ड रूप देने के लिए समर्पित होना ही साधना है, यही जैन धर्म की तात्विक मीमांसा की आधारशिला है। जैन धर्म ने जीवात्मा, पुद्गल-परमाणु आदि षट-द्रव्यों का विवेचन करके उनके संयोग एवं विभाग द्वारा विश्व-सृष्टि की जो अवधारणा प्रस्तुत की, वह भी विज्ञान से तुलनीय है। अतः कहा जा सकता है, जैन संस्कृति, जैन दर्शन की धारा बड़ी समृद्ध परम्परा है / जैसे सूर्य सबके लिए प्रकाशक है, वैसे ही जिनशासन/जैन धर्म है, सबके लिए कल्याणकारी, अमृततुल्य / जिनशासन के धर्म-संध/तीर्थ में आने से पूर्व चाहे कोई किसी भी जाति, वर्ण, वर्ग आदि के घेरे में रहा हो पर इसमें सम्मिलित होने के बाद कोई भेद-भाव नहीं रहता। सब एक हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। संक्षेप में, जैनधर्म की मूलभूत सिखावन यही है कि व्यक्ति को “खाओ, पिओ और मौज उड़ाओ" की भौतिक भूमिका अथवा बाह्य जीवन से ऊपर उठकर आभ्यन्तर जीवन का दर्शन करना चाहिये और विवेकपूर्वक श्रद्धा, ज्ञान एवं चारित्र रूप त्रिविध साधना-मार्ग में विचरण करना चाहिये / इस पर विहार करके ही व्यक्ति वीगराग बन सकता है, 'अर्हत्'-अरिहन्त पद प्राप्त कर सकता है / अतः वृत्ति में अनासक्ति, विचार में अनाग्रह और वैयक्तिक जीवन में अहिंसा को ही महत्व देना चाहिये। संक्षेप में यही जिनशासन है, जैन धर्म है। खण्ड 4/12 www.jainelibrary.org For Private & Personal Use Only