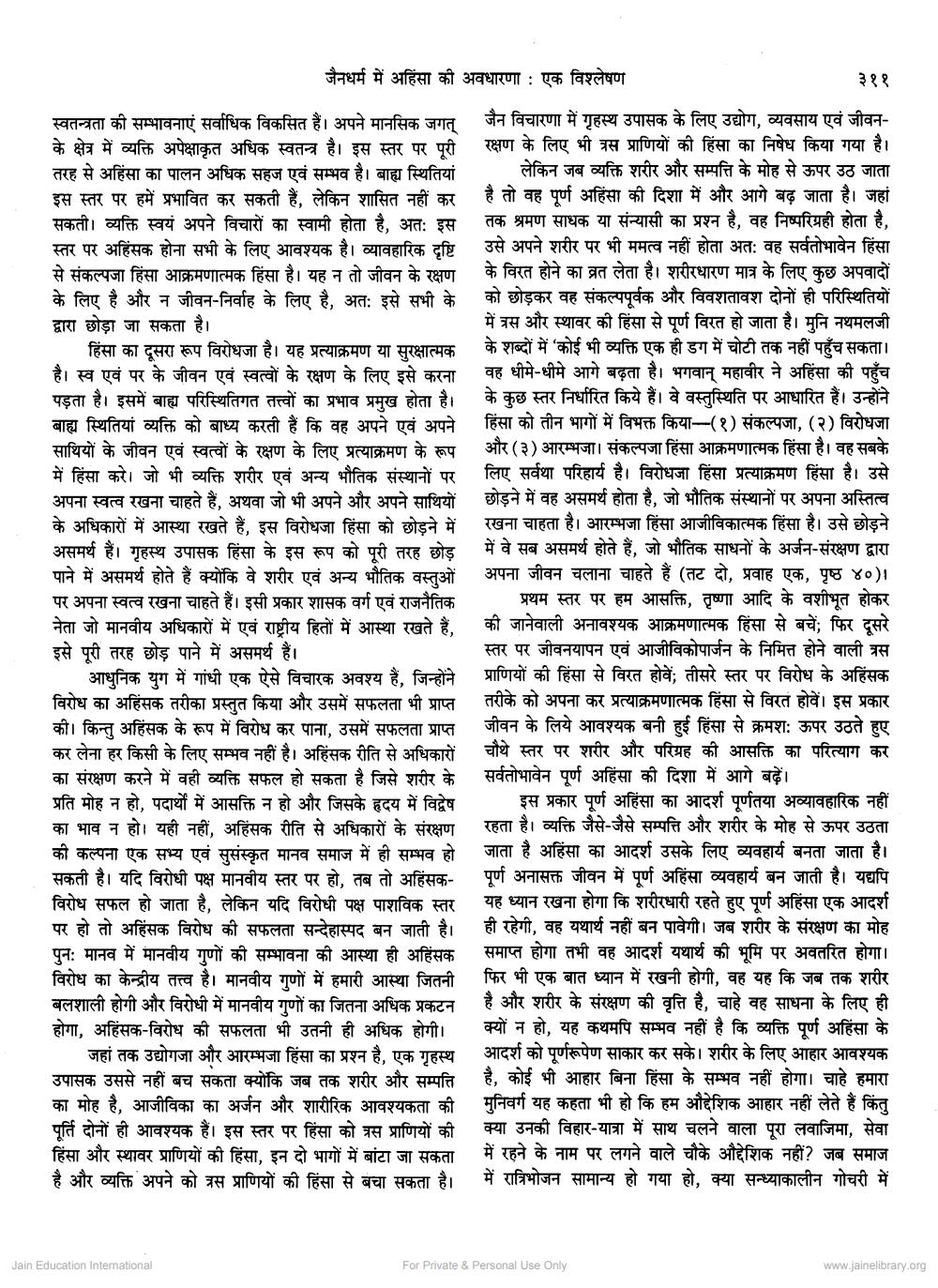________________
स्वतन्त्रता की सम्भावनाएं सर्वाधिक विकसित हैं। अपने मानसिक जगत् के क्षेत्र में व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र है। इस स्तर पर पूरी तरह से अहिंसा का पालन अधिक सहज एवं सम्भव है। बाह्य स्थितियां इस स्तर पर हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन शासित नहीं कर सकती। व्यक्ति स्वयं अपने विचारों का स्वामी होता है, अतः इस स्तर पर अहिंसक होना सभी के लिए आवश्यक है । व्यावहारिक दृष्टि से संकल्पजा हिंसा आक्रमणात्मक हिंसा है। यह न तो जीवन के रक्षण के लिए है और न जीवन-निर्वाह के लिए है, अतः इसे सभी के द्वारा छोड़ा जा सकता है।
जैनधर्म में अहिंसा की अवधारणा एक विश्लेषण
हिंसा का दूसरा रूप विरोधजा है यह प्रत्याक्रमण या सुरक्षात्मक है। स्व एवं पर के जीवन एवं स्वत्वों के रक्षण के लिए इसे करना पड़ता है। । इसमें बाह्य परिस्थितिगत तत्त्वों का प्रभाव प्रमुख होता है। बाह्य स्थितियां व्यक्ति को बाध्य करती हैं कि वह अपने एवं अपने साथियों के जीवन एवं स्वत्वों के रक्षण के लिए प्रत्याक्रमण के रूप में हिंसा करे जो भी व्यक्ति शरीर एवं अन्य भौतिक संस्थानों पर अपना स्वत्व रखना चाहते हैं, अथवा जो भी अपने और अपने साथियों के अधिकारों में आस्था रखते हैं, इस विरोधजा हिंसा को छोड़ने में असमर्थ हैं। गृहस्थ उपासक हिंसा के इस रूप को पूरी तरह छोड़ पाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे शरीर एवं अन्य भौतिक वस्तुओं पर अपना स्वत्व रखना चाहते हैं। इसी प्रकार शासक वर्ग एवं राजनैतिक नेता जो मानवीय अधिकारों में एवं राष्ट्रीय हितों में आस्था रखते हैं, इसे पूरी तरह छोड़ पाने में असमर्थ हैं।
आधुनिक युग में गांधी एक ऐसे विचारक अवश्य हैं, जिन्होंने विरोध का अहिंसक तरीका प्रस्तुत किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। किन्तु अहिंसक के रूप में विरोध कर पाना, उसमें सफलता प्राप्त कर लेना हर किसी के लिए सम्भव नहीं है। अहिंसक रीति से अधिकारों का संरक्षण करने में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे शरीर के प्रति मोह न हो, पदार्थों में आसक्ति न हो और जिसके हृदय में विद्वेष का भाव न हो। यही नहीं, अहिंसक रीति से अधिकारों के संरक्षण की कल्पना एक सभ्य एवं सुसंस्कृत मानव समाज में ही सम्भव हो सकती है। यदि विरोधी पक्ष मानवीय स्तर पर हो, तब तो अहिंसकविरोध सफल हो जाता है, लेकिन यदि विरोधी पक्ष पाशविक स्तर पर हो तो अहिंसक विरोध की सफलता सन्देहास्पद बन जाती है। पुनः मानव में मानवीय गुणों की सम्भावना की आस्था ही अहिंसक विरोध का केन्द्रीय तत्व है। मानवीय गुणों में हमारी आस्था जितनी बलशाली होगी और विरोधी में मानवीय गुणों का जितना अधिक प्रकटन होगा, अहिंसक विरोध की सफलता भी उतनी ही अधिक होगी। जहां तक उद्योगजा और आरम्भजा हिंसा का प्रश्न है, एक गृहस्थ उपासक उससे नहीं बच सकता क्योंकि जब तक शरीर और सम्पत्ति का मोह है, आजीविका का अर्जन और शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति दोनों ही आवश्यक हैं। इस स्तर पर हिंसा को उस प्राणियों की हिंसा और स्थावर प्राणियों की हिंसा, इन दो भागों में बांटा जा सकता है और व्यक्ति अपने को उस प्राणियों की हिंसा से बचा सकता है।
-
Jain Education International
३११
जैन विचारणा में गृहस्थ उपासक के लिए उद्योग, व्यवसाय एवं जीवनरक्षण के लिए भी त्रस प्राणियों की हिंसा का निषेध किया गया है।
लेकिन जब व्यक्ति शरीर और सम्पत्ति के मोह से ऊपर उठ जाता है तो वह पूर्ण अहिंसा की दिशा में और आगे बढ़ जाता है। जहां तक श्रमण साधक या संन्यासी का प्रश्न है, वह निष्परिग्रही होता है, उसे अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं होता अतः वह सर्वतोभावेन हिंसा के विरत होने का व्रत लेता है। शरीरधारण मात्र के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर वह संकल्पपूर्वक और विवशतावश दोनों ही परिस्थितियों में बस और स्थावर की हिंसा से पूर्ण विरत हो जाता है। मुनि नथमलजी के शब्दों में 'कोई भी व्यक्ति एक ही डग में चोटी तक नहीं पहुँच सकता। वह धीमे-धीमे आगे बढ़ता है भगवान् महावीर ने अहिंसा की पहुँच के कुछ स्तर निर्धारित किये हैं। वे वस्तुस्थिति पर आधारित हैं। उन्होंने हिंसा को तीन भागों में विभक्त किया- ( १ ) संकल्पजा, (२) विरोधजा और (३) आरम्भजा संकल्पजा हिंसा आक्रमणात्मक हिंसा है वह सबके लिए सर्वथा परिहार्य है। विरोधजा हिंसा प्रत्याक्रमण हिंसा है उसे छोड़ने में वह असमर्थ होता है, जो भौतिक संस्थानों पर अपना अस्तित्व रखना चाहता है। आरम्भजा हिंसा आजीविकात्मक हिंसा है। उसे छोड़ने में वे सब असमर्थ होते हैं, जो भौतिक साधनों के अर्जन-संरक्षण द्वारा अपना जीवन चलाना चाहते हैं (तट दो, प्रवाह एक पृष्ठ ४० ) 1
"
प्रथम स्तर पर हम आसक्ति, तृष्णा आदि के वशीभूत होकर की जानेवाली अनावश्यक आक्रमणात्मक हिंसा से बचें, फिर दूसरे स्तर पर जीवनयापन एवं आजीविकोपार्जन के निमित्त होने वाली स प्राणियों की हिंसा से विरत होवें; तीसरे स्तर पर विरोध के अहिंसक तरीके को अपना कर प्रत्याक्रमणात्मक हिंसा से विरत होवें इस प्रकार जीवन के लिये आवश्यक बनी हुई हिंसा से क्रमश: ऊपर उठते हुए चौथे स्तर पर शरीर और परिग्रह की आसक्ति का परित्याग कर सर्वतोभावेन पूर्ण अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ें।
इस प्रकार पूर्ण अहिंसा का आदर्श पूर्णतया अव्यावहारिक नहीं रहता है। व्यक्ति जैसे-जैसे सम्पत्ति और शरीर के मोह से ऊपर उठता जाता है अहिंसा का आदर्श उसके लिए व्यवहार्य बनता जाता है। पूर्ण अनासक्त जीवन में पूर्ण अहिंसा व्यवहार्य बन जाती है। यद्यपि यह ध्यान रखना होगा कि शरीरधारी रहते हुए पूर्ण अहिंसा एक आदर्श ही रहेगी, वह यथार्थ नहीं बन पावेगी। जब शरीर के संरक्षण का मोह समाप्त होगा तभी वह आदर्श यथार्थ की भूमि पर अवतरित होगा। फिर भी एक बात ध्यान में रखनी होगी, वह यह कि जब तक शरीर है और शरीर के संरक्षण की वृत्ति है, चाहे वह साधना के लिए ही क्यों न हो, यह कथमपि सम्भव नहीं है कि व्यक्ति पूर्ण अहिंसा के आदर्श को पूर्णरूपेण साकार कर सके। शरीर के लिए आहार आवश्यक है, कोई भी आहार बिना हिंसा के सम्भव नहीं होगा। चाहे हमारा मुनिवर्ग यह कहता भी हो कि हम औदेशिक आहार नहीं लेते हैं किंतु क्या उनकी विहार यात्रा में साथ चलने वाला पूरा लवाजमा सेवा में रहने के नाम पर लगने वाले चौके औरेशिक नहीं? जब समाज में रात्रिभोजन सामान्य हो गया हो, क्या सन्ध्याकालीन गोवरी में
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.