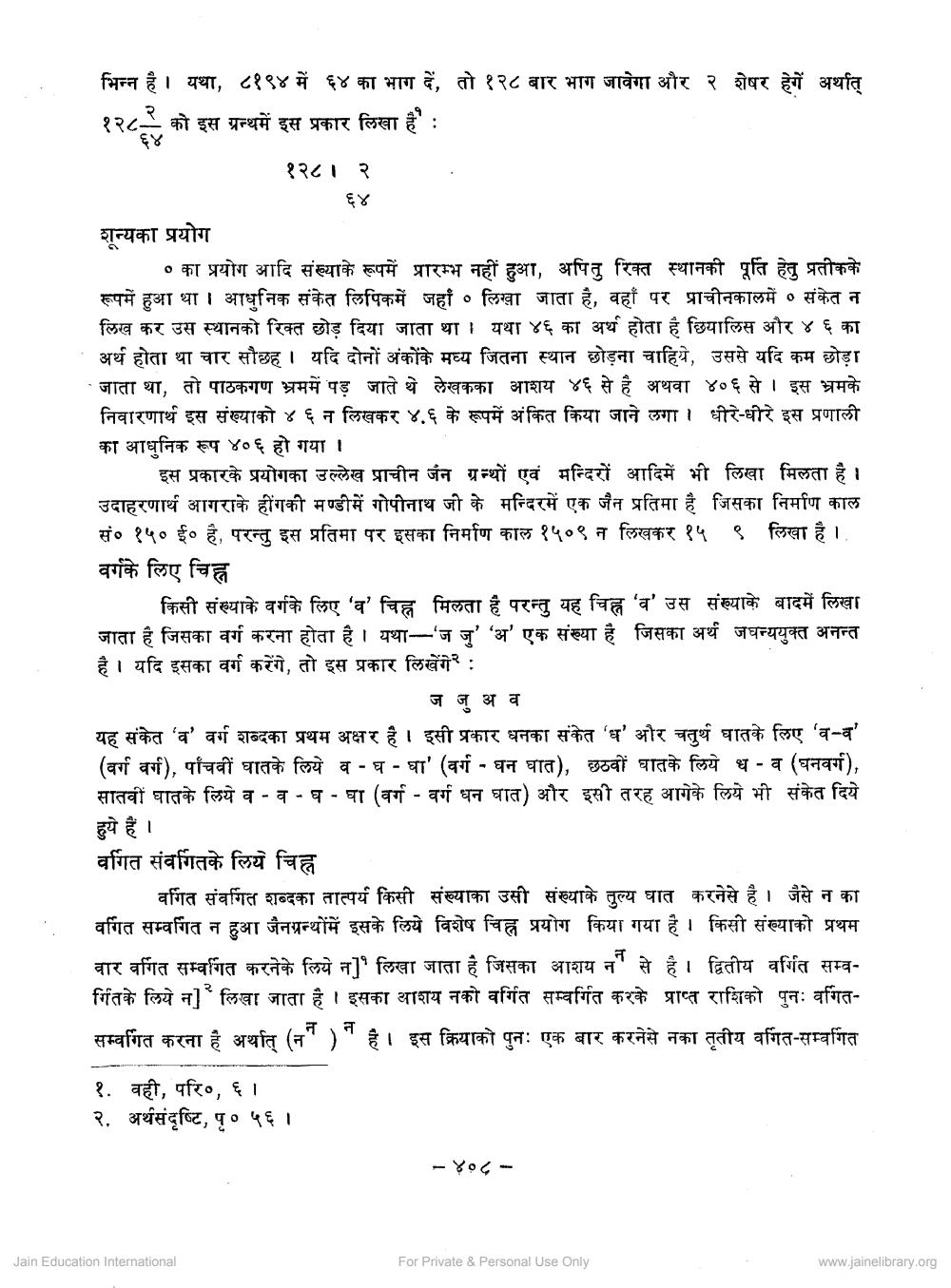________________
भिन्न है । यथा, ८१९४ में ६४ का भाग दें, तो १२८ बार भाग जावेगा और २ शेषर हेगें अर्थात् १२८२ को इस ग्रन्थमें इस प्रकार लिखा है :
१२८ ।
२
शून्यका प्रयोग
___० का प्रयोग आदि संख्याके रूपमें प्रारम्भ नहीं हुआ, अपितु रिक्त स्थानकी पूर्ति हेतु प्रतीकके रूपमें हुआ था । आधुनिक संकेत लिपिकमें जहाँ • लिखा जाता है, वहाँ पर प्राचीनकालमें ० संकेत न लिख कर उस स्थानको रिक्त छोड़ दिया जाता था। यथा ४६ का अर्थ होता है छियालिस और ४ ६ का अर्थ होता था चार सौछह । यदि दोनों अंकोंके मध्य जितना स्थान छोड़ना चाहिये, उससे यदि कम छोड़ा जाता था, तो पाठकगण भ्रममें पड़ जाते थे लेखकका आशय ४६ से है अथवा ४०६ से । इस भ्रमके निवारणार्थ इस संख्याको ४६ न लिखकर ४.६ के रूपमें अंकित किया जाने लगा। धीरे-धीरे इस प्रणाली का आधुनिक रूप ४०६ हो गया ।
इस प्रकारके प्रयोगका उल्लेख प्राचीन जैन ग्रन्थों एवं मन्दिरों आदिमें भी लिखा मिलता है। उदाहरणार्थ आगराके हींगकी मण्डीमें गोपीनाथ जी के मन्दिरमें एक जैन प्रतिमा है जिसका निर्माण काल सं० १५० ई० है, परन्तु इस प्रतिमा पर इसका निर्माण काल १५०९ न लिखकर १५ ९ लिखा है । वर्गके लिए चिह्न
__ किसी संख्याके वर्गके लिए 'व' चिह्न मिलता है परन्तु यह चिह्न 'व' उस संख्याके बादमें लिखा जाता है जिसका वर्ग करना होता है। यथा-'जज' 'अ' एक संख्या है जिसका अर्थ जघन्ययुक्त अनन्त है। यदि इसका वर्ग करेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे :
ज जु अ व यह संकेत 'व' वर्ग शब्दका प्रथम अक्षर है। इसी प्रकार धनका संकेत 'ध' और चतुर्थ घातके लिए 'व-व' (वर्ग वर्ग), पाँचवीं घातके लिये व - घ - घा' (वर्ग - घन घात), छठवों घातके लिये ध - व (घनवर्ग), सातवीं घातके लिये व - व - घ - घा (वर्ग - वर्ग धन घात) और इसी तरह आगेके लिये भी संकेत दिये हुये हैं। वर्गित संवर्गितके लिये चिह्न
वर्गित संवर्गित शब्दका तात्पर्य किसी संख्याका उसी संख्याके तुल्य घात करनेसे है। जैसे न का वर्गित सम्वन्ति न हुआ जैनग्रन्थोंमें इसके लिये विशेष चिह्न प्रयोग किया गया है । किसी संख्याको प्रथम वार वर्गित सम्वगित करनेके लिये न]' लिखा जाता है जिसका आशय न' से है। द्वितीय वर्गित सम्वर्गितके लिये न] लिखा जाता है । इसका आशय नको वर्गित सम्वर्गित करके प्राप्त राशिको पुनः वगितसम्वगित करना है अर्थात् (नन )न है। इस क्रियाको पुनः एक बार करनेसे नका तृतीय वर्गित-सम्बगित
१. वही, परि०, ६ । २. अर्थसंदृष्टि, पृ० ५६ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org