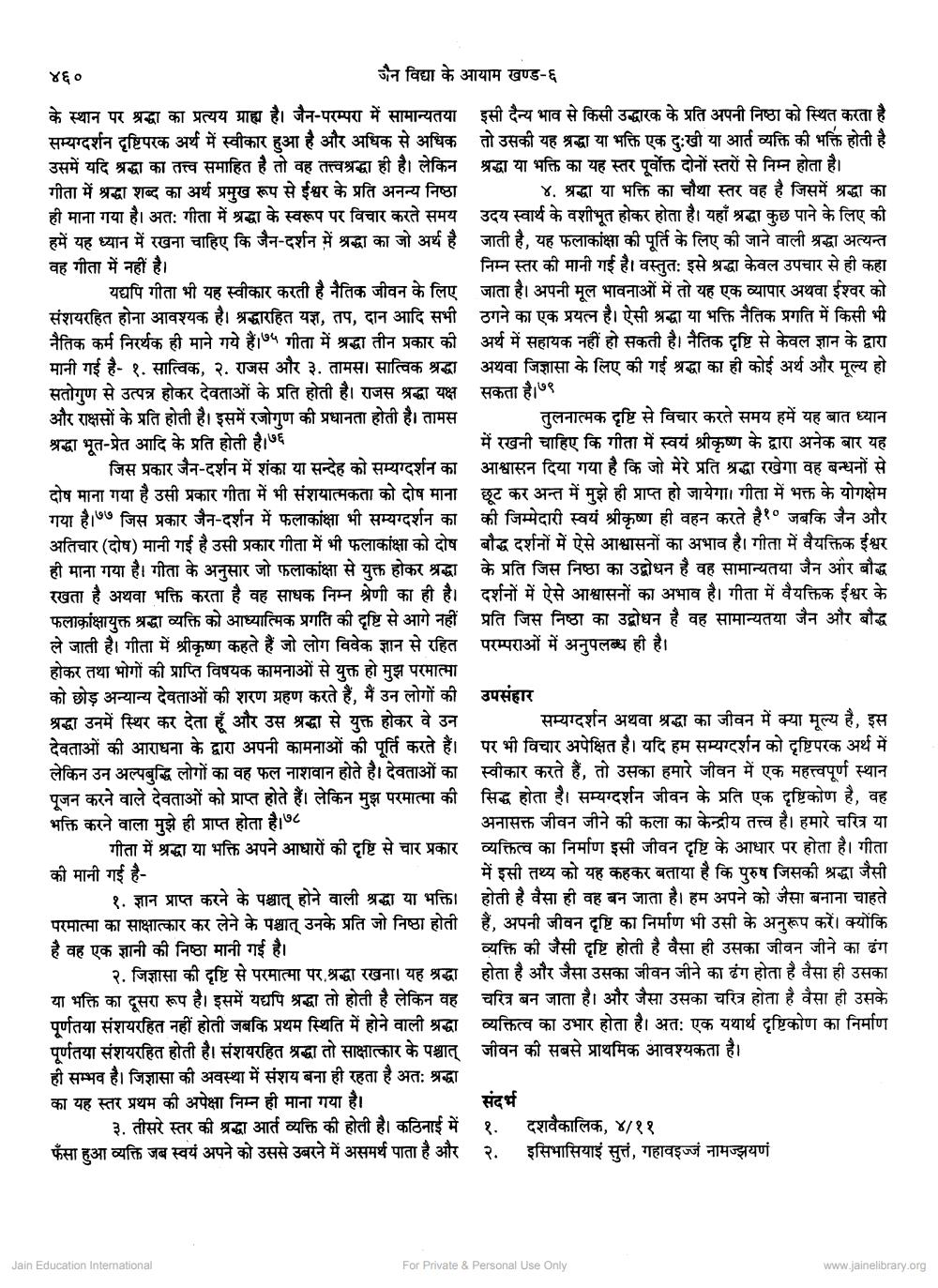________________ 460 जैन विद्या के आयाम खण्ड-६ के स्थान पर श्रद्धा का प्रत्यय ग्राह्य है। जैन-परम्परा में सामान्यतया इसी दैन्य भाव से किसी उद्धारक के प्रति अपनी निष्ठा को स्थित करता है सम्यग्दर्शन दृष्टिपरक अर्थ में स्वीकार हुआ है और अधिक से अधिक तो उसकी यह श्रद्धा या भक्ति एक दुःखी या आर्त व्यक्ति की भक्ति होती है उसमें यदि श्रद्धा का तत्त्व समाहित है तो वह तत्त्वश्रद्धा ही है। लेकिन श्रद्धा या भक्ति का यह स्तर पूर्वोक्त दोनों स्तरों से निम्न होता है। गीता में श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रमुख रूप से ईश्वर के प्रति अनन्य निष्ठा 4. श्रद्धा या भक्ति का चौथा स्तर वह है जिसमें श्रद्धा का ही माना गया है। अत: गीता में श्रद्धा के स्वरूप पर विचार करते समय उदय स्वार्थ के वशीभूत होकर होता है। यहाँ श्रद्धा कुछ पाने के लिए की हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जैन-दर्शन में श्रद्धा का जो अर्थ है जाती है, यह फलाकांक्षा की पूर्ति के लिए की जाने वाली श्रद्धा अत्यन्त वह गीता में नहीं है। निम्न स्तर की मानी गई है। वस्तुत: इसे श्रद्धा केवल उपचार से ही कहा यद्यपि गीता भी यह स्वीकार करती है नैतिक जीवन के लिए जाता है। अपनी मूल भावनाओं में तो यह एक व्यापार अथवा ईश्वर को संशयरहित होना आवश्यक है। श्रद्धारहित यज्ञ, तप, दान आदि सभी ठगने का एक प्रयत्न है। ऐसी श्रद्धा या भक्ति नैतिक प्रगति में किसी भी नैतिक कर्म निरर्थक ही माने गये हैं।७५ गीता में श्रद्धा तीन प्रकार की अर्थ में सहायक नहीं हो सकती है। नैतिक दृष्टि से केवल ज्ञान के द्वारा मानी गई है- 1. सात्विक, 2. राजस और 3. तामस। सात्विक श्रद्धा अथवा जिज्ञासा के लिए की गई श्रद्धा का ही कोई अर्थ और मूल्य हो सतोगुण से उत्पन्न होकर देवताओं के प्रति होती है। राजस श्रद्धा यक्ष सकता है।७९ / और राक्षसों के प्रति होती है। इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। तामस तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते समय हमें यह बात ध्यान श्रद्धा भूत-प्रेत आदि के प्रति होती है।७६ में रखनी चाहिए कि गीता में स्वयं श्रीकृष्ण के द्वारा अनेक बार यह जिस प्रकार जैन-दर्शन में शंका या सन्देह को सम्यग्दर्शन का आश्वासन दिया गया है कि जो मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा वह बन्धनों से दोष माना गया है उसी प्रकार गीता में भी संशयात्मकता को दोष माना छूट कर अन्त में मुझे ही प्राप्त हो जायेगा। गीता में भक्त के योगक्षेम गया है।७७ जिस प्रकार जैन-दर्शन में फलाकांक्षा भी सम्यग्दर्शन का की जिम्मेदारी स्वयं श्रीकृष्ण ही वहन करते है१० जबकि जैन और अतिचार (दोष) मानी गई है उसी प्रकार गीता में भी फलाकांक्षा को दोष बौद्ध दर्शनों में ऐसे आश्वासनों का अभाव है। गीता में वैयक्तिक ईश्वर ता के अनुसार जो फलाकांक्षा से युक्त होकर श्रद्धा के प्रति जिस निष्ठा का उद्बोधन है वह सामान्यतया जैन और बौद्ध रखता है अथवा भक्ति करता है वह साधक निम्न श्रेणी का ही है। दर्शनों में ऐसे आश्वासनों का अभाव है। गीता में वैयक्तिक ईश्वर के फलाकांक्षायुक्त श्रद्धा व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से आगे नहीं प्रति जिस निष्ठा का उद्बोधन है वह सामान्यतया जैन और बौद्ध ले जाती है। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं जो लोग विवेक ज्ञान से रहित परम्पराओं में अनुपलब्ध ही है। होकर तथा भोगों की प्राप्ति विषयक कामनाओं से युक्त हो मुझ परमात्मा को छोड़ अन्यान्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, मैं उन लोगों की उपसंहार श्रद्धा उनमें स्थिर कर देता हूँ और उस श्रद्धा से युक्त होकर वे उन सम्यग्दर्शन अथवा श्रद्धा का जीवन में क्या मूल्य है, इस देवताओं की आराधना के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। पर भी विचार अपेक्षित है। यदि हम सम्यग्दर्शन को दृष्टिपरक अर्थ में लेकिन उन अल्पबुद्धि लोगों का वह फल नाशवान होते है। देवताओं का स्वीकार करते हैं, तो उसका हमारे जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन मुझ परमात्मा की सिद्ध होता है। सम्यग्दर्शन जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, वह भक्ति करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है।७८ अनासक्त जीवन जीने की कला का केन्द्रीय तत्त्व है। हमारे चरित्र या गीता में श्रद्धा या भक्ति अपने आधारों की दृष्टि से चार प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण इसी जीवन दृष्टि के आधार पर होता है। गीता की मानी गई है में इसी तथ्य को यह कहकर बताया है कि पुरुष जिसकी श्रद्धा जैसी 1. ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् होने वाली श्रद्धा या भक्ति। होती है वैसा ही वह बन जाता है। हम अपने को जैसा बनाना चाहते परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के पश्चात् उनके प्रति जो निष्ठा होती हैं, अपनी जीवन दृष्टि का निर्माण भी उसी के अनुरूप करें। क्योंकि है वह एक ज्ञानी की निष्ठा मानी गई है। व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसा ही उसका जीवन जीने का ढंग 2. जिज्ञासा की दृष्टि से परमात्मा पर श्रद्धा रखना। यह श्रद्धा होता है और जैसा उसका जीवन जीने का ढंग होता है वैसा ही उसका या भक्ति का दूसरा रूप है। इसमें यद्यपि श्रद्धा तो होती है लेकिन वह चरित्र बन जाता है। और जैसा उसका चरित्र होता है वैसा ही उसके पूर्णतया संशयरहित नहीं होती जबकि प्रथम स्थिति में होने वाली श्रद्धा व्यक्तित्व का उभार होता है। अत: एक यथार्थ दृष्टिकोण का निर्माण पूर्णतया संशयरहित होती है। संशयरहित श्रद्धा तो साक्षात्कार के पश्चात् जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। ही सम्भव है। जिज्ञासा की अवस्था में संशय बना ही रहता है अत: श्रद्धा का यह स्तर प्रथम की अपेक्षा निम्न ही माना गया है। संदर्भ 3. तीसरे स्तर की श्रद्धा आर्त व्यक्ति की होती है। कठिनाई में 1. दशवैकालिक, 4/11 फँसा हुआ व्यक्ति जब स्वयं अपने को उससे उबरने में असमर्थ पाता है और 2. इसिभासियाई सुत्तं, गहावइज्जं नामज्झयणं Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org