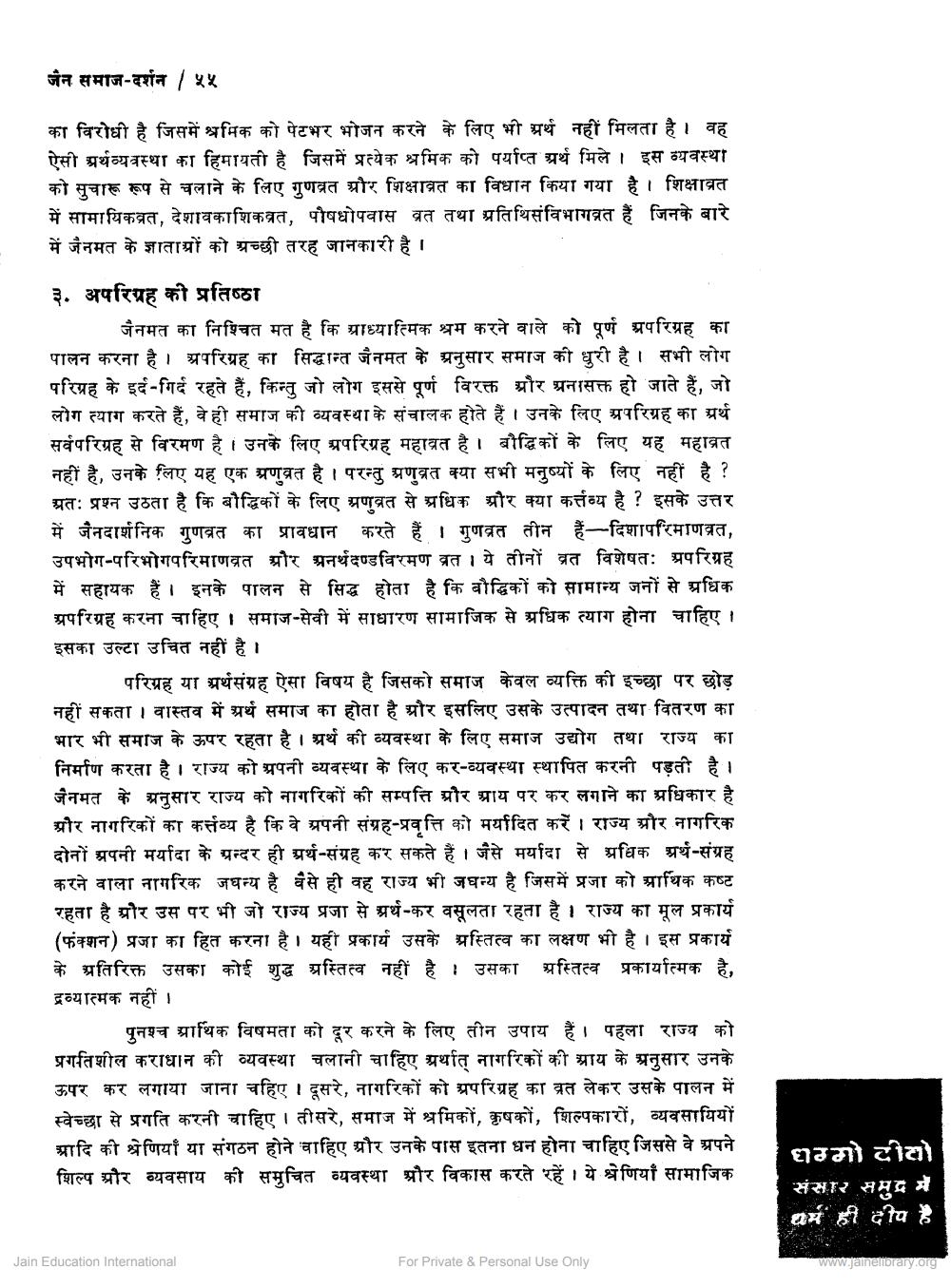________________
जैन समाज दर्शन / ५५
का विरोधी है जिसमें श्रमिक को पेटभर भोजन करने के लिए भी अर्थ नहीं मिलता है। वह ऐसी अर्थव्यवस्था का हिमायती है जिसमें प्रत्येक श्रमिक को पर्याप्त अर्थ मिले। इस व्यवस्था को 'सुचारू रूप से चलाने के लिए गुणव्रत और शिक्षाव्रत का विधान किया गया है। शिक्षाव्रत में सामायिकप्रत, देशावका शिकव्रत, पौषधोपवास व्रत तथा प्रतिथिसंविभायव्रत हैं जिनके बारे में जैनमत के ज्ञाताओं को अच्छी तरह जानकारी है ।
३. अपरिग्रह की प्रतिष्ठा
जैनमत का निश्चित मत है कि प्राध्यात्मिक श्रम करने वाले को पूर्ण अपरिग्रह का पालन करना है। अपरिग्रह का सिद्धान्त जैनमत के अनुसार समाज की धुरी है। सभी लोग परिग्रह के इर्द-गिर्द रहते हैं, किन्तु जो लोग इससे पूर्ण विरक्त और अनासक्त हो जाते हैं, जो लोग श्याग करते हैं, वे ही समाज की व्यवस्था के संचालक होते हैं। उनके लिए अपरिग्रह का पर्व सर्वपरिग्रह से विरमण है । उनके लिए अपरिग्रह महाव्रत है। बौद्धिकों के लिए यह महाव्रत
सभी मनुष्यों के लिए नहीं है ?
नहीं है, उनके लिए यह एक घणुव्रत है परन्तु प्रणुव्रत क्या अतः प्रश्न उठता है कि बौद्धिकों के लिए अणुव्रत से अधिक और क्या कर्तव्य है ? इसके उत्तर में जैनदार्शनिक गुणव्रत का प्रावधान करते हैं गुणव्रत तीन हैं दिशापरिमाणव्रत, उपभोग- परिभोगपरिमाणव्रत और अनर्थदण्डविरमण व्रत ये तीनों व्रत विशेषतः अपरिग्रह में सहायक हैं। इनके पालन से सिद्ध होता है कि बौद्धिकों को सामान्य जनों से अधिक अपरिग्रह करना चाहिए। समाज सेवी में साधारण सामाजिक से अधिक त्याग होना चाहिए । इसका उल्टा उचित नहीं है।
परिग्रह या अर्थसंग्रह ऐसा विषय है जिसको समाज केवल व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ नहीं सकता । वास्तव में अर्थ समाज का होता है और इसलिए उसके उत्पादन तथा वितरण का भार भी समाज के ऊपर रहता है। अर्थ की व्यवस्था के लिए समाज उद्योग तथा राज्य का निर्माण करता है । राज्य को अपनी व्यवस्था के लिए कर व्यवस्था स्थापित करनी पड़ती है । जैनमत के अनुसार राज्य को नागरिकों की सम्पत्ति और प्राय पर कर लगाने का अधिकार है और नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपनी संग्रह प्रवृत्ति को मर्यादित करें राज्य और नागरिक दोनों अपनी मर्यादा के अन्दर ही अर्थ संग्रह कर सकते हैं। जैसे मर्यादा से अधिक अर्थ-संग्रह करने वाला नागरिक जघन्य है वैसे ही वह राज्य भी जघन्य है जिसमें प्रजा को आर्थिक कष्ट रहता है और उस पर भी जो राज्य प्रजा से अर्थ कर वसूलता रहता है। राज्य का मूल प्रकार्य प्रस्तित्व का लक्षण भी है। इस प्रकार्य
( फंक्शन) प्रजा का हित करना है। यही प्रकार्य उसके के अतिरिक्त उसका कोई शुद्ध अस्तित्व नहीं है द्रव्यात्मक नहीं ।
। उसका अस्तित्व प्रकार्यात्मक है,
पुनश्च प्रार्थिक विषमता को दूर करने के लिए तीन उपाय हैं। पहला राज्य को प्रगतिशील कराधान की व्यवस्था चलानी चाहिए अर्थात् नागरिकों की प्राय के अनुसार उनके ऊपर कर लगाया जाना चहिए। दूसरे, नागरिकों को अपरिग्रह का व्रत लेकर उसके पालन में स्वेच्छा से प्रगति करनी चाहिए। तीसरे, समाज में श्रमिकों, कृषकों, शिल्पकारों, व्यवसायियों आदि की श्रेणियाँ या संगठन होने चाहिए और उनके पास इतना धन होना चाहिए जिससे वे अपने शिल्प मौर व्यवसाय की समुचित व्यवस्था और विकास करते रहें। ये श्रेणियाँ सामाजिक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
धम्मो दीयो संसार समुद्र में धर्म ही दीप है
www.jainelibrary.org