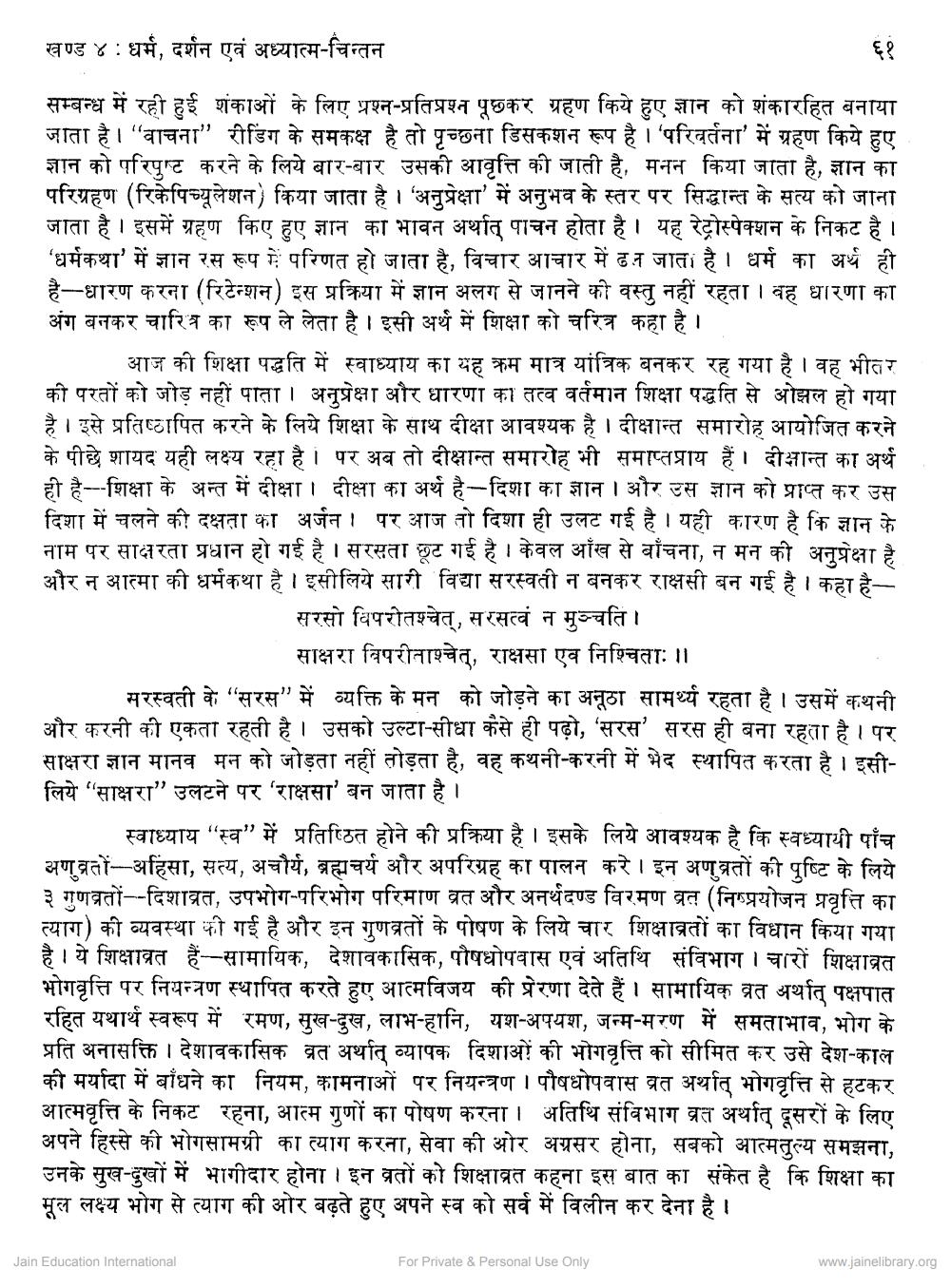________________
खण्ड ४ : धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म-चिन्तन
६१
सम्बन्ध में रही हुई शंकाओं के लिए प्रश्न - प्रतिप्रश्न पूछकर ग्रहण किये हुए ज्ञान को शंकारहित बनाया जाता है । "वाचना" रीडिंग के समकक्ष है तो पृच्छना डिसकशन रूप है । 'परिवर्तना' में ग्रहण किये हुए ज्ञान को परिपुष्ट करने के लिये बार-बार उसकी आवृत्ति की जाती है, मनन किया जाता है, ज्ञान का परिग्रहण ( रिकेपिच्यूलेशन) किया जाता है । 'अनुप्रेक्षा' में अनुभव के स्तर पर सिद्धान्त के सत्य को जाना जाता है । इसमें ग्रहण किए हुए ज्ञान का भावन अर्थात् पाचन होता है । यह रेट्रोस्पेक्शन के निकट है । 'धर्मकथा' में ज्ञान रस रूप में परिणत हो जाता है, विचार आचार में ढल जाता है । धर्म का अर्थ ही है- धारण करना ( रिटेन्शन) इस प्रक्रिया में ज्ञान अलग से जानने की वस्तु नहीं रहता । वह धारणा का अंग बनकर चारित्र का रूप ले लेता है । इसी अर्थ में शिक्षा को चरित्र कहा है ।
आज की शिक्षा पद्धति में स्वाध्याय का यह क्रम मात्र यांत्रिक बनकर रह गया है । वह भीतर की परतों को जोड़ नहीं पाता । अनुप्रेक्षा और धारणा का तत्व वर्तमान शिक्षा पद्धति से ओझल हो गया है । इसे प्रतिष्ठापित करने के लिये शिक्षा के साथ दीक्षा आवश्यक है । दीक्षान्त समारोह आयोजित करने के पीछे शायद यही लक्ष्य रहा है । पर अब तो दीक्षान्त समारोह भी समाप्तप्राय हैं। दीक्षान्त का अर्थ ही है - शिक्षा के अन्त में दीक्षा । दीक्षा का अर्थ है - दिशा का ज्ञान । और उस ज्ञान को प्राप्त कर उस दिशा में चलने की दक्षता का अर्जन । पर आज तो दिशा ही उलट गई है । यही कारण है कि ज्ञान के नाम पर साक्षरता प्रधान हो गई है । सरसता छूट गई है। केवल आँख से बाँचना, न मन की अनुप्रेक्षा है और न आत्मा की धर्मकथा है । इसीलिये सारी विद्या सरस्वती न बनकर राक्षसी बन गई है । कहा हैसरसो विपरीतश्चेत्, सरसत्वं न मुञ्चति ।
साक्षरा विपरीताश्चेत्, राक्षसा एव निश्चिताः ॥
मरस्वती के "सरस" में व्यक्ति के मन को जोड़ने का अनूठा सामर्थ्य रहता है । उसमें कथनी और करनी की एकता रहती है । उसको उल्टा सीधा कैसे ही पढ़ो, 'सरस' सरस ही बना रहता है । पर साक्षरा ज्ञान मानव मन को जोड़ता नहीं तोड़ता है, वह कथनी-करनी में भेद स्थापित करता है । इसीलिये " साक्षरा" उलटने पर 'राक्षसा' बन जाता है ।
स्वाध्याय "स्व" में प्रतिष्ठित होने की प्रक्रिया है । इसके लिये आवश्यक है कि स्वध्यायी पाँच अणुव्रतों-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करे । इन अणुव्रतों की पुष्टि के लिये ३ गुणव्रतों -- दिशाव्रत, उपभोग- परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थदण्ड विरमण व्रत (निष्प्रयोजन प्रवृत्ति का त्याग) की व्यवस्था की गई है और इन गुणव्रतों के पोषण के लिये चार शिक्षाव्रतों का विधान किया गया है । ये शिक्षाव्रत हैं- सामायिक, देशावकासिक, पौषधोपवास एवं अतिथि संविभाग । चारों शिक्षाव्रत भोगवृत्ति पर नियन्त्रण स्थापित करते हुए आत्मविजय की प्रेरणा देते हैं । सामायिक व्रत अर्थात् पक्षपात रहित यथार्थ स्वरूप में रमण, सुख-दुख, लाभ-हानि, यश-अपयश, जन्म-मरण में समताभाव, भोग के प्रति अनासक्ति । देशावकासिक व्रत अर्थात् व्यापक दिशाओं की भोगवृत्ति को सीमित कर उसे देश-काल की मर्यादा में बाँधने का नियम, कामनाओं पर नियन्त्रण । पौषधोपवास व्रत अर्थात् भोगवृत्ति से हटकर आत्मवृत्ति के निकट रहना, आत्म गुणों का पोषण करना । अतिथि संविभाग व्रत अर्थात् दूसरों के लिए अपने हिस्से की भोगसामग्री का त्याग करना, सेवा की ओर अग्रसर होना, सबको आत्मतुल्य समझना, उनके सुख-दुखों में भागीदार होना । इन व्रतों को शिक्षाव्रत कहना इस बात का संकेत है कि शिक्षा का मूल लक्ष्य भोग से त्याग की ओर बढ़ते हुए अपने स्व को सर्व में विलीन कर देना है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org