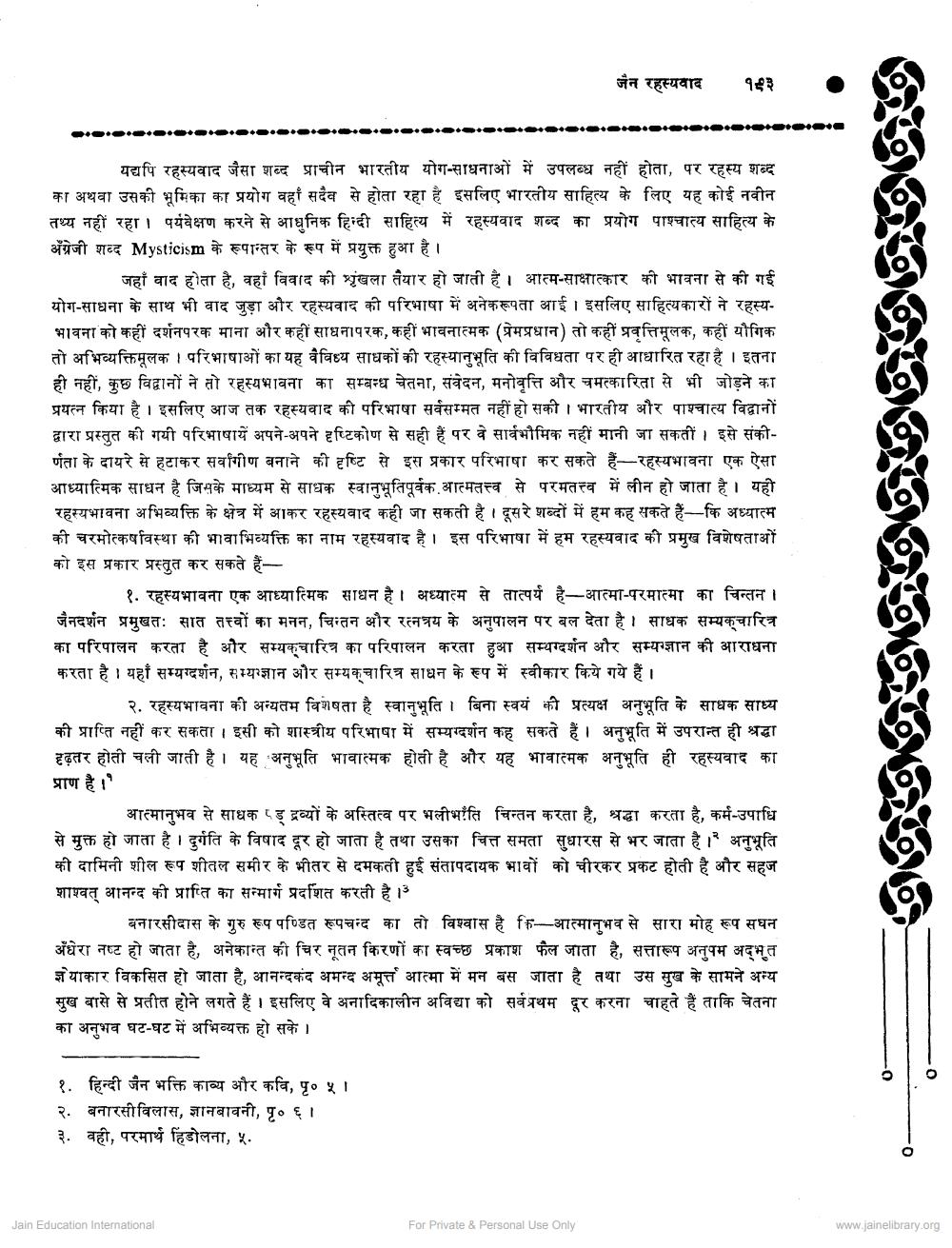________________
यद्यपि रहस्यवाद जैसा शब्द प्राचीन भारतीय योग-साधनाओं में उपलब्ध नहीं होता, पर रहस्य शब्द का अथवा उसकी भूमिका का प्रयोग वहाँ सदैव से होता रहा है इसलिए भारतीय साहित्य के लिए यह कोई नवीन तथ्य नहीं रहा । पर्यवेक्षण करने से आधुनिक हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद शब्द का प्रयोग पाश्चात्य साहित्य के अँग्रेजी शब्द Mysticism के रूपान्तर के रूप में प्रयुक्त हुआ है ।
जैन रहस्यवाद
जहाँ वाद होता है, वहाँ विवाद की श्रृंखला तैयार हो जाती है। आत्म-साक्षात्कार की भावना से की गई योग-साधना के साथ भी वाद जुड़ा और रहस्यवाद की परिभाषा में अनेकरूपता आई । इसलिए साहित्यकारों ने रहस्यभावना को कहीं दर्शनपरक माना और कहीं साधनापरक कहीं भावनात्मक (प्रेमप्रधान) तो कहीं प्रवृत्तिमूलक, कहीं यौगिक तो अभिव्यक्तिमूलक । परिभाषाओं का यह वैविध्य साधकों की रहस्यानुभूति की विविधता पर ही आधारित रहा है । इतना ही नहीं, कुछ विद्वानों ने तो रहस्यभावना का सम्बन्ध चेतना, संवेदन, मनोवृत्ति और चमत्कारिता से भी जोड़ने का प्रयत्न किया है। इसलिए आज तक रहस्यवाद की परिभाषा सर्वसम्मत नहीं हो सकी । भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गयी परिभाषायें अपने-अपने दृष्टिकोण से सही हैं पर वे सार्वभौमिक नहीं मानी जा सकतीं। इसे कीपता के दायरे से हटाकर सर्वांगीण बनाने की दृष्टि से इस प्रकार परिभाषा कर सकते हैं-रहस्यभावना एक ऐसा आध्यात्मिक साधन है जिसके माध्यम से साधक स्वानुभूतिपूर्वक आत्मतत्त्व से परमतत्त्व में लीन हो जाता है । यही रहस्यभावना अभिव्यक्ति के क्षेत्र में आकर रहस्यवाद कही जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अध्यात्म की चरमोत्कर्षाfवस्था की भावाभिव्यक्ति का नाम रहस्यवाद है । इस परिभाषा में हम रहस्यवाद की प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं
१६३
१. रहस्यभावना एक आध्यात्मिक साधन है । अध्यात्म से तात्पर्य है— आत्मा-परमात्मा का चिन्तन | जैनदर्शन प्रमुखतः सात सस्यों का मनन, चिन्तन और रत्नत्रय के अनुपासन पर बल देता है। साधक सम्यकुचारित्र का परिपालन करता है और सम्यक्चारित्र का परिपालन करता हुआ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की आराधना करता है। यहाँ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकृपारित साधन के रूप में स्वीकार किये गये हैं।
२. रहस्यभावना की अन्यतम विशेषता है स्वानुभूति । बिना स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति के साधक साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी को शास्त्रीय परिभाषा में सम्यग्दर्शन कह सकते हैं। अनुभूति में उपरान्त ही श्रद्धा हतर होती चली जाती है। यह अनुभूति भावात्मक होती है और यह भावात्मक अनुभूति ही रहस्यवाद का प्राण है ।'
आत्मानुभव से साधक ५ड् द्रव्यों के अस्तित्व पर भलीभाँति चिन्तन करता है, श्रद्धा करता है, कर्म-उपाधि से मुक्त हो जाता है। दुर्गति के विषाद दूर हो जाता है तथा उसका पित्त समता सुधारस से भर जाता है।" अनुभूति की वामिनीशील रूपी समीर के भीतर से दमकती हुई संतापदायक भावों को चीरकर प्रकट होती है और सहज शाश्वत् आनन्द की प्राप्ति का सन्मार्ग प्रदर्शित करती है । 3
१. हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि, पृ० ५ ।
२. बनारसीविलास, ज्ञानबावनी, पृ० ६ ।
३. वही, परमार्थ हिंडोलना, ५.
बनारसीदास के गुरु रूप पण्डित रूपचन्द का तो विश्वास है कि आत्मानुभव से सारा मोह रूप सघन अँधेरा नष्ट हो जाता है, अनेकान्त की चिर नूतन किरणों का स्वच्छ प्रकाश फैल जाता है, सत्तारूप अनुपम अद्भुत ज्ञेयाकार विकसित हो जाता है, आनन्दकंद अमन्द अमूर्त आत्मा में मन बस जाता है तथा उस सुख के सामने अन्य सुख बासे से प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए वे अनादिकालीन अविद्या को सर्वप्रथम दूर करना चाहते हैं ताकि चेतना का अनुभव घट-घट में अभिव्यक्त हो सके ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
-0
·0
0
www.jainelibrary.org.