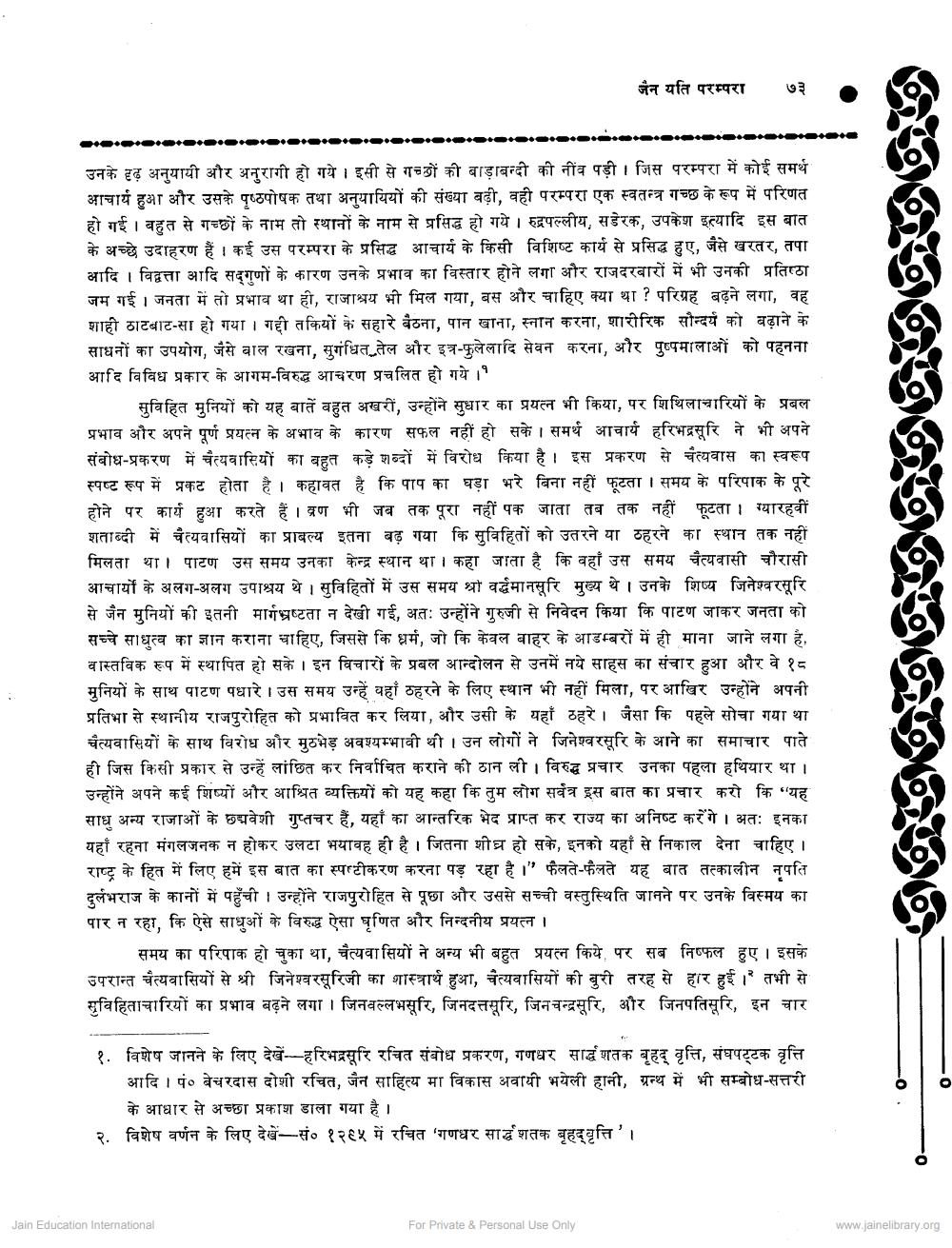________________
उनके दृढ़ अनुयायी और अनुरागी हो गये। इसी से गच्छों की बाड़ाबन्दी की नींव पड़ी। जिस परम्परा में कोई समर्थ आचार्य हुआ और उसके पृष्ठपोषक तथा अनुपायियों की संख्या बढ़ी, वही परम्परा एक स्वतन्त्र गच्छ के रूप में परिणत हो गई। बहुत से गच्छों के नाम तो स्थानों के नाम से प्रसिद्ध हो गये। रुद्रपल्लीय, सडेरक, उपकेश इत्यादि इस बात के अच्छे उदाहरण हैं। कई उस परम्परा के प्रसिद्ध आचार्य के किसी विशिष्ट कार्य से प्रसिद्ध हुए, जैसे खरतर, तपा आदि विद्वत्ता आदि सद्गुणों के कारण उनके प्रभाव का विस्तार होने लगा और राजदरबारों में भी उनकी प्रतिष्ठा जम गई । जनता में तो प्रभाव था ही, राजाश्रय भी मिल गया, बस और चाहिए क्या था ? परिग्रह बढ़ने लगा, वह शाही ठाटबाट सा हो गया । गद्दी तकियों के सहारे बैठना, पान खाना, स्नान करना, शारीरिक सौन्दर्य को बढ़ाने के साधनों का उपयोग जैसे बाल रखना, सुगंधित तेल और इत्र-लेवादि सेवन करना और पुष्पमालाओं को पहनना
1
आदि विविध प्रकार के आगम-विरुद्ध आचरण प्रचलित हो गये । १
जैन यति परम्परा
है
सुविहित मुनियों को यह बातें बहुत अखरीं, उन्होंने सुधार का प्रयत्न भी किया, पर शिथिलाचारियों के प्रबल प्रभाव और अपने पूर्ण प्रयत्न के अभाव के कारण सफल नहीं हो सके । समर्थ आचार्य हरिभद्रसूरि ने भी अपने संबोध - प्रकरण में चैत्यवासियों का बहुत कड़े शब्दों में विरोध किया है। इस प्रकरण से चैत्यवास का स्वरूप स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। कहावत कि पाप का घड़ा भरे बिना नहीं फूटता । समय के परिपाक के पूरे होने पर कार्य हुआ करते हैं । व्रण भी जब तक पूरा नहीं पक जाता तब तक नहीं फूटता । ग्यारहवीं शताब्दी में चैत्यवासियों का प्राबल्य इतना बढ़ गया कि सुविहितों को उतरने या ठहरने का स्थान तक नहीं मिलता था। पाटण उस समय उनका केन्द्र स्थान था । कहा जाता है कि वहाँ उस समय चैत्यवासी चौरासी आचार्यों के अलग-अलग उपाश्रय थे। सुविहितों में उस समय श्री वर्द्धमानसूरि मुख्य थे । उनके शिष्य जिनेश्वरसूरि से जैन मुनियों की इतनी मार्गभ्रष्टता न देखी गई, अतः उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि पाटण जाकर जनता को सच्चे साधुत्व का ज्ञान कराना चाहिए, जिससे कि धर्म, जो कि केवल बाहर के आडम्बरों में ही माना जाने लगा है, वास्तविक रूप में स्थापित हो सके। इन विचारों के प्रबल आन्दोलन से उनमें नये साहस का संचार हुआ और वे १८ मुनियों के साथ पाटण पधारे। उस समय उन्हें वहाँ ठहरने के लिए स्वान भी नहीं मिला पर आखिर उन्होंने अपनी प्रतिभा से स्थानीय राजपुरोहित को प्रभावित कर लिया, और उसी के यहाँ ठहरे। जैसा कि पहले सोचा गया था चैत्यवासियों के साथ विरोध और मुठभेड़ अवश्यम्भावी थी। उन लोगों ने जिनेश्वरसूरि के आने का समाचार पाते ही जिस किसी प्रकार से उन्हें लांछित कर निर्वाचित कराने की ठान ली । विरुद्ध प्रचार उनका पहला हथियार था । उन्होंने अपने कई शिष्यों और आश्रित व्यक्तियों को यह कहा कि तुम लोग सर्वत्र इस बात का प्रचार करो कि "यह साधु अन्य राजाओं के छद्मवेशी गुप्तचर हैं, यहाँ का आन्तरिक भेद प्राप्त कर राज्य का अनिष्ट करेंगे । अतः इनका यहाँ रहना मंगलजनक न होकर उलटा भयावह ही है । जितना शीघ्र हो सके, इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए । राष्ट्र के हित में लिए हमें इस बात का स्पष्टीकरण करना पड़ रहा है ।" फैलते फैलते यह बात तत्कालीन नृपति दुर्लभराज के कानों में पहुँची । उन्होंने राजपुरोहित से पूछा और उससे सच्ची वस्तुस्थिति जानने पर उनके विस्मय का पार न रहा, कि ऐसे साधुओं के विरुद्ध ऐसा घृणित और निन्दनीय प्रयत्न ।
७३
समय का परिपाक हो चुका था, चैत्यवासियों ने अन्य भी बहुत प्रयत्न किये पर सब निष्फल हुए । इसके उपरान्त चत्यवासियों से श्री जिनेश्वरसूरिजी का शास्त्रार्य हुआ, चैत्यवासियों की बुरी तरह से हार हुई। तभी से सुविहिताचारियों का प्रभाव बढ़ने लगा । जिनवल्लभसूरि, जिनदत्तसूरि, जिनचन्द्रसूरि और जिनपतिसूरि, इन चार
के आधार से अच्छा प्रकाश डाला गया है ।
3
२. विशेष वर्णन के लिए देखें- ० १२६५ में रचित 'गणधर सार्द्धशतक बृहद्वृत्ति' ।
१. विशेष जानने के लिए देखें- हरिभद्रसूरि रचित संबोध प्रकरण, गणधर सार्द्धशतक वृहद्वृत्ति, संघट्टक वृत्ति आदि पं० बेचरदास दोशी रचित, जैन साहित्य मा विकास अवायी भवेली हानी ग्रन्थ में भी सम्बोध-सत्तरी
|
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
-
www.jainelibrary.org.