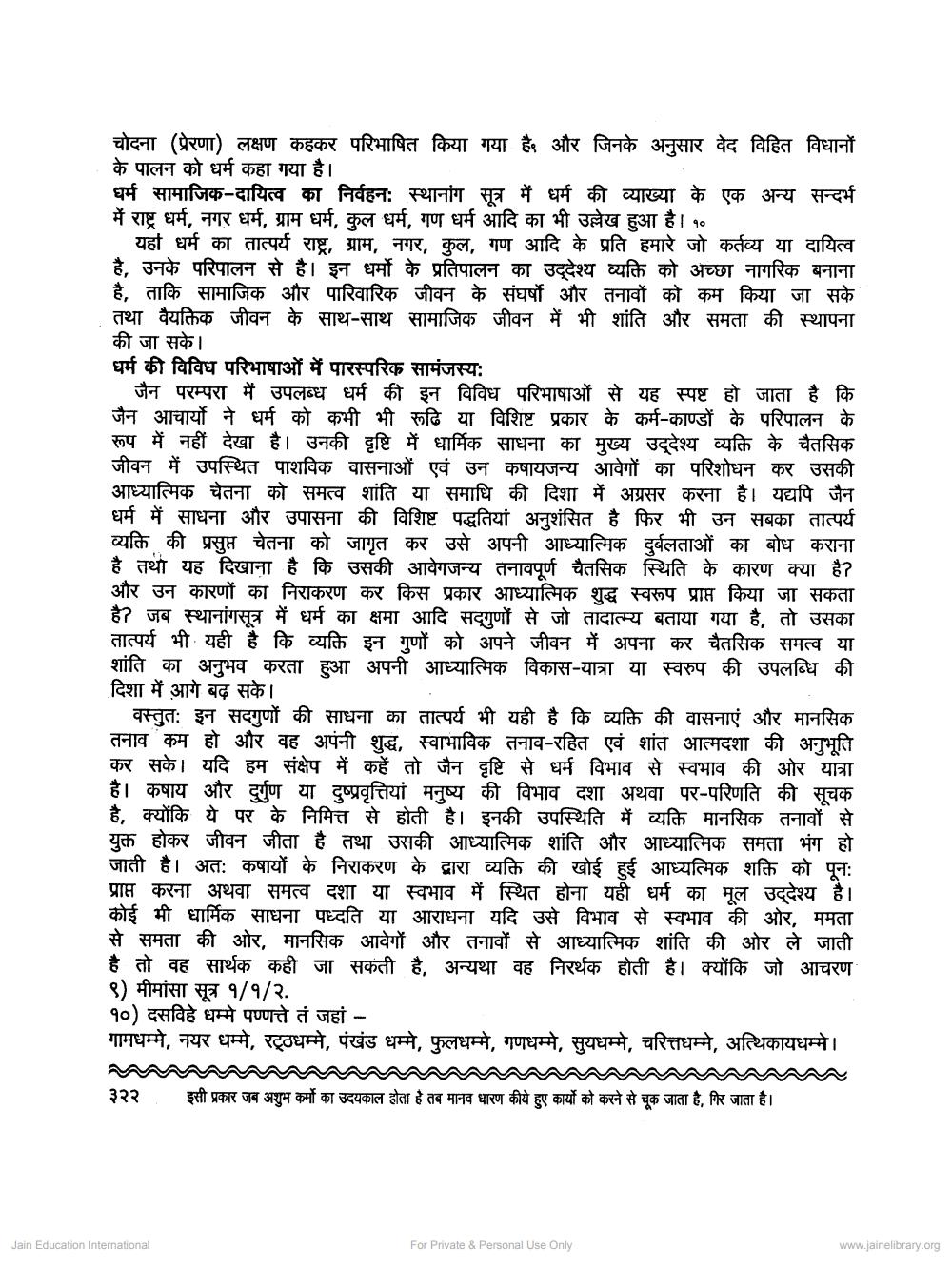________________
चोदना (प्रेरणा) लक्षण कहकर परिभाषित किया गया है और जिनके अनुसार वेद विहित विधानों के पालन को धर्म कहा गया है। धर्म सामाजिक-दायित्व का निर्वहन: स्थानांग सूत्र में धर्म की व्याख्या के एक अन्य सन्दर्भ में राष्ट्र धर्म, नगर धर्म, ग्राम धर्म, कुल धर्म, गण धर्म आदि का भी उल्लेख हुआ है। १०
यहाँ धर्म का तात्पर्य राष्ट्र, ग्राम, नगर, कुल, गण आदि के प्रति हमारे जो कर्तव्य या दायित्व है, उनके परिपालन से है। इन धर्मों के प्रतिपालन का उद्देश्य व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना है, ताकि सामाजिक और पारिवारिक जीवन के संघर्षों और तनावों को कम किया जा सके तथा वैयक्तिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी शांति और समता की स्थापना की जा सके। धर्म की विविध परिभाषाओं में पारस्परिक सामंजस्य:
जैन परम्परा में उपलब्ध धर्म की इन विविध परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन आचार्यों ने धर्म को कभी भी रूढि या विशिष्ट प्रकार के कर्म-काण्डों के परिपालन के रूप में नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में धार्मिक साधना का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के चैतसिक जीवन में उपस्थित पाशविक वासनाओं एवं उन कषायजन्य आवेगों का परिशोधन कर उसकी आध्यात्मिक चेतना को समत्व शांति या समाधि की दिशा में अग्रसर करना है। यद्यपि जैन धर्म में साधना और उपासना की विशिष्ट पद्धतियां अनुशंसित है फिर भी उन सबका तात्पर्य व्यक्ति की प्रसुप्त चेतना को जागृत कर उसे अपनी आध्यात्मिक दुर्बलताओं का बोध कराना है तथा यह दिखाना है कि उसकी आवेगजन्य तनावपूर्ण चैतसिक स्थिति के कारण क्या है?
और उन कारणों का निराकरण कर किस प्रकार आध्यात्मिक शुद्ध स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है? जब स्थानांगसूत्र में धर्म का क्षमा आदि सद्गुणों से जो तादात्म्य बताया गया है, तो उसका तात्पर्य भी यही है कि व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपना कर चैतसिक समत्व या शांति का अनुभव करता हुआ अपनी आध्यात्मिक विकास-यात्रा या स्वरुप की उपलब्धि की दिशा में आगे बढ़ सके। । वस्तुत: इन सदगुणों की साधना का तात्पर्य भी यही है कि व्यक्ति की वासनाएं और मानसिक तनाव कम हो और वह अपनी शुद्ध, स्वाभाविक तनाव-रहित एवं शांत आत्मदशा की अनुभूति कर सके। यदि हम संक्षेप में कहें तो जैन दृष्टि से धर्म विभाव से स्वभाव की ओर यात्रा है। कषाय और दुर्गुण या दुष्प्रवृत्तियां मनुष्य की विभाव दशा अथवा पर-परिणति की सूचक है, क्योंकि ये पर के निमित्त से होती है। इनकी उपस्थिति में व्यक्ति मानसिक तनावों से युक्त होकर जीवन जीता है तथा उसकी आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक समता भंग हो जाती है। अत: कषायों के निराकरण के द्वारा व्यक्ति की खोई हुई आध्यत्मिक शक्ति को पून: प्राप्त करना अथवा समत्व दशा या स्वभाव में स्थित होना यही धर्म का मूल उद्देश्य है। कोई भी धार्मिक साधना पध्दति या आराधना यदि उसे विभाव से स्वभाव की ओर, ममता से समता की ओर, मानसिक आवेगों और तनावों से आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाती है तो वह सार्थक कही जा सकती है, अन्यथा वह निरर्थक होती है। क्योंकि जो आचरण ९) मीमांसा सूत्र १/१/२. १०) दसविहे धम्मे पण्णत्ते तं जहांगामधम्मे, नयर धम्मे, रठ्ठधम्मे, पंखंड धम्मे, फुलधम्मे, गणधम्मे, सुयधम्मे, चरित्तधम्मे, अत्थिकायधम्मे।
३२२
इसी प्रकार जब अशुभ कर्मो का उदयकाल होता है तब मानव धारण कीये हुए कार्यो को करने से चूक जाता है, गिर जाता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org