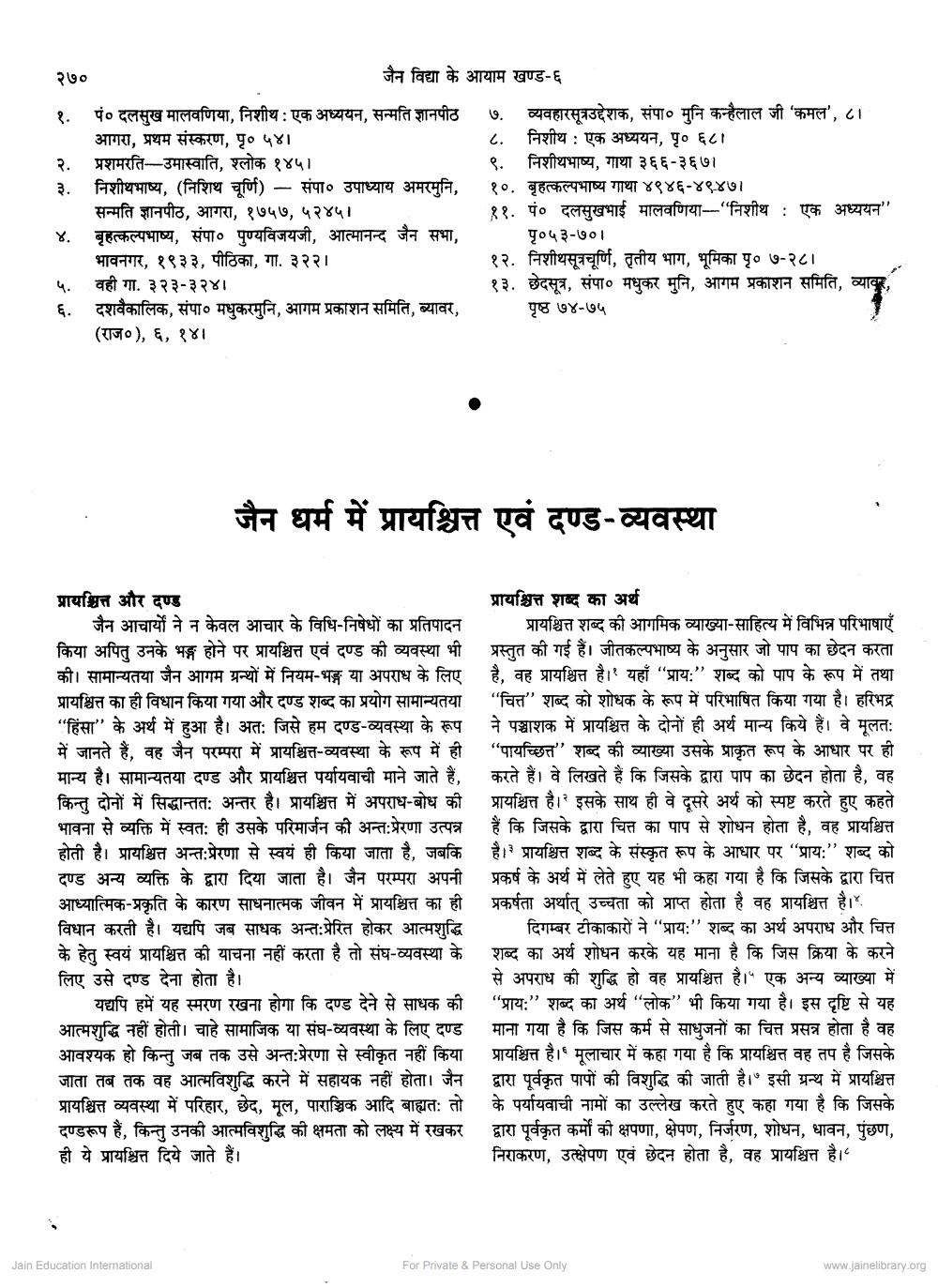________________ 270 जैन विद्या के आयाम खण्ड-६ 1. पं० दलसुख मालवणिया, निशीथ : एक अध्ययन, सन्मति ज्ञानपीठ आगरा, प्रथम संस्करण, पृ० 54 / प्रशमरति-उमास्वाति, श्लोक 145 / / 3. निशीथभाष्य, (निशिथ चूर्णि) - संपा० उपाध्याय अमरमुनि, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, 1757, 5245 / बृहत्कल्पभाष्य, संपा० पुण्यविजयजी, आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर, 1933, पीठिका, गा. 322 / वही गा. 323-324 / 6. दशवकालिक, संपा० मधुकरमुनि, आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर, (राज.), 6, 14 / 7. व्यवहारसूत्रउद्देशक, संपा० मुनि कन्हैलाल जी 'कमल',८ 8. निशीथ : एक अध्ययन, पृ० 68 / 9. निशीथभाष्य, गाथा 366-367 / 10. बृहत्कल्पभाष्य गाथा 4946-4947 / 11. पं० दलसुखभाई मालवणिया-"निशीथ : एक अध्ययन" पृ०५३-७०। 12. निशीथसूत्रचूर्णि, तृतीय भाग, भूमिका पृ० 7-28 / 13. छेदसूत्र, संपा० मधुकर मुनि, आगम प्रकाशन समिति, व्याव पृष्ठ 74-75 जैन धर्म में प्रायश्चित्त एवं दण्ड-व्यवस्था प्रायश्चित्त और दण्ड प्रायश्चित्त शब्द का अर्थ जैन आचार्यों ने न केवल आचार के विधि-निषेधों का प्रतिपादन प्रायश्चित्त शब्द की आगमिक व्याख्या-साहित्य में विभिन्न परिभाषाएँ किया अपितु उनके भङ्ग होने पर प्रायश्चित्त एवं दण्ड की व्यवस्था भी प्रस्तुत की गई हैं। जीतकल्पभाष्य के अनुसार जो पाप का छेदन करता की। सामान्यतया जैन आगम ग्रन्थों में नियम-भङ्ग या अपराध के लिए है, वह प्रायश्चित्त है। यहाँ “प्रायः" शब्द को पाप के रूप में तथा प्रायश्चित्त का ही विधान किया गया और दण्ड शब्द का प्रयोग सामान्यतया “चित्त' शब्द को शोधक के रूप में परिभाषित किया गया है। हरिभद्र "हिंसा' के अर्थ में हुआ है। अत: जिसे हम दण्ड-व्यवस्था के रूप ने पञ्चाशक में प्रायश्चित्त के दोनों ही अर्थ मान्य किये हैं। वे मूलतः में जानते हैं, वह जैन परम्परा में प्रायश्चित्त-व्यवस्था के रूप में ही “पायच्छित्त" शब्द की व्याख्या उसके प्राकृत रूप के आधार पर ही मान्य है। सामान्यतया दण्ड और प्रायश्चित्त पर्यायवाची माने जाते हैं, करते हैं। वे लिखते हैं कि जिसके द्वारा पाप का छेदन होता है, वह किन्तु दोनों में सिद्धान्तत: अन्तर है। प्रायश्चित्त में अपराध-बोध की प्रायश्चित्त है। इसके साथ ही वे दूसरे अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते भावना से व्यक्ति में स्वतः ही उसके परिमार्जन की अन्त:प्रेरणा उत्पन्न हैं कि जिसके द्वारा चित्त का पाप से शोधन होता है, वह प्रायश्चित्त होती है। प्रायश्चित्त अन्त:प्रेरणा से स्वयं ही किया जाता है, जबकि है। प्रायश्चित्त शब्द के संस्कृत रूप के आधार पर “प्रायः" शब्द को दण्ड अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। जैन परम्परा अपनी प्रकर्ष के अर्थ में लेते हुए यह भी कहा गया है कि जिसके द्वारा चित्त आध्यात्मिक-प्रकृति के कारण साधनात्मक जीवन में प्रायश्चित्त का ही प्रकर्षता अर्थात् उच्चता को प्राप्त होता है वह प्रायश्चित्त है। विधान करती है। यद्यपि जब साधक अन्त:प्रेरित होकर आत्मशुद्धि दिगम्बर टीकाकारों ने "प्राय:' शब्द का अर्थ अपराध और चित्त के हेतु स्वयं प्रायश्चित्त की याचना नहीं करता है तो संघ-व्यवस्था के शब्द का अर्थ शोधन करके यह माना है कि जिस क्रिया के करने लिए उसे दण्ड देना होता है। से अपराध की शुद्धि हो वह प्रायश्चित्त है। एक अन्य व्याख्या में यद्यपि हमें यह स्मरण रखना होगा कि दण्ड देने से साधक की "प्रायः" शब्द का अर्थ "लोक" भी किया गया है। इस दृष्टि से यह आत्मशुद्धि नहीं होती। चाहे सामाजिक या संघ-व्यवस्था के लिए दण्ड माना गया है कि जिस कर्म से साधुजनों का चित्त प्रसन्न होता है वह आवश्यक हो किन्तु जब तक उसे अन्त:प्रेरणा से स्वीकृत नहीं किया प्रायश्चित्त है। मूलाचार में कहा गया है कि प्रायश्चित्त वह तप है जिसके जाता तब तक वह आत्मविशुद्धि करने में सहायक नहीं होता। जैन द्वारा पूर्वकृत पापों की विशुद्धि की जाती है। इसी ग्रन्थ में प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त व्यवस्था में परिहार, छेद, मूल, पाराञ्चिक आदि बाह्यत: तो के पर्यायवाची नामों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जिसके दण्डरूप हैं, किन्तु उनकी आत्मविशुद्धि की क्षमता को लक्ष्य में रखकर द्वारा पूर्वकृत कर्मों की क्षपणा, क्षेपण, निर्जरण, शोधन, धावन, पुंछण, ही ये प्रायश्चित्त दिये जाते हैं। निराकरण, उत्क्षेपण एवं छेदन होता है, वह प्रायश्चित्त है। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org