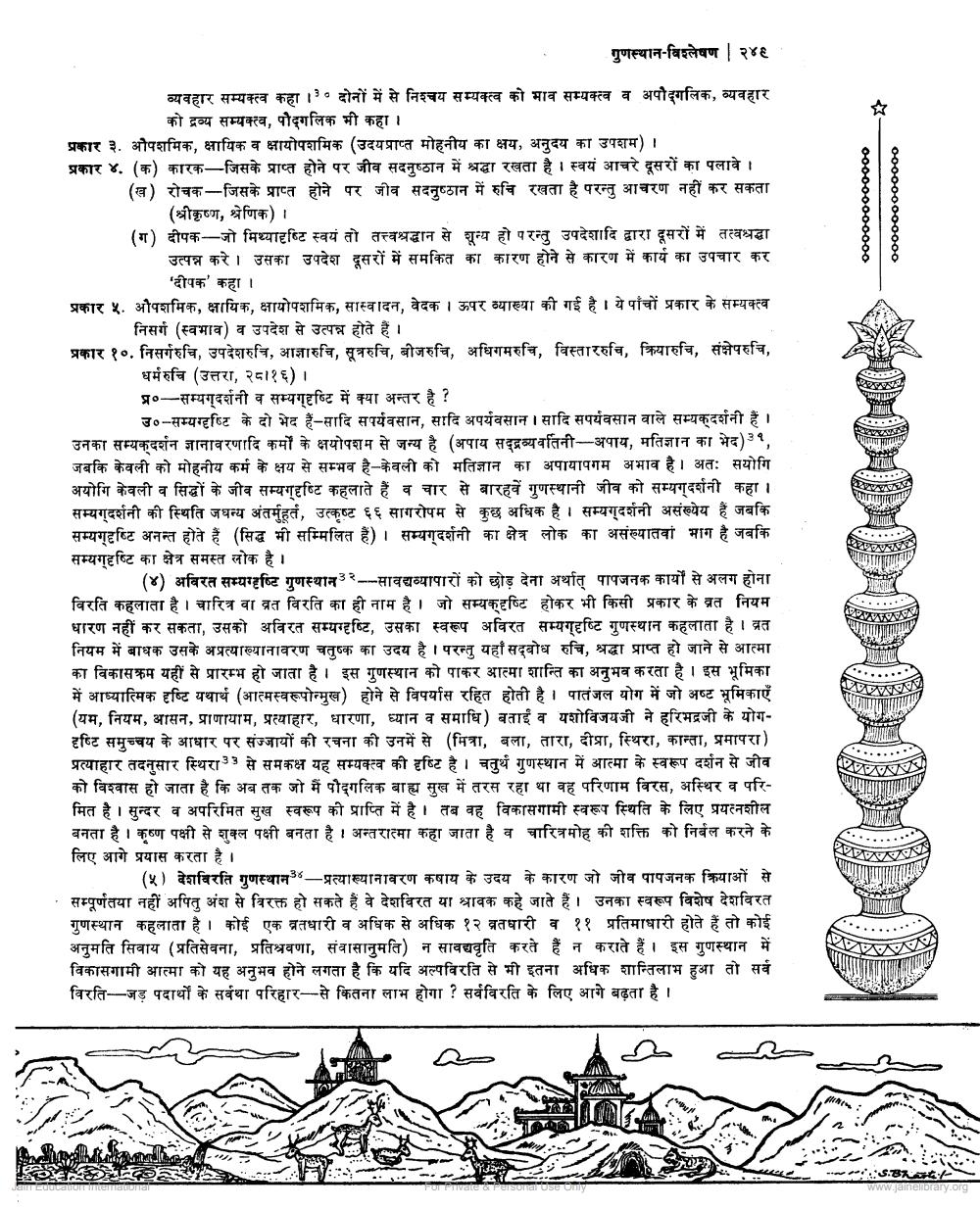________________
गुणस्थान-विश्लेषण | २४९
व्यवहार सम्यक्त्व कहा।
दोनों में से निश्चय सम्यक्त्व को भाव सम्यक्त्व व अपौद्गलिक, व्यवहार को द्रव्य सम्यक्त्व, पौद्गलिक भी कहा ।
प्रकार ३. औपशमिक, क्षायिक व क्षायोपशमिक ( उदयप्राप्त मोहनीय का क्षय, अनुदय का उपशम ) |
प्रकार ४. ( क ) कारक – जिसके प्राप्त होने पर जीव सदनुष्ठान में श्रद्धा रखता है । स्वयं आचरे दूसरों का पलावे ।
(ख) रोचक - जिसके प्राप्त होने पर जीव सदनुष्ठान में रुचि रखता है परन्तु आचरण नहीं कर सकता ( श्रीकृष्ण, श्रेणिक ) ।
-
(ग) दीपक – जो मिथ्यादृष्टि स्वयं तो तत्त्वश्रद्धान से शून्य हो परन्तु उपदेशादि द्वारा दूसरों में तत्वश्रद्धा का कारण होने से कारण में कार्य का उपचार कर
उत्पन्न करे । उसका उपदेश दूसरों में समकित 'दीपक' कहा ।
प्रकार ५. औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, सास्वादन, वेदक । ऊपर व्याख्या की गई है। ये पाँचों प्रकार के सम्यक्त्व
निसर्ग (स्वभाव) व उपदेश से उत्पन्न होते हैं ।
प्रकार १०. निसर्गचि उपदेश आताच सूत्ररुचि, बीजरुचि, अधिगमर्शन, विस्ताररुचि, कियारुचि, प
धर्म रुचि (उत्तरा, २८।१६) ।
प्र० - सम्पदर्शनी व सम्पदृष्टि में क्या अन्तर है ?
1
उ०- सम्यग्दृष्टि के दो भेद है-सादि सपर्यवसान, सादि अपर्यवसान सादि सपर्यवसान वाले सी है। उनका सम्यदर्शन ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोपशम से जन्य है (अपाय सर्तनीय, मतिज्ञान का भेद ) 1 जबकि केवली को मोहनीय कर्म के क्षय से सम्भव है - केवली को मतिज्ञान का अपायापगम अभाव है। अतः सयोगि अयोगिकेवली व सिद्धों के जीव सम्यष्टि कहलाते हैं व चार से बारहवें गुणस्थानी जीव को सम्यग्दर्शन कहा। सम्यग्दर्शनी की स्थिति जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट ६६ सागरोपम से कुछ अधिक है । सम्यग्दर्शनी असंख्येय हैं जबकि सम्यग्दृष्टि अनन्त होते हैं ( सिद्ध भी सम्मिलित हैं) । सम्यग्दर्शनी का क्षेत्र लोक का असंख्यातवां भाग है जबकि सम्यग्दृष्टि का क्षेत्र समस्त लोक है ।
(४) अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान ३२- सावद्यव्यापारों को छोड़ देना अर्थात् पापजनक कार्यों से अलग होना विरति कहलाता है । चारित्र वा व्रत विरति का ही नाम है। जो सम्यकदृष्टि होकर भी किसी प्रकार के व्रत नियम धारण नहीं कर सकता, उसको अविरत सम्यग्दृष्टि, उसका स्वरूप अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान कहलाता है । व्रत नियम में बाधक उसके अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय है । परन्तु यहाँ सद्बोध रुचि, श्रद्धा प्राप्त हो जाने से आत्मा का विकासक्रम यहीं से प्रारम्भ हो जाता है। इस गुणस्थान को पाकर आत्मा शान्ति का अनुभव करता है । इस भूमिका में आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ (आत्मस्वरूपोन्मुख ) होने से विपय पातंजल योग में जो अष्ट भूमिकाएँ ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व यशोविजयजी ने हरिभद्रजी के योगदृष्टि समुच्चय के आधार पर संज्जायों की रचना की उनमें से (मित्रा, बला, तारा, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रमापरा ) प्रत्याहार तदनुसार स्थिरा से समकक्ष यह सम्यक्त्व की दृष्टि है। चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा के स्वरूप दर्शन से जीव को विश्वास हो जाता है कि अब तक जो मैं पौद्गलिक बाह्य सुख में तरस रहा था वह परिणाम विरस, अस्थिर व परिमित है । सुन्दर व अपरिमित सुख स्वरूप की प्राप्ति में है। तब वह विकासगामी स्वरूप स्थिति के लिए प्रयत्नशील बनता है । कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी बनता है । अन्तरात्मा कहा जाता है व चारित्रमोह की शक्ति को निर्बल करने के लिए आगे प्रयास करता है।
रहित होती है। समाधि) बताईं व
(५) देशविरति गुणस्थान. - प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के कारण जो जीव पापजनक क्रियाओं से सम्पूर्णतया नहीं अपितु अंश से विरक्त हो सकते हैं वे देशविरत या श्रावक कहे जाते हैं। उनका स्वरूप विशेष देशविरत गुणस्थान कहलाता है। कोई एक व्रतधारी व अधिक से अधिक १२ व्रतधारी व ११ प्रतिमाधारी होते हैं तो कोई अनुमति सिवाय ( प्रतिसेवना, प्रतिश्रवणा, संवासानुमति) न सावद्यवृति करते हैं न कराते हैं। इस गुणस्थान में विकासगामी आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि यदि अल्पविरति से भी इतना अधिक शान्तिलाभ हुआ तो सर्व विरति जड़ पदार्थों के सर्वथा परिहार से कितना लाभ होगा ? सर्वविरति के लिए आगे बढ़ता है।
Jain Education international
tera, arsonal use only
000000000000
Ple
*
0000000000
32
000000000000
.:S.Bhast/ www.jainelibrary.org