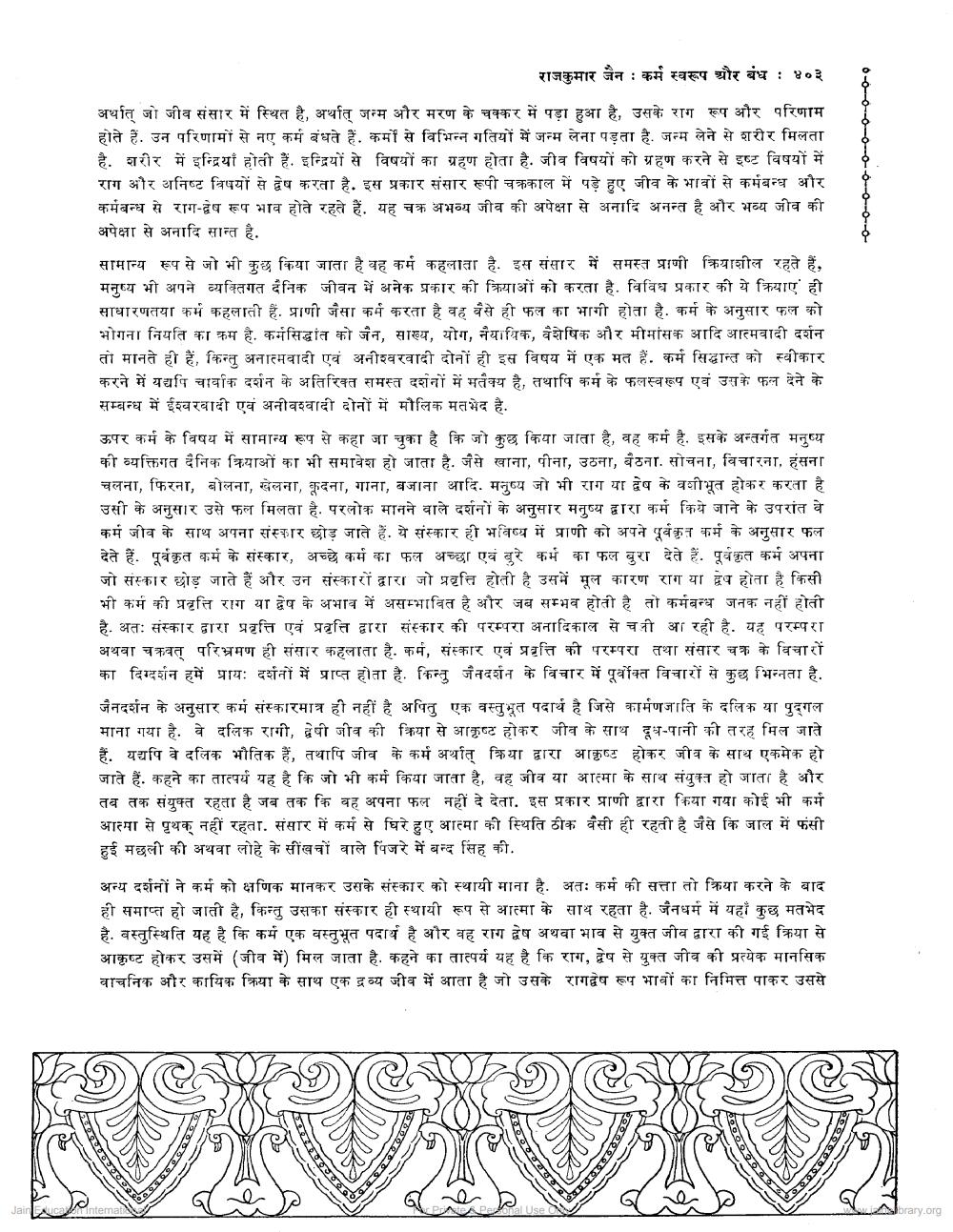________________
राजकुमार जैन : कर्म स्वरूप और बंध : ४०३
अर्थात् जो जीव संसार में स्थित है, अर्थात् जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसके राग रूप और परिणाम होते हैं. उन परिणामों से नए कर्म बंधते हैं. कर्मों से विभिन्न गतियों में जन्म लेना पड़ता है. जन्म लेने से शरीर मिलता है. शरीर में इन्द्रियाँ होती हैं. इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण होता है. जीव विषयों को ग्रहण करने से इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों से द्वेष करता है. इस प्रकार संसार रूपी चक्रकाल में पड़े हुए जीव के भावों से कर्मबन्ध और कर्मबन्ध से राग-द्वेष रूप भाव होते रहते हैं. यह चक्र अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनन्त है और भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि सान्त है. सामान्य रूप से जो भी कुछ किया जाता है वह कर्म कहलाता है. इस संसार में समस्त प्राणी क्रियाशील रहते हैं, मनुष्य भी अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है. विविध प्रकार की ये क्रियाएं ही साधारणतया कर्म कहलाती हैं. प्राणी जैसा कर्म करता है वह वैसे ही फल का भागी होता है. कर्म के अनुसार फल को भोगना नियति का कम है. कर्मसिद्धांत को जैन, साख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसक आदि आत्मवादी दर्शन तो मानते ही हैं, किन्तु अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों ही इस विषय में एक मत हैं. कर्म सिद्धान्त को स्वीकार करने में यद्यपि चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त समस्त दर्शनों में मतैक्य है, तथापि कर्म के फलस्वरूप एवं उसके फल देने के सम्बन्ध में ईश्वरवादी एवं अनीवश्वादी दोनों में मौलिक मतभेद है. ऊपर कर्म के विषय में सामान्य रूप से कहा जा चुका है कि जो कुछ किया जाता है, वह कर्म है. इसके अन्तर्गत मनुष्य की व्यक्तिगत दैनिक क्रियाओं का भी समावेश हो जाता है. जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना. सोचना, विचारना, हंसना चलना, फिरना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना आदि. मनुष्य जो भी राग या द्वेष के वशीभूत होकर करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है. परलोक मानने वाले दर्शनों के अनुसार मनुष्य द्वारा कर्म किये जाने के उपरांत वे कर्म जीव के साथ अपना संस्कार छोड़ जाते हैं. ये संस्कार ही भविष्य में प्राणी को अपने पूर्वकृत कर्म के अनुसार फल देते हैं. पूर्वकृत कर्म के संस्कार, अच्छे कर्म का फल अच्छा एवं बुरे कर्म का फल बुरा देते हैं. पूर्वकृत कर्म अपना जो संस्कार छोड़ जाते हैं और उन संस्कारों द्वारा जो प्रवृत्ति होती है उसमें मूल कारण राग या द्वेष होता है किसी भी कर्म की प्रवृत्ति राग या द्वेष के अभाव में असम्भावित है और जब सम्भव होती है तो कर्मबन्ध जनक नहीं होती है. अतः संस्कार द्वारा प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति द्वारा संस्कार की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है. यह परम्परा अथवा चक्रवत् परिभ्रमण ही संसार कहलाता है. कर्म, संस्कार एवं प्रवृत्ति की परम्परा तथा संसार चक्र के विचारों का दिग्दर्शन हमें प्रायः दर्शनों में प्राप्त होता है. किन्तु जैनदर्शन के विचार में पूर्वोक्त विचारों से कुछ भिन्नता है. जैनदर्शन के अनुसार कर्म संस्कारमात्र ही नहीं है अपितु एक वस्तुभुत पदार्थ है जिसे कार्मणजाति के दलिक या पुद्गल माना गया है. वे दलिक रागी, द्वेषी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ दूध-पानी की तरह मिल जाते हैं. यद्यपि वे दलिक भौतिक हैं, तथापि जीव के कर्म अर्थात् क्रिया द्वारा आकृष्ट होकर जीव के साथ एकमेक हो जाते हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म किया जाता है, वह जीव या आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है और तब तक संयुक्त रहता है जब तक कि वह अपना फल नहीं दे देता. इस प्रकार प्राणी द्वारा किया गया कोई भी कर्म आत्मा से पृथक् नहीं रहता. संसार में कर्म से घिरे हुए आत्मा की स्थिति ठीक वैसी ही रहती है जैसे कि जाल में फंसी हुई मछली की अथवा लोहे के सींखचों वाले पिंजरे में बन्द सिंह की.
अन्य दर्शनों ने कर्म को क्षणिक मानकर उसके संस्कार को स्थायी माना है. अतः कर्म की सत्ता तो क्रिया करने के बाद ही समाप्त हो जाती है, किन्तु उसका संस्कार ही स्थायी रूप से आत्मा के साथ रहता है. जैनधर्म में यहाँ कुछ मतभेद है. वस्तुस्थिति यह है कि कर्म एक वस्तुभूत पदार्थ है और वह राग द्वेष अथवा भाव से युक्त जीव द्वारा की गई क्रिया से आकृष्ट होकर उसमें (जीव में) मिल जाता है. कहने का तात्पर्य यह है कि राग, द्वेष से युक्त जीव की प्रत्येक मानसिक वाचनिक और कायिक क्रिया के साथ एक द्रव्य जीव में आता है जो उसके रागद्वेष रूप भावों का निमित्त पाकर उससे
299
काठ9
Jain Luca
A
brary.org