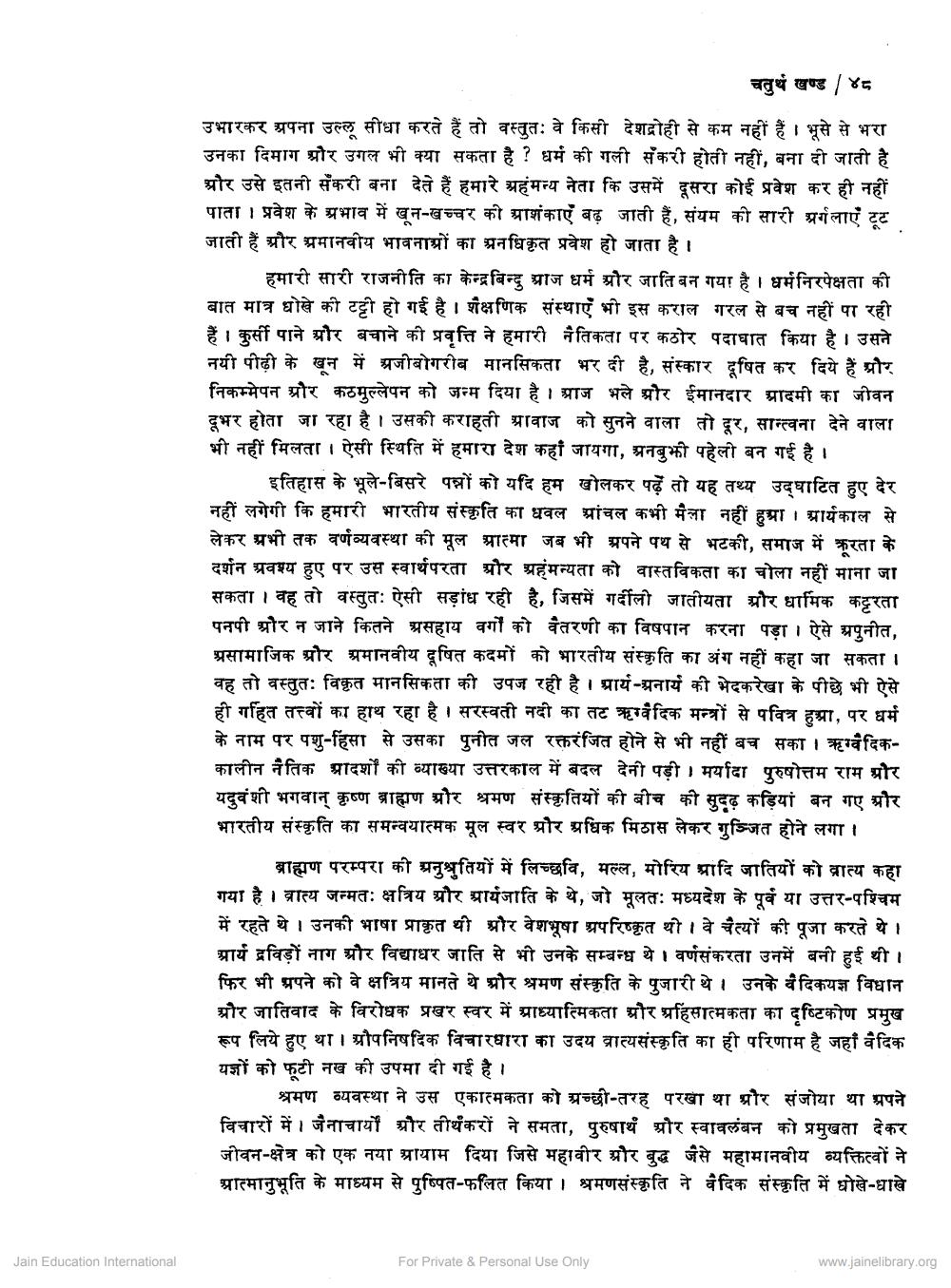________________
चतुर्थ खण्ड / ४८
उभारकर अपना उल्ल सीधा करते हैं तो वस्तुतः वे किसी देशद्रोही से कम नहीं हैं। भूसे से भरा उनका दिमाग और उगल भी क्या सकता है ? धर्म की गली संकरी होती नहीं, बना दी जाती है और उसे इतनी संकरी बना देते हैं हमारे अहंमन्य नेता कि उसमें दूसरा कोई प्रवेश कर ही नहीं पाता । प्रवेश के अभाव में खून-खच्चर की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, संयम की सारी अर्गलाएं टूट । जाती हैं और अमानवीय भावनाओं का अनधिकृत प्रवेश हो जाता है।
हमारी सारी राजनीति का केन्द्रबिन्दु अाज धर्म और जाति बन गया है। धर्मनिरपेक्षता की बात मात्र धोखे की टट्टी हो गई है। शैक्षणिक संस्थाएं भी इस कराल गरल से बच नहीं पा रही हैं । कुर्सी पाने और बचाने की प्रवृत्ति ने हमारी नैतिकता पर कठोर पदाघात किया है। उसने नयी पीढ़ी के खून में अजीबोगरीब मानसिकता भर दी है, संस्कार दूषित कर दिये हैं और निकम्मेपन और कठमुल्लेपन को जन्म दिया है। आज भले और ईमानदार आदमी का जीवन भर होता जा रहा है। उसकी कराहती आवाज को सुनने वाला तो दूर, सान्त्वना देने वाला भी नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में हमारा देश कहाँ जायगा, अनबुझी पहेली बन गई है।
इतिहास के भूले-बिसरे पन्नों को यदि हम खोलकर पढ़ें तो यह तथ्य उद्घाटित हुए देर नहीं लगेगी कि हमारी भारतीय संस्कृति का धवल प्रांचल कभी मैला नहीं हुआ। प्रार्यकाल से लेकर अभी तक वर्णव्यवस्था की मूल प्रात्मा जब भी अपने पथ से भटकी, समाज में क्रूरता के दर्शन अवश्य हुए पर उस स्वार्थपरता और अहंमन्यता को वास्तविकता का चोला नहीं माना जा सकता । वह तो वस्तुत: ऐसी सड़ांध रही है, जिसमें गर्दीली जातीयता और धार्मिक कट्टरता पनपी और न जाने कितने असहाय वर्गों को वैतरणी का विषपान करना पड़ा। ऐसे अपनीत, असामाजिक और अमानवीय दूषित कदमों को भारतीय संस्कृति का अंग नहीं कहा जा सकता। वह तो वस्तुतः विकृत मानसिकता की उपज रही है। प्रार्य-अनार्य की भेदकरेखा के पीछे भी ऐसे ही गहित तत्त्वों का हाथ रहा है। सरस्वती नदी का तट ऋग्वैदिक मन्त्रों से पवित्र हा, पर धर्म के नाम पर पशु-हिंसा से उसका पुनीत जल रक्तरंजित होने से भी नहीं बच सका। ऋग्वैदिककालीन नैतिक आदर्शों की व्याख्या उत्तरकाल में बदल देनी पड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और यदवंशी भगवान कृष्ण ब्राह्मण और श्रमण संस्कृतियों की बीच की सूदढ कडियां बन गए और भारतीय संस्कृति का समन्वयात्मक मूल स्वर और अधिक मिठास लेकर गुञ्जित होने लगा।
ब्राह्मण परम्परा की अनुश्रुतियों में लिच्छवि, मल्ल, मोरिय प्रादि जातियों को व्रात्य कहा गया है। व्रात्य जन्मतः क्षत्रिय और प्रार्यजाति के थे, जो मूलतः मध्यदेश के पूर्व या उत्तर-पश्चिम में रहते थे। उनकी भाषा प्राकृत थी और वेशभूषा अपरिष्कृत थी। वे चैत्यों की पूजा करते थे। प्रार्य द्रविड़ों नाग और विद्याधर जाति से भी उनके सम्बन्ध थे। वर्णसंकरता उनमें बनी हुई थी। फिर भी अपने को वे क्षत्रिय मानते थे और श्रमण संस्कृति के पुजारी थे। उनके वैदिकयज्ञ विधान और जातिवाद के विरोधक प्रखर स्वर में आध्यात्मिकता और अहिंसात्मकता का दृष्टिकोण प्रमुख रूप लिये हए था। औपनिषदिक विचारधारा का उदय व्रात्यसंस्कृति का ही परिणाम है जहाँ वैदिक यज्ञों को फुटी नख की उपमा दी गई है।
श्रमण व्यवस्था ने उस एकात्मकता को अच्छी-तरह परखा था और संजोया था अपने विचारों में। जैनाचार्यों और तीर्थंकरों ने समता, पुरुषार्थ और स्वावलंबन को प्रमुखता देकर जीवन-क्षेत्र को एक नया आयाम दिया जिसे महावीर और बुद्ध जैसे महामानवीय व्यक्तित्वों ने प्रात्मानुभूति के माध्यम से पुष्पित-फलित किया। श्रमणसंस्कृति ने वैदिक संस्कृति में धोखे-धाखे
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org