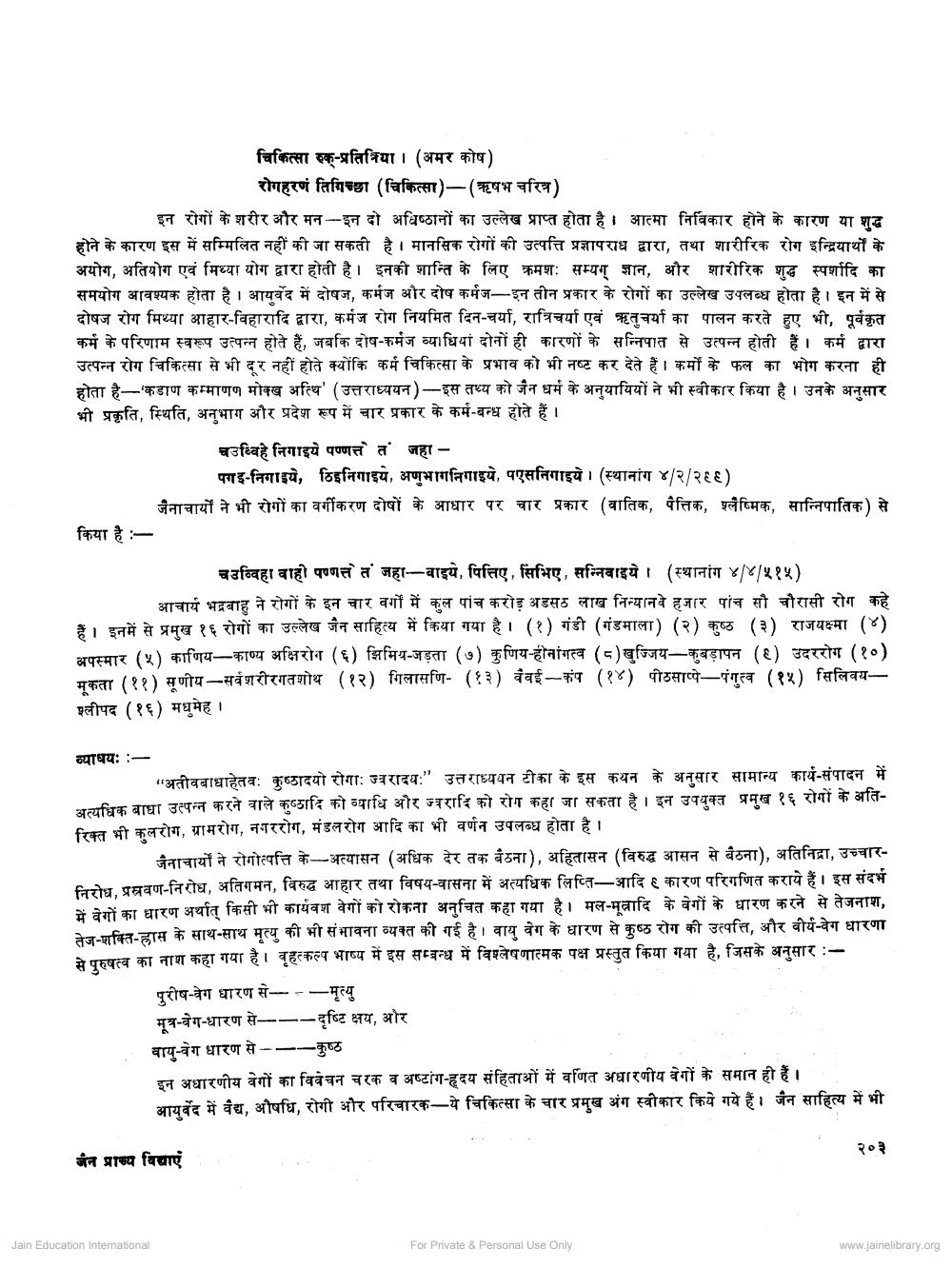________________
इन रोगों के शरीर और मन -इन दो अधिष्ठानों का उल्लेख प्राप्त होता है। आत्मा निर्विकार होने के कारण या शुद्ध होने के कारण इस में सम्मिलित नहीं की जा सकती है। मानसिक रोगों की उत्पत्ति प्रज्ञापराध द्वारा, तथा शारीरिक रोग इन्द्रियार्थों के अयोग, अतियोग एवं मिथ्या योग द्वारा होती है। इनकी शान्ति के लिए क्रमशः सम्यग् ज्ञान, और शारीरिक शुद्ध स्पर्शादि का समयोग आवश्यक होता है । आयुर्वेद में दोषज, कर्मज और दोष कर्मज – इन तीन प्रकार के रोगों का उल्लेख उपलब्ध होता है । इनमें से दोषज रोग मिथ्या आहार-विहारादि द्वारा, कर्मज रोग नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन करते हुए भी पूर्वकृत कर्म के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जबकि दोष-कर्मज व्याधियां दोनों ही कारणों के सन्निपात से उत्पन्न होती हैं । कर्म द्वारा उत्पन्न रोग चिकित्सा से भी दूर नहीं होते क्योंकि कर्म चिकित्सा के प्रभाव को भी नष्ट कर देते हैं। कर्मों के फल का भोग करना ही होता है— 'कडाण कम्माणण मोक्ख अस्थि' (उत्तराध्ययन) – इस तथ्य को जैन धर्म के अनुयायियों ने भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप में चार प्रकार के कर्म-बन्ध होते हैं ।
--
किया है :
व्याधयः
चिकित्सा र प्रतिनिया (अमर कोष)
रोगहरणं तिमिच्छा (चिकित्सा ) - ( ऋषभ चरित्र)
व्हिा वाही पण्णत्तं तं जहा - बाइये, पित्तिए, सिभिए, सन्निवाइये । ( स्थानांग ४/४ / ५१५ )
आचार्य भद्रबाहु ने रोगों के इन चार वर्गों में कुल पांच करोड़ अडसठ लाख निन्यानवे हजार पांच सौ चौरासी रोग कहे हैं। इनमें से प्रमुख १६ रोगों का उल्लेख जैन साहित्य में किया गया है । ( १ ) गंडी (गंडमाला) (२) कुष्ठ ( ३ ) राजयक्ष्मा ( ४ ) अपस्मार ( ५ ) कार्णिय - काव्य अक्षिरोग (६) झिमिय जड़ता (७) कुणिय-हीनांगत्व ( ८ ) खुज्जिय — कुबड़ापन ( 8 ) उदररोग (१०) मूकता (११) मृणीय सर्वशरीरगतशोध (१२) विलास (१३) बैंबई-कंप (१४) पीठसाप्ये पंगुत्व (१५) सिनिय श्लीपद (१६) मधुमेह ।
-
-
विहे निगाइये पण्णत्त त जहा -
पगड - निगाइये, ठिनिगाइये, अणुभागनिगाइये, पएसनिगाइये (स्थानांग ४ / २ / २६६ )
जैनाचार्यों ने भी रोगों का वर्गीकरण दोषों के आधार पर चार प्रकार ( वातिक, पैतिक, श्लैष्मिक सान्निपातिक) से
Jain Education International
"अतीवबाधाहेतवः कुष्ठादयो रोगाः ज्वरादयः" उत्तराध्ययन टीका के इस कथन के अनुसार सामान्य कार्य संपादन में अत्यधिक बाधा उत्पन्न करने वाले कुष्ठादि को व्याधि और ज्वरादि को रोग कहा जा सकता है । इन उपयुक्त प्रमुख १६ रोगों के अतिरिक्त भी कुलरोग, ग्रामरोग, नगररोग, मंडलरोग आदि का भी वर्णन उपलब्ध होता है।
ε
जैनाचायों ने रोगोत्पत्ति के अध्यासन (अधिक देर तक बैठना अहितासन (विरुद्ध आसन से बैठना ), अतिनिद्रा, उच्चारनिरोध, प्रस्रवण-निरोध, अतिगमन विरुद्ध आहार तथा विषय-वासना में अत्यधिक लिप्ति - आदि कारण परिगणित कराये हैं । इस संदर्भ में वेगों का धारण अर्थात् किसी भी कार्यवश वेगों को रोकना अनुचित कहा गया है। मल-मूत्रादि के वेगों के धारण करने से तेजनाश, तेज-शक्ति- ह्रास के साथ-साथ मृत्यु की भी संभावना व्यक्त की गई है। वायु वेग के धारण से कुष्ठ रोग की उत्पत्ति, और वीर्य-वेग धारणा से पुरुषत्व का नाश कहा गया है। वृहत्कल्प भाष्य में इस सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक पक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार :पुरीष-वेग धारण सेमूत्र वेग-धारण से दृष्टि और वायु-वेग धारण से - - कुष्ठ
:
- मृत्यु क्षय,
जन प्राच्य विद्याएं
-
———
———
1
इन अधारणीय वेगों का विवेचन चरक व अष्टांग हृदय संहिताओं में वर्णित अधारणीय वेगों के समान ही है।
आयुर्वेद में वैद्य, औषधि, रोगी और परिचारक - ये चिकित्सा के चार प्रमुख अंग स्वीकार किये गये हैं । जैन साहित्य में भी
For Private & Personal Use Only
२०३
www.jainelibrary.org