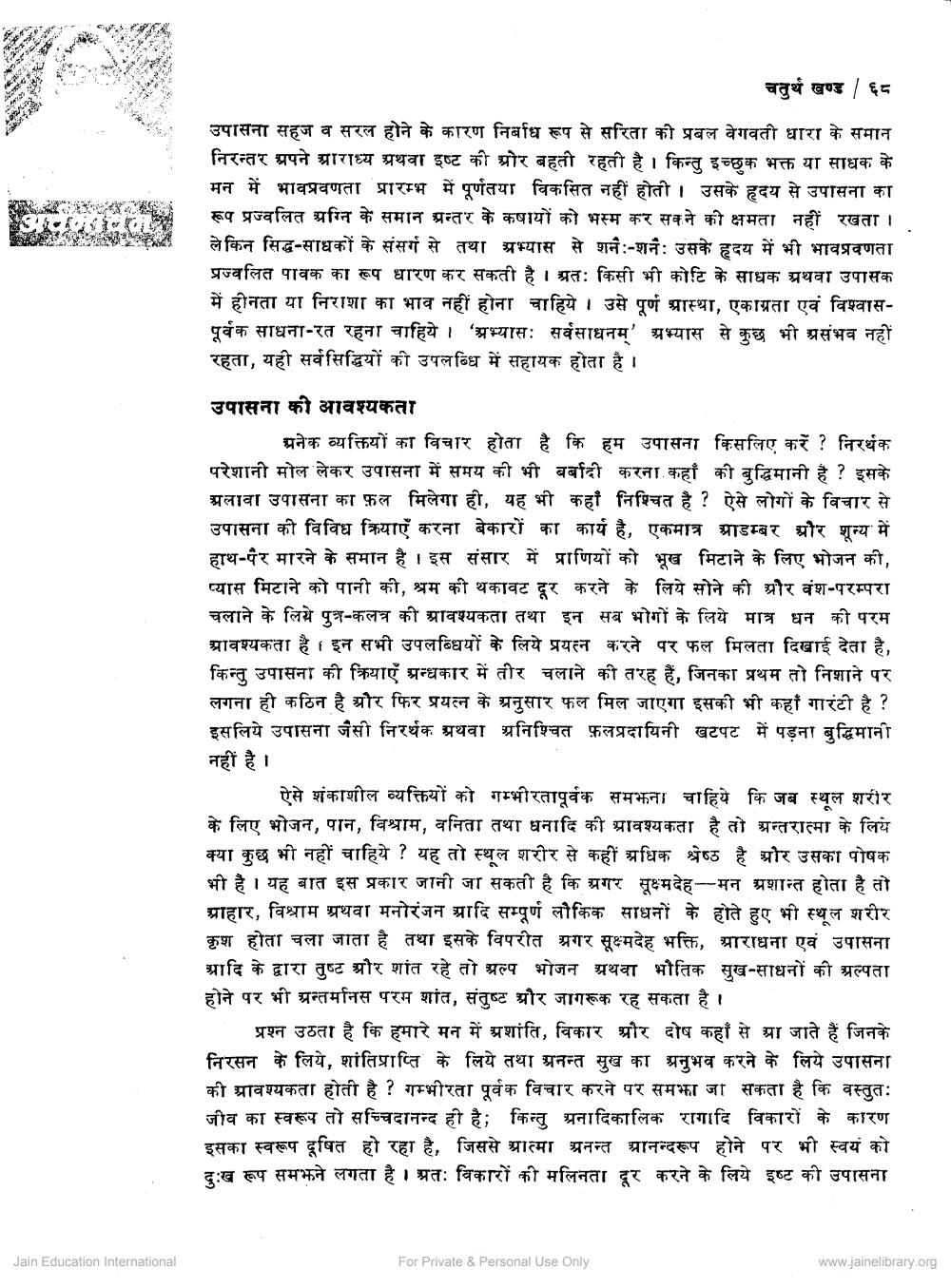________________
Tatara
चतुर्थ खण्ड ६८
act
andry Aaskar
उपासना सहज व सरल होने के कारण निर्बाध रूप से सरिता की प्रबल वेगवती धारा के समान निरन्तर अपने आराध्य अथवा इष्ट की ओर बहती रहती है। किन्तु इच्छुक भक्त या साधक के मन में भावप्रवणता प्रारम्भ में पूर्णतया विकसित नहीं होती। उसके हृदय से उपासना का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान अन्तर के कषायों को भस्म कर सकने की क्षमता नहीं रखता । लेकिन सिद्ध-साधकों के संसर्ग से तथा अभ्यास से शनैः-शनैः उसके हृदय में भी भावप्रवणता प्रज्वलित पावक का रूप धारण कर सकती है। अत: किसी भी कोटि के साधक अथवा उपासक में हीनता या निराशा का भाव नहीं होना चाहिये । उसे पूर्ण आस्था, एकाग्रता एवं विश्वासपूर्वक साधना-रत रहना चाहिये । 'अभ्यास: सर्वसाधनम' अभ्यास से कुछ भी असंभव नहीं रहता, यही सर्वसिद्धियों की उपलब्धि में सहायक होता है।
उपासना की आवश्यकता
अनेक व्यक्तियों का विचार होता है कि हम उपासना किसलिए करें ? निरर्थक परेशानी मोल लेकर उपासना में समय की भी बर्बादी करना कहाँ की बुद्धिमानी है ? इसके अलावा उपासना का फल मिलेगा ही, यह भी कहाँ निश्चित है ? ऐसे लोगों के विचार से उपासना की विविध क्रियाएँ करना बेकारों का कार्य है, एकमात्र आडम्बर और शून्य में हाथ-पैर मारने के समान है । इस संसार में प्राणियों को भूख मिटाने के लिए भोजन की, प्यास मिटाने को पानी की, श्रम की थकावट दूर करने के लिये सोने की और वंश-परम्परा चलाने के लिये पुत्र-कलत्र की आवश्यकता तथा इन सब भोगों के लिये मात्र धन की परम आवश्यकता है। इन सभी उपलब्धियों के लिये प्रयत्न करने पर फल मिलता दिखाई देता है, किन्तु उपासना की क्रियाएँ अन्धकार में तीर चलाने की तरह हैं, जिनका प्रथम तो निशाने पर लगना ही कठिन है और फिर प्रयत्न के अनुसार फल मिल जाएगा इसकी भी कहाँ गारंटी है ? इसलिये उपासना जैसी निरर्थक अथवा अनिश्चित फलप्रदायिनी खटपट में पड़ना बुद्धिमानी नहीं है।
ऐसे शंकाशील व्यक्तियों को गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिये कि जब स्थूल शरीर के लिए भोजन, पान, विश्राम, वनिता तथा धनादि की आवश्यकता है तो अन्तरात्मा के लिये क्या कुछ भी नहीं चाहिये ? यह तो स्थूल शरीर से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और उसका पोषक भी है। यह बात इस प्रकार जानी जा सकती है कि अगर सूक्ष्मदेह-मन प्रशान्त होता है तो पाहार, विश्राम अथवा मनोरंजन आदि सम्पूर्ण लौकिक साधनों के होते हुए भी स्थूल शरीर कृश होता चला जाता है तथा इसके विपरीत अगर सूक्ष्मदेह भक्ति, आराधना एवं उपासना आदि के द्वारा तुष्ट और शांत रहे तो अल्प भोजन अथवा भौतिक सुख-साधनों की अल्पता होने पर भी अन्तर्मानस परम शांत, संतुष्ट और जागरूक रह सकता है।
प्रश्न उठता है कि हमारे मन में अशांति, विकार और दोष कहाँ से आ जाते हैं जिनके निरसन के लिये, शांतिप्राप्ति के लिये तथा अनन्त सुख का अनुभव करने के लिये उपासना की आवश्यकता होती है ? गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर समझा जा सकता है कि वस्तुतः जीव का स्वरूप तो सच्चिदानन्द ही है; किन्तु अनादिकालिक रागादि विकारों के कारण इसका स्वरूप दूषित हो रहा है, जिससे प्रात्मा अनन्त प्रानन्दरूप होने पर भी स्वयं को दःख रूप समझने लगता है। अतः विकारों की मलिनता दूर करने के लिये इष्ट की उपासना
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org