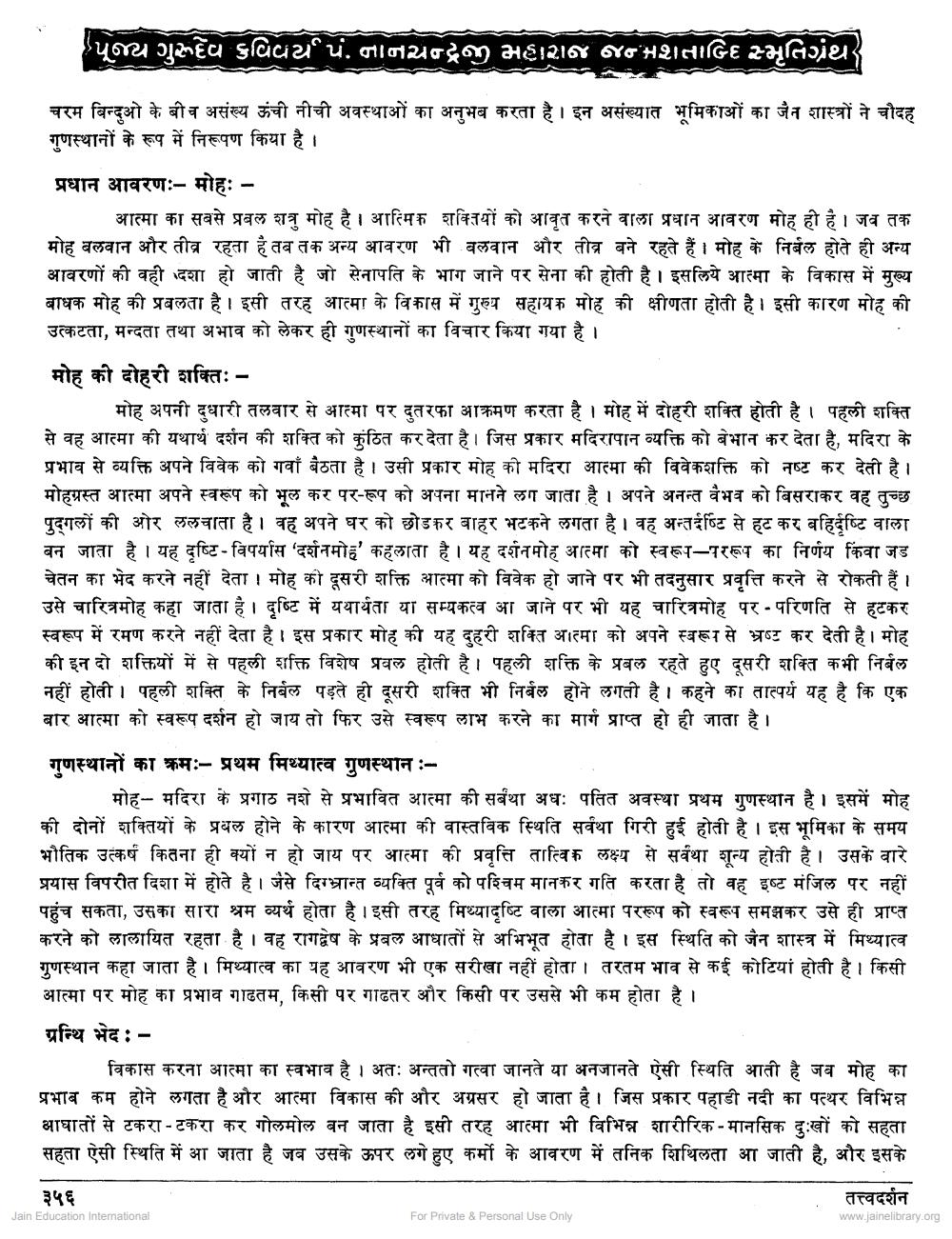________________
ઉપય ગુરુદેવ કવિવર્ય પ. નાનચન્દ્રજી મહારાજ જમશતાલિદ સ્મૃતિગ્રંથ
मिकाओं का जैन शास्त्रों ने चौदह
चरम बिन्दुओ के बीच असंख्य ऊंची नीची अवस्थाओं का अनुभव करता है। इन असंख्यात गणस्थानों के रूप में निरूपण किया है।
प्रधान आवरणः- मोहः -
आत्मा का सबसे प्रबल शत्रु मोह है। आत्मिक शक्तियों को आवृत करने वाला प्रधान आवरण मोह ही है। जब तक मोह बलवान और तीव्र रहता है तब तक अन्य आवरण भी बलवान और तीव्र बने रहते हैं। मोह के निर्बल होते ही अन्य आवरणों की वही दशा हो जाती है जो सेनापति के भाग जाने पर सेना की होती है। इसलिये आत्मा के विकास में मुख्य बाधक मोह की प्रबलता है। इसी तरह आत्मा के विकास में मुख्य सहायक मोह की क्षीणता होती है। इसी कारण मोह की उत्कटता, मन्दता तथा अभाव को लेकर ही गुणस्थानों का विचार किया गया है। मोह की दोहरी शक्तिः -
मोह अपनी दुधारी तलवार से आत्मा पर दुतरफा आक्रमण करता है। मोह में दोहरी शक्ति होती है। पहली शक्ति से वह आत्मा की यथार्थ दर्शन की शक्ति को कुंठित कर देता है। जिस प्रकार मदिरापान व्यक्ति को बेभान कर देता है, मदिरा के प्रभाव से व्यक्ति अपने विवेक को गवाँ बैठता है। उसी प्रकार मोह की मदिरा आत्मा की विवेकशक्ति को नष्ट कर देती है। मोहग्रस्त आत्मा अपने स्वरूप को भूल कर पर-रूप को अपना मानने लग जाता है। अपने अनन्त वैभव को बिसराकर वह तुच्छ पुद्गलों की ओर ललचाता है। वह अपने घर को छोडकर बाहर भटकने लगता है। वह अन्तर्दष्टि से हट कर बहिर्दष्टि वाला बन जाता है । यह दृष्टि - विपर्यास 'दर्शनमोह' कहलाता है। यह दर्शनमोह आत्मा को स्वरूप-पररूप का निर्णय किंवा जड चेतन का भेद करने नहीं देता। मोह को दूसरी शक्ति आत्मा को विवेक हो जाने पर भी तदनुसार प्रवृत्ति करने से रोकती हैं। उसे चारित्रमोह कहा जाता है। दृष्टि में यथार्थता या सम्यकत्व आ जाने पर भी यह चारित्रमोह पर - परिणति से हटकर स्वरूप में रमण करने नहीं देता है। इस प्रकार मोह की यह दुहरी शक्ति आत्मा को अपने स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है। मोह की इन दो शक्तियों में से पहली शक्ति विशेष प्रवल होती है। पहली शक्ति के प्रबल रहते हुए दूसरी शक्ति कभी निर्बल नहीं होती। पहली शक्ति के निर्बल पड़ते ही दूसरी शक्ति भी निर्बल होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार आत्मा को स्वरूप दर्शन हो जाय तो फिर उसे स्वरूप लाभ करने का मार्ग प्राप्त हो ही जाता है।
गुणस्थानों का क्रमः- प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान :
मोह- मदिरा के प्रगाठ नशे से प्रभावित आत्मा की सबंथा अधः पतित अवस्था प्रथम गुणस्थान है। इसमें मोह की दोनों शक्तियों के प्रबल होने के कारण आत्मा की वास्तविक स्थिति सर्वथा गिरी हुई होती है। इस भूमिका के समय भौतिक उत्कर्ष कितना ही क्यों न हो जाय पर आत्मा की प्रवृत्ति तात्विक लक्ष्य से सर्वथा शून्य होती है। उसके बारे प्रयास विपरीत दिशा में होते है। जैसे दिग्भ्रान्त व्यक्ति पूर्व को पश्चिम मानकर गति करता है तो वह इष्ट मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, उसका सारा श्रम व्यर्थ होता है। इसी तरह मिथ्यादृष्टि वाला आत्मा पररूप को स्वरूप समझकर उसे ही प्राप्त करने को लालायित रहता है । वह रागद्वेष के प्रबल आधातों से अभिभूत होता है । इस स्थिति को जैन शास्त्र में मिथ्यात्व
न कहा जाता है। मिथ्यात्व का यह आवरण भी एक सरीखा नहीं होता। तरतम भाव से कई कोटियां होती है। किसी आत्मा पर मोह का प्रभाव गाढतम, किसी पर गाढतर और किसी पर उससे भी कम होता है। ग्रन्थि भेद:
विकास करना आत्मा का स्वभाव है । अतः अन्ततो गत्वा जानते या अनजानते ऐसी स्थिति आती है जब मोह का प्रभाब कम होने लगता है और आत्मा विकास की और अग्रसर हो जाता है। जिस प्रकार पहाडी नदी का पत्थर विभिन्न आघातों से टकरा - टकरा कर गोलमोल बन जाता है इसी तरह आत्मा भी विभिन्न शारीरिक-मानसिक दुःखों को सहता सहता ऐसी स्थिति में आ जाता है जब उसके ऊपर लगे हुए कर्मो के आवरण में तनिक शिथिलता आ जाती है, और इसके
तत्त्वदर्शन www.jainelibrary.org
Jain Education International
For Private & Personal Use Only