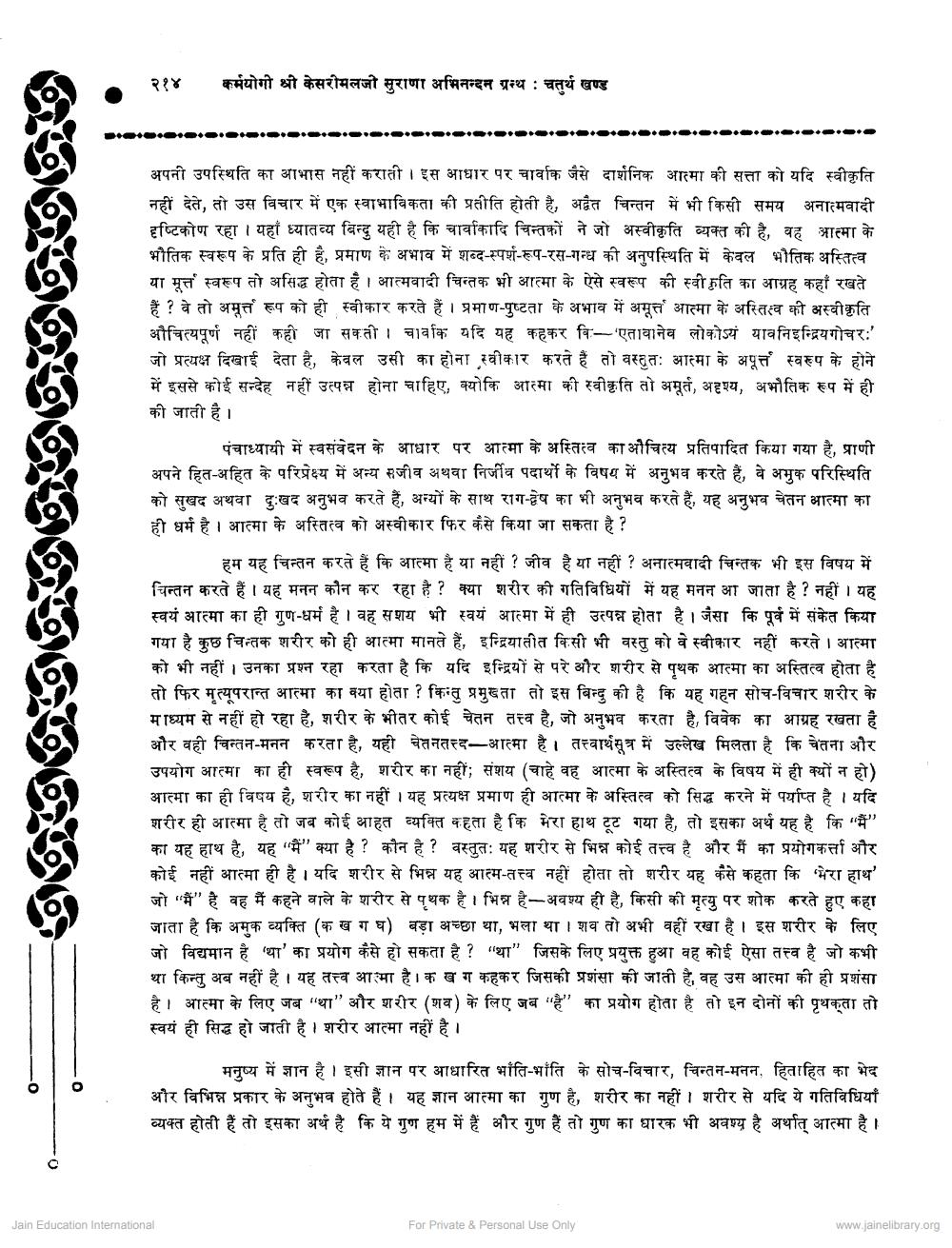________________
२१४
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड
अपनी उपस्थिति का आभास नहीं कराती । इस आधार पर चार्वाक जैसे दार्शनिक आत्मा की सत्ता को यदि स्वीकृति नहीं देते, तो उस विचार में एक स्वाभाविकता की प्रतीति होती है, अद्वैत चिन्तन में भी किसी समय अनात्मवादी दृष्टिकोण रहा । यहाँ ध्यातव्य बिन्दु यही है कि चार्वाकादि चिन्तकों ने जो अस्वीकृति व्यक्त की है, वह आत्मा के भौतिक स्वरूप के प्रति ही है, प्रमाण के अभाव में शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध की अनुपस्थिति में केवल भौतिक अस्तित्व या मूर्त स्वरूप तो असिद्ध होता है । आत्मवादी चिन्तक भी आत्मा के ऐसे स्वरूप की स्वीकृति का आग्रह कहाँ रखते हैं ? वे तो अमूर्त रूप को ही स्वीकार करते हैं । प्रमाण-पुष्टता के अभाव में अमूर्त आत्मा के अस्तित्व की अस्वीकृति औचित्यपूर्ण नहीं कही जा सकती। चावकि यदि यह कहकर वि.- 'एतावानेव लोकोऽयं यावनिइन्द्रियगोचरः' जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, केवल उसी का होना स्वीकार करते हैं तो वस्तुत: आत्मा के अपूर्त स्वरूप के होने में इससे कोई सन्देह नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योकि आत्मा की स्वीकृति तो अमूर्त, अदृश्य, अभौतिक रूप में ही की जाती है।
पंचाध्यायी में स्वसंवेदन के आधार पर आत्मा के अस्तित्व का औचित्य प्रतिपादित किया गया है, प्राणी अपने हित-अहित के परिप्रेक्ष्य में अन्य सजीव अथवा निर्जीव पदार्थो के विषय में अनुभव करते हैं, वे अमुक परिस्थिति को सुखद अथवा दुःखद अनुभव करते हैं, अन्यों के साथ राग-द्वेष का भी अनुभव करते हैं, यह अनुभव चेतन आत्मा का ही धर्म है । आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार फिर कैसे किया जा सकता है ?
हम यह चिन्तन करते हैं कि आत्मा है या नहीं ? जीव है या नहीं ? अनात्मवादी चिन्तक भी इस विषय में चिन्तन करते हैं । यह मनन कौन कर रहा है ? क्या शरीर की गतिविधियों में यह मनन आ जाता है ? नहीं। यह स्वयं आत्मा का ही गुण-धर्म है । वह सशय भी स्वयं आत्मा में ही उत्पन्न होता है। जैसा कि पूर्व में संकेत किया गया है कुछ चिन्तक शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इन्द्रियातीत किसी भी वस्तु को वे स्वीकार नहीं करते । आत्मा को भी नहीं। उनका प्रश्न रहा करता है कि यदि इन्द्रियों से परे और शरीर से पृथक आत्मा का अस्तित्व होता है तो फिर मृत्यूपरान्त आत्मा का क्या होता? किन्तु प्रमुखता तो इस बिन्दु की है कि यह गहन सोच-विचार शरीर के माध्यम से नहीं हो रहा है, शरीर के भीतर कोई चेतन तत्त्व है, जो अनुभव करता है, विवेक का आग्रह रखता है और वही चिन्तन-मनन करता है, यही चेतनतत्त्द-आत्मा है। तत्त्वार्थसूत्र में उल्लेख मिलता है कि चेतना और उपयोग आत्मा का ही स्वरूप है, शरीर का नहीं; संशय (चाहे वह आत्मा के अस्तित्व के विषय में ही क्यों न हो) आत्मा का ही विषय है, शरीर का नहीं । यह प्रत्यक्ष प्रमाण ही आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने में पर्याप्त है । यदि शरीर ही आत्मा है तो जब कोई आहत व्यक्ति कहता है कि मेरा हाथ टूट गया है, तो इसका अर्थ यह है कि "मैं" का यह हाथ है, यह “मैं” क्या है ? कौन है ? वस्तुत: यह शरीर से भिन्न कोई तत्त्व है और मैं का प्रयोगकर्ता और कोई नहीं आत्मा ही है । यदि शरीर से भिन्न यह आत्म-तत्त्व नहीं होता तो शरीर यह कैसे कहता कि 'मेरा हाथ' जो "मैं" है वह मैं कहने वाले के शरीर से पृथक है। भिन्न है-अवश्य ही है, किसी की मृत्यु पर शोक करते हुए कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति (क ख ग घ) बड़ा अच्छा था, भला था। शव तो अभी वहीं रखा है। इस शरीर के लिए जो विद्यमान है 'था' का प्रयोग कैसे हो सकता है ? "था" जिसके लिए प्रयुक्त हुआ वह कोई ऐसा तत्त्व है जो कभी था किन्तु अब नहीं है । यह तत्त्व आत्मा है। क ख ग कहकर जिसकी प्रशंसा की जाती है, वह उस आत्मा की ही प्रशंसा है। आत्मा के लिए जब "था" और शरीर (शव) के लिए जब "है" का प्रयोग होता है तो इन दोनों की पृथक्ता तो स्वयं ही सिद्ध हो जाती है । शरीर आत्मा नहीं है।
___ मनुष्य में ज्ञान है । इसी ज्ञान पर आधारित भाँति-भाँति के सोच-विचार, चिन्तन-मनन, हिताहित का भेद और विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। यह ज्ञान आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। शरीर से यदि ये गतिविधियाँ व्यक्त होती हैं तो इसका अर्थ है कि ये गुण हम में हैं और गुण हैं तो गुण का धारक भी अवश्य है अर्थात् आत्मा है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org