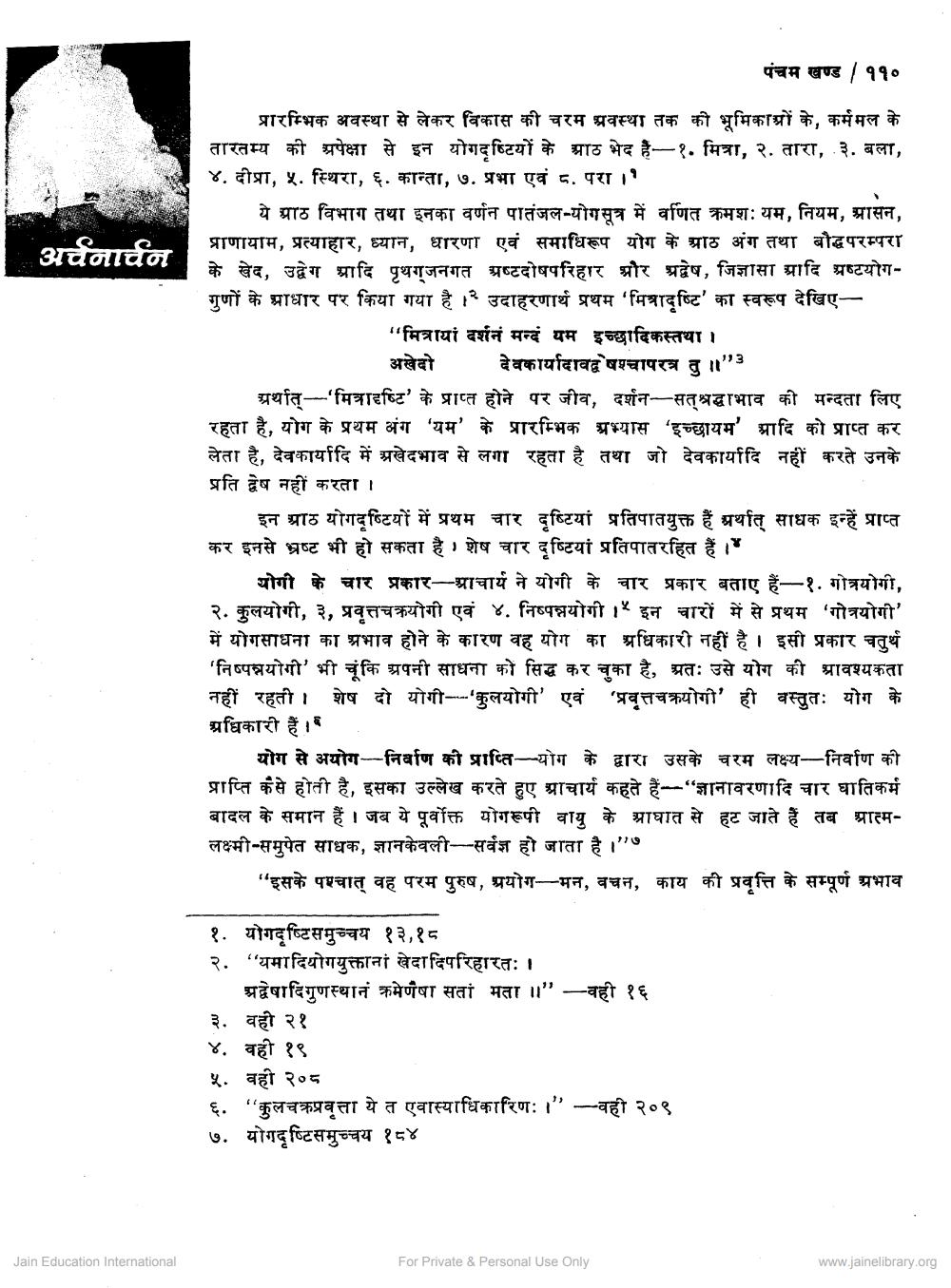________________
पंचम खण्ड / ११०
अर्चनार्चन
प्रारम्भिक अवस्था से लेकर विकास की चरम अवस्था तक की भूमिकाओं के, कर्ममल के तारतम्य की अपेक्षा से इन योगदष्टियों के आठ भेद है-१. मित्रा, २. तारा, ३. बला, ४. दीप्रा, ५. स्थिरा, ६. कान्ता, ७. प्रभा एवं ८. परा।
ये पाठ विभाग तथा इनका वर्णन पातंजल-योगसूत्र में वणित क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधिरूप योग के पाठ अंग तथा बौद्धपरम्परा के खेद, उद्वेग आदि प्रथगजनगत अष्टदोषपरिहार और अद्वेष, जिज्ञासा आदि अष्टयोगगुणों के आधार पर किया गया है। उदाहरणार्थ प्रथम 'मित्रादष्टि' का स्वरूप देखिए
"मित्रायां दर्शनं मन्दं यम इच्छादिकस्तथा।
__ अखेदो देवकार्यादावद्वषश्चापरत्र तु॥"3 अर्थात्-'मित्राष्टि' के प्राप्त होने पर जीव, दर्शन-सत्श्रद्धाभाव की मन्दता लिए रहता है, योग के प्रथम अंग 'यम' के प्रारम्भिक अभ्यास 'इच्छायम' आदि को प्राप्त कर लेता है, देवकार्यादि में अखेदभाव से लगा रहता है तथा जो देवकार्यादि नहीं करते उनके प्रति द्वेष नहीं करता।
इन पाठ योगदष्टियों में प्रथम चार दृष्टियां प्रतिपातयुक्त हैं अर्थात् साधक इन्हें प्राप्त कर इनसे भ्रष्ट भी हो सकता है। शेष चार दृष्टियां प्रतिपातरहित हैं।
योगी के चार प्रकार-प्राचार्य ने योगी के चार प्रकार बताए हैं-१. गोत्रयोगी, २. कुलयोगी, ३, प्रवृत्तचक्रयोगी एवं ४. निष्पन्नयोगी। इन चारों में से प्रथम 'गोत्रयोगी' में योगसाधना का अभाव होने के कारण वह योग का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार चतुर्थ 'निष्पन्नयोगी' भी चूंकि अपनी साधना को सिद्ध कर चुका है, अतः उसे योग की आवश्यकता नहीं रहती। शेष दो योगी----'कुलयोगी' एवं 'प्रवृत्तचक्रयोगी' ही वस्तुतः योग के अधिकारी हैं।
योग से अयोग-निर्वाण की प्राप्तियोग के द्वारा उसके चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है, इसका उल्लेख करते हुए प्राचार्य कहते हैं-"ज्ञानावरणादि चार घातिकर्म बादल के समान हैं। जब ये पूर्वोक्त योगरूपी वायु के आघात से हट जाते हैं तब प्रात्मलक्ष्मी-समुपेत साधक, ज्ञानकेवली-सर्वज्ञ हो जाता है।"
"इसके पश्चात् वह परम पुरुष, अयोग-मन, वचन, काय की प्रवृत्ति के सम्पूर्ण अभाव
१. योगदृष्टिसमुच्चय १३,१८ २. "यमादियोगयुक्तानां खेदादिपरिहारतः ।
अद्वेषादिगुणस्थानं क्रमेणषा सतां मता ॥" -वही १६ ३. वही २१ ४. वही १९ ५. वही २०८ ६. "कुलचक्रप्रवृत्ता ये त एवास्याधिकारिणः।" वही २०९ ७. योगदृष्टिसमुच्चय १८४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org