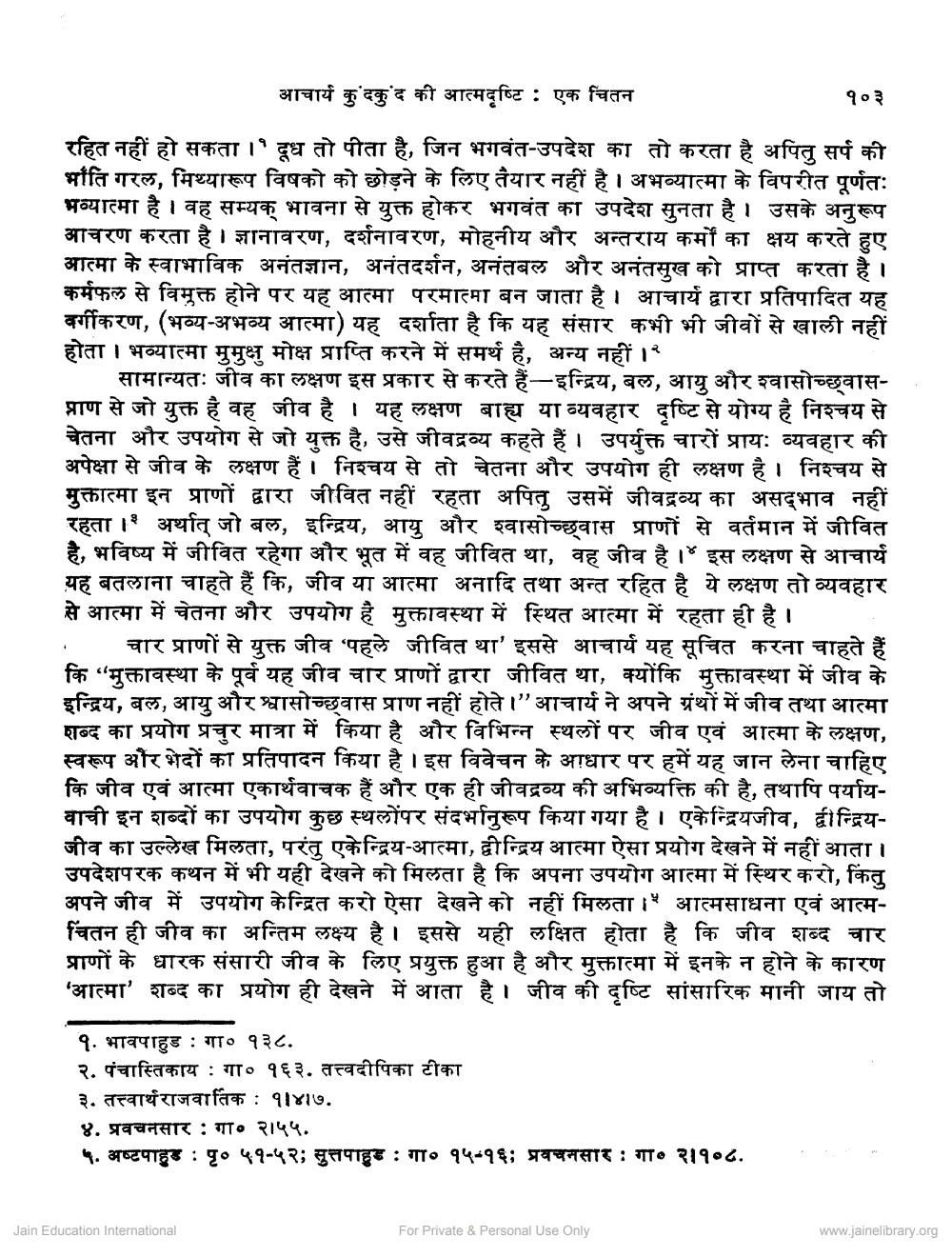________________
आचार्य कुरूंदकुद की आत्मदृष्टि : एक चितन
१
रहित नहीं हो सकता । दूध तो पीता है, जिन भगवंत-उपदेश का तो करता है अपितु सर्प की भाँति गरल, मिथ्यारूप विषको को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है । अभव्यात्मा के विपरीत पूर्णतः भव्यात्मा है । वह सम्यक् भावना से युक्त होकर भगवंत का उपदेश सुनता है । उसके अनुरूप आचरण करता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मों का क्षय करते हुए आत्मा के स्वाभाविक अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतबल और अनंतसुख को प्राप्त करता है । कर्मफल से विमुक्त होने पर यह आत्मा परमात्मा बन जाता है । आचार्य द्वारा प्रतिपादित यह वर्गीकरण, ( भव्य - अभव्य आत्मा ) यह दर्शाता है कि यह संसार कभी भी जीवों से खाली नहीं होता । भव्यात्मा मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति करने में समर्थ है, अन्य नहीं ।
सामान्यतः जीव का लक्षण इस प्रकार से करते हैं - इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वासप्राण से जो युक्त है वह जीव है । यह लक्षण बाह्य या व्यवहार दृष्टि से योग्य है निश्चय से चेतना और उपयोग से जो युक्त है, उसे जीवद्रव्य कहते हैं । उपर्युक्त चारों प्रायः व्यवहार की अपेक्षा से जीव के लक्षण हैं । निश्चय से तो चेतना और उपयोग ही लक्षण है । निश्चय से मुक्तात्मा इन प्राणों द्वारा जीवित नहीं रहता अपितु उसमें जीवद्रव्य का असद्भाव नहीं रहता । अर्थात् जो बल, इन्द्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास प्राणों से वर्तमान में जीवित है, भविष्य में जीवित रहेगा और भूत में वह जीवित था, वह जीव है । इस लक्षण से आचार्य यह बतलाना चाहते हैं कि, जीव या आत्मा अनादि तथा अन्त रहित है ये लक्षण तो व्यवहार से आत्मा में चेतना और उपयोग है मुक्तावस्था में स्थित आत्मा में रहता ही है ।
चार प्राणों से युक्त जीव 'पहले जीवित था' इससे आचार्य यह सूचित करना चाहते हैं कि "मुक्तावस्था के पूर्व यह जीव चार प्राणों द्वारा जीवित था, क्योंकि मुक्तावस्था में जीव के इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते ।" आचार्य ने अपने ग्रंथों में जीव तथा आत्मा शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है और विभिन्न स्थलों पर जीव एवं आत्मा के लक्षण, स्वरूप और भेदों का प्रतिपादन किया है । इस विवेचन के आधार पर हमें यह जान लेना चाहिए कि जीव एवं आत्मा एकार्थवाचक हैं और एक ही जीवद्रव्य की अभिव्यक्ति की है, तथापि पर्यायवाची इन शब्दों का उपयोग कुछ स्थलोंपर संदर्भानुरूप किया गया है । एकेन्द्रियजीव, द्वीन्द्रियजीव का उल्लेख मिलता, परंतु एकेन्द्रिय- आत्मा, द्वीन्द्रिय आत्मा ऐसा प्रयोग देखने में नहीं आता । उपदेशपरक कथन में भी यही देखने को मिलता है कि अपना उपयोग आत्मा में स्थिर करो, किंतु अपने जीव में उपयोग केन्द्रित करो ऐसा देखने को नहीं मिलता। आत्मसाधना एवं आत्मचिंतन ही जीव का अन्तिम लक्ष्य है । इससे यही लक्षित होता है कि जीव शब्द चार प्राणों के धारक संसारी जीव के लिए प्रयुक्त हुआ है और मुक्तात्मा में इनके न होने के कारण 'आत्मा' शब्द का प्रयोग ही देखने में आता है । जीव की दृष्टि सांसारिक मानी जाय तो
१. भावपाहुड : गा० १३८.
२. पंचास्तिकाय: गा० १६३. तत्त्वदीपिका टीका
३. तत्त्वार्थ राजवार्तिक
११४१७.
४. प्रवचनसार : गा० २।५५.
५. अष्टपाहुड : पृ० ५१-५२; सुत्तपाहुड : गा० १५-१६ प्रवचनसार : गा० २।१०८.
Jain Education International
१०३
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org