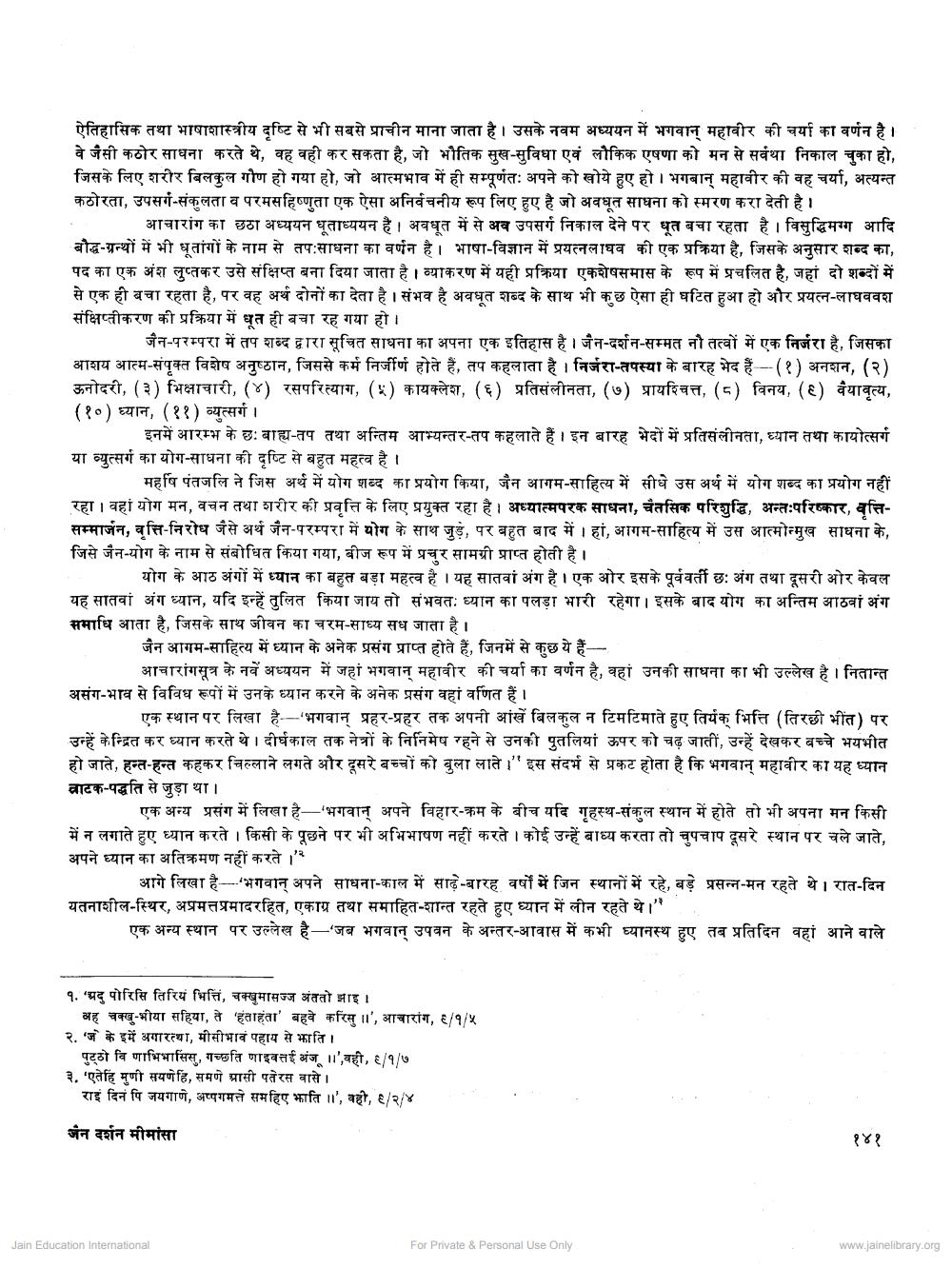________________
ऐतिहासिक तथा भाषाशास्त्रीय दृष्टि से भी सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके नवम अध्ययन में भगवान महावीर की चर्या का वर्णन है। वे जैसी कठोर साधना करते थे, वह वही कर सकता है, जो भौतिक सुख-सुविधा एवं लौकिक एषणा को मन से सर्वथा निकाल चुका हो, जिसके लिए शरीर बिलकुल गौण हो गया हो, जो आत्मभाव में ही सम्पूर्णतः अपने को खोये हुए हो । भगवान् महावीर की वह चर्या, अत्यन्त कठोरता, उपसर्ग-संकुलता व परमसहिष्णुता एक ऐसा अनिर्वचनीय रूप लिए हुए है जो अवधूत साधना को स्मरण करा देती है। - आचारांग का छठा अध्ययन धूताध्ययन है। अवधूत में से अव उपसर्ग निकाल देने पर धूत बचा रहता है । विसुद्धिमग्ग आदि बौद्ध-ग्रन्थों में भी धूतांगों के नाम से तप:साधना का वर्णन है। भाषा-विज्ञान में प्रयत्नलाघव की एक प्रक्रिया है, जिसके अनुसार शब्द का, पद का एक अंश लुप्तकर उसे संक्षिप्त बना दिया जाता है। व्याकरण में यही प्रक्रिया एकशेषसमास के रूप में प्रचलित है, जहां दो शब्दों में से एक ही बचा रहता है, पर वह अर्थ दोनों का देता है । संभव है अवधूत शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ हो और प्रयत्न-लाघववश संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में धूत ही बचा रह गया हो।
जैन-परम्परा में तप शब्द द्वारा सूचित साधना का अपना एक इतिहास है । जैन-दर्शन-सम्मत नौ तत्वों में एक निर्जरा है, जिसका आशय आत्म-संपृक्त विशेष अनुष्ठान, जिससे कर्म निर्जीर्ण होते हैं, तप कहलाता है । निर्जरा-तपस्या के बारह भेद हैं --(१) अनशन, (२) ऊनोदरी, (३) भिक्षाचारी, (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेश, (६) प्रतिसंलीनता, (७) प्रायश्चित्त, (८) विनय, (६) वैयावृत्य, (१०) ध्यान, (११) व्युत्सर्ग।।
इनमें आरम्भ के छः बाह्य-तप तथा अन्तिम आभ्यन्तर-तप कहलाते हैं। इन बारह भेदों में प्रतिसंलीनता, ध्यान तथा कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग का योग-साधना की दृष्टि से बहुत महत्व है।
महर्षि पंतजलि ने जिस अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया, जैन आगम-साहित्य में सीधे उस अर्थ में योग शब्द का प्रयोग नहीं रहा। वहां योग मन, वचन तथा शरीर की प्रवृत्ति के लिए प्रयुक्त रहा है। अध्यात्मपरक साधना, चैतसिक परिशुद्धि, अन्तःपरिष्कार, वृत्तिसम्माजन, वृत्ति-निरोध जैसे अर्थ जैन-परम्परा में योग के साथ जुड़े, पर बहुत बाद में। हां, आगम-साहित्य में उस आत्मोन्मुख साधना के, जिसे जैन-योग के नाम से संबोधित किया गया, बीज रूप में प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है।
योग के आठ अंगों में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है । यह सातवां अंग है । एक ओर इसके पूर्ववर्ती छ: अंग तथा दूसरी ओर केवल यह सातवां अंग ध्यान, यदि इन्हें तुलित किया जाय तो संभवतः ध्यान का पलड़ा भारी रहेगा। इसके बाद योग का अन्तिम आठवां अंग समाधि आता है, जिसके साथ जीवन का चरम-साध्य सध जाता है।
जैन आगम-साहित्य में ध्यान के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं---
आचारांगसूत्र के नवें अध्ययन में जहां भगवान महावीर की चर्या का वर्णन है, वहां उनकी साधना का भी उल्लेख है । नितान्त असंग-भाव से विविध रूपों में उनके ध्यान करने के अनेक प्रसंग वहां वर्णित हैं।
एक स्थान पर लिखा है--'भगवान् प्रहर-प्रहर तक अपनी आंखें बिलकुल न टिमटिमाते हुए तिर्यक् भित्ति (तिरछी भीत) पर उन्हें केन्द्रित कर ध्यान करते थे। दीर्घकाल तक नेत्रों के निनिमेष रहने से उनकी पुतलियां ऊपर को चढ़ जातीं, उन्हें देखकर बच्चे भयभीत हो जाते, हन्त-हन्त कहकर चिल्लाने लगते और दूसरे बच्चों को बुला लाते।" इस संदर्भ से प्रकट होता है कि भगवान महावीर का यह ध्यान वाटक-पद्धति से जुड़ा था।
एक अन्य प्रसंग में लिखा है—'भगवान् अपने विहार-क्रम के बीच यदि गृहस्थ-संकुल स्थान में होते तो भी अपना मन किसी में न लगाते हुए ध्यान करते । किसी के पूछने पर भी अभिभाषण नहीं करते । कोई उन्हें बाध्य करता तो चुपचाप दूसरे स्थान पर चले जाते, अपने ध्यान का अतिक्रमण नहीं करते ।२
आगे लिखा है.--.'भगवान् अपने साधना-काल में साढ़े -बारह वर्षों में जिन स्थानों में रहे, बड़े प्रसन्न-मन रहते थे। रात-दिन यतनाशील-स्थिर, अप्रमत्तप्रमादरहित, एकाग्र तथा समाहित-शान्त रहते हुए ध्यान में लीन रहते थे।
एक अन्य स्थान पर उल्लेख है-'जब भगवान् उपवन के अन्तर-आवास में कभी ध्यानस्थ हुए तब प्रतिदिन वहां आने वाले
१. 'अदु पोरिसि तिरियं भित्ति, चक्खुमासज्ज अंततो झाइ।
अह चक्खु-भीया सहिया, ते 'हताहता' बहवे करिस् ।।', आचारांग, ९/१/५ २. 'जे के इमें अगारत्था, मीसीभावं पहाय से झाति ।
पुट्ठो वि णाभिभासिस, गच्छति णाइवत्तई अंजू ।',वही, ६/१/७ ३. 'एतेहिं मुणी सयणेहि, समणे पासी पतेरस वासे।
राई दिन पि जयगाणे, अप्पगमत्ते समहिए झाति ॥', वही, ६/२/४
जैन दर्शन मीमांसा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org