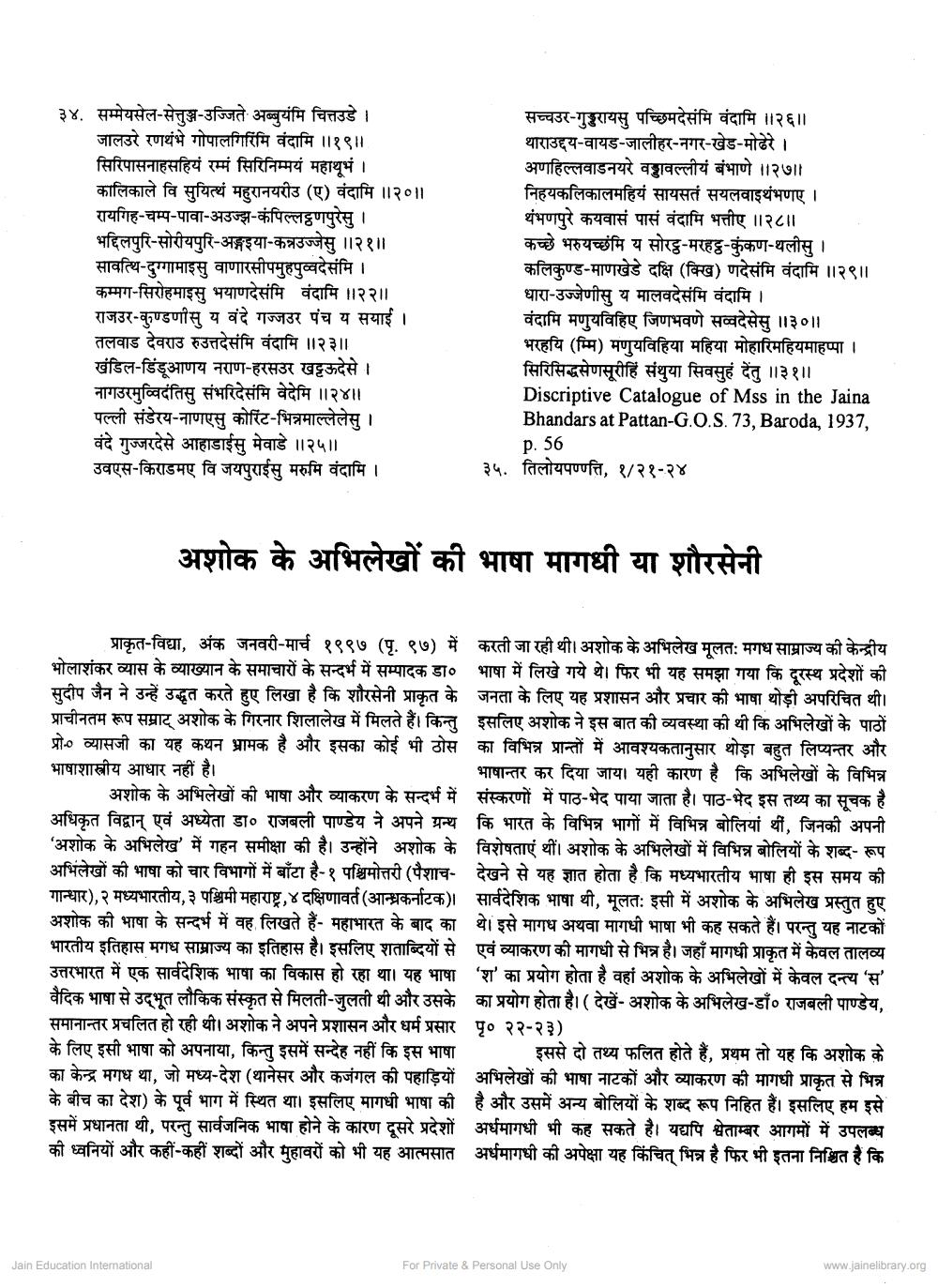________________
३४. सम्मेयसेल-सेत्तुञ्ज - उज्जिते अब्बुयंमि चित्तउडे ।
जालउरे रणथंभे गोपालगिरिमि वंदामि ॥ १९ ॥ सिरिपासनाहसहियं रम्मं सिरिनिम्मयं महाबूभं । कालिकाले वि सुयित्थं महुरानयरीउ (ए) वंदामि ॥ २० ॥ रायगिह-चम्प-पावा- अउज्झ - कंपिल्लट्ठणपुरे । भद्दिलपुरि-सोरीयपुरि-अङ्गइया कनउज्जे ॥२१॥ सावत्वि दुग्गामाइसु वाणारसीपमुहपुव्वदेसंमि । कम्मग- सिरोहमाइसु भयाणदेसंमि वंदामि ॥ २२ ॥ राजर कुण्डणीसु य वंदे गज्जठर पंच व सचाई । तलवाड देवराउ रुउत्तदेसंमि वंदामि ||२३|| खंडिल - डिंडूआणय नराण हरसउर खट्टऊदेसे । नागउरमुव्विदंतिसु संभरिदेसंमि वेदेमि ||२४|| पल्ली संडेरय-नाणएसु कोरिंट - भिन्नमाल्लेलेसु । वंदे गुज्जरदेसे आहाडाईसु मेवाडे ।। २५ । उवएस-किराडमए विजयपुराईसु मरुमि वंदामि ।
प्राकृत विद्या, अंक जनवरी-मार्च १९९७ (पृ. ९७) में भोलाशंकर व्यास के व्याख्यान के समाचारों के सन्दर्भ में सम्पादक डा० सुदीप जैन ने उन्हें उद्धृत करते हुए लिखा है कि शौरसेनी प्राकृत के प्राचीनतम रूप सम्राट अशोक के गिरनार शिलालेख में मिलते हैं। किन्तु प्रो-० व्यासजी का यह कथन भ्रामक है और इसका कोई भी ठोस भाषाशास्त्रीय आधार नहीं है।
अशोक के अभिलेखों की भाषा और व्याकरण के सन्दर्भ में अधिकृत विद्वान् एवं अध्येता डा० राजबली पाण्डेय ने अपने ग्रन्थ 'अशोक के अभिलेख' में गहन समीक्षा की है। उन्होंने अशोक के अभिलेखों की भाषा को चार विभागों में बाँटा है- १ पश्चिमोत्तरी (पैशाच गान्धार), २ मध्यभारतीय, ३ पश्चिमी महाराष्ट्र, ४ दक्षिणावर्त (आन्ध्रकर्नाटक)। अशोक की भाषा के सन्दर्भ में वह लिखते हैं- महाभारत के बाद का भारतीय इतिहास मगध साम्राज्य का इतिहास है। इसलिए शताब्दियों से उत्तरभारत में एक सार्वदेशिक भाषा का विकास हो रहा था। यह भाषा वैदिक भाषा से उद्भूत लौकिक संस्कृत से मिलती-जुलती थी और उसके समानान्तर प्रचलित हो रही थी। अशोक ने अपने प्रशासन और धर्म प्रसार के लिए इसी भाषा को अपनाया, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस भाषा का केन्द्र मगध था, जो मध्य-देश (थानेसर और कजंगल की पहाड़ियों के बीच का देश) के पूर्व भाग में स्थित था। इसलिए मागधी भाषा की इसमें प्रधानता थी, परन्तु सार्वजनिक भाषा होने के कारण दूसरे प्रदेशों की ध्वनियों और कहीं-कहीं शब्दों और मुहावरों को भी यह आत्मसात
Jain Education International
सच्चउर-गुङ्कुरायसु पच्छिमदेसंमि वंदामि ||२६|| थारा उद्दय-वायड - जालीहर- नगर - खेड - मोढेरे । अणहिल्लवाडनपरे वङ्गावल्लीयं बंभाणे ||२७॥ निहयकलिकालमहियं सायसतं सयलवाइयंभणए । भणपुरे कयवासं पासं वंदामि भत्तीए ||२८|| कच्छे भरुवच्छंमि व सोरदु-मरहट्ठ-कुंकण-वलीसु । कलिकुण्ड-माणखेडे दक्षि (खि) गदेसंमि वंदामि ॥२९॥ धारा-उज्जेणीसु य मालवदेसंमि वंदामि । वंदामि मणुयविहिए जिणभवणे सव्वदेसेसु ॥ ३० ॥ भरयि (म्मि) मणुयविहिया महिया मोहारिमहियमाहप्पा । सिरिसिद्धसेणसूरीहि संधुया सिवसुहं तु ॥ ३२॥ Discriptive Catalogue of Mss in the Jaina Bhandars at Pattan-G.O.S. 73, Baroda, 1937, p.56
३५. तिलोयपण्णत्त, १/२१-२४
अशोक के अभिलेखों की भाषा मागधी वा शौरसेनी
करती जा रही थी। अशोक के अभिलेख मूलतः मगध साम्राज्य की केन्द्रीय भाषा में लिखे गये थे फिर भी यह समझा गया कि दूरस्थ प्रदेशों की जनता के लिए यह प्रशासन और प्रचार की भाषा थोड़ी अपरिचित थी । इसलिए अशोक ने इस बात की व्यवस्था की थी कि अभिलेखों के पाठों का विभिन्न प्रान्तों में आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत लिप्यन्तर और भाषान्तर कर दिया जाय। यही कारण है कि अभिलेखों के विभिन्न संस्करणों में पाठभेद पाया जाता है। पाठभेद इस तथ्य का सूचक है कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न बोलियां थीं, जिनकी अपनी विशेषताएं थीं। अशोक के अभिलेखों में विभिन्न बोलियों के शब्द रूप देखने से यह ज्ञात होता है कि मध्यभारतीय भाषा ही इस समय की सार्वदेशिक भाषा थी, मूलतः इसी में अशोक के अभिलेख प्रस्तुत हुए थे। इसे मागध अथवा मागधी भाषा भी कह सकते हैं। परन्तु यह नाटकों एवं व्याकरण की मागधी से भिन्न है जहाँ मागधी प्राकृत में केवल तालव्य 'श' का प्रयोग होता है वहां अशोक के अभिलेखों में केवल दन्त्य 'स' का प्रयोग होता है (देखें- अशोक के अभिलेख डॉ० राजबली पाण्डेय, पृ० २२-२३)
इससे दो तथ्य फलित होते हैं, प्रथम तो यह कि अशोक के अभिलेखों की भाषा नाटकों और व्याकरण की मागधी प्राकृत से भिन्न है और उसमें अन्य बोलियों के शब्द रूप निहित हैं। इसलिए हम इसे अर्धमागधी भी कह सकते है। यद्यपि श्वेताम्बर आगमों में उपलब्ध अर्धमागधी की अपेक्षा यह किंचित् भिन्न है फिर भी इतना निश्चित है कि
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.