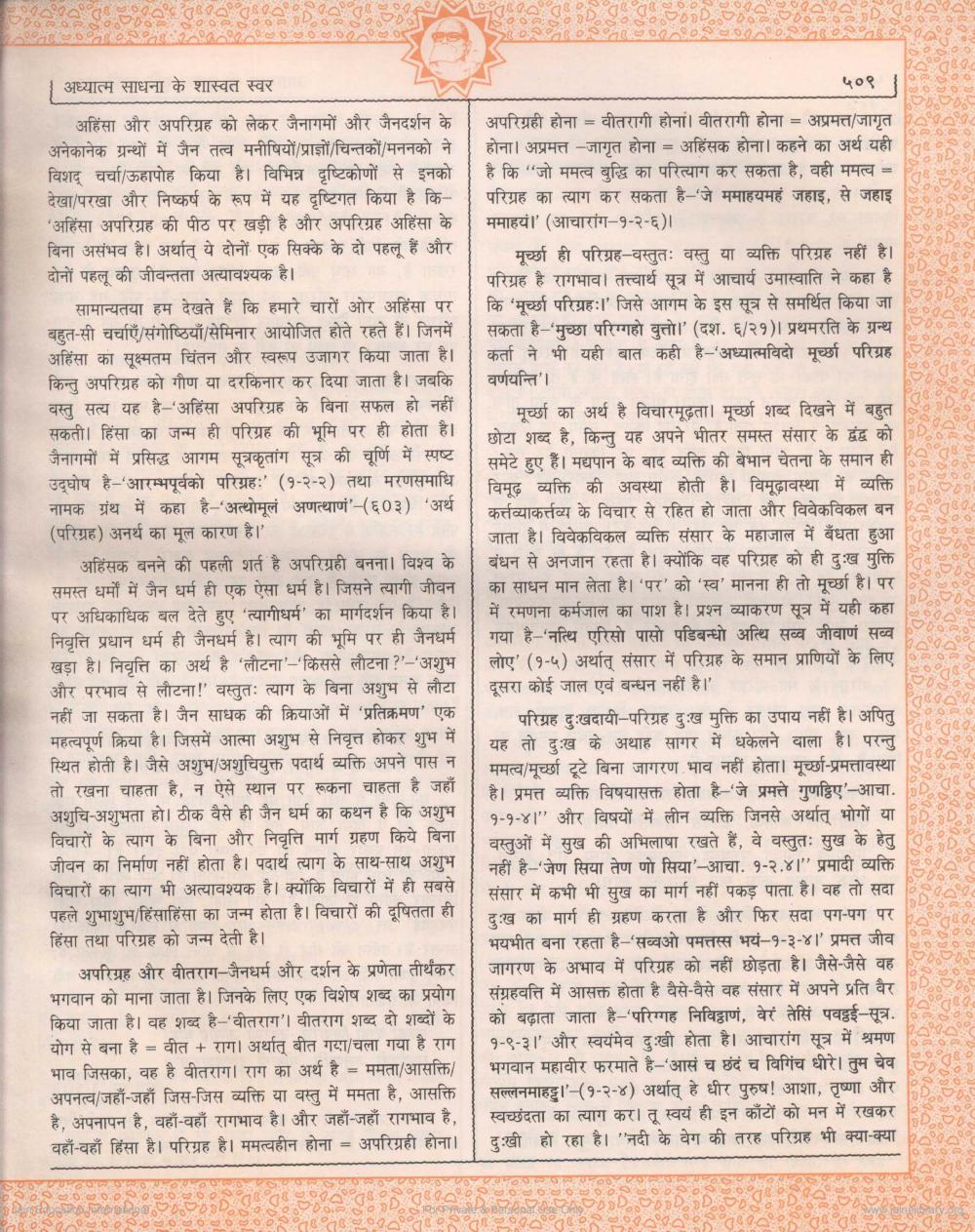________________
अध्यात्म साधना के शास्वत स्वर
अहिंसा और अपरिग्रह को लेकर जैनागमों और जैनदर्शन के अनेकानेक ग्रन्थों में जैन तत्व मनीषियों / प्राज्ञों/चिन्तकों/मननको ने विशद् चर्चा / ऊहापोह किया है। विभिन्न दृष्टिकोणों से इनको देखा परखा और निष्कर्ष के रूप में यह दृष्टिगत किया है कि'अहिंसा अपरिग्रह की पीठ पर खड़ी है और अपरिग्रह अहिंसा के बिना असंभव है। अर्थात् वे दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों पहलू की जीवन्तता अत्यावश्यक है।
सामान्यतया हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर अहिंसा पर बहुत-सी चर्चाएँ / संगोष्ठियाँ / सेमिनार आयोजित होते रहते हैं। जिनमें अहिंसा का सूक्ष्मतम चिंतन और स्वरूप उजागर किया जाता है। किन्तु अपरिग्रह को गीण या दरकिनार कर दिया जाता है जबकि वस्तु सत्य यह है-अहिंसा अपरिग्रह के बिना सफल हो नहीं सकती हिंसा का जन्म ही परिग्रह की भूमि पर ही होता है। जैनागमों में प्रसिद्ध आगम सूत्रकृतांग सूत्र की चूर्णि में स्पष्ट उद्घोष है आरम्भपूर्वको परिग्रहः" (१-२-२) तथा मरणसमाथि नामक ग्रंथ में कहा है-अत्योमूल अणत्थाणं' (६०३) 'अर्थ (परिग्रह) अनर्थ का मूल कारण है।'
अहिंसक बनने की पहली शर्त है अपरिग्रही बनना। विश्व के समस्त धर्मों में जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है। जिसने त्यागी जीवन पर अधिकाधिक बल देते हुए 'त्यागीधर्म' का मार्गदर्शन किया है। निवृत्ति प्रधान धर्म ही जैनधर्म है। त्याग की भूमि पर ही जैनधर्म खड़ा है । निवृत्ति का अर्थ है 'लौटना'-'किससे लौटना ?'-'अशुभ और परभाव से लीटना! वस्तुतः त्याग के बिना अशुभ से लौटा नहीं जा सकता है। जैन साधक की क्रियाओं में 'प्रतिक्रमण' एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जिसमें आत्मा अशुभ से निवृत्त होकर शुभ में स्थित होती है जैसे अशुभ अशुचियुक्त पदार्थ व्यक्ति अपने पास न तो रखना चाहता है, न ऐसे स्थान पर रूकना चाहता है जहाँ अशुचि-अशुभता हो। ठीक वैसे ही जैन धर्म का कथन है कि अशुभ विचारों के त्याग के बिना और निवृत्ति मार्ग ग्रहण किये बिना जीवन का निर्माण नहीं होता है पदार्थ त्याग के साथ-साथ अशुभ विचारों का त्याग भी अत्यावश्यक है। क्योंकि विचारों में ही सबसे पहले शुभाशुभ / हिंसाहिंसा का जन्म होता है। विचारों की दूषितता ही हिंसा तथा परिग्रह को जन्म देती है।
अपरिग्रह और वीतराग जैनधर्म और दर्शन के प्रणेता तीर्थंकर भगवान को माना जाता है। जिनके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह शब्द है-'वीतराग'। वीतराग शब्द दो शब्दों के योग से बना है = वीत + राग। अर्थात् बीत गया / चला गया है राग भाव जिसका, वह है बीतराग राग का अर्थ है ममता / आसक्ति / अपनत्व / जहाँ-जहाँ जिस-जिस व्यक्ति या वस्तु में ममता है, आसक्ति है, अपनापन है, वहाँ-वहाँ रागभाव है। और जहाँ-जहाँ रागभाव है, यहाँ-वहाँ हिंसा है परिग्रह है। ममत्वहीन होना अपरिग्रही होना।
=
५०९
अपरिग्रही होना वीतरागी होनां वीतरागी होना अप्रमत्त / जागृत होना अप्रमत्त जागृत होना अहिंसक होना। कहने का अर्थ यही हैं कि "जो ममत्व बुद्धि का परित्याग कर सकता है, वही ममत्व = परिग्रह का त्याग कर सकता है-'जे ममाहयमहं जहाइ, से जहाइ ममाहये।' (आचारांग - १-२-६)।
=
=
=
मूर्च्छा ही परिग्रह- यस्तुतः वस्तु या व्यक्ति परिग्रह नहीं है। परिग्रह है रागभाव तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वाति ने कहा है कि 'मूर्च्छा परिग्रहः ।' जिसे आगम के इस सूत्र से समर्थित किया जा सकता है-'मुच्छा परिग्गहो वृत्तो ।' (दश. ६/२१ ) । प्रथमरति के ग्रन्थ कर्ता ने भी यही बात कही है- 'अध्यात्मविदो मूर्च्छा परिग्रह वर्णयन्ति ।
मूर्च्छा का अर्थ है विचारमूढ़ता। मूर्च्छा शब्द दिखने में बहुत छोटा शब्द है, किन्तु यह अपने भीतर समस्त संसार के द्वंद्व को समेटे हुए हैं। मद्यपान के बाद व्यक्ति की बेभान चेतना के समान ही विमूढ़ व्यक्ति की अवस्था होती है। विमूढावस्था में व्यक्ति कर्तव्याकर्तव्य के विचार से रहित हो जाता और विवेकविकल बन जाता है। विवेकविकल व्यक्ति संसार के महाजाल में बँधता हुआ बंधन से अनजान रहता है। क्योंकि वह परिग्रह को ही दुःख मुक्ति का साधन मान लेता है। 'पर' को 'स्व' मानना ही तो मूर्च्छा है। पर में रमणना कर्मजाल का पाश है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में यही कहा गया है- 'नत्थि एरिसो पासो पडिबन्धो अत्थि सव्व जीवाणं सव्व लोए' (१-५) अर्थात् संसार में परिग्रह के समान प्राणियों के लिए दूसरा कोई जाल एवं बन्धन नहीं है।'
परिग्रह दुःखदायी - परिग्रह दुःख मुक्ति का उपाय नहीं है। अपितु यह तो दुःख के अथाह सागर में धकेलने वाला है। परन्तु ममत्व / मूर्च्छा टूटे बिना जागरण भाव नहीं होता। मूर्च्छा-प्रमत्तावस्था है। प्रमत्त व्यक्ति विषयासक्त होता है- 'जे प्रमत्ते गुणट्ठिए'-आचा. १-१-४१" और विषयों में लीन व्यक्ति जिनसे अर्थात् भोगों या वस्तुओं में सुख की अभिलाषा रखते हैं, वे वस्तुतः सुख के हेतु नहीं है-'जेण सिया तेण णो सिया'- आचा. १२.४। प्रमादी व्यक्ति संसार में कभी भी सुख का मार्ग नहीं पकड़ पाता है। वह तो सदा दुःख का मार्ग ही ग्रहण करता है और फिर सदा पग-पग पर भयभीत बना रहता है-'सव्वओ पमत्तस्स भयं-१-३-४।' प्रमत्त जीव जागरण के अभाव में परिग्रह को नहीं छोड़ता है जैसे-जैसे वह संग्रहवत्ति में आसक्त होता है वैसे-वैसे यह संसार में अपने प्रति बैर को बढ़ाता जाता है- परिग्गह निविट्ठाणं, वेरं तेसिं पवट्ठई-सूत्र. १-९-३।' और स्वयंमेव दुःखी होता है। आचारांग सूत्र में भ्रमण भगवान महावीर फरमाते है- 'आसं च छंदं च विगिंच धीरे। तुम चेव सल्लनमाहड्ड । - (१-२-४) अर्थात् हे धीर पुरुष! आशा तृष्णा और स्वच्छंदता का त्याग कर। तू स्वयं ही इन काँटों को मन में रखकर दुःखी हो रहा है। "नदी के वेग की तरह परिग्रह भी क्या क्या