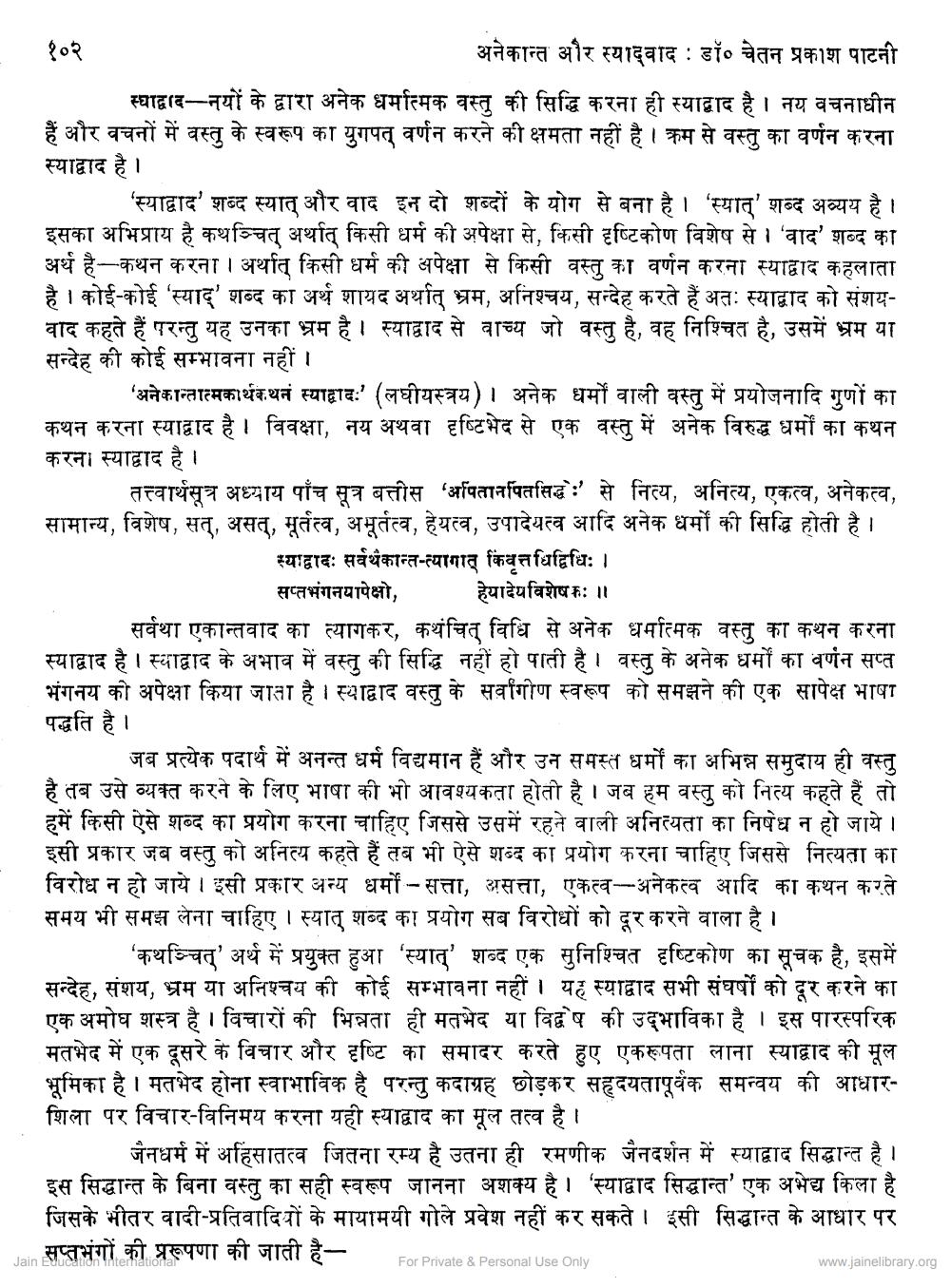________________
१०२
अनेकान्त और स्याद्वाद : डॉ० चेतन प्रकाश पाटनी स्थाद्वाद-नयों के द्वारा अनेक धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि करना ही स्याद्वाद है। नय वचनाधीन हैं और वचनों में वस्तु के स्वरूप का युगपत् वर्णन करने की क्षमता नहीं है । क्रम से वस्तु का वर्णन करना स्याद्वाद है।
'स्याद्वाद' शब्द स्यात् और वाद इन दो शब्दों के योग से बना है। 'स्यात्' शब्द अव्यय है। इसका अभिप्राय है कथञ्चित् अर्थात् किसी धर्म की अपेक्षा से, किसी दृष्टिकोण विशेष से । 'वाद' शब्द का अर्थ है-कथन करना । अर्थात् किसी धर्म की अपेक्षा से किसी वस्तु का वर्णन करना स्याद्वाद कहलाता है। कोई-कोई 'स्याद्' शब्द का अर्थ शायद अर्थात् भ्रम, अनिश्चय, सन्देह करते हैं अतः स्याद्वाद को संशयवाद कहते हैं परन्तु यह उनका भ्रम है । स्याद्वाद से वाच्य जो वस्तु है, वह निश्चित है, उसमें भ्रम या सन्देह की कोई सम्भावना नहीं ।
'अनेकान्तात्मकार्थकथनं स्याद्वादः' (लघीयस्त्रय)। अनेक धर्मों वाली वस्तु में प्रयोजनादि गुणों का कथन करना स्याद्वाद है। विवक्षा, नय अथवा दृष्टिभेद से एक वस्तु में अनेक विरुद्ध धर्मों का कथन करना स्याद्वाद है।
तत्त्वार्थसूत्र अध्याय पाँच सूत्र बत्तीस 'अपितानपितसिद्धः' से नित्य, अनित्य, एकत्व, अनेकत्व, सामान्य, विशेष, सत्, असत्, मूर्तत्व, अभूर्तत्व, हेयत्व, उपादेयत्व आदि अनेक धर्मों की सिद्धि होती है।
स्याद्वादः सर्वथैकान्त-त्यागात् किंवृत्तधिद्विधिः ।
सप्तभंगनयापेक्षो, हेयादेयविशेषकः ॥ सर्वथा एकान्तवाद का त्यागकर, कथंचित् विधि से अनेक धर्मात्मक वस्तु का कथन करना स्याद्वाद है । स्थाद्वाद के अभाव में वस्तु की सिद्धि नहीं हो पाती है। वस्तु के अनेक धर्मों का वर्णन सप्त भंगनय को अपेक्षा किया जाता है। स्थाद्वाद वस्तु के सर्वागीण स्वरूप को समझने की एक सापेक्ष भाषा पद्धति है।
जब प्रत्येक पदार्थ में अनन्त धर्म विद्यमान हैं और उन समस्त धर्मों का अभिन्न समुदाय ही वस्तु है तब उसे व्यक्त करने के लिए भाषा की भी आवश्यकता होती है । जब हम वस्तु को नित्य कहते हैं तो हमें किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसमें रहने वाली अनित्यता का निषेध न हो जाये । इसी प्रकार जब वस्तु को अनित्य कहते हैं तब भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिससे नित्यता का विरोध न हो जाये । इसी प्रकार अन्य धर्मों - सत्ता, असत्ता, एकत्व-अनेकत्व आदि का कथन करते समय भी समझ लेना चाहिए । स्यात् शब्द का प्रयोग सब विरोधों को दूर करने वाला है।
___ 'कथञ्चित्' अर्थ में प्रयुक्त हुआ 'स्यात्' शब्द एक सुनिश्चित दृष्टिकोण का सूचक है, इसमें सन्देह, संशय, भ्रम या अनिश्चय की कोई सम्भावना नहीं। यह स्याद्वाद सभी संघर्षों को दूर करने का एक अमोघ शस्त्र है । विचारों की भिन्नता ही मतभेद या विद्वष की उद्भाविका है । इस पारस्परिक मतभेद में एक दूसरे के विचार और दृष्टि का समादर करते हुए एकरूपता लाना स्याद्वाद की मूल भूमिका है । मतभेद होना स्वाभाविक है परन्तु कदाग्रह छोड़कर सहृदयतापूर्वक समन्वय की आधारशिला पर विचार-विनिमय करना यही स्याद्वाद का मूल तत्व है।
जैनधर्म में अहिंसातत्व जितना रम्य है उतना ही रमणीक जैनदर्शन में स्याद्वाद सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के बिना वस्तु का सही स्वरूप जानना अशक्य है। 'स्याद्वाद सिद्धान्त' एक अभेद्य किला है जिसके भीतर वादी-प्रतिवादियों के मायामयी गोले प्रवेश नहीं कर सकते। इसी सिद्धान्त के आधार पर सप्तभंगों की प्ररूपणा की जाती है
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org