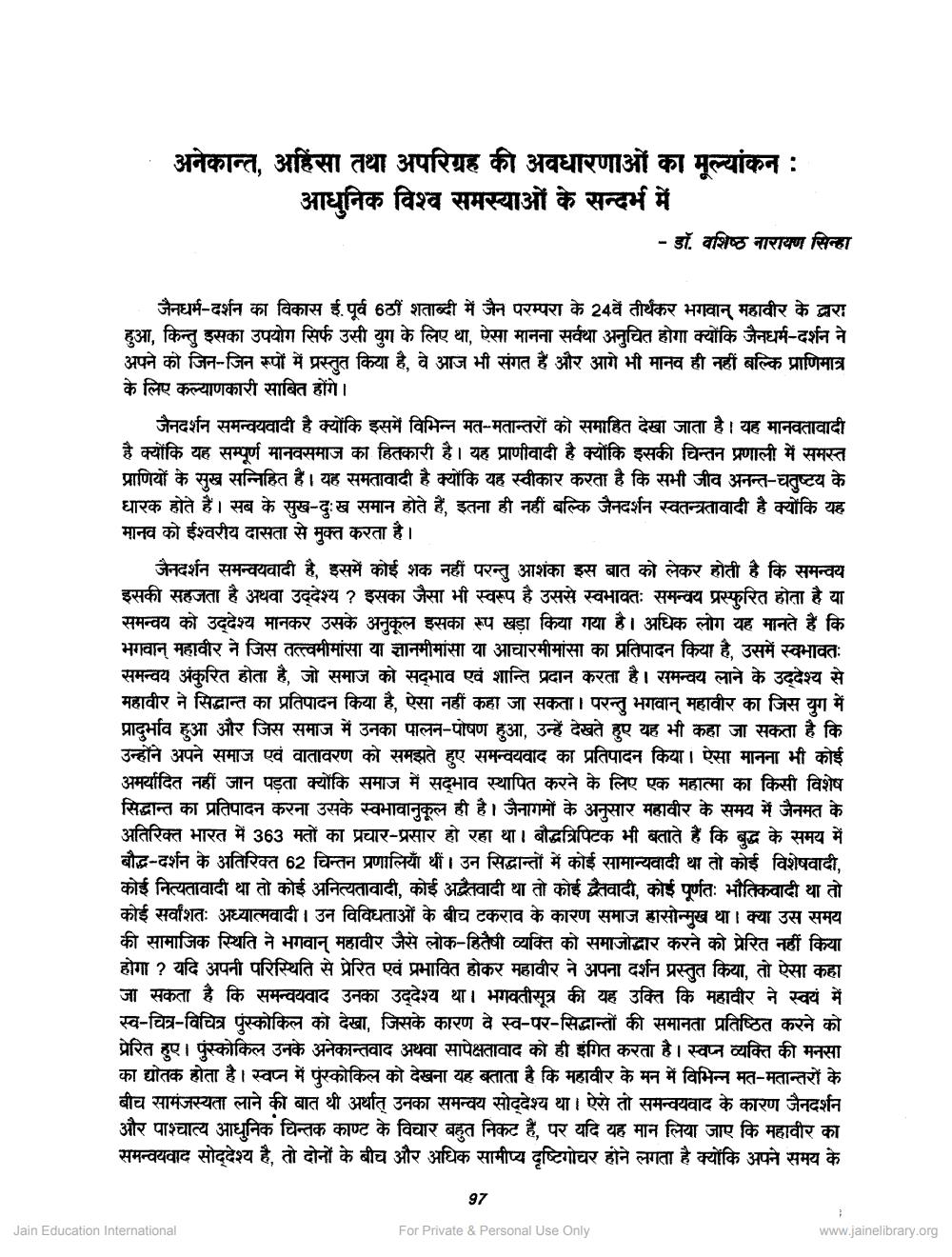________________
अनेकान्त, अहिंसा तथा अपरिग्रह की अवधारणाओं का मूल्यांकन : आधुनिक विश्व समस्याओं के सन्दर्भ में
- डॉ. वशिष्ठ नारायण सिन्हा
जैनधर्म-दर्शन का विकास ई.पूर्व 6ठीं शताब्दी में जैन परम्परा के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के बरा हुआ, किन्तु इसका उपयोग सिर्फ उसी युग के लिए था, ऐसा मानना सर्वथा अनुचित होगा क्योंकि जैनधर्म-दर्शन ने अपने को जिन-जिन रूपों में प्रस्तुत किया है, वे आज भी संगत हैं और आगे भी मानव ही नहीं बल्कि प्राणिमात्र के लिए कल्याणकारी साबित होंगे।
जैनदर्शन समन्वयवादी है क्योंकि इसमें विभिन्न मत-मतान्तरों को समाहित देखा जाता है। यह मानवतावादी है क्योंकि यह सम्पूर्ण मानवसमाज का हितकारी है। यह प्राणीवादी है क्योंकि इसकी चिन्तन प्रणाली में समस्त प्राणियों के सुख सन्निहित है। यह समतावादी है क्योंकि यह स्वीकार करता है कि सभी जीव अनन्त-चतुष्टय के धारक होते हैं। सब के सुख-दुःख समान होते हैं, इतना ही नहीं बल्कि जैनदर्शन स्वतन्त्रतावादी है क्योंकि यह मानव को ईश्वरीय दासता से मुक्त करता है।
जैनदर्शन समन्वयवादी है, इसमें कोई शक नहीं परन्तु आशंका इस बात को लेकर होती है कि समन्वय इसकी सहजता है अथवा उद्देश्य ? इसका जैसा भी स्वरूप है उससे स्वभावतः समन्वय प्रस्फुरित होता है या समन्वय को उद्देश्य मानकर उसके अनुकूल इसका स्प खड़ा किया गया है। अधिक लोग यह मानते हैं कि भगवान् महावीर ने जिस तत्त्वमीमांसा या ज्ञानमीमांसा या आचारमीमांसा का प्रतिपादन किया है, उसमें स्वभावतः समन्वय अंकुरित होता है, जो समाज को सद्भाव एवं शान्ति प्रदान करता है। समन्वय लाने के उद्देश्य से महावीर ने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परन्तु भगवान महावीर का जिस युग में प्रादुर्भाव हुआ और जिस समाज में उनका पालन-पोषण हुआ, उन्हें देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने समाज एवं वातावरण को समझते हुए समन्वयवाद का प्रतिपादन किया। ऐसा मानना भी कोई अमर्यादित नहीं जान पड़ता क्योंकि समाज में सदभाव स्थापित करने के लिए एक महात्मा का किसी कि सिद्धान्त का प्रतिपादन करना उसके स्वभावानुकूल ही है। जैनागमों के अनुसार महावीर के समय में जैनमत के अतिरिक्त भारत में 363 मतों का प्रचार-प्रसार हो रहा था। बौद्धत्रिपिटक भी बताते हैं कि बुद्ध के समय में बौद्ध-दर्शन के अतिरिक्त 62 चिन्तन प्रणालियाँ थीं। उन सिद्धान्तों में कोई सामान्यवादी था तो कोई विशेषवादी, कोई नित्यतावादी था तो कोई अनित्यतावादी, कोई अद्वैतवादी था तो कोई द्वैतवादी, कोई पूर्णतः भौतिकवादी था तो कोई सर्वांशतः अध्यात्मवादी। उन विविधताओं के बीच टकराव के कारण समाज हासोन्मुख था। क्या उस समय की सामाजिक स्थिति ने भगवान महावीर जैसे लोक-हितैषी व्यक्ति को समाजोद्धार करने को प्रेरित नहीं किया होगा ? यदि अपनी परिस्थिति से प्रेरित एवं प्रभावित होकर महावीर ने अपना दर्शन प्रस्तुत किया, तो ऐसा कहा जा सकता है कि समन्वयवाद उनका उद्देश्य था। भगवतीसूत्र की यह उक्ति कि महावीर ने स्वयं में स्व-चित्र-विचित्र पुस्कोकिल को देखा, जिसके कारण वे स्व-पर-सिद्धान्तों की समानता प्रतिष्ठित करने को प्रेरित हुए। पुंस्कोकिल उनके अनेकान्तवाद अथवा सापेक्षतावाद को ही इंगित करता है। स्वप्न व्यक्ति की मनसा का द्योतक होता है। स्वप्न में पुरकोकिल को देखना यह बताता है कि महावीर के मन में विभिन्न मत-मतान्तरों के बीच सामंजस्यता लाने की बात थी अर्थात उनका समन्वय सोददेश्य था। ऐसे तो समन्वयवाद के कारण जैनदर्शन
और पाश्चात्य आधुनिक चिन्तक काण्ट के विचार बहुत निकट है, पर यदि यह मान लिया जाए कि महावीर का समन्वयवाद सोद्देश्य है, तो दोनों के बीच और अधिक सामीप्य दृष्टिगोचर होने लगता है क्योंकि अपने समय के
97
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org